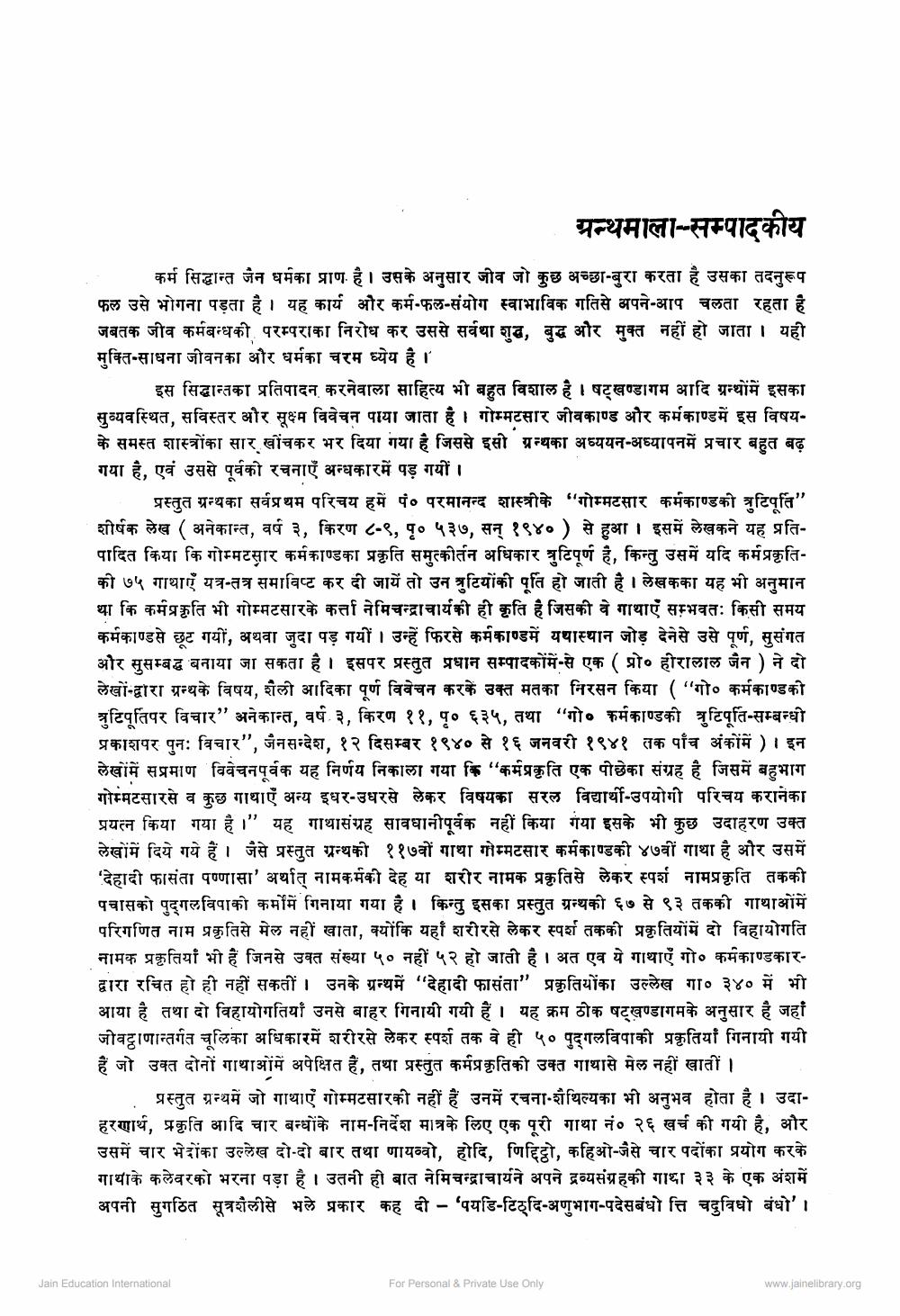________________
ग्रन्थमाला-सम्पादकीय
कर्म सिद्धान्त जैन धर्मका प्राण है। उसके अनुसार जीव जो कुछ अच्छा-बुरा करता है उसका तदनुरूप फल उसे भोगना पड़ता है। यह कार्य और कर्म-फल-संयोग स्वाभाविक गतिसे अपने-आप चलता रहता है जबतक जीव कर्मबन्धकी परम्पराका निरोध कर उससे सर्वथा शुद्ध, बुद्ध और मुक्त नहीं हो जाता। यही मुक्ति-साधना जीवनका और धर्मका चरम ध्येय है।
इस सिद्धान्तका प्रतिपादन करनेवाला साहित्य भी बहुत विशाल है । षट्खण्डागम आदि ग्रन्थोंमें इसका सुव्यवस्थित, सविस्तर और सूक्ष्म विवेचन पाया जाता है। गोम्मटसार जीवकाण्ड और कर्मकाण्डमें इस विषयके समस्त शास्त्रोंका सार खोंचकर भर दिया गया है जिससे इसी ग्रन्थका अध्ययन-अध्यापनमें प्रचार बहुत बढ़ गया है, एवं उससे पूर्वको रचनाएँ अन्धकारमें पड़ गयीं।
प्रस्तुत ग्रन्थका सर्वप्रथम परिचय हमें पं० परमानन्द शास्त्रीके "गोम्मटसार कर्मकाण्डको त्रुटिपूर्ति" शीर्षक लेख (अनेकान्त, वर्ष ३, किरण ८-९, पृ० ५३७, सन् १९४०) से हुआ। इसमें लेखकने यह प्रतिपादित किया कि गोम्मटसार कर्मकाण्डका प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार है, किन्तु उसमें यदि कर्मप्रकृतिकी ७५ गाथाएँ यत्र-तत्र समाविष्ट कर दी जायें तो उन त्रुटियोंकी पति हो जाती है। लेखकका यह भी अनुमान था कि कर्मप्रकृति भी गोम्मटसारके कर्ता नेमिचन्द्राचार्यकी ही कृति है जिसकी वे गाथाएं सम्भवतः किसी समय कर्मकाण्डसे छूट गयीं, अथवा जुदा पड़ गयीं। उन्हें फिरसे कर्मकाण्डमें यथास्थान जोड़ देनेसे उसे पूर्ण, सुसंगत और सुसम्बद्ध बनाया जा सकता है। इसपर प्रस्तुत प्रधान सम्पादकोंमें से एक (प्रो० हीरालाल जैन ) ने दो लेखों-द्वारा ग्रन्थके विषय, शैली आदिका पूर्ण विवेचन करके उक्त मतका निरसन किया ( "गो० कर्मकाण्डको अटिपतिपर विचार" अनेकान्त, वर्ष ३, किरण ११, १० ६३५, तथा "गो. कर्मकाण्डकी त्रुटिपूर्ति-सम्बन्धी प्रकाशपर पुनः विचार", जैनसन्देश, १२ दिसम्बर १९४० से १६ जनवरी १९४१ तक पांच अंकोंमें )। इन लेखोंमें सप्रमाण विवेचनपूर्वक यह निर्णय निकाला गया कि "कर्मप्रकृति एक पोछेका संग्रह है जिसमें बहुभाग गोम्मटसारसे व कुछ गाथाएँ अन्य इधर-उधरसे लेकर विषयका सरल विद्यार्थी-उपयोगी परिचय करानेका प्रयत्न किया गया है ।" यह गाथासंग्रह सावधानीपूर्वक नहीं किया गया इसके भी कुछ उदाहरण उक्त लेखोंमें दिये गये हैं। जैसे प्रस्तुत ग्रन्थकी ११७वों गाथा गोम्मटसार कर्मकाण्डकी ४७वीं गाथा है और उसमें 'देहादी फासंता पण्णासा' अर्थात् नामकर्मकी देह या शरीर नामक प्रकृतिसे लेकर स्पर्श नामप्रकृति तककी पचासको पुद्गलविपाको कर्मोमें गिनाया गया है। किन्तु इसका प्रस्तुत ग्रन्थकी ६७ से ९३ तककी गाथाओंमें परिगणित नाम प्रकृतिसे मेल नहीं खाता, क्योंकि यहाँ शरीरसे लेकर स्पर्श तककी प्रकृतियों में दो विहायोगति नामक प्रकृतियां भी हैं जिनसे उक्त संख्या ५० नहीं ५२ हो जाती है । अत एव ये गाथाएँ गो० कर्मकाण्डकारद्वारा रचित हो ही नहीं सकतीं। उनके ग्रन्थमें "देहादी फासंता" प्रकृतियोंका उल्लेख गा० ३४० में भी आया है तथा दो विहायोगतियाँ उनसे बाहर गिनायी गयी हैं। यह क्रम ठोक षट्खण्डागमके अनुसार है जहां जीवाणान्तर्गत चूलिका अधिकारमें शरीरसे लेकर स्पर्श तक वे ही ५० पुद्गलविपाकी प्रकृतियां गिनायी गयी हैं जो उक्त दोनों गाथाओंमें अपेक्षित हैं, तथा प्रस्तुत कर्मप्रकृतिको उक्त गाथासे मेल नहीं खातीं।
. प्रस्तुत ग्रन्थमें जो गाथाएँ गोम्मटसारकी नहीं हैं उनमें रचना-शैथिल्यका भी अनुभव होता है। उदाहरणार्थ, प्रकृति आदि चार बन्धोंके नाम-निर्देश मात्रके लिए एक पूरी गाथा नं० २६ खर्च की गयी है, और उसमें चार भेदोंका उल्लेख दो-दो बार तथा णायन्वो, होदि, णिद्दिट्ठो, कहिओ-जैसे चार पदोंका प्रयोग करके गाथाके कलेवरको भरना पड़ा है। उतनी ही बात नेमिचन्द्राचार्यने अपने द्रव्यसंग्रहकी गाथा ३३ के एक अंशमें अपनी सुगठित सूत्रशैलीसे भले प्रकार कह दी - 'पयडि-टिल्दि-अणुभाग-पदेसबंधो त्ति चदुविधो बंधो' ।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org