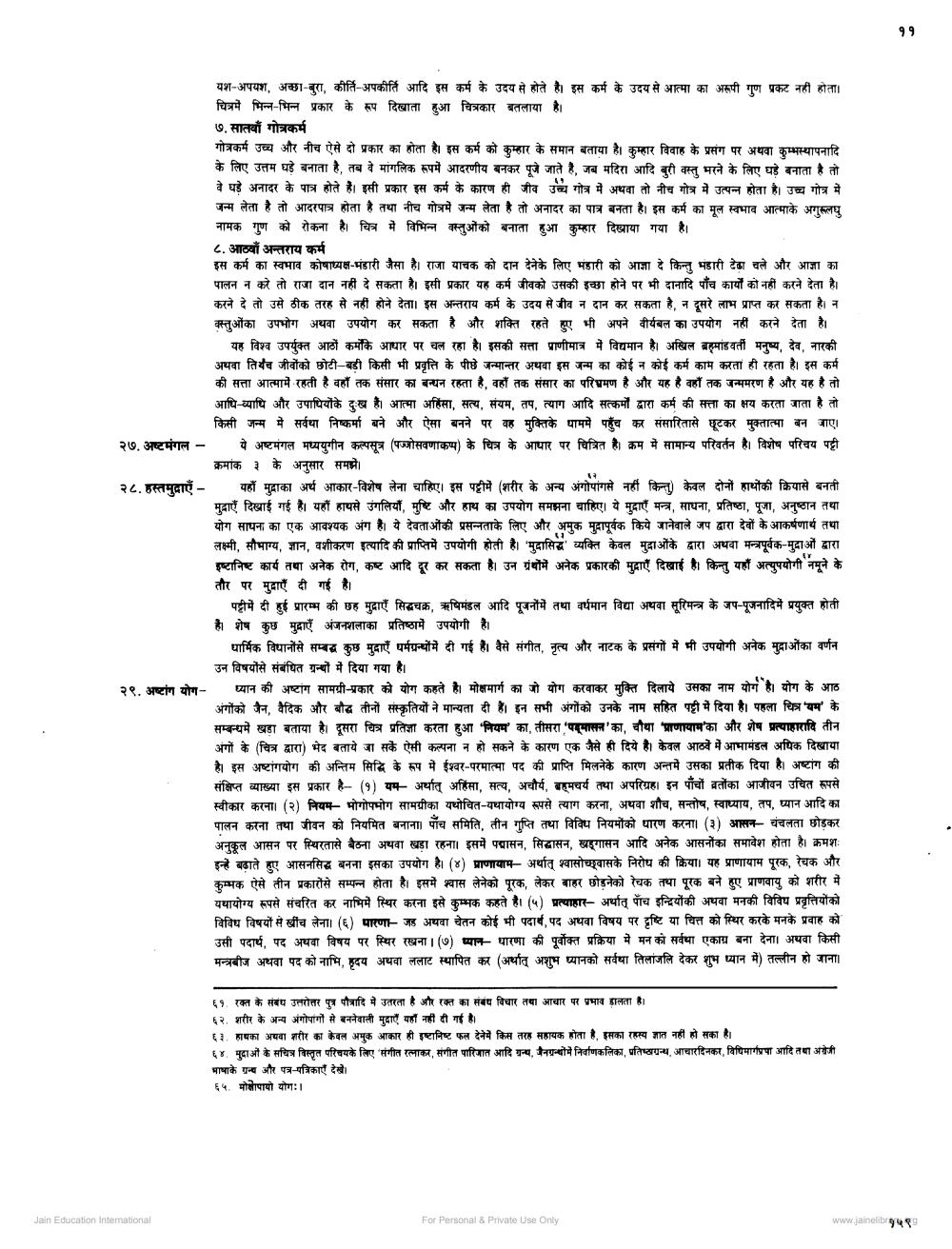________________
यश-अपयश, अच्छा-बुरा, कीर्ति-अपकीर्ति आदि इस कर्म के उदय से होते है। इस कर्म के उदय से आत्मा का अरूपी गुण प्रकट नहीं होता। चित्रमें भिन्न-भिन्न प्रकार के रूप दिखाता हुआ चित्रकार बतलाया है। ७. सातवाँ गोत्रकर्म गोत्रकर्म उच्च और नीच ऐसे दो प्रकार का होता है। इस कर्म को कुम्हार के समान बताया है। कुम्हार विवाह के प्रसंग पर अथवा कुम्भस्थापनादि के लिए उत्तम घड़े बनाता है, तब वे मांगलिक रूपमें आदरणीय बनकर पूजे जाते है, जब मदिरा आदि बुरी वस्तु भरने के लिए घड़े बनाता है तो वे घड़े अनादर के पात्र होते है। इसी प्रकार इस कर्म के कारण ही जीव उच्च गोत्र में अथवा तो नीच गोत्र में उत्पन्न होता है। उच्च गोत्र में जन्म लेता है तो आदरपात्र होता है तथा नीच गोत्रमें जन्म लेता है तो अनादर का पात्र बनता है। इस कर्म का मूल स्वभाव आत्माके अगुरूलघु नामक गुण को रोकना है। चित्र में विभिन्न वस्तुओंको बनाता हुआ कुम्हार दिखाया गया है। ८. आठवाँ अन्तराय कर्म इस कर्म का स्वभाव कोषाध्यक्ष-मंहारी जैसा है। राजा याचक को दान देनेके लिए भंडारी को आज्ञा दे किन्त भडारी टेढा चले और आज्ञा का पालन न करे तो राजा दान नहीं दे सकता है। इसी प्रकार यह कर्म जीवको उसकी इच्छा होने पर भी दानादि पाँच कार्यों को नहीं करने देता है। करने दे तो उसे ठीक तरह से नहीं होने देता। इस अन्तराय कर्म के उदय से जीव न दान कर सकता है, न दूसरे लाभ प्राप्त कर सकता है। न वस्तुओंका उपभोग अथवा उपयोग कर सकता है और शक्ति रहते हुए भी अपने वीर्यबल का उपयोग नहीं करने देता है।
यह विश्व उपर्युक्त आठों कोंक आधार पर चल रहा है। इसकी सत्ता प्राणीमात्र में विद्यमान है। अखिल ब्रहमांडवर्ती मनुष्य, देव, नारकी अथवा तिथंच जीवोंको छोटी-बड़ी किसी भी प्रवृत्ति के पीछे जन्मान्तर अथवा इस जन्म का कोई न कोई कर्म काम करता ही रहता है। इस कर्म की सत्ता आत्मामें रहती है वहाँ तक संसार का बन्धन रहता है, वहाँ तक संसार का परिभ्रमण है और यह है वहाँ तक जन्ममरण है और यह है तो आधि-व्याधि और उपाधियोंके दुःख है। आत्मा अहिंसा, सत्य, संयम, तप, त्याग आदि सत्कर्मों द्वारा कर्म की सत्ता का क्षय करता जाता है तो
किसी जन्म में सर्वथा निष्कर्मा बने और ऐसा बनने पर वह मुक्तिके घाममें पहुँच कर संसारितासे छूटकर मुक्तात्मा बन जाए। २७. अष्टमंगल - ये अष्टमंगल मध्ययुगीन कल्पसूत्र (पज्जोसवणाकप्प) के चित्र के आधार पर चित्रित है। क्रम में सामान्य परिवर्तन है। विशेष परिचय पट्टी
क्रमांक ३ के अनुसार समझे। २८. हस्तमुद्राएँ - यहाँ मुद्राका अर्थ आकार-विशेष लेना चाहिए। इस पट्टीमें (शरीर के अन्य अंगोपांगसे नहीं किन्तु) केवल दोनों हाथोकी क्रियासे बनती
मुद्राएँ दिखाई गई है। यहाँ हाथसे उंगलियाँ, मुषि और हाथ का उपयोग समझना चाहिए। ये मुद्राएँ मन्त्र, साधना, प्रतिष्ठा, पूजा, अनुष्ठान तथा योग साधना का एक आवश्यक अंग है। ये देवताओंकी प्रसन्नताके लिए और अमुक मुद्रापूर्वक किये जानेवाले जप द्वारा देवों के आकर्षणार्थ तथा लक्ष्मी, सौभाग्य, ज्ञान, वशीकरण इत्यादि की प्राप्तिमें उपयोगी होती है। मुद्रासिद्ध' व्यक्ति केवल मुद्राओंके द्वारा अथवा मन्त्रपूर्वक-मुद्राओं द्वारा इष्टानिष्ट कार्य तथा अनेक रोग, कष्ट आदि दूर कर सकता है। उन ग्रंथोंमें अनेक प्रकारकी मुद्राएँ दिखाई है। किन्तु यहाँ अत्युपयोगी नमूने के तौर पर मुद्राएँ दी गई है। ___ पट्टीमें दी हुई प्रारम्भ की छह मुद्राएँ सिद्धचक्र, ऋषिमंडल आदि पूजनोंमें तथा वर्धमान विद्या अथवा सूरिमन्त्र के जप-पूजनादिमें प्रयुक्त होती है। शेष कुछ मुद्राएँ अंजनशलाका प्रतिष्ठामें उपयोगी हैं।
धार्मिक विधानोंसे सम्बद्ध कुछ मुद्राएँ धर्मग्रन्थों में दी गई है। वैसे संगीत, नृत्य और नाटक के प्रसंगों में भी उपयोगी अनेक मुद्राओंका वर्णन
उन विषयोंसे संबंधित ग्रन्थों में दिया गया है। २९. अष्टांग योग- ध्यान की अष्टांग सामग्री-प्रकार को योग कहते है। मोक्षमार्ग का जो योग करवाकर मुक्ति दिलाये उसका नाम योग है। योग के आठ
अंगोंको जैन, वैदिक और बौद्ध तीनों संस्कृतियों ने मान्यता दी है। इन सभी अंगोंको उनके नाम सहित पट्टी में दिया है। पहला चित्र 'यम' के सम्बन्धमें खड़ा बताया है। दूसरा चित्र प्रतिज्ञा करता हुआ 'नियम' का, तीसरा 'पद्मासन' का, चौथा 'प्राणायाम'का और शेष प्रत्याहारावि तीन अगों के (चित्र द्वारा) भेद बताये जा सके ऐसी कल्पना न हो सकने के कारण एक जैसे ही दिये है। केवल आठवें में आभामंडल अधिक दिखाया है। इस अष्टांगयोग की अन्तिम सिद्धि के रूप में ईश्वर-परमात्मा पद की प्राप्ति मिलनेके कारण अन्तमें उसका प्रतीक दिया है। अष्टांग की संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकार है- (9) यम- अर्थात् अहिंसा, सत्य, अचौर्य, बह्मचर्य तथा अपरिग्रह। इन पाँचों व्रतोंका आजीवन उचित रूपसे स्वीकार करना। (२) नियम- भोगोपभोग सामग्रीका यथोचित-यथायोग्य रूपसे त्याग करना, अथवा शौच, सन्तोष, स्वाध्याय, तप, प्यान आदि का पालन करना तथा जीवन को नियमित बनाना। पाँच समिति, तीन गुप्ति तथा विविध नियमोंको धारण करना। (३) आसन-चंचलता छोड़कर अनुकूल आसन पर स्थिरतासे बैठना अथवा खड़ा रहना। इसमें पद्मासन, सिद्धासन, खड्गासन आदि अनेक आसनोंका समावेश होता है। क्रमशः इन्हे बढ़ाते हुए आसनसिद्ध बनना इसका उपयोग है। (४) प्राणायाम- अर्थात् श्वासोच्छवासके निरोध की क्रिया। यह प्राणायाम पूरक, रेचक और कुम्भक ऐसे तीन प्रकारोंसे सम्पन्न होता है। इसमें श्वास लेनेको पूरक, लेकर बाहर छोड़नेको रेचक तथा पूरक बने हुए प्राणवायु को शरीर में यथायोग्य रूपसे संचरित कर नाभिमें स्थिर करना इसे कुम्भक कहते है। (५) प्रत्याहार- अर्थात् पाँच इन्द्रियोंकी अथवा मनकी विविध प्रवृत्तियोंको विविध विषयों से खींच लेना। (६) पारणा-जह अथवा चेतन कोई भी पदार्थ, पद अथवा विषय पर दृष्टि या चित्त को स्थिर करके मनके प्रवाह को उसी पदार्थ, पद अथवा विषय पर स्थिर रखना । (७) प्यान- धारणा की पूर्वोक्त प्रक्रिया में मन को सर्वथा एकाग्र बना देना। अथवा किसी मन्त्रबीज अथवा पद को नाभि, हृदय अथवा ललाट स्थापित कर (अर्थात् अशुभ ध्यानको सर्वथा तिलांजलि देकर शुभ ध्यान में) तल्लीन हो जाना।
६१, रक्त के संबंध उत्तरोत्तर पुत्र पौत्रादि मे उतरता है और रक्त का संबंध विचार तथा आचार पर प्रभाव डालता है। ६२. शरीर के अन्य अंगोपागों से बननेवाली मुदाएँ यहाँ नही दी गई है। ६३. हापका अथवा शरीर का केवल अमुक आकार ही इष्टानिष्ट फल देने में किस तरह सहायक होता है, इसका रहस्य ज्ञात नहीं हो सका है। ६४. मुदाओं के सचित्र विस्तृत परिचयके लिए संगीत रत्नाकर, संगीत पारिजात आदि ग्रन्थ, नग्रन्थोंमें निर्वाणकलिका, प्रतिष्यग्रन्थ, आचारदिनकर, विधिमार्गप्रपा आदि तथा अंग्रेजी भाषाके गन्ध और पत्र-पत्रिकाएँ देखें। ६५. मोक्षोपायो योगः।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibr१५९४