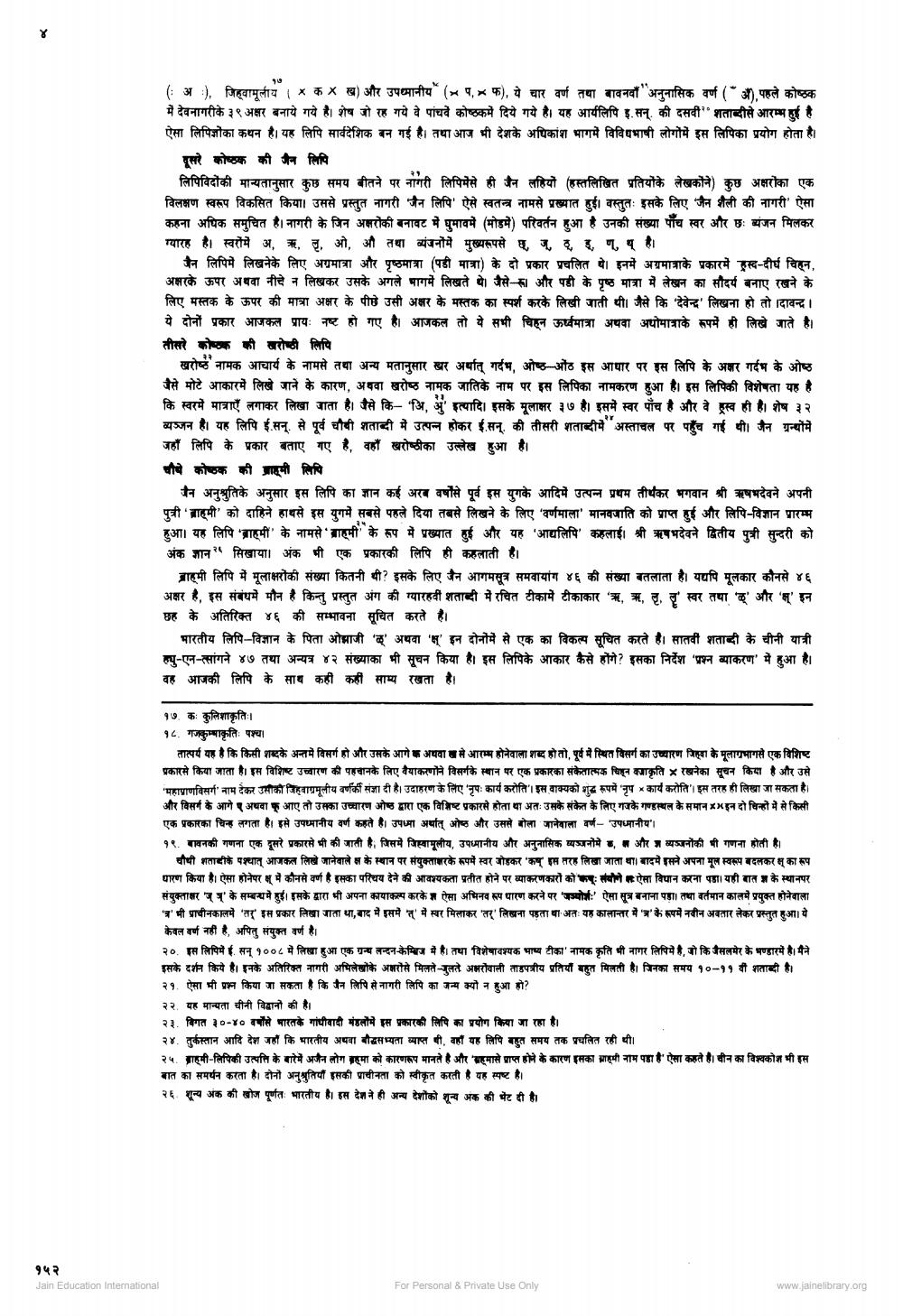________________
(: अ), जिह्वामूलाय । x क र ख) और उपध्मानीय (प, x फ), ये चार वर्ण तथा बावनवाँ"अनुनासिक वर्ण (अ.पहले कोष्ठक में देवनागरीके ३९ अक्षर बनाये गये है। शेष जो रह गये वे पांचवें कोष्ठकमें दिये गये है। यह आर्यलिपि इ.सन्. की दसवीं शताब्दीसे आरम्भ हुई है ऐसा लिपिज्ञोका कथन है। यह लिपि सार्वदेशिक बन गई है। तथा आज भी देशके अधिकांश भागमे विविधभाषी लोगोंमें इस लिपिका प्रयोग होता है।
दूसरे कोष्ठक की जैन लिपि लिपिविदोंकी मान्यतानुसार कुछ समय बीतने पर नागरी लिपिमेसे ही जैन लहियों (हस्तलिखित प्रतियोंके लेखकोने) कुछ अक्षरोका एक विलक्षण स्वरूप विकसित किया। उससे प्रस्तुत नागरी 'जैन लिपि' ऐसे स्वतन्त्र नामसे प्रख्यात हुई। वस्तुतः इसके लिए जैन शैली की नागरी' ऐसा कहना अधिक समुचित है। नागरी के जिन अक्षरोकी बनावट में घुमाव (मोडमें) परिवर्तन हुआ है उनकी संख्या पाँच स्वर और छः व्यंजन मिलकर ग्यारह है। स्वरोंमें अ, ऋ, लु, ओ, औ तथा व्यंजनोंमें मुख्यरूपसे छ, ज, द, इ, ण, ८ है।
जैन लिपिमे लिखनेके लिए अग्रमात्रा और पृष्ठमात्रा (पड़ी मात्रा) के दो प्रकार प्रचलित थे। इनमें अग्रमात्राके प्रकारमें हुस्द-दीर्घ चिह्न, अक्षरके ऊपर अथवा नीचे न लिखकर उसके अगले भाग लिखते थे। जैसे-सा और पड़ी के पृष्ठ मात्रा में लेखन का सौदर्य बनाए रखने के लिए मस्तक के ऊपर की मात्रा अक्षर के पीछे उसी अक्षर के मस्तक का स्पर्श करके लिखी जाती थी। जैसे कि 'देवेन्द्र' लिखना हो तो |दावन्द्र । ये दोनों प्रकार आजकल प्रायः नष्ट हो गए है। आजकल तो ये सभी चिह्न ऊर्ध्वमात्रा अथवा अधोमात्राके रूपमें ही लिखे जाते है। तीसरे कोष्ठक की खरोष्ठी लिपि ___ खरोष्ठं नामक आचार्य के नामसे तथा अन्य मतानुसार खर अर्थात् गर्दभ, ओष्ठ-ओठ इस आधार पर इस लिपि के अक्षर गर्दभ के ओष्ठ जैसे मोटे आकारमे लिखे जाने के कारण, अथवा खरोष्ठ नामक जातिके नाम पर इस लिपिका नामकरण हुआ है। इस लिपिकी विशेषता यह है कि स्वरमें मात्राएँ लगाकर लिखा जाता है। जैसे कि- 'अि, ' इत्यादि। इसके मूलाक्षर ३७ है। इसमें स्वर पाँच है और वे ह्रस्व ही है। शेष ३२ व्यञ्जन है। यह लिपि ई.सन्. से पूर्व चौथी शताब्दी में उत्पन्न होकर ई.सन्. की तीसरी शताब्दीमें अस्ताचल पर पहुँच गई थी। जैन ग्रन्थोंमें जहाँ लिपि के प्रकार बताए गए है, वहाँ खरोष्ठीका उल्लेख हुआ है। चौधे कोष्ठक की ब्राह्मी लिपि
जैन अनुश्रुतिके अनुसार इस लिपि का ज्ञान कई अरब वर्षोंसे पूर्व इस युगके आदिमें उत्पन्न प्रथम तीर्थकर भगवान श्री ऋषभदेवने अपनी पुत्री 'ब्राह्मी' को दाहिने हाथसे इस युगमे सबसे पहले दिया तबसे लिखने के लिए 'वर्णमाला' मानवजाति को प्राप्त हुई और लिपि-विज्ञान प्रारम्भ हुआ। यह लिपि 'ब्राह्मीं' के नामसे ब्राह्मी' के रूप में प्रख्यात हुई और यह 'आधलिपि' कहलाई। श्री ऋषभदेवने द्वितीय पुत्री सुन्दरी को अंक ज्ञान सिखाया। अंक भी एक प्रकारकी लिपि ही कहलाती है।
ब्राह्मी लिपि में मूलाक्षरोकी संख्या कितनी थी? इसके लिए जैन आगमसूत्र समवायांग ४६ की संख्या बतलाता है। यद्यपि मूलकार कौनसे ४६ अक्षर है. इस संबंधमे मौन है किन्तु प्रस्तुत अंग की ग्यारहवीं शताब्दी में रचित टीका टीकाकार 'ऋ, ऋ, लू, लू' स्वर तथा '' और 'म्' इन छह के अतिरिक्त ४६ की सम्भावना सूचित करते है।
भारतीय लिपि-विज्ञान के पिता ओझाजी '' अथवा '' इन दोनोंमें से एक का विकल्प सूचित करते है। सातवीं शताब्दी के चीनी यात्री हप-एन-सांगने ४७ तथा अन्यत्र ४२ संख्याका भी सुचन किया है। इस लिपिके आकार कैसे होंगे? इसका निर्देश 'प्रश्न व्याकरण' में हुआ है। वह आजकी लिपि के साथ कही कहीं साम्य रखता है।
१७ कः कुलिशाकृतिः। १८. गजकुम्बाकृतिः पश्या
तात्पर्य यह है कि किसी शब्दके अन्तमें विसर्ग हो और उसके आगे क अथवा खसे आरम्भ होनेवाला शब्द होतो, पूर्व में स्थित विसर्ग का उच्चारण जिल्ला के मूलाग्रभागसे एक विशिष्ट प्रकारसे किया जाता है। इस विशिष्ट उच्चारण की पहचानके लिए वैयाकरणोंने विसर्गके स्थान पर एक प्रकारका संकेतात्मक चिहन वाकृति ४ रखनेका सूचन किया है और उसे 'महापाणविसर्ग' नाम देकर उसाको जिहवाग्रमूलीय वर्णर्की संज्ञा दी है। उदाहरण के लिए 'नृपः कार्य करोति'। इस वाक्यको शुद्ध रूपमें 'नृप x कार्य करोति'। इस तरह ही लिखा जा सकता है।
और विसर्ग के आगे एअथवा आए तो उसका उच्चारण ओष्ठ द्वारा एक विशिष्ट प्रकारसे होता था अतः उसके संकेत के लिए गजके गण्डस्थल के समान xxइन दो चिन्हों में से किसी एक प्रकारका चिन्ह लगता है। इसे उपध्मानीय वर्ण कहते है। उपध्मा अर्थात् ओष्ठ और उससे बोला जानेवाला वर्ण- 'उपध्मानीय'। १९. बावनकी गणना एक दूसरे प्रकारसे भी की जाती है, जिसमे जिह्वामूलीय, उपध्मानीय और अनुनासिक व्यजनोंमेल और व्यजनोंकी भी गणना होती है।
चौथी शतादीके पश्चात् आजकल लिखे जानेवाले न के स्थान पर संयुक्ताक्षरके रूपमें स्वर जोडकर 'का इस तरह लिखा जाता था। बादमें इसने अपना मूल स्वरूप बदलकर स् का रूप धारण किया है। ऐसा होनेपर में कौनसे वर्ण है इसका परिचय देने की आवश्यकता प्रतीत होने पर व्याकरणकारों को कः संयोगे ऐसा विधान करना पड़ा। यही बात श के स्थानपर संयुक्ताक्षर 'ज' के सम्बन्ध में हुई। इसके द्वारा भी अपना कायाकल्प करकेश ऐसा अभिनव रूप धारण करने पर 'जयोः ' ऐसा सूत्र बनाना पड़ा। तथा वर्तमान कालमें प्रयुक्त होनेवाला ''मी प्राचीनकालमें 'तर' इस प्रकार लिखा जाता था,बाद में इसमें 'न' में स्वर मिलाकर 'तर' लिखना पड़ता था अतः यह कालान्तर में 'त्र' के रूपमें नवीन अवतार लेकर प्रस्तुत हुआ। ये केवल वर्ण नहीं है, अपितु संयुक्त वर्ण है। २०. इस लिपिमें ई. सन् १००८ में लिखा हुआ एक ग्रन्थ लन्दन केम्बिज में है। तथा विशेषावश्यक भाष्य टीका' नामक कृति भी नागर लिपिये है, जो कि जैसलमेर के भण्डारमें है। मैंने इसके दर्शन किये है। इनके अतिरिक्त नागरी अभिलेखोंके अमरोसे मिलते-जुलते अक्षरोवाली ताडपत्रीय प्रतियाँ बहुत मिलती है। जिनका समय १०-११ वी शताब्दी है। २१. ऐसा भी प्रश्न किया जा सकता है कि जैन लिपि से नागरी लिपि का जन्म क्यो न हुआ हो? २२, यह मान्यता चीनी विद्वानों की है। २३. विगत ३०-४० वर्चासे भारतके गांधीवादी मंडलोंमें इस प्रकारकी लिपि का प्रयोग किया जा रहा है। २४. तुर्कस्तान आदि देश जहाँ कि भारतीय अथवा बौद्धसभ्यता व्याप्त बी, वहाँ यह लिपि बहुत समय तक प्रचलित रही थी। २५. ब्रामी-लिपिकी उत्पत्ति के बारेमें अजैन लोग ब्रह्मा को कारणरूप मानते है और बहमासे प्राप्त होने के कारण इसका ग्रामी नाम पहा है ऐसा कहते है। चीन का विश्वकोश भी इस बात का समर्थन करता है। दोनों अनुश्रुतियाँ इसकी प्राचीनता को स्वीकृत करती है यह स्पष्ट है। २६. शून्य अंक की खोज पूर्णतः भारतीय है। इस देश ने ही अन्य देशोको शून्य अक की भेट दी है।
१५२ Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org