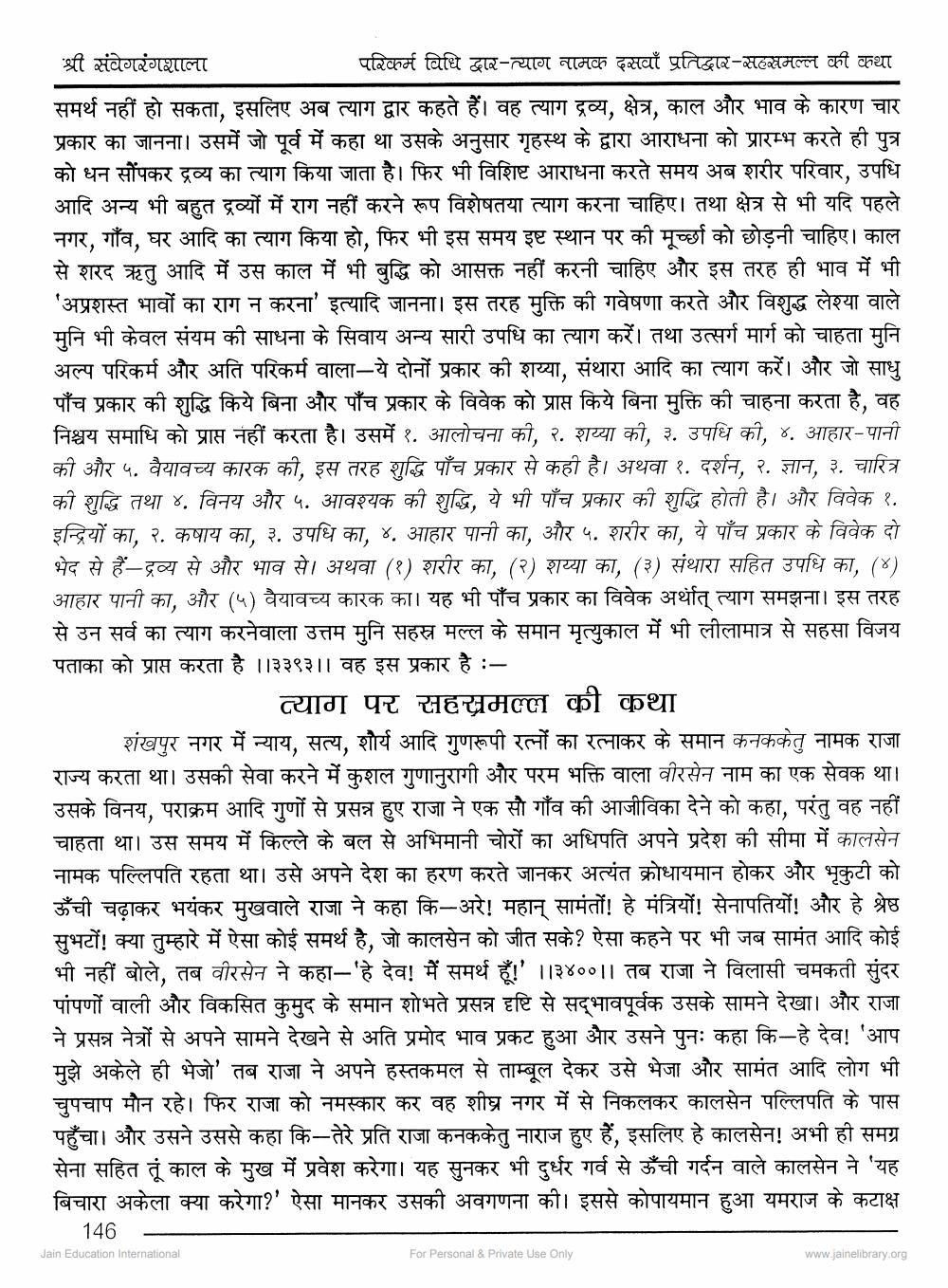________________
श्री संवेगरंगशाला
परिकर्म विधि द्वार-त्याग नामक दसवाँ प्रतिद्धार-सहसमल्ल की कथा समर्थ नहीं हो सकता, इसलिए अब त्याग द्वार कहते हैं। वह त्याग द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के कारण चार प्रकार का जानना। उसमें जो पूर्व में कहा था उसके अनुसार गृहस्थ के द्वारा आराधना को प्रारम्भ करते ही पुत्र को धन सौंपकर द्रव्य का त्याग किया जाता है। फिर भी विशिष्ट आराधना करते समय अब शरीर परिवार, उपधि आदि अन्य भी बहत द्रव्यों में राग नहीं करने रूप विशेषतया त्याग करना चाहिए। तथा क्षेत्र से भी यदि पहले नगर, गाँव, घर आदि का त्याग किया हो, फिर भी इस समय इष्ट स्थान पर की मूर्छा को छोड़नी चाहिए। काल से शरद ऋतु आदि में उस काल में भी बुद्धि को आसक्त नहीं करनी चाहिए और इस तरह ही भाव में भी 'अप्रशस्त भावों का राग न करना' इत्यादि जानना। इस तरह मुक्ति की गवेषणा करते और विशुद्ध लेश्या वाले मुनि भी केवल संयम की साधना के सिवाय अन्य सारी उपधि का त्याग करें। तथा उत्सर्ग मार्ग को चाहता मुनि अल्प परिकर्म और अति परिकर्म वाला—ये दोनों प्रकार की शय्या, संथारा आदि का त्याग करें। और जो साधु पाँच प्रकार की शुद्धि किये बिना और पाँच प्रकार के विवेक को प्राप्त किये बिना मुक्ति की चाहना करता है, वह निश्चय समाधि को प्राप्त नहीं करता है। उसमें १. आलोचना की, २. शय्या की, ३. उपधि की, ४. आहार-पानी की और ५. वैयावच्य कारक की, इस तरह शुद्धि पाँच प्रकार से कही है। अथवा १. दर्शन, २. ज्ञान, ३. चारित्र की शुद्धि तथा ४. विनय और ५. आवश्यक की शुद्धि, ये भी पाँच प्रकार की शुद्धि होती है। और विवेक १. इन्द्रियों का, २. कषाय का, ३. उपधि का, ४. आहार पानी का, और ५. शरीर का, ये पाँच प्रकार के विवेक दो भेद से हैं-द्रव्य से और भाव से। अथवा (१) शरीर का, (२) शय्या का, (३) संथारा सहित उपधि का, (४) आहार पानी का, और (५) वैयावच्य कारक का। यह भी पाँच प्रकार का विवेक अर्थात् त्याग समझना। इस तरह से उन सर्व का त्याग करनेवाला उत्तम मुनि सहस्र मल्ल के समान मृत्युकाल में भी लीलामात्र से सहसा विजय पताका को प्राप्त करता है ।।३३९३ ।। वह इस प्रकार है :
त्याग पर सहलमल्ल की कथा शंखपुर नगर में न्याय, सत्य, शौर्य आदि गुणरूपी रत्नों का रत्नाकर के समान कनककेतु नामक राजा राज्य करता था। उसकी सेवा करने में कुशल गुणानुरागी और परम भक्ति वाला वीरसेन नाम का एक सेवक था। उसके विनय, पराक्रम आदि गुणों से प्रसन्न हुए राजा ने एक सौ गाँव की आजीविका देने को कहा, परंतु वह नहीं चाहता था। उस समय में किल्ले के बल से अभिमानी चोरों का अधिपति अपने प्रदेश की सीमा में कालसेन नामक पल्लिपति रहता था। उसे अपने देश का हरण करते जानकर अत्यंत क्रोधायमान होकर और भृकुटी को ऊँची चढ़ाकर भयंकर मुखवाले राजा ने कहा कि-अरे! महान् सामंतों! हे मंत्रियों! सेनापतियों! और हे श्रेष्ठ सुभटों! क्या तुम्हारे में ऐसा कोई समर्थ है, जो कालसेन को जीत सके? ऐसा कहने पर भी जब सामंत आदि कोई भी नहीं बोले, तब वीरसेन ने कहा-'हे देव! मैं समर्थ हूँ!' ।।३४००।। तब राजा ने विला पांपणों वाली और विकसित कुमुद के समान शोभते प्रसन्न दृष्टि से सद्भावपूर्वक उसके सामने देखा। और राजा ने प्रसन्न नेत्रों से अपने सामने देखने से अति प्रमोद भाव प्रकट हुआ और उसने पुनः कहा कि-हे देव! 'आप मुझे अकेले ही भेजो' तब राजा ने अपने हस्तकमल से ताम्बूल देकर उसे भेजा और सामंत आदि लोग भी चुपचाप मौन रहे। फिर राजा को नमस्कार कर वह शीघ्र नगर में से निकलकर कालसेन पल्लिपति के पास पहुँचा। और उसने उससे कहा कि-तेरे प्रति राजा कनककेतु नाराज हुए हैं, इसलिए हे कालसेन! अभी ही समग्र सेना सहित तूं काल के मुख में प्रवेश करेगा। यह सुनकर भी दुर्धर गर्व से ऊँची गर्दन वाले कालसेन ने 'यह बिचारा अकेला क्या करेगा?' ऐसा मानकर उसकी अवगणना की। इससे कोपायमान हुआ यमराज के कटाक्ष 146 -
For Personal & Private Use Only
Jain Education International
www.jainelibrary.org