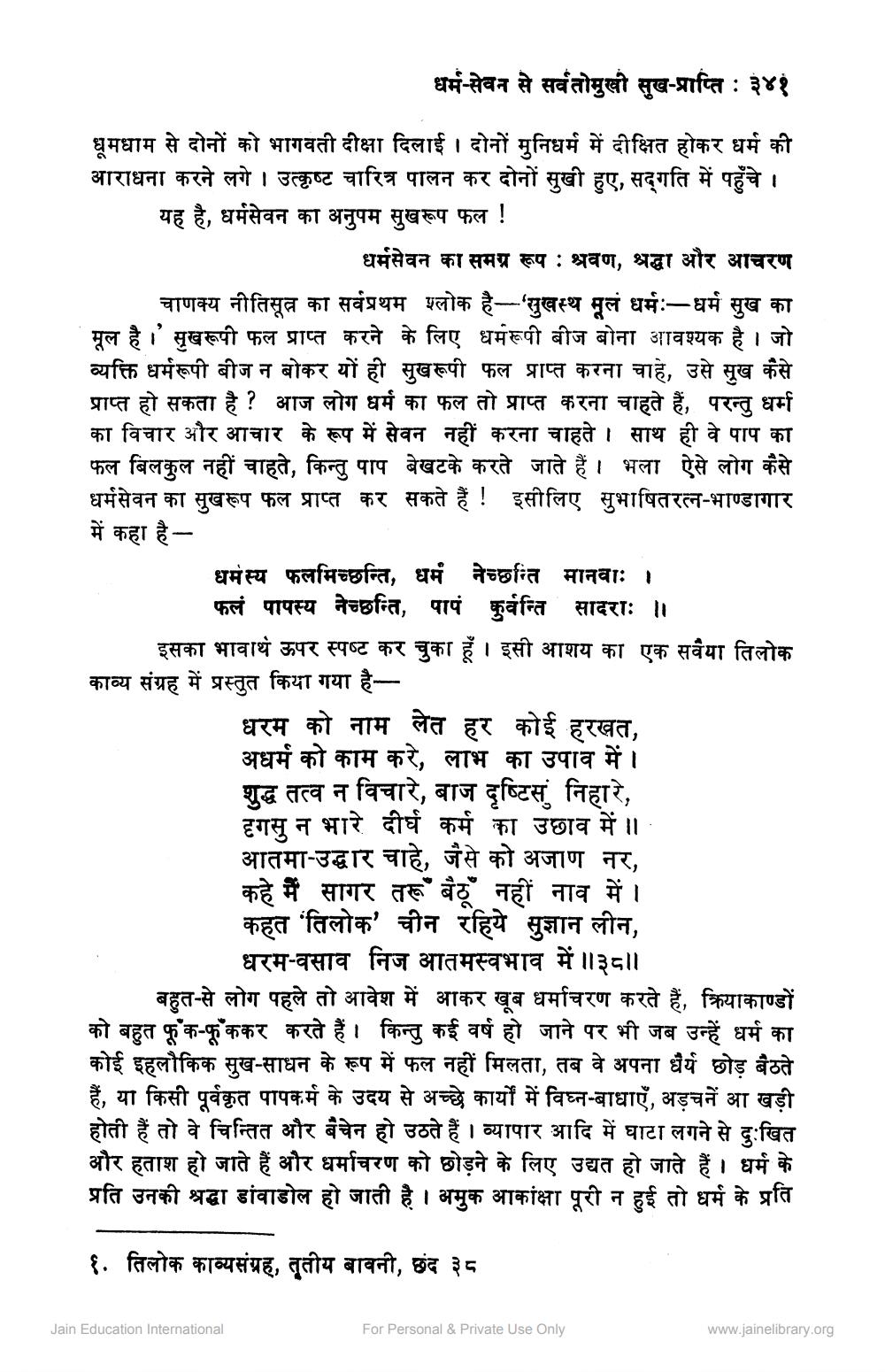________________
धर्म-सेवन से सर्वतोमुखी सुख-प्राप्ति : ३४१ धूमधाम से दोनों को भागवती दीक्षा दिलाई। दोनों मुनिधर्म में दीक्षित होकर धर्म की आराधना करने लगे। उत्कृष्ट चारित्र पालन कर दोनों सुखी हुए, सद्गति में पहुंचे। यह है, धर्मसेवन का अनुपम सुखरूप फल !
धर्मसेवन का समग्न रूप : श्रवण, श्रद्धा और आचरण चाणक्य नीतिसूत्र का सर्वप्रथम श्लोक है- 'सुखस्थ मूलं धर्मः-धर्म सुख का मूल है।' सुखरूपी फल प्राप्त करने के लिए धर्मरूपी बीज बोना आवश्यक है। जो व्यक्ति धर्मरूपी बीज न बोकर यों ही सुखरूपी फल प्राप्त करना चाहे, उसे सुख कैसे प्राप्त हो सकता है ? आज लोग धर्म का फल तो प्राप्त करना चाहते हैं, परन्तु धर्म का विचार और आचार के रूप में सेवन नहीं करना चाहते । साथ ही वे पाप का फल बिलकुल नहीं चाहते, किन्तु पाप बेखटके करते जाते हैं। भला ऐसे लोग कैसे धर्मसेवन का सुखरूप फल प्राप्त कर सकते हैं ! इसीलिए सुभाषितरत्न-भाण्डागार में कहा है
धर्मस्य फलमिच्छन्ति, धर्म नेच्छन्ति मानवाः ।
फलं पापस्य नेच्छन्ति, पापं कुर्वन्ति सादराः ॥ इसका भावार्थ ऊपर स्पष्ट कर चुका हूँ। इसी आशय का एक सवैया तिलोक काव्य संग्रह में प्रस्तुत किया गया है
धरम को नाम लेत हर कोई हरखत, अधर्म को काम करे, लाभ का उपाव में। शुद्ध तत्व न विचारे, बाज दृष्टिसं निहारे, दृगसु न भारे दीर्घ कर्म का उछाव में । आतमा-उद्धार चाहे, जैसे को अजाण नर, कहे मैं सागर तरू बैठ नहीं नाव में। कहत तिलोक' चीन रहिये सुज्ञान लीन,
धरम-वसाव निज आतमस्वभाव में ॥३८॥ बहुत-से लोग पहले तो आवेश में आकर खूब धर्माचरण करते हैं, क्रियाकाण्डों को बहुत फूंक-फूककर करते हैं। किन्तु कई वर्ष हो जाने पर भी जब उन्हें धर्म का कोई इहलौकिक सुख-साधन के रूप में फल नहीं मिलता, तब वे अपना धैर्य छोड़ बैठते हैं, या किसी पूर्वकृत पापकर्म के उदय से अच्छे कार्यों में विघ्न-बाधाएँ, अड़चनें आ खड़ी होती हैं तो वे चिन्तित और बैचेन हो उठते हैं । व्यापार आदि में घाटा लगने से दुःखित और हताश हो जाते हैं और धर्माचरण को छोड़ने के लिए उद्यत हो जाते हैं। धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा डांवाडोल हो जाती है । अमुक आकांक्षा पूरी न हुई तो धर्म के प्रति
१. तिलोक काव्यसंग्रह, तृतीय बावनी, छंद ३८
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org