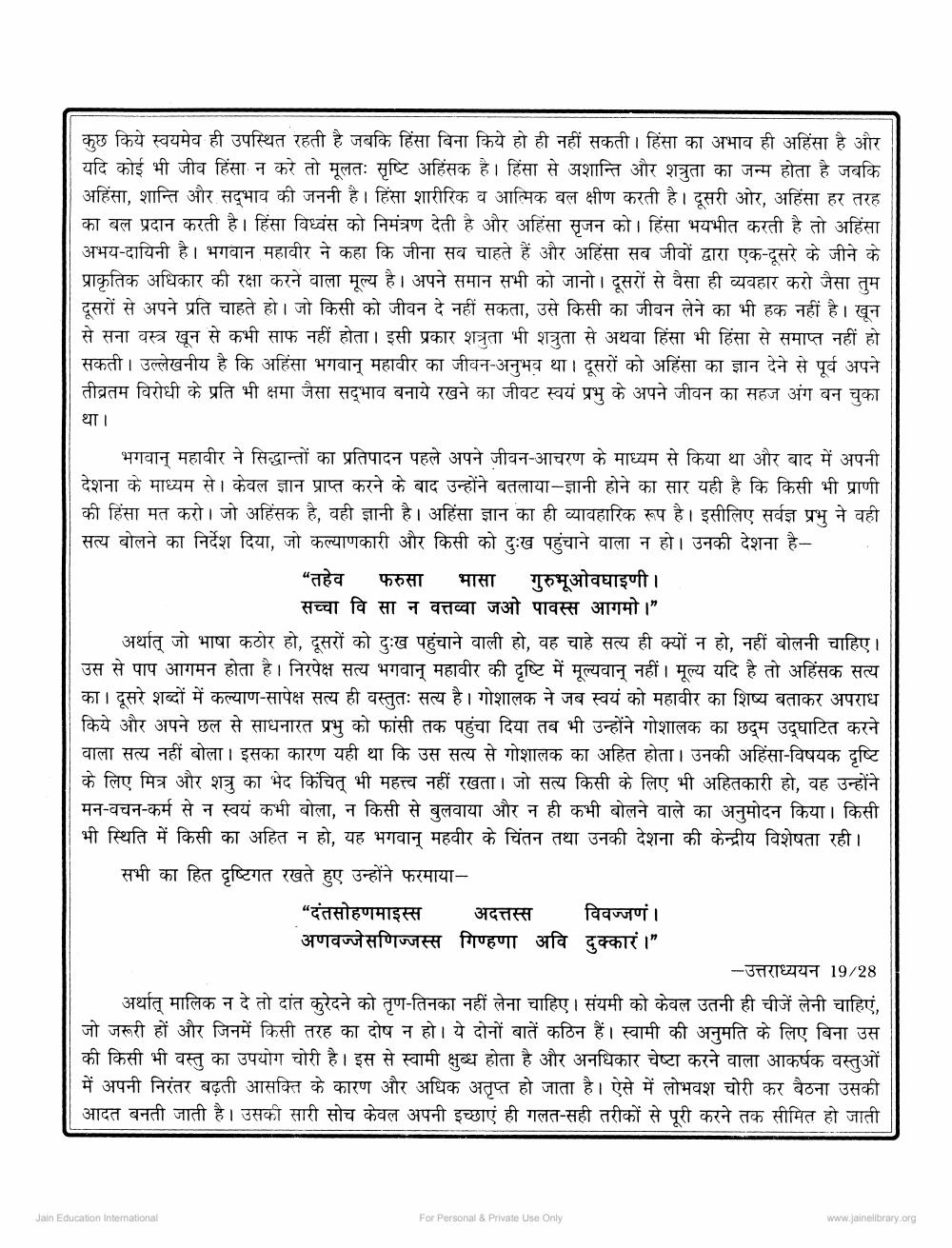________________
कुछ किये स्वयमेव ही उपस्थित रहती है जबकि हिंसा बिना किये हो ही नहीं सकती। हिंसा का अभाव ही अहिंसा है और यदि कोई भी जीव हिंसा न करे तो मूलतः सृष्टि अहिंसक है। हिंसा से अशान्ति और शत्रुता का जन्म होता है जबकि अहिंसा, शान्ति और सद्भाव की जननी है। हिंसा शारीरिक व आत्मिक बल क्षीण करती है। दूसरी ओर, अहिंसा हर तरह का बल प्रदान करती है। हिंसा विध्वंस को निमंत्रण देती है और अहिंसा सृजन को। हिंसा भयभीत करती है तो अहिंसा अभय-दायिनी है। भगवान महावीर ने कहा कि जीना सब चाहते हैं और अहिंसा सब जीवों द्वारा एक-दूसरे के जीने के प्राकृतिक अधिकार की रक्षा करने वाला मूल्य है। अपने समान सभी को जानो। दूसरों से वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। जो किसी को जीवन दे नहीं सकता, उसे किसी का जीवन लेने का भी हक नहीं है। खून से सना वस्त्र खून से कभी साफ नहीं होता। इसी प्रकार शत्रुता भी शत्रुता से अथवा हिंसा भी हिंसा से समाप्त नहीं हो सकती। उल्लेखनीय है कि अहिंसा भगवान महावीर का जीवन-अनुभव था। दूसरों को अहिंसा का ज्ञान देने से पूर्व अपने तीव्रतम विरोधी के प्रति भी क्षमा जैसा सदभाव बनाये रखने का जीवट स्वयं प्रभु के अपने जीवन का सहज अंग बन चुका था।
भगवान् महावीर ने सिद्धान्तों का प्रतिपादन पहले अपने जीवन-आचरण के माध्यम से किया था और बाद में अपनी देशना के माध्यम से। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने बतलाया-ज्ञानी होने का सार यही है कि किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। जो अहिंसक है, वही ज्ञानी है। अहिंसा ज्ञान का ही व्यावहारिक रूप है। इसीलिए सर्वज्ञ प्रभु ने वही सत्य बोलने का निर्देश दिया, जो कल्याणकारी और किसी को दुःख पहुंचाने वाला न हो। उनकी देशना है
"तहेव फरुसा भासा गुरुभूओवघाइणी।
सच्चा वि सा न वत्तव्वा जओ पावस्स आगमो।" अर्थात् जो भाषा कठोर हो, दूसरों को दुःख पहुंचाने वाली हो, वह चाहे सत्य ही क्यों न हो, नहीं बोलनी चाहिए। उस से पाप आगमन होता है। निरपेक्ष सत्य भगवान् महावीर की दृष्टि में मूल्यवान् नहीं। मूल्य यदि है तो अहिंसक सत्य का। दूसरे शब्दों में कल्याण-सापेक्ष सत्य ही वस्तुतः सत्य है। गोशालक ने जब स्वयं को महावीर का शिष्य बताकर अपराध किये और अपने छल से साधनारत प्रभु को फांसी तक पहुंचा दिया तब भी उन्होंने गोशालक का छद्म उद्घाटित करने वाला सत्य नहीं बोला। इसका कारण यही था कि उस सत्य से गोशालक का अहित होता। उनकी अहिंसा-विषयक दृष्टि के लिए मित्र और शत्रु का भेद किंचित् भी महत्त्व नहीं रखता। जो सत्य किसी के लिए भी अहितकारी हो, वह उन्होंने मन-वचन-कर्म से न स्वयं कभी बोला, न किसी से बुलवाया और न ही कभी बोलने वाले का अनुमोदन किया। किसी भी स्थिति में किसी का अहित न हो, यह भगवान् महवीर के चिंतन तथा उनकी देशना की केन्द्रीय विशेषता रही। सभी का हित दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने फरमाया
"दंतसोहणमाइस्स अदत्तस्स विवज्जणं। अणवज्जेसणिज्जस्स गिण्हणा अवि दुक्कारं।"
-उत्तराध्ययन 19/28 अर्थात् मालिक न दे तो दांत कुरेदने को तृण-तिनका नहीं लेना चाहिए। संयमी को केवल उतनी ही चीजें लेनी चाहिएं, जो जरूरी हों और जिनमें किसी तरह का दोष न हो। ये दोनों बातें कठिन हैं। स्वामी की अनुमति के लिए बिना उस की किसी भी वस्तु का उपयोग चोरी है। इस से स्वामी क्षुब्ध होता है और अनधिकार चेष्टा करने वाला आकर्षक वस्तुओं में अपनी निरंतर बढ़ती आसक्ति के कारण और अधिक अतृप्त हो जाता है। ऐसे में लोभवश चोरी कर बैठना उसकी आदत बनती जाती है। उसकी सारी सोच केवल अपनी इच्छाएं ही गलत-सही तरीकों से पूरी करने तक सीमित हो जाती
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org