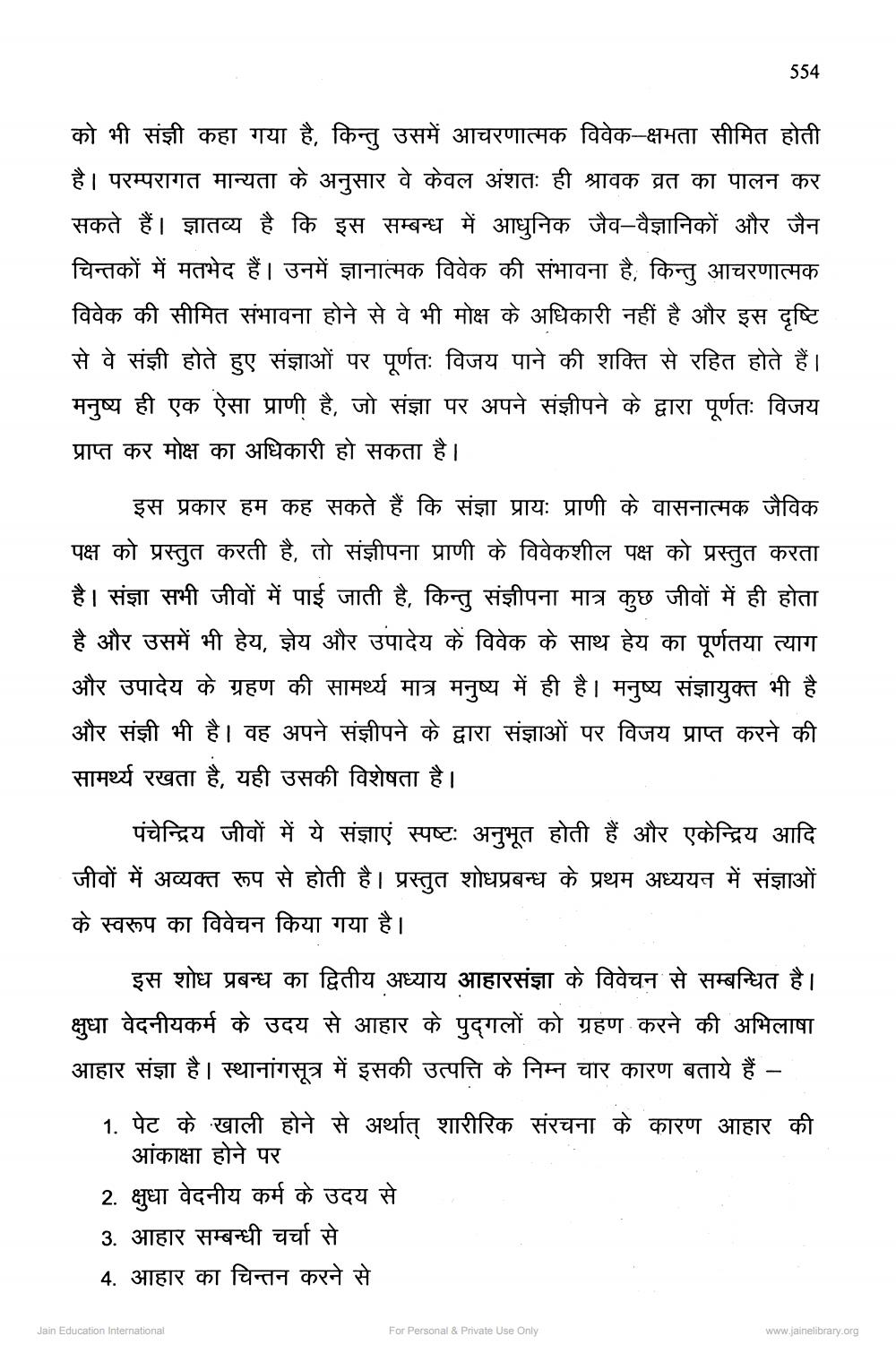________________
554
को भी संज्ञी कहा गया है, किन्तु उसमें आचरणात्मक विवेक-क्षमता सीमित होती है। परम्परागत मान्यता के अनुसार वे केवल अंशतः ही श्रावक व्रत का पालन कर सकते हैं। ज्ञातव्य है कि इस सम्बन्ध में आधुनिक जैव-वैज्ञानिकों और जैन चिन्तकों में मतभेद हैं। उनमें ज्ञानात्मक विवेक की संभावना है, किन्तु आचरणात्मक विवेक की सीमित संभावना होने से वे भी मोक्ष के अधिकारी नहीं है और इस दृष्टि से वे संज्ञी होते हुए संज्ञाओं पर पूर्णतः विजय पाने की शक्ति से रहित होते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, जो संज्ञा पर अपने संज्ञीपने के द्वारा पूर्णतः विजय प्राप्त कर मोक्ष का अधिकारी हो सकता है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा प्रायः प्राणी के वासनात्मक जैविक पक्ष को प्रस्तुत करती है, तो संज्ञीपना प्राणी के विवेकशील पक्ष को प्रस्तुत करता है। संज्ञा सभी जीवों में पाई जाती है, किन्तु संज्ञीपना मात्र कुछ जीवों में ही होता है और उसमें भी हेय, ज्ञेय और उपादेय के विवेक के साथ हेय का पूर्णतया त्याग और उपादेय के ग्रहण की सामर्थ्य मात्र मनुष्य में ही है। मनुष्य संज्ञायुक्त भी है और संज्ञी भी है। वह अपने संज्ञीपने के द्वारा संज्ञाओं पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य रखता है, यही उसकी विशेषता है।
पंचेन्द्रिय जीवों में ये संज्ञाएं स्पष्ट: अनुभूत होती हैं और एकेन्द्रिय आदि जीवों में अव्यक्त रूप से होती है। प्रस्तुत शोधप्रबन्ध के प्रथम अध्ययन में संज्ञाओं के स्वरूप का विवेचन किया गया है।
इस शोध प्रबन्ध का द्वितीय अध्याय आहारसंज्ञा के विवेचन से सम्बन्धित है। क्षुधा वेदनीयकर्म के उदय से आहार के पुद्गलों को ग्रहण करने की अभिलाषा आहार संज्ञा है। स्थानांगसूत्र में इसकी उत्पत्ति के निम्न चार कारण बताये हैं - 1. पेट के खाली होने से अर्थात् शारीरिक संरचना के कारण आहार की
आंकाक्षा होने पर 2. क्षुधा वेदनीय कर्म के उदय से 3. आहार सम्बन्धी चर्चा से 4. आहार का चिन्तन करने से
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org