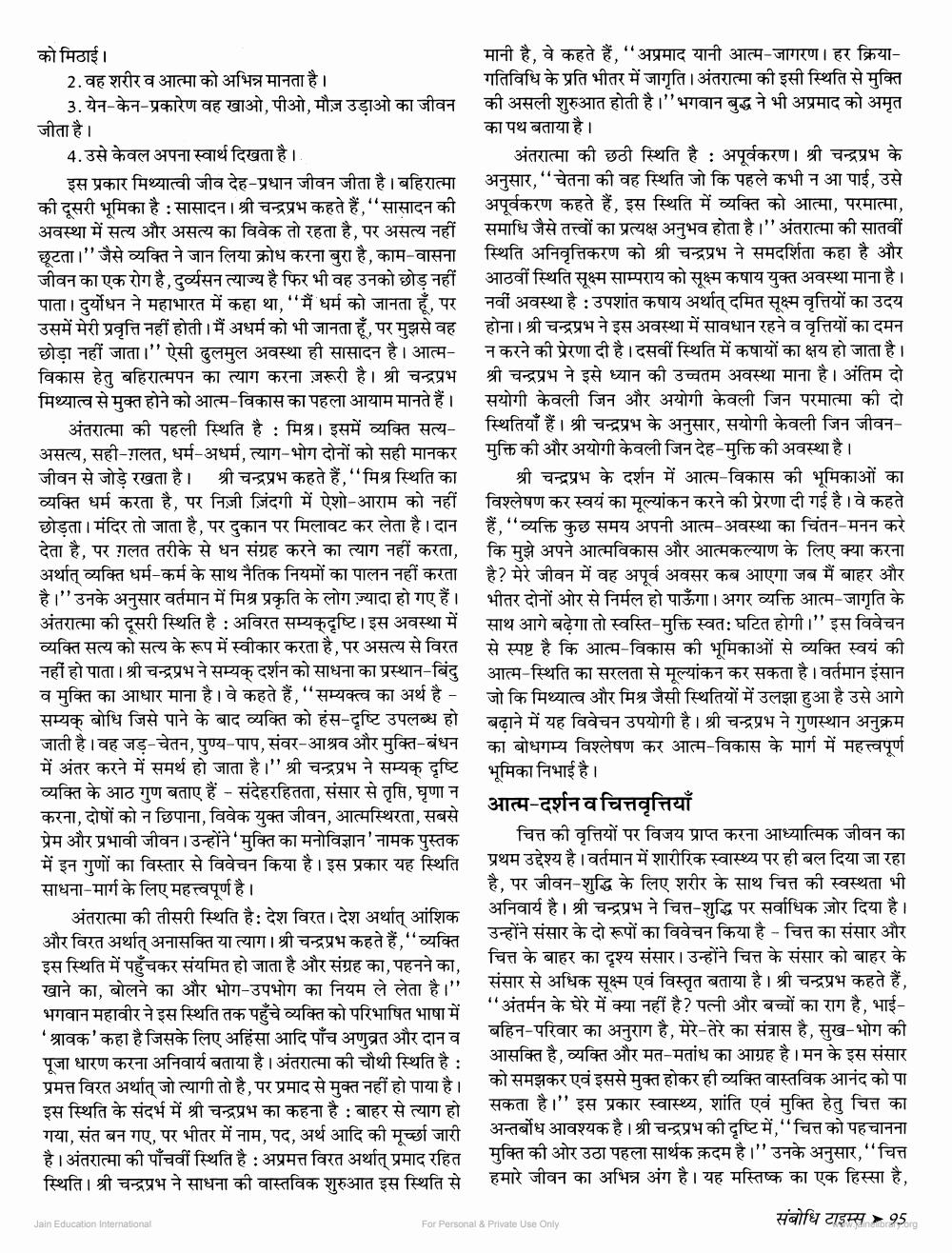________________
को मिठाई।
मानी है, वे कहते हैं, "अप्रमाद यानी आत्म-जागरण। हर क्रिया2. वह शरीर व आत्मा को अभिन्न मानता है।
गतिविधि के प्रति भीतर में जागृति । अंतरात्मा की इसी स्थिति से मुक्ति 3. येन-केन-प्रकारेण वह खाओ, पीओ, मौज़ उड़ाओ का जीवन की असली शुरुआत होती है।" भगवान बुद्ध ने भी अप्रमाद को अमृत जीता है।
का पथ बताया है। 4. उसे केवल अपना स्वार्थ दिखता है।
__अंतरात्मा की छठी स्थिति है : अपूर्वकरण। श्री चन्द्रप्रभ के इस प्रकार मिथ्यात्वी जीव देह-प्रधान जीवन जीता है। बहिरात्मा अनुसार, "चेतना की वह स्थिति जो कि पहले कभी न आ पाई, उसे की दूसरी भूमिका है : सासादन। श्री चन्द्रप्रभ कहते हैं, "सासादन की अपूर्वकरण कहते हैं, इस स्थिति में व्यक्ति को आत्मा, परमात्मा, अवस्था में सत्य और असत्य का विवेक तो रहता है, पर असत्य नहीं समाधि जैसे तत्त्वों का प्रत्यक्ष अनुभव होता है।" अंतरात्मा की सातवीं छूटता।" जैसे व्यक्ति ने जान लिया क्रोध करना बुरा है, काम-वासना स्थिति अनिवृत्तिकरण को श्री चन्द्रप्रभ ने समदर्शिता कहा है और जीवन का एक रोग है, दुर्व्यसन त्याज्य है फिर भी वह उनको छोड़ नहीं आठवीं स्थिति सूक्ष्म साम्पराय को सूक्ष्म कषाय युक्त अवस्था माना है। पाता। दुर्योधन ने महाभारत में कहा था, "मैं धर्म को जानता हूँ, पर नवी अवस्था है : उपशांत कषाय अर्थात् दमित सूक्ष्म वृत्तियों का उदय उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को भी जानता हूँ, पर मुझसे वह होना। श्री चन्द्रप्रभ ने इस अवस्था में सावधान रहने व वृत्तियों का दमन छोड़ा नहीं जाता।" ऐसी ढुलमुल अवस्था ही सासादन है। आत्म- न करने की प्रेरणा दी है। दसवीं स्थिति में कषायों का क्षय हो जाता है। विकास हेतु बहिरात्मपन का त्याग करना ज़रूरी है। श्री चन्द्रप्रभ श्री चन्द्रप्रभ ने इसे ध्यान की उच्चतम अवस्था माना है। अंतिम दो मिथ्यात्व से मुक्त होने को आत्म-विकास का पहला आयाम मानते हैं। सयोगी केवली जिन और अयोगी केवली जिन परमात्मा की दो
अंतरात्मा की पहली स्थिति है : मिश्र। इसमें व्यक्ति सत्य- स्थितियाँ हैं। श्री चन्द्रप्रभ के अनुसार, सयोगी केवली जिन जीवनअसत्य, सही-ग़लत, धर्म-अधर्म, त्याग-भोग दोनों को सही मानकर मुक्ति की और अयोगी केवली जिन देह-मुक्ति की अवस्था है। जीवन से जोड़े रखता है। श्री चन्द्रप्रभ कहते हैं, "मिश्र स्थिति का श्री चन्द्रप्रभ के दर्शन में आत्म-विकास की भूमिकाओं का व्यक्ति धर्म करता है, पर निजी जिंदगी में ऐशो-आराम को नहीं विश्लेषण कर स्वयं का मूल्यांकन करने की प्रेरणा दी गई है। वे कहते छोड़ता। मंदिर तो जाता है, पर दुकान पर मिलावट कर लेता है। दान हैं, "व्यक्ति कुछ समय अपनी आत्म-अवस्था का चिंतन-मनन करे देता है, पर ग़लत तरीके से धन संग्रह करने का त्याग नहीं करता, कि मुझे अपने आत्मविकास और आत्मकल्याण के लिए क्या करना अर्थात् व्यक्ति धर्म-कर्म के साथ नैतिक नियमों का पालन नहीं करता है? मेरे जीवन में वह अपूर्व अवसर कब आएगा जब मैं बाहर और है।" उनके अनुसार वर्तमान में मिश्र प्रकृति के लोग ज़्यादा हो गए हैं। भीतर दोनों ओर से निर्मल हो पाऊँगा। अगर व्यक्ति आत्म-जागृति के अंतरात्मा की दूसरी स्थिति है : अविरत सम्यक्दृष्टि। इस अवस्था में साथ आगे बढ़ेगा तो स्वस्ति-मुक्ति स्वत: घटित होगी।" इस विवेचन व्यक्ति सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार करता है, पर असत्य से विरत से स्पष्ट है कि आत्म-विकास की भूमिकाओं से व्यक्ति स्वयं की नहीं हो पाता। श्री चन्द्रप्रभ ने सम्यक् दर्शन को साधना का प्रस्थान-बिंदु आत्म-स्थिति का सरलता से मूल्यांकन कर सकता है। वर्तमान इंसान व मुक्ति का आधार माना है। वे कहते हैं, "सम्यक्त्व का अर्थ है - जो कि मिथ्यात्व और मिश्र जैसी स्थितियों में उलझा हुआ है उसे आगे सम्यक बोधि जिसे पाने के बाद व्यक्ति को हंस-दृष्टि उपलब्ध हो बढाने में यह विवेचन उपयोगी है। श्री चन्द्रप्रभ ने गुणस्थान अनुक्रम जाती है। वह जड़-चेतन, पुण्य-पाप, संवर-आश्रव और मुक्ति-बंधन का बोधगम्य विश्लेषण कर आत्म-विकास के मार्ग में महत्त्वपूर्ण में अंतर करने में समर्थ हो जाता है।" श्री चन्द्रप्रभ ने सम्यक् दृष्टि भूमिका निभाई है। व्यक्ति के आठ गुण बताए हैं - संदेहरहितता, संसार से तृप्ति, घृणा न
आत्म-दर्शन वचित्तवृत्तियाँ करना, दोषों को न छिपाना, विवेक युक्त जीवन, आत्मस्थिरता, सबसे प्रेम और प्रभावी जीवन । उन्होंने मुक्ति का मनोविज्ञान' नामक पुस्तक
चित्त की वृत्तियों पर विजय प्राप्त करना आध्यात्मिक जीवन का में इन गुणों का विस्तार से विवेचन किया है। इस प्रकार यह स्थिति
प्रथम उद्देश्य है। वर्तमान में शारीरिक स्वास्थ्य पर ही बल दिया जा रहा साधना-मार्ग के लिए महत्त्वपूर्ण है।
है, पर जीवन-शुद्धि के लिए शरीर के साथ चित्त की स्वस्थता भी अंतरात्मा की तीसरी स्थिति है: देश विरत । देश अर्थात् आंशिक
__ अनिवार्य है। श्री चन्द्रप्रभ ने चित्त-शुद्धि पर सर्वाधिक ज़ोर दिया है। और विरत अर्थात् अनासक्ति या त्याग। श्री चन्द्रप्रभ कहते हैं, "व्यक्ति
उन्होंने संसार के दो रूपों का विवेचन किया है - चित्त का संसार और इस स्थिति में पहुँचकर संयमित हो जाता है और संग्रह का, पहनने का,
चित्त के बाहर का दृश्य संसार। उन्होंने चित्त के संसार को बाहर के खाने का, बोलने का और भोग-उपभोग का नियम ले लेता है।"
संसार से अधिक सूक्ष्म एवं विस्तृत बताया है। श्री चन्द्रप्रभ कहते हैं, भगवान महावीर ने इस स्थिति तक पहुँचे व्यक्ति को परिभाषित भाषा में
"अंतर्मन के घेरे में क्या नहीं है? पत्नी और बच्चों का राग है, भाई'श्रावक' कहा है जिसके लिए अहिंसा आदि पाँच अणुव्रत और दान व बाहन
बहिन-परिवार का अनुराग है, मेरे-तेरे का संत्रास है, सुख-भोग की पूजा धारण करना अनिवार्य बताया है। अंतरात्मा की चौथी स्थिति है :
आसक्ति है, व्यक्ति और मत-मतांध का आग्रह है। मन के इस संसार प्रमत्त विरत अर्थात् जो त्यागी तो है, पर प्रमाद से मुक्त नहीं हो पाया है। का समझकर एव इसस मुक्त होकर हा व्याक्त वास्तावक आनद का पा इस स्थिति के संदर्भ में श्री चन्द्रप्रभ का कहना है : बाहर से त्याग हो सकता है।" इस प्रकार स्वास्थ्य, शांति एवं मुक्ति हेतु चित्त का गया संत बन गए पर भीतर में नाम पट अर्थ आदि की मर्जी जारी अन्तर्बोध आवश्यक है। श्री चन्द्रप्रभ की दृष्टि में, "चित्त को पहचानना है। अंतरात्मा की पाँचवीं स्थिति है : अप्रमत्त विरत अर्थात प्रमाद रहित मुक्ति की और उठा पहला सार्थक क़दम है।" उनके अनुसार, "चित्त स्थिति। श्री चन्द्रप्रभ ने साधना की वास्तविक शरुआत इस स्थिति से हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। यह मस्तिष्क का एक हिस्सा है.
Jain Education International
संबोधि टाइम्स-95
For Personal & Private Use Only