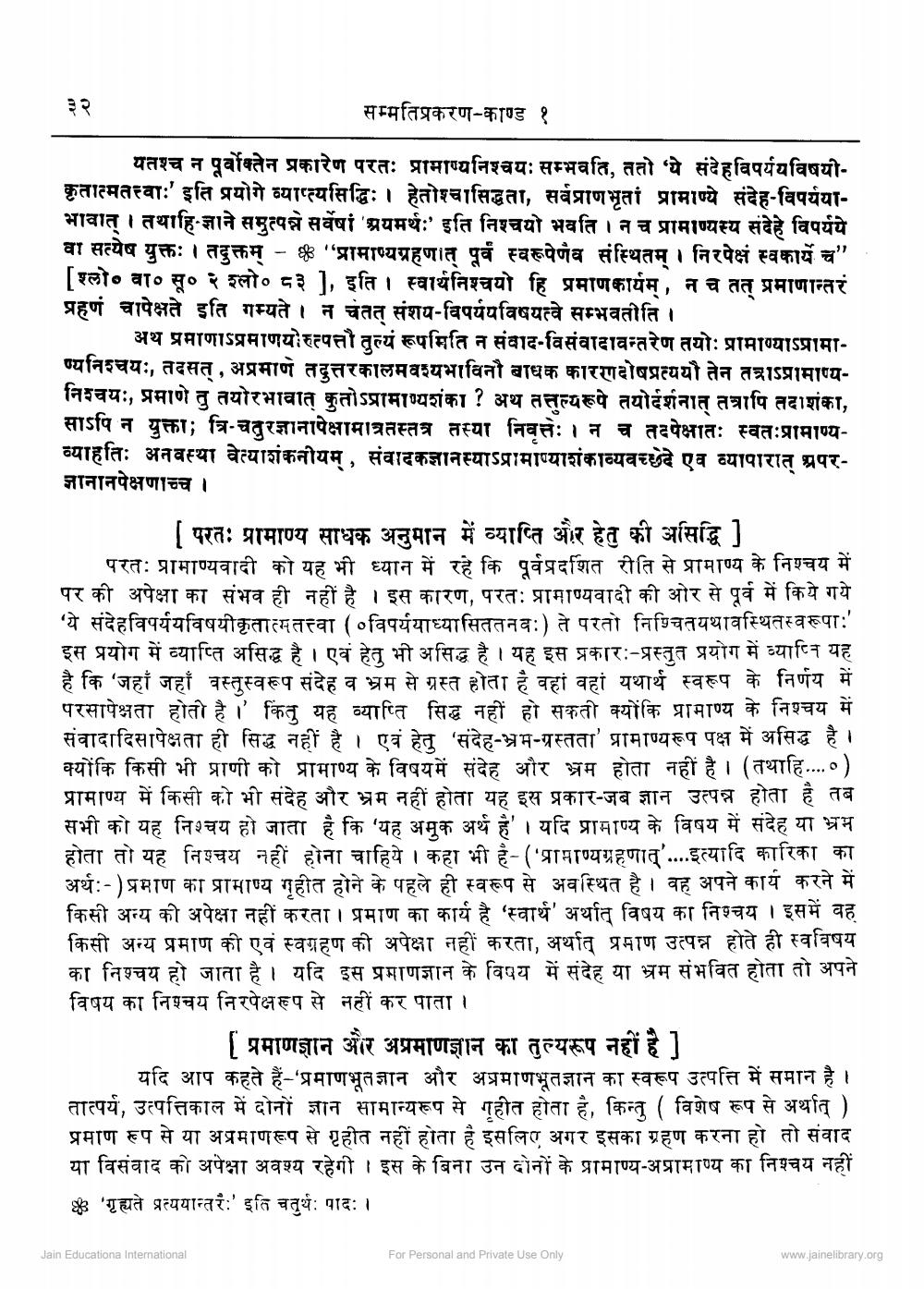________________
सम्मतिप्रकरण-काण्ड १
यतश्च न पूर्वोक्तेन प्रकारेण परतः प्रामाण्यनिश्चयः सम्भवति, ततो ये संदेहविपर्ययविषयीकृतात्मतत्वाः' इति प्रयोगे व्याप्त्यसिद्धिः। हेतोश्चासिद्धता, सर्वप्राणभृतां प्रामाण्ये संदेह-विपर्ययाभावात् । तथाहि-ज्ञाने समुत्पन्ने सर्वेषां 'अयमर्थः' इति निश्चयो भवति । न च प्रामाण्यस्य संदेहे विपर्यये वा सत्येष युक्तः । तदुक्तम् - * "प्रामाण्यग्रहणात पूर्व स्वरूपेणैव संस्थितम् । निरपेक्षं स्वकार्ये च" [श्लो० वा० सू०२ श्लो० ८३ ], इति । स्वार्थनिश्चयो हि प्रमाणकार्यम् , न च तत् प्रमाणान्तरं प्रहणं चापेक्षते इति गम्यते। न चतत् संशय-विपर्ययविषयत्वे सम्भवतीति ।
अथ प्रमाणाऽप्रमाणयोरुत्पत्तौ तुल्यं रूपमिति न संवाद-विसंवादावन्तरेण तयोः प्रामाण्याऽप्रामाण्यनिश्चयः, तदसत् , अप्रमाणे तदुत्तरकालमवश्यभाविनौ बाधक कारणदोषप्रत्ययौ तेन तत्राप्रामाण्यनिश्चयः, प्रमाणे तु तयोरभावात् कुतोऽप्रामाण्यशंका ? अथ तत्तुल्यरूपे तयोर्दर्शनात् तत्रापि तदाशंका, साऽपि न युक्ता; त्रि-चतुरज्ञानापेक्षामात्रतस्तत्र तस्या निवृत्तेः । न च तदपेक्षातः स्वतःप्रामाण्यव्याहतिः अनवस्था वेत्याशंकनीयम् , संवादकज्ञानस्याऽप्रामाण्याशंकाव्यवच्छेदे एव व्यापारात् अपरज्ञानानपेक्षणाच्च ।
[परतः प्रामाण्य साधक अनुमान में व्याप्ति और हेतु की असिद्धि ] परतः प्रामाण्यवादी को यह भी ध्यान में रहे कि पूर्वप्रदशित रीति से प्रामाण्य के निश्चय में पर की अपेक्षा का संभव ही नहीं है । इस कारण, परतः प्रामाण्यवादी की ओर से पूर्व में किये गये 'ये संदेहविपर्ययविषयीकृतात्मतत्त्वा (विपर्ययाध्यासिततनवः) ते परतो निश्चितयथावस्थितस्वरूपाः' इस प्रयोग में व्याप्ति असिद्ध है । एवं हेतु भी असिद्ध है । यह इस प्रकार:-प्रस्तुत प्रयोग में व्याप्नि यह है कि 'जहाँ जहाँ वस्तुस्वरूप संदेह व भ्रम से ग्रस्त होता है वहां वहां यथार्थ स्वरूप के निर्णय में परसापेक्षता होती है। किंतु यह व्याप्ति सिद्ध नहीं हो सकती क्योंकि प्रामाण्य के निश्चय में संवादादिसापेक्षता ही सिद्ध नहीं है । एवं हेतु 'संदेह-भ्रम-ग्रस्तता' प्रामाण्यरूप पक्ष में असिद्ध है। क्योंकि किसी भी प्राणी को प्रामाण्य के विषय में संदेह और भ्रम होता नहीं है । (तथाहि .....)
माण्य में किसी को भी संदेह और भ्रम नहीं होता यह इस प्रकार-जब ज्ञान उत्पन्न होता है तब सभी को यह निश्चय हो जाता है कि 'यह अमक अर्थ है । यदि प्रामाण्य के विषय में संदेह या भ्रम होता तो यह निश्चय नहीं होना चाहिये । कहा भी है- ('प्रामाण्यग्रहणात्'....इत्यादि कारिका का अर्थः-) प्रमाण का प्रामाण्य गृहीत होने के पहले ही स्वरूप से अवस्थित है। वह अपने कार्य करने में किसी अन्य की अपेक्षा नहीं करता। प्रमाण का कार्य है 'स्वार्थ' अर्थात् विषय का निश्चय । इसमें वह किसी अन्य प्रमाण की एवं स्वग्रहण की अपेक्षा नहीं करता, अर्थात् प्रमाण उत्पन्न होते ही स्वविषय का निश्चय हो जाता है। यदि इस प्रमाणज्ञान के विषय में संदेह या भ्रम संभवित होता तो अपने विषय का निश्चय निरपेक्षरूप से नहीं कर पाता।
[प्रमाणज्ञान और अप्रमाणज्ञान का तुल्यरूप नहीं है ] यदि आप कहते हैं-'प्रमाणभूत ज्ञान और अप्रमाणभूतज्ञान का स्वरूप उत्पत्ति में समान है। तात्पर्य, उत्पत्तिकाल में दोनों ज्ञान सामान्यरूप से गृहीत होता है, किन्तु ( विशेष रूप से अर्थात् ) प्रमाण रूप से या अप्रमाणरूप से गृहीत नहीं होता है इसलिए अगर इसका ग्रहण करना हो तो संवाद या विसंवाद को अपेक्षा अवश्य रहेगी । इस के बिना उन दोनों के प्रामाण्य-अप्रामाण्य का निश्चय नहीं * 'गृह्यते प्रत्ययान्तरैः' इति चतुर्थः पादः ।
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org