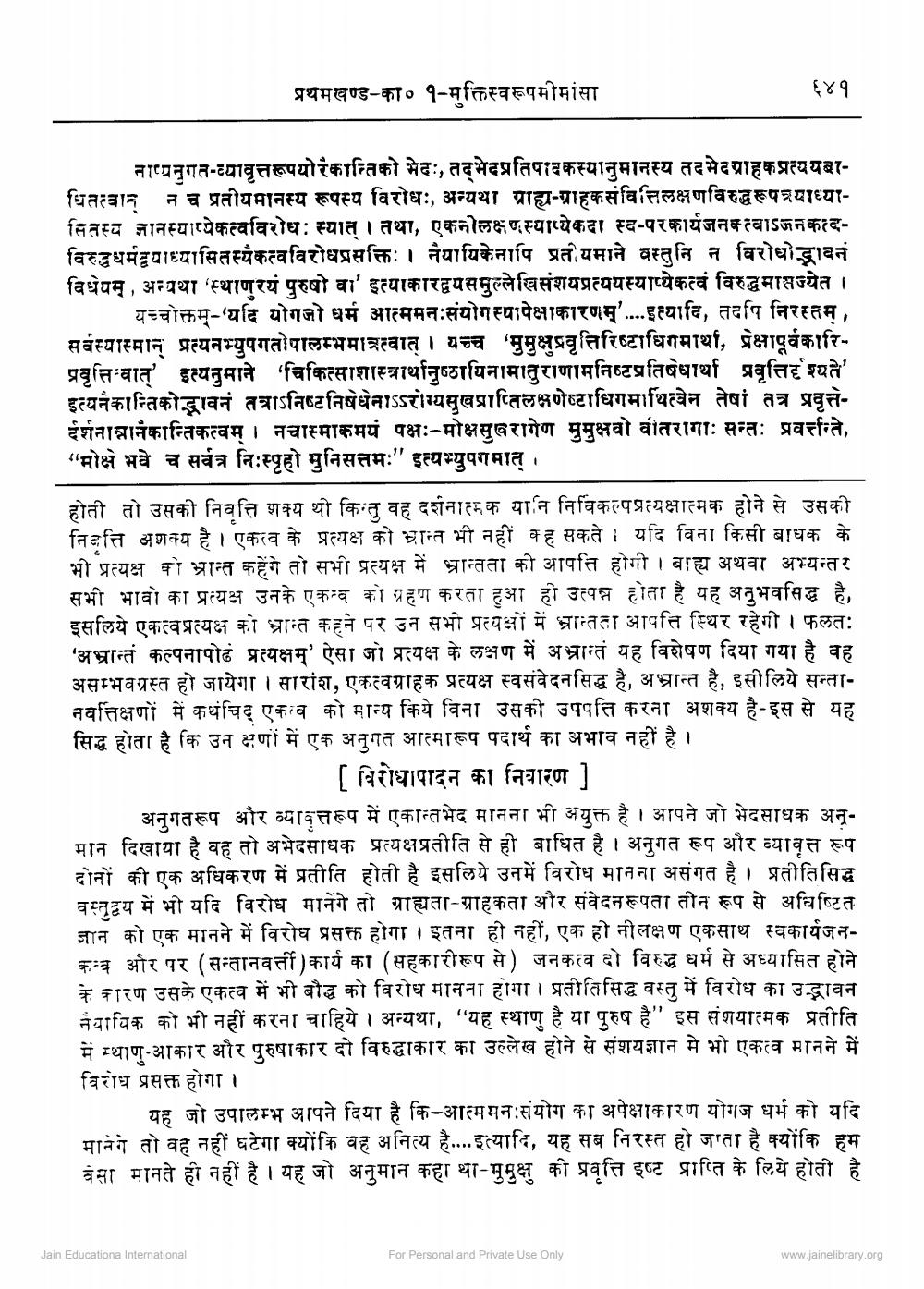________________
प्रथमखण्ड-का० १-मुक्तिस्वरूपमीमांसा
६४१
नाप्यनुगत-व्यावृत्तरूपयोरैकान्तिको भेदः, तभेदप्रतिपादकस्यानुमानस्य तदभेद ग्राहकप्रत्ययबाधितत्वात न च प्रतीयमानस्य रूपस्य विरोधः, अन्यथा ग्राह्य-ग्राहकसंवित्तिलक्षणविरुद्धरूपत्रयाध्यासितस्य ज्ञानस्याप्येकत्वविरोध: स्यात् । तथा, एकनोलक्षणस्याप्येकदा स्व-परकार्यजनकत्वाऽजनकादविरुद्धधर्मद्वयाध्यासितस्यैकत्वविरोधप्रसक्तिः । नैयायिकेनापि प्रतीयमाने वस्तुनि न विरोधोद्धावनं विधेयम् , अन्यथा स्थाणुरयं पुरुषो वा' इत्याकारद्वयसमुल्लेखिसंशयप्रत्ययस्याप्येकत्वं विरुद्धमासज्येत ।
यच्चोक्तम्-'यदि योगजो धर्म आत्ममनःसंयोगस्थापेक्षाकारणम्'....इत्यादि, तदपि निरस्तम, सर्वस्यास्मान् प्रत्यनभ्युपगतोपालम्भमात्रत्वात् । यच्च 'मुमुक्षुप्रवृत्तिरिष्टाधिगमार्था, प्रेक्षापूर्वकारिप्रवृत्ति वात्' इत्यनुमाने चिकित्साशास्त्रार्थानुष्ठायिनामातुराणामनिष्टप्रतिषेधार्था प्रवृत्तिदृश्यते' इत्यनैकान्तिकोद्भावनं तत्राऽनिष्ट निषेधेनाऽऽरोग्यसुखप्राप्तिलक्षणेष्टाधिगमाथित्वेन तेषां तत्र प्रवृत्तेदर्शनान्नानकान्तिकत्वम् । नचास्माकमयं पक्षः-मोक्षसुखरागेण मुमुक्षवो वीतरागाः सन्त: प्रवर्त्तन्ते, "मोक्षे भवे च सर्वत्र निःस्पृहो मुनिसत्तमः" इत्यभ्युपगमात् । होती तो उसकी निवृत्ति शक्य थी किन्तु वह दर्शनात्मक यानि निर्विकल्पप्रत्यक्षात्मक होने से उसकी निदत्ति अशक्य है। एकत्व के प्रत्यक्ष को भ्रान्त भी नहीं कह सकते। यदि विना किसी बाधक के भी प्रत्यक्ष को भ्रान्त कहेंगे तो सभी प्रत्यक्ष में भ्रान्तता को आपत्ति होगी । बाह्य अथवा अभ्यन्तर सभी भावो का प्रत्यक्ष उनके एकत्व को ग्रहण करता हुआ ही उत्पन्न होता है यह अनुभवसिद्ध है, इसलिये एकत्वप्रत्यक्ष को भ्रान्त कहने पर उन सभी प्रत्यक्षों में भ्रान्तता आपत्ति स्थिर रहेगी। फलत: 'अभ्रान्तं कल्पनापोढं प्रत्यक्षम्' ऐसा जो प्रत्यक्ष के लक्षण में अभ्रान्तं यह विशेषण दिया गया है वह असम्भवग्रस्त हो जायेगा। सारांश, एकत्वग्राहक प्रत्यक्ष स्वसंवेदनसिद्ध है, अभ्रान्त है, इसीलिये सन्तानवत्तिक्षणों में कथंचिद् एकत्व को मान्य किये विना उसकी उपपत्ति करना अशक्य है-इस से यह सिद्ध होता है कि उन क्षणों में एक अनुगत. आत्मारूप पदार्थ का अभाव नहीं है।
[विरोधापादन का निवारण ] अनुगतरूप और व्याक्त्तरूप में एकान्तभेद मानना भी अयुक्त है । आपने जो भेदसाधक अनूमान दिखाया है वह तो अभेदसाधक प्रत्यक्षप्रतीति से ही बाधित है । अनुगत रूप और व्यावृत्त रूप दोनों की एक अधिकरण में प्रतीति होती है इसलिये उनमें विरोध मानना असंगत है। प्रतीतिसिद्ध वस्तुहय में भी यदि विरोध मानेंगे तो ग्राह्यता-ग्राहकता और संवेदनरूपता तीन रूप से अधिष्टित ज्ञान को एक मानने में विरोध प्रसक्त होगा। इतना ही नहीं, एक हो नीलक्षण एकसाथ स्वकार्यजनकन्व और पर (सन्तानवर्ती) कार्य का (सहकारीरूप से) जनकत्व दो विरुद्ध धर्म से अध्यासित होने के कारण उसके एकत्व में भी बौद्ध को विरोध मानना होगा। प्रतीति सिद्ध वस्तु में विरोध का उद्भावन नैयायिक को भी नहीं करना चाहिये । अन्यथा, "यह स्थाणु है या पुरुष है'' इस संशयात्मक प्रतीति में स्थाणु-आकार और पुरुषाकार दो विरुद्धाकार का उल्लेख होने से संशयज्ञान मे भो एकत्व मानने में विरोध प्रसक्त होगा।
यह जो उपालम्भ आपने दिया है कि-आत्ममनःसंयोग का अपेक्षाकारण योगज धर्म को यदि मानेगे तो वह नहीं घटेगा क्योंकि वह अनित्य है....इत्यादि, यह सब निरस्त हो जाता है क्योंकि हम वेसा मानते ही नहीं है । यह जो अनुमान कहा था-मुमुक्षु की प्रवृत्ति इष्ट प्राप्ति के लिये होती है
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org