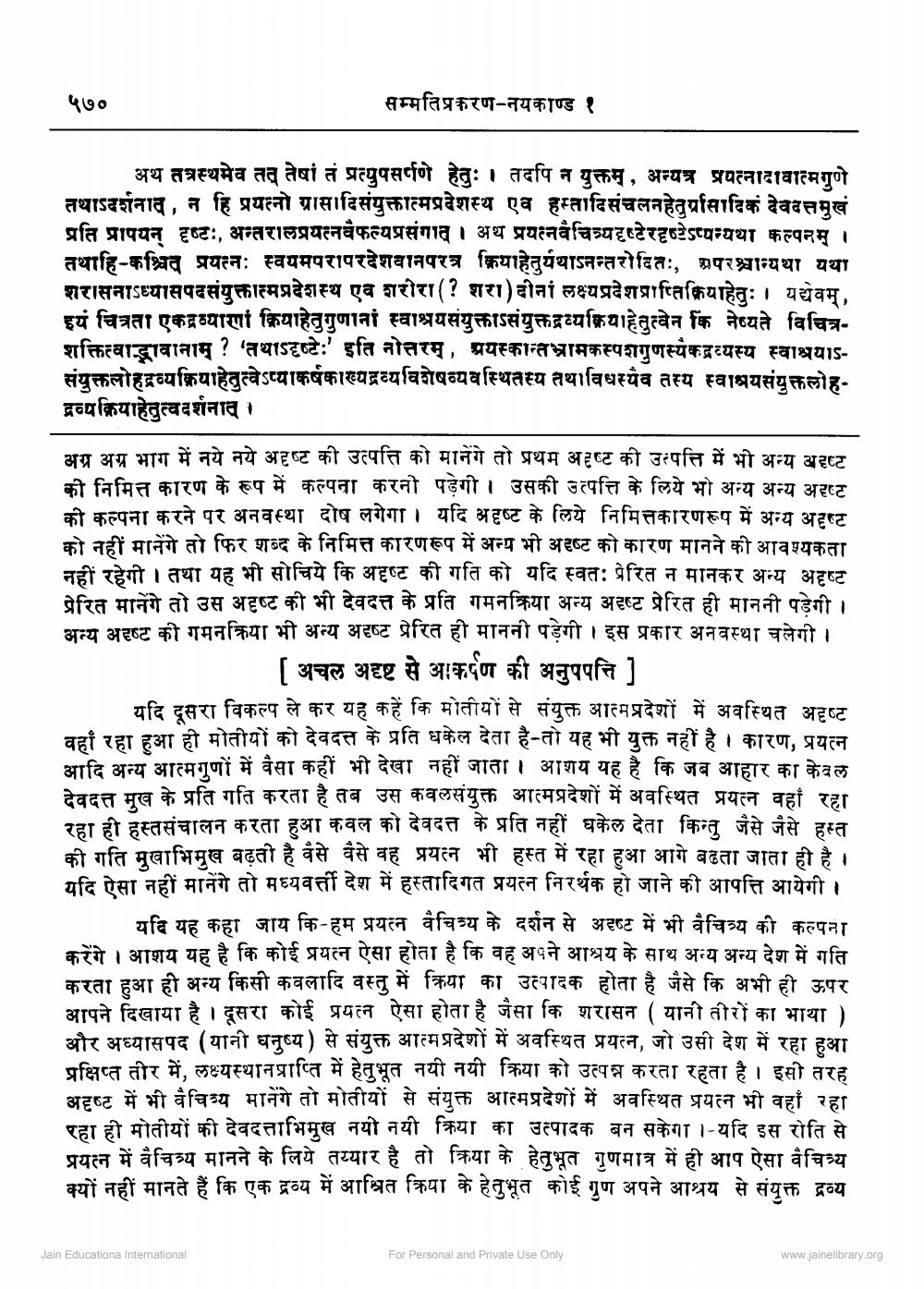________________
५७०
सम्मतिप्रकरण-नयकाण्ड १
अथ तत्रस्थमेव तव तेषां तं प्रत्युपसणे हेतुः । तदपि न युक्तम् , अन्यत्र प्रयत्नादावात्मगुणे तथाऽदर्शनाव , न हि प्रयत्नो ग्रासादिसंयुक्तात्मप्रदेशस्थ एव हस्तादिसंचलनहेतुर्गासादिकं देवदत्तमुखं प्रति प्रापयन् दृष्टः, अन्तरालप्रयत्नवैफल्यप्रसंगात । अथ प्रयत्नवैचित्र्यदृष्टेरदृष्टेऽप्यन्यथा कल्पनम् । तथाहि-कश्चित प्रयत्नः स्वयमपरापरदेशवानपरत्र क्रियाहेतुर्यथाऽनन्तरोदितः, अपरश्चान्यथा यथा शरासनाऽध्यासपदसंयुक्तात्मप्रदेशस्थ एव शरीरा(? शरा) दीनां लक्ष्यप्रदेशप्राप्तिक्रियाहेतुः। यद्येवम् , इयं चित्रता एकद्रव्यारणां क्रियाहेतुगुणानां स्वाश्रयसंयुक्ताऽसंयुक्तद्रव्यक्रियाहेतुत्वेन कि नेष्यते विचित्रशक्तित्वाद्धावानाम् ? 'तथाऽदृष्टेः' इति नोत्तरम् , अयस्कान्तभ्रामकस्पशगुणस्यैकद्रव्यस्य स्वाश्रयाsसंयुक्तलोहद्रव्यक्रियाहेतुत्वेऽप्याकर्षकाख्यद्रव्यविशेषव्यवस्थितस्य तथाविधस्यैव तस्य स्वाश्रयसंयुक्तलोहद्रव्य क्रियाहेतुत्वदर्शनात।
अग्र अग्र भाग में नये नये अदृष्ट की उत्पत्ति को मानेंगे तो प्रथम अदृष्ट की उत्पत्ति में भी अन्य अदृष्ट को निमित्त कारण के रूप में कल्पना करनी पड़ेगी। उसकी उत्पत्ति के लिये भो अन्य अन्य अष्ट की कल्पना करने पर अनवस्था दोष लगेगा। यदि अदृष्ट के लिये निमित्तकारणरूप में अन्य अदृष्ट को नहीं मानेंगे तो फिर शब्द के निमित्त कारणरूप में अन्य भी अदृष्ट को कारण मानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तथा यह भी सोचिये कि अदृष्ट की गति को यदि स्वतः प्रेरित न मानकर अन्य अदृष्ट प्रेरित मानेंगे तो उस अदृष्ट की भी देवदत्त के प्रति गमनक्रिया अन्य अदृष्ट प्रेरित ही माननी पडेगी। अन्य अदृष्ट की गमनक्रिया भी अन्य अदृष्ट प्रेरित ही माननी पड़ेगी। इस प्रकार अनवस्था चलेगी।
[ अचल अदृष्ट से आकर्षण की अनुपपत्ति ] यदि दसरा विकल्प ले कर यह कहें कि मोतीयों से संयुक्त आत्मप्रदेशों में अवस्थित अदृष्ट वहाँ रहा हआ ही मोतीयों को देवदत्त के प्रति धकेल देता है-तो यह भी युक्त नहीं है । कारण, प्रयत्न आदि अन्य आत्मगुणों में वैसा कहीं भी देखा नहीं जाता। आशय यह है कि जब आहार का केवल देवदत्त मुख के प्रति गति करता है तब उस कवलसंयुक्त आत्मप्रदेशों में अवस्थित प्रयत्न वहाँ रक्षा रहा ही हस्तसंचालन करता हुआ कवल को देवदत्त के प्रति नहीं धकेल देता किन्तु जैसे जैसे हस्त की गति मुखाभिमूख बढ़ती है वैसे वैसे वह प्रयत्न भी हस्त में रहा हुआ आगे बढता जाता ही है । यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो मध्यवर्ती देश में हस्तादिगत प्रयत्न निरर्थक हो जाने की आपत्ति आयेगी।
यदि यह कहा जाय कि-हम प्रयत्न वैचित्र्य के दर्शन से अदृष्ट में भी वैचित्र्य की कल्पना करेंगे । आशय यह है कि कोई प्रयत्न ऐसा होता है कि वह अपने आश्रय के साथ अन्य अन्य देश में गति करता हआ ही अन्य किसी कवलादि वस्तु में क्रिया का उत्पादक होता है जैसे कि अभी ही ऊपर आपने दिखाया है । दूसरा कोई प्रयत्न ऐसा होता है जैसा कि शरासन ( यानी तीरों का भाथा ) और अध्यासपद (यानी धनुष्य) से संयुक्त आत्मप्रदेशों में अवस्थित प्रयत्न, जो उसी देश में रहा हआ प्रक्षिप्त तीर में, लक्ष्यस्थानप्राप्ति में हेतुभूत नयी नयी क्रिया को उत्पन्न करता रहता है। इसी तरह अदृष्ट में भी वैचित्र्य मानेंगे तो मोतीयों से संयुक्त आत्मप्रदेशों में अवस्थित प्रयत्न भी वहाँ रहा रहा ही मोतीयों की देवदत्ताभिमुख नयी नयी क्रिया का उत्पादक बन सकेगा। यदि इस रोति से प्रयत्न में वैचित्र्य मानने के लिये तय्यार है तो क्रिया के हेतुभूत गुणमात्र में ही आप ऐसा वैचित्र्य क्यों नहीं मानते हैं कि एक द्रव्य में आश्रित क्रिया के हेतुभूत कोई गुण अपने आश्रय से संयुक्त द्रव्य
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org