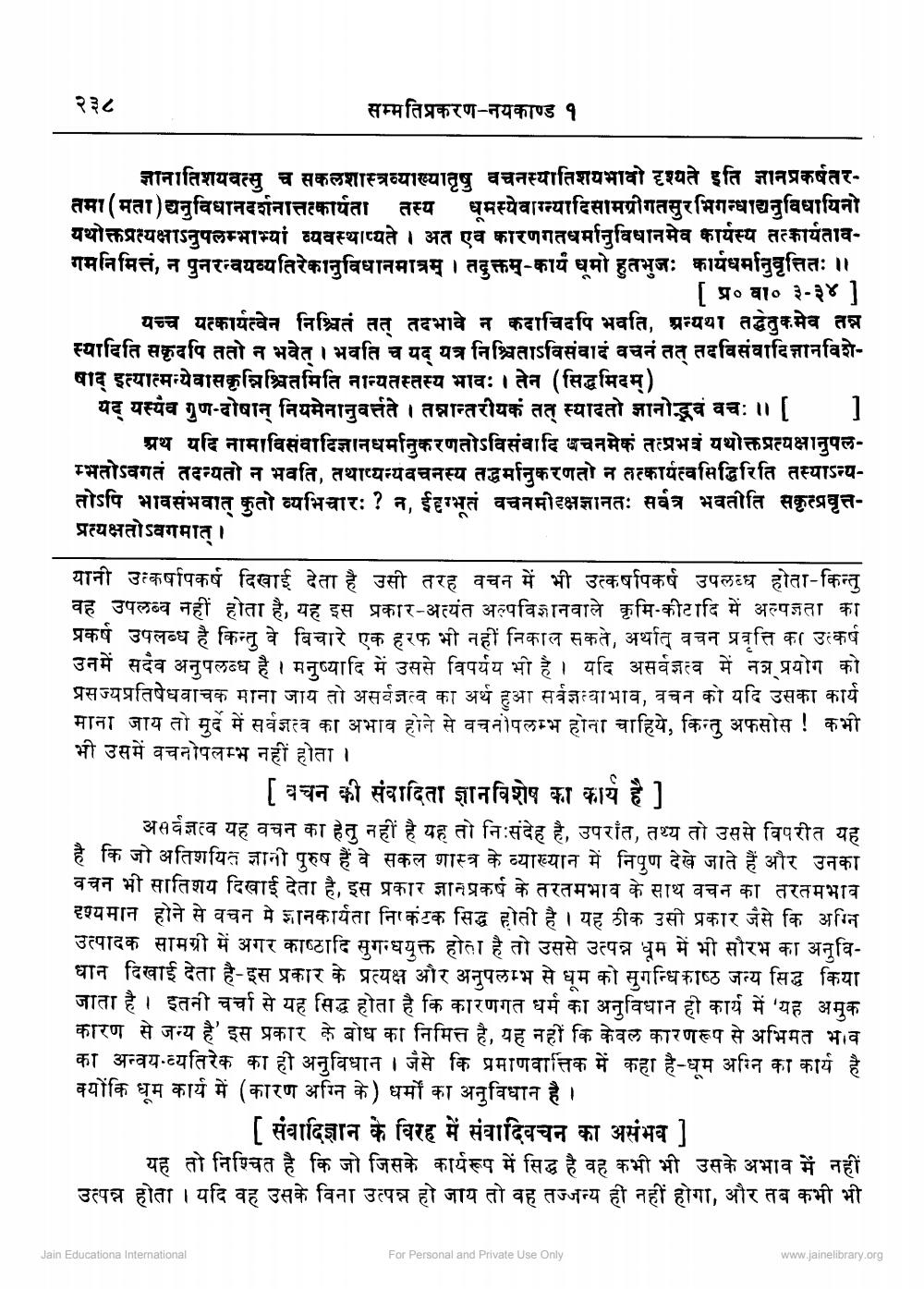________________
२३८
सम्मतिप्रकरण-नयकाण्ड १
ज्ञानातिशयवत्सु च सकलशास्त्रव्याख्यातृषु वचनस्यातिशयभावो दृश्यते इति ज्ञानप्रकर्षतरतमा (मता)धनुविधानदर्शनात्तत्कार्यता तस्य धमस्येवाग्न्यादिसामग्रीगतसुरभिगन्धाधनुविधायिनो यथोक्तप्रत्यक्षाऽनुपलम्भाभ्यां व्यवस्थाप्यते । अत एव कारणगतधर्मानुविधानमेव कार्यस्य तत्कार्यतावगमनिमित्तं, न पुनरन्वयव्यतिरेकानुविधानमात्रम् । तदुक्तम्-कायं धूमो हुतभुजः कार्यधर्मानुवृत्तितः ॥
[प्र० वा० ३-३४ ] यच्च यत्कार्यत्वेन निश्चितं तत् तदभावे न कदाचिदपि भवति, अन्यथा तहेतुकमेव तन्न स्यादिति सकृदपि ततो न भवेत् । भवति च यद् यत्र निश्चिताऽविसंवादं वचनं तत् तदविसंवादिज्ञानविशेषाद् इत्यात्मन्येवासकृनिश्चितमिति नान्यतस्तस्य भावः । तेन (सिद्धमिदम्) यद् यस्यैव गुण-दोषान् नियमेनानुवर्तते । तन्नान्तरीयकं तत् स्यादतो ज्ञानोद्भवं वचः ॥ [ ]
अथ यदि नामाविसंवादिज्ञानधर्मानुकरणतोऽविसंवादि वचनमेकं तत्प्रभवं यथोक्तप्रत्यक्षानुपलम्भतोऽवगतं तदन्यतो न भवति, तथाप्यन्यवचनस्य तद्धर्मानुकरणतो न लत्कार्यत्वसिद्धिरिति तस्याऽन्यतोऽपि भावसंभवात् कुतो व्यभिचारः ? न, ईदृग्भूतं वचनमोक्षज्ञानतः सर्वत्र भवतीति सकृत्प्रवृत्तप्रत्यक्षतोऽवगमात्।
यानी उत्कर्षापकर्ष दिखाई देता है उसी तरह वचन में भी उत्कर्षापकर्ष उपलब्ध होता-किन्तु वह उपलब्व नहीं होता है, यह इस प्रकार-अत्यंत अल्पविज्ञानवाले कृमि-कीटादि में अल्पजता का प्रकर्ष उपलब्ध है किन्तु वे बिचारे एक हरफ भी नहीं निकाल सकते, अर्थात् वचन प्रवृत्ति का उत्कर्ष उनमें सदैव अनुपलब्ध है। मनुष्यादि में उससे विपर्यय भी है। यदि असर्वज्ञत्व में नत्र प्रयोग को प्रसज्यप्रतिषेधवाचक माना जाय तो असर्वजत्व का अर्थ हुआ सर्वज्ञवाभाव, वचन को यदि उसका कार्य माना जाय तो मुर्दे में सर्वज्ञत्व का अभाव होने से वचनोपलम्भ होना चाहिये, किन्तु अफसोस ! कभी भी उसमें वचनोपलम्भ नहीं होता।
[वचन की संवादिता ज्ञान विशेष का कार्य है ] __ असर्वज्ञत्व यह वचन का हेतु नहीं है यह तो निःसंदेह है, उपरांत, तथ्य तो उससे विपरीत यह है कि जो अतिशयित ज्ञानी पुरुष हैं वे सकल शास्त्र के व्याख्यान में निपुण देखे जाते हैं और उनका वचन भी सातिशय दिखाई देता है, इस प्रकार ज्ञानप्रकर्ष के तरतमभाव के साथ वचन का तरतमभाव दृश्यमान होने से वचन मे ज्ञान कार्यता नि कंटक सिद्ध होती है । यह ठीक उसी प्रकार जैसे कि अग्नि उत्पादक सामग्री में अगर काष्ठादि सुगन्धयुक्त होता है तो उससे उत्पन्न धूम में भी सौरभ का अनुविधान दिखाई देता है-इस प्रकार के प्रत्यक्ष और अनुपलम्भ से धूम को सुगन्धिकाष्ठ जन्य सिद्ध किया जाता है। इतनी चर्चा से यह सिद्ध होता है कि कारणगत धर्म का अनविधान ही कार्य
ही कार्य में 'यह अमुक कारण से जन्य है' इस प्रकार के बोध का निमित्त है. यह नहीं कि केवल कारणरूप से अभिमत में का अन्वय व्यतिरेक का ही अनुविधान । जैसे कि प्रमाणवात्तिक में कहा है-धूम अग्नि का कार्य है क्योंकि धूम कार्य में (कारण अग्नि के) धर्मों का अनुविधान है।
[संवादिज्ञान के विरह में संवादिवचन का असंभव ] यह तो निश्चित है कि जो जिसके कार्यरूप में सिद्ध है वह कभी भी उसके अभाव में नहीं उत्पन्न होता । यदि वह उसके विना उत्पन्न हो जाय तो वह तज्जन्य ही नहीं होगा, और तब कभी भी
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org