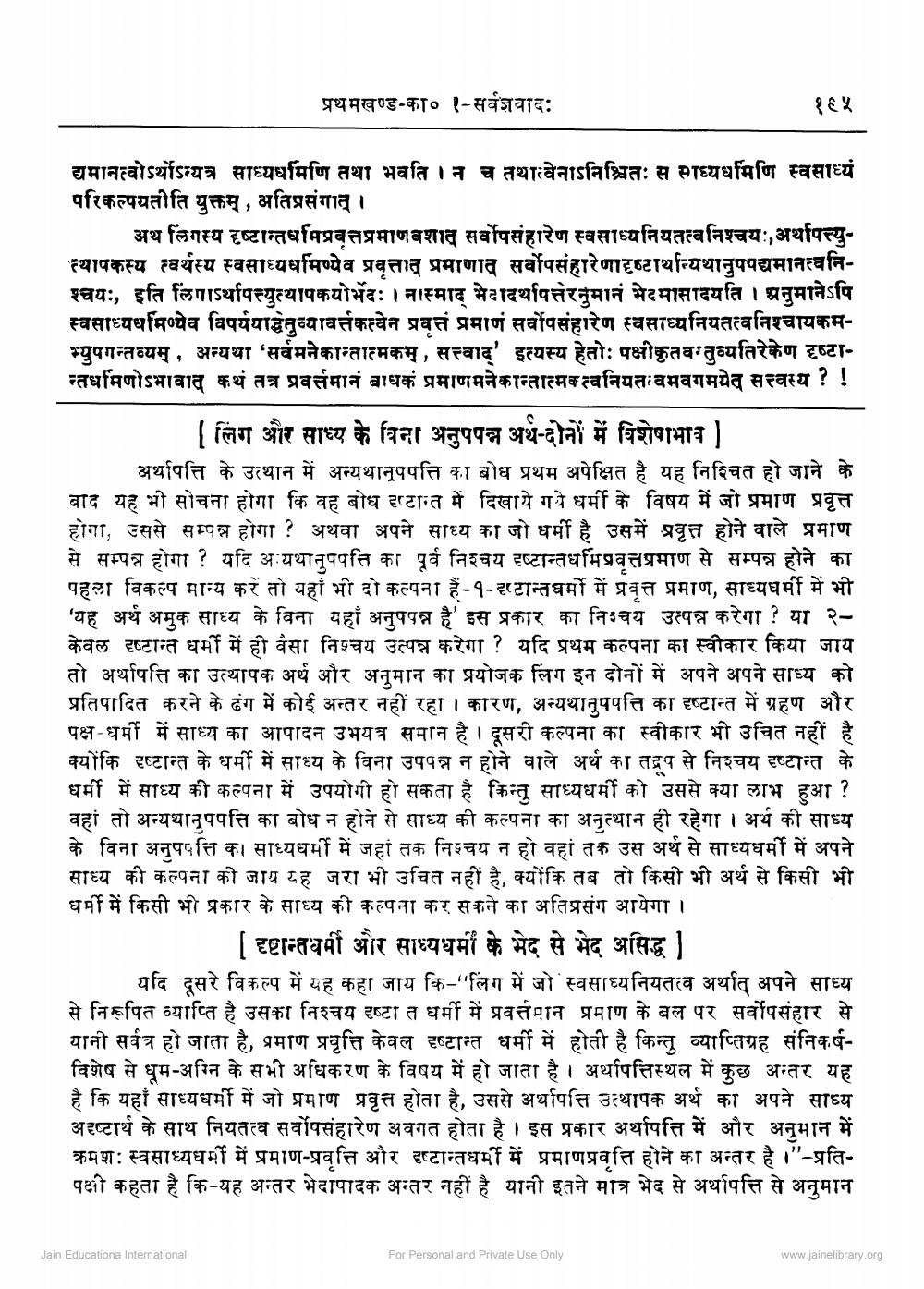________________
प्रथमखण्ड-का० १-सर्वज्ञवादः
द्यमानत्वोऽर्थोऽन्यत्र साध्यमिणि तथा भवति । न च तथात्वेनाऽनिश्चितः स साध्यमिणि स्वसाध्यं परिकल्पयतीति युक्तम् , अतिप्रसंगात् ।
अथ लिंगस्य दृष्टान्तर्धामप्रवृत्तप्रमाणवशात सर्वोपसंहारेण स्वसाध्यनियतत्वनिश्चयः,अर्थापत्त्युत्यापकस्य त्वर्थस्य स्वसाध्यमिण्येव प्रवृत्तात प्रमाणात सर्वोपसंहारेणादृष्टार्थान्यथानुपपद्यमानत्वनिश्चयः, इति लिंगाऽर्थापत्त्युत्थापकयोर्भेदः । नास्माद् भेदादापत्तेरनुमानं भेदमासादयति । अनुमानेऽपि स्वसाध्यमिण्येव विपर्ययाद्धतुव्यावर्तकत्वेन प्रवृत्तं प्रमाणं सर्वोपसंहारेण स्वसाध्यनियतत्वनिश्चायकमभ्युपगन्तव्यम् , अन्यथा 'सर्वमनेकान्तात्मकम् , सत्त्वाद' इत्यस्य हेतोः पक्षीकृतवन्तव्यतिरेकेण दृष्टान्तर्धामणोऽभावात कथं तत्र प्रवर्तमानं बाधकं प्रमाणमनेकान्तात्मक त्वनियतावमवगमयेत सत्त्वस्य ? !
[लिंग और साध्य के विना अनुपपन्न अर्थ-दोनों में विशेषाभाव ] अर्थापत्ति के उत्थान में अन्यथानुपपत्ति का बोध प्रथम अपेक्षित है यह निश्चित हो जाने के बाद यह भी सोचना होगा कि वह बोध हटान्त में दिखाये गये धर्मी के विषय में जो प्रमाण प्रवृत्त होगा, उससे सम्पन्न होगा ? अथवा अपने साध्य का जो धर्मी है उसमें प्रवृत्त होने वाले प्रमाण से सम्पन्न होगा? यदि अयथानुपपत्ति का पूर्व निश्चय दृष्टान्तर्मिप्रवृत्तप्रमाण से सम्पन्न होने का पहला विकल्प मान्य करें तो यहाँ भी दो कल्पना हैं-१-दृष्टान्तधर्मों में प्रवृत्त प्रमाण, साध्यधर्मी में भी 'यह अर्थ अमुक साध्य के विना यहाँ अनुपपन्न है' इस प्रकार का निश्चय उत्पन्न करेगा? या २केवल दृष्टान्त धर्मी में ही वैसा निश्चय उत्पन्न करेगा ? यदि प्रथम कल्पना का स्वीकार किया जाय तो अर्थापत्ति का उत्थापक अर्थ और अनुमान का प्रयोजक लिंग इन दोनों में अपने अपने साध्य को प्रतिपादित करने के ढंग में कोई अन्तर नहीं रहा । कारण, अन्यथानुपपत्ति का दृष्टान्त में ग्रहण और पक्ष-धर्मी में साध्य का आपादन उभयत्र समान है। दूसरी कल्पना का स्वीकार भी उचित नहीं है क्योंकि दृष्टान्त के धर्मी में साध्य के विना उपपन्न न होने वाले अर्थ का तद्रूप से निश्चय दृष्टान्त के धर्मी में साध्य की कल्पना में उपयोगी हो सकता है किन्तु साध्यधर्मी को उससे क्या लाभ हुआ? वहां तो अन्यथानुपपत्ति का बोध न होने से साध्य की कल्पना का अनुत्थान ही रहेगा। अर्थ की साध्य के विना अनुपपत्ति का साध्यधर्मी में जहां तक निश्चय न हो वहां तक उस अर्थ से साध्यधर्मी में अपने साध्य की कल्पना को जाय यह जरा भी उचित नहीं है, क्योंकि तब तो किसी भी अर्थ से किसी भी धर्मी में किसी भी प्रकार के साध्य की कल्पना कर सकने का अतिप्रसंग आयेगा।
[ दृष्टान्तवर्मी और साध्यधर्मी के भेद से भेद असिद्ध] यदि दूसरे विकल्प में यह कहा जाय कि-"लिंग में जो स्वसाध्यनियतत्व अर्थात् अपने साध्य से निरूपित व्याप्ति है उसका निश्चय दृष्टा त धर्मी में प्रवर्तमान प्रमाण के बल पर सर्वोपसंहार से यानी सर्वत्र हो जाता है, प्रमाण प्रवृत्ति केवल दृष्टान्त धर्मी में होती है किन्तु व्याप्तिग्रह संनिकर्षविशेष से धूम-अग्नि के सभी अधिकरण के विषय में हो जाता है। अर्थापत्तिस्थल में कुछ अन्तर यह है कि यहाँ साध्यधर्मी में जो प्रमाण प्रवृत्त होता है, उससे अर्थापत्ति उत्थापक अर्थ का अपने साध्य अष्टार्थ के साथ नियतत्व सर्वोपसंहारेण अवगत होता है । इस प्रकार अर्थापत्ति में और अनुमान में क्रमशः स्वसाध्यधर्मी में प्रमाण-प्रवृत्ति और दृष्टान्तधर्मी में प्रमाणप्रवृत्ति होने का अन्तर है।"-प्रतिपक्षी कहता है कि-यह अन्तर भेदापादक अन्तर नहीं है यानी इतने मात्र भेद से अर्थापत्ति से अनुमान
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org