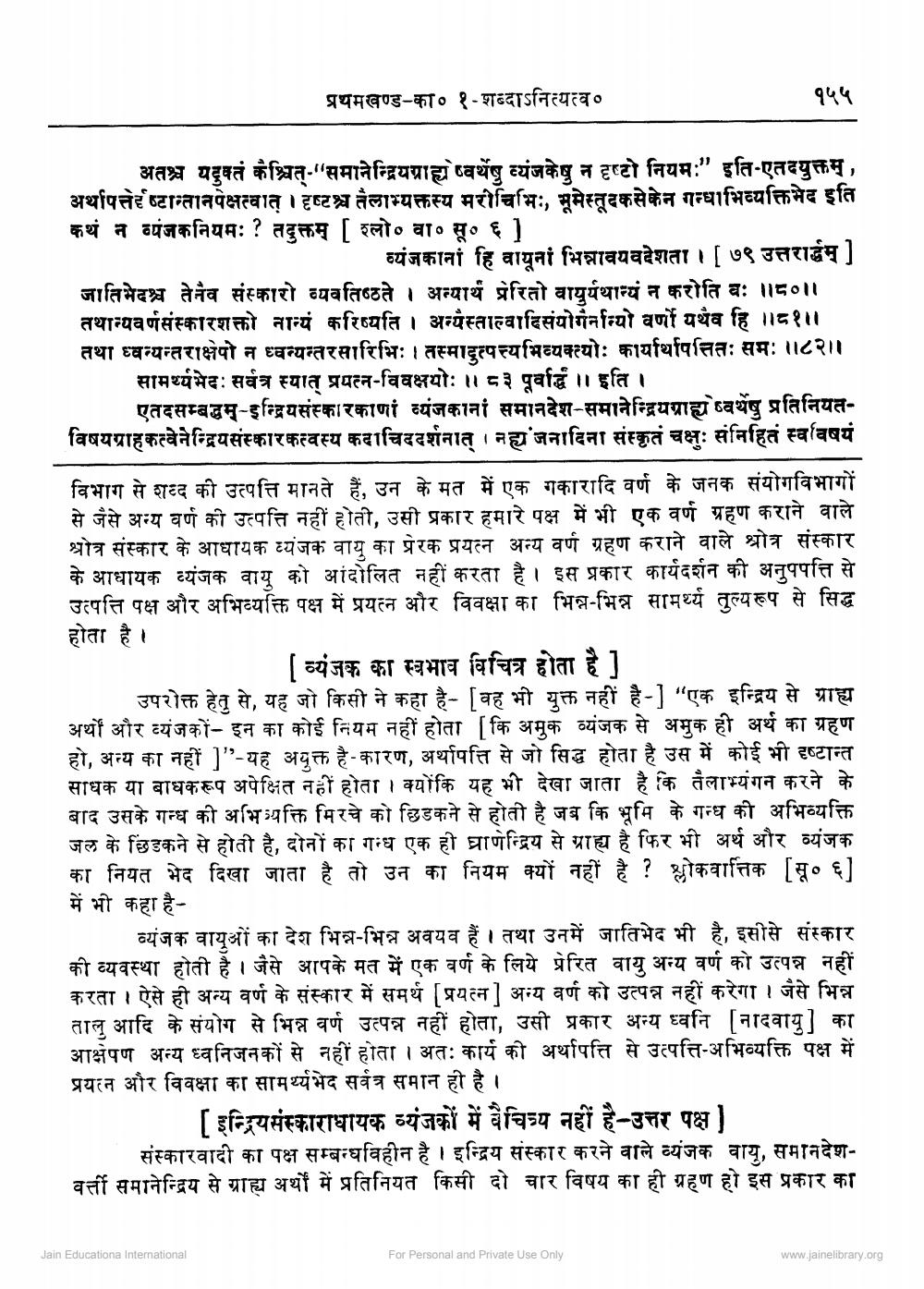________________
प्रथमखण्ड-का० १-शब्दाऽनित्यत्व०
१५५
अतश्च यदुक्तं कैश्चित्-"समानेन्द्रियग्राह्य ष्वर्थेषु व्यंजकेषु न दृष्टो नियमः" इति-एतदयुक्तम् , अर्थापत्तष्टान्तानपेक्षत्वात दृष्टश्च लाभ्यक्तस्य मरीचिभिः. ममेस्तरकसेकेन गन्धाभिव्यक्तिभेद कथं न व्यंजकनियमः ? तदुक्तम् [ श्लो० वा० सू० ६ ]
व्यंजकानां हि वायूनां भिन्नावयवदेशता । [ ७९ उत्तरार्द्धम् ] जातिभेदश्च तेनैव संस्कारो व्यवतिष्ठते । अन्यार्थ प्रेरितो वायुर्यथान्यं न करोति वः ॥५०॥ तथान्यवर्णसंस्कारशक्तो नान्यं करिष्यति । अन्यस्ताल्वादिसंयोग न्यो वर्णो यथैव हि ॥१॥ तथा ध्वन्यन्तराक्षेपो न ध्वन्यन्तरसारिभिः । तस्मादुत्पत्त्यभिव्यक्त्योः कार्यार्थापत्तितः समः ॥८२॥
सामर्थ्य भेदः सर्वत्र स्यात् प्रयत्न-विवक्षयोः ।।८३ पूर्वार्द्ध ॥ इति ।।
एतदसम्बद्धम्-इन्द्रियसंस्कारकाणां व्यंजकानां समानदेश-समानेन्द्रियग्राह्य ष्वर्थेषु प्रतिनियतविषयग्राहकत्वेनेन्द्रियसंस्कारकत्वस्य कदाचिददर्शनात् । नाजनादिना संस्कृतं चक्षुः संनिहितं स्वविषयं विभाग से शब्द की उत्पत्ति मानते हैं, उन के मत में एक गकारादि वर्ण के जनक संयोगविभागों से जैसे अन्य वर्ण की उत्पत्ति नहीं होती, उसी प्रकार हमारे पक्ष में भी एक वर्ण ग्रहण कराने वाले श्रोत्र संस्कार के आधायक व्यंजक वायु का प्रेरक प्रयत्न अन्य वर्ण ग्रहण कराने वाले श्रोत्र संस्कार के आधायक व्यंजक वायु को आंदोलित नहीं करता है। इस प्रकार कार्यदर्शन की अनुपपत्ति से उत्पत्ति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष में प्रयत्न और विवक्षा का भिन्न-भिन्न सामर्थ्य तुल्यरूप से सिद्ध होता है।
[ व्यंजक का स्वभाव विचित्र होता है ] उपरोक्त हेतु से, यह जो किसी ने कहा है- [वह भी युक्त नहीं है-] “एक इन्द्रिय से ग्राह्य अर्थों और व्यंजकों- इन का कोई नियम नहीं होता [कि अमुक व्यंजक से अमुक ही अर्थ का ग्रहण हो, अन्य का नहीं ]''- यह अयुक्त है- कारण, अर्थापत्ति से जो सिद्ध होता है उस में कोई भी दृष्टान्त साधक या बाधकरूप अपेक्षित नहीं होता। क्योंकि यह भी देखा जाता है कि तैलाभ्यंगन करने के बाद उसके गन्ध की अभिव्यक्ति मिरचे को छिडकने से होती है जब कि भूमि के गन्ध की अभिव्यक्ति जल के छिडकने से होती है, दोनों का गन्ध एक ही घ्राणेन्द्रिय से ग्राह्य है फिर भी अर्थ और व्यंजक का नियत भेद दिखा जाता है तो उन का नियम क्यों नहीं है ? श्लोकवात्तिक [सू० ६] में भी कहा है
व्यंजक वायुओं का देश भिन्न-भिन्न अवयव हैं। तथा उनमें जातिभेद भी है, इसीसे संस्कार की व्यवस्था होती है । जैसे आपके मत में एक वर्ण के लिये प्रेरित वायु अन्य वर्ण को उत्पन्न नहीं करता । ऐसे ही अन्य वर्ण के संस्कार में समर्थ [प्रयत्न] अन्य वर्ण को उत्पन्न नहीं करेगा । जैसे भिन्न तालु आदि के संयोग से भिन्न वर्ण उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार अन्य ध्वनि [नादवायु] का आक्षेपण अन्य ध्वनिजनकों से नहीं होता । अतः कार्य को अर्थापत्ति से उत्पत्ति-अभिव्यक्ति पक्ष में प्रयत्न और विवक्षा का सामर्थ्य भेद सर्वत्र समान ही है ।
[इन्द्रियसंस्काराधायक व्यंजकों में वैचित्र्य नहीं है-उत्तर पक्ष) संस्कारवादी का पक्ष सम्बन्धविहीन है । इन्द्रिय संस्कार करने वाले व्यंजक वायु, समानदेशवर्ती समानेन्द्रिय से ग्राह्य अर्थों में प्रतिनियत किसी दो चार विषय का ही ग्रहण हो इस प्रकार का
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org