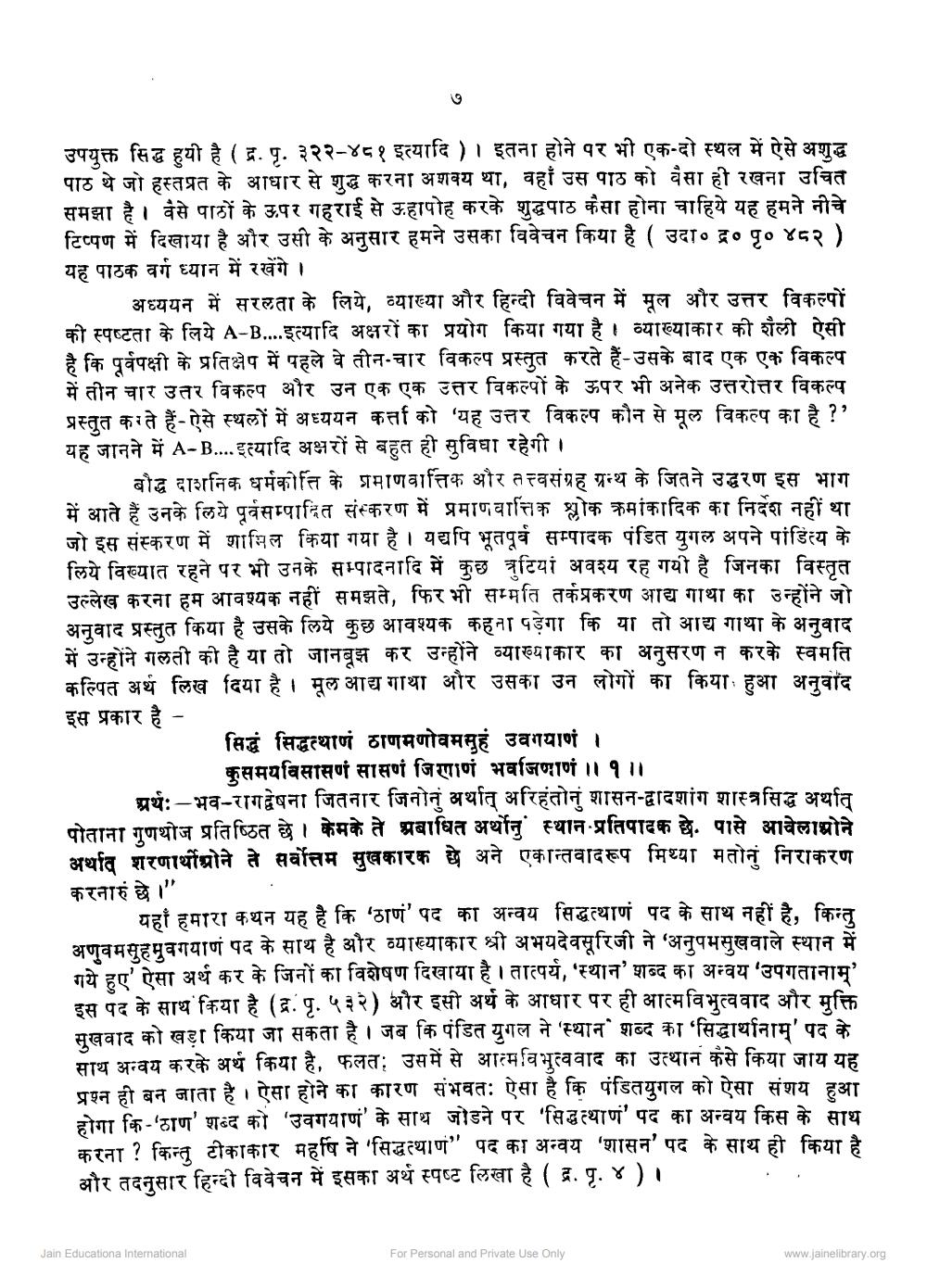________________
67
उपयुक्त सिद्ध हुयी है (द्र. पृ. ३२२- ४८१ इत्यादि ) । इतना होने पर भी एक-दो स्थल में ऐसे अशुद्ध पाठ थे जो हस्तप्रत के आधार से शुद्ध करना अशक्य था, वहाँ उस पाठ को वैसा ही रखना उचित समझा है। वैसे पाठों के ऊपर गहराई से ऊहापोह करके शुद्धपाठ कैसा होना चाहिये यह हमने नीचे टिप्पण में दिखाया है और उसी के अनुसार हमने उसका विवेचन किया है ( उदा० द्र० पृ० ४८२ ) यह पाठक वर्ग ध्यान में रखेंगे ।
अध्ययन में सरलता के लिये, व्याख्या और हिन्दी विवेचन में मूल और उत्तर विकल्पों की स्पष्टता के लिये A - B .... इत्यादि अक्षरों का प्रयोग किया गया है । व्याख्याकार की शैली ऐसी है कि पूर्वपक्षी के प्रतिक्षेप में पहले वे तीन-चार विकल्प प्रस्तुत करते हैं- उसके बाद एक एक विकल्प में तीन चार उत्तर विकल्प और उन एक एक उत्तर विकल्पों के ऊपर भी अनेक उत्तरोत्तर विकल्प प्रस्तुत करते हैं - ऐसे स्थलों में अध्ययन कर्ता को 'यह उत्तर विकल्प कौन से मूल विकल्प का है ?" यह जानने में A-B.... इत्यादि अक्षरों से बहुत ही सुविधा रहेगी ।
बौद्ध दार्शनिक धर्मकोत्ति के प्रमाणवात्र्तिक और तत्त्वसंग्रह ग्रन्थ के जितने उद्धरण इस भाग में आते हैं उनके लिये पूर्वसम्पादित संस्करण में प्रमाणवार्तिक श्लोक क्रमांकादिक का निर्देश नहीं था जो इस संस्करण में शामिल किया गया है । यद्यपि भूतपूर्व सम्पादक पंडित युगल अपने पांडित्य के लिये विख्यात रहने पर भी उनके सम्पादनादि में कुछ त्रुटियां अवश्य रह गयी है जिनका विस्तृत उल्लेख करना हम आवश्यक नहीं समझते, फिर भी सम्मति तर्कप्रकरण आद्य गाथा का उन्होंने जो अनुवाद प्रस्तुत किया है उसके लिये कुछ आवश्यक कहना पड़ेगा कि या तो आद्य गाथा के अनुवाद में उन्होंने गलती की है या तो जानबूझ कर उन्होंने व्याख्याकार का अनुसरण न करके स्वमति कल्पित अर्थ लिख दिया है। मूल आद्य गाथा और उसका उन लोगों का किया हुआ अनुवाद इस प्रकार है
सिद्धं सिद्धत्थाणं ठाणमणोवमसुहं उवगयाणं । कुसमयविसासणं सासणं जिरगाणं भर्वाजिणाणं ।। १ ।।
प्रर्थः - भव- रागद्वेषना जितनार जिनोनुं अर्थात् अरिहंतोनुं शासन द्वादशांग शास्त्रसिद्ध अर्थात् पोताना गुणथोज प्रतिष्ठित छे । केमके ते अबाधित अर्थोनुं स्थान प्रतिपादक छे. पासे आवेलानोने अर्थात् शरणार्थीनीने ते सर्वोत्तम सुखकारक छे अने एकान्तवादरूप मिथ्या मतोनुं निराकरण करनारुं छे ।"
यहाँ हमारा कथन यह है कि 'ठाणं' पद का अन्वय सिद्धत्थाणं पद के साथ नहीं है, किन्तु अणुवमसुहमुवगयाणं पद के साथ है और व्याख्याकार श्री अभयदेवसूरिजी ने 'अनुपमसुखवाले स्थान में गये हुए' ऐसा अर्थ कर के जिनों का विशेषण दिखाया है। तात्पर्य, 'स्थान' शब्द का अन्वय 'उपगतानाम् ' इस पद के साथ किया है (द्र पृ. ५३२) और इसी अर्थ के आधार पर ही आत्मविभुत्ववाद और मुक्ति सुखवाद को खड़ा किया जा सकता है। जब कि पंडित युगल ने 'स्थान' शब्द का 'सिद्धार्थानाम् ' पद के साथ अन्वय करके अर्थ किया है, फलतः उसमें से आत्मविभुत्ववाद का उत्थानं कैसे किया जाय यह प्रश्न ही बन जाता है । ऐसा होने का कारण संभवत: ऐसा है कि पंडितयुगल को ऐसा संशय हुआ होगा कि - 'ठाण' शब्द को 'उवगयाणं' के साथ जोडने पर 'सिद्धत्थाणं' पद का अन्वय किस के साथ करना ? किन्तु टीकाकार महर्षि ने 'सिद्धत्थाणं" पद का अन्वय 'शासन' पद के साथ ही किया है और तदनुसार हिन्दी विवेचन में इसका अर्थ स्पष्ट लिखा है ( द्र. पू. ४ ) ।
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org