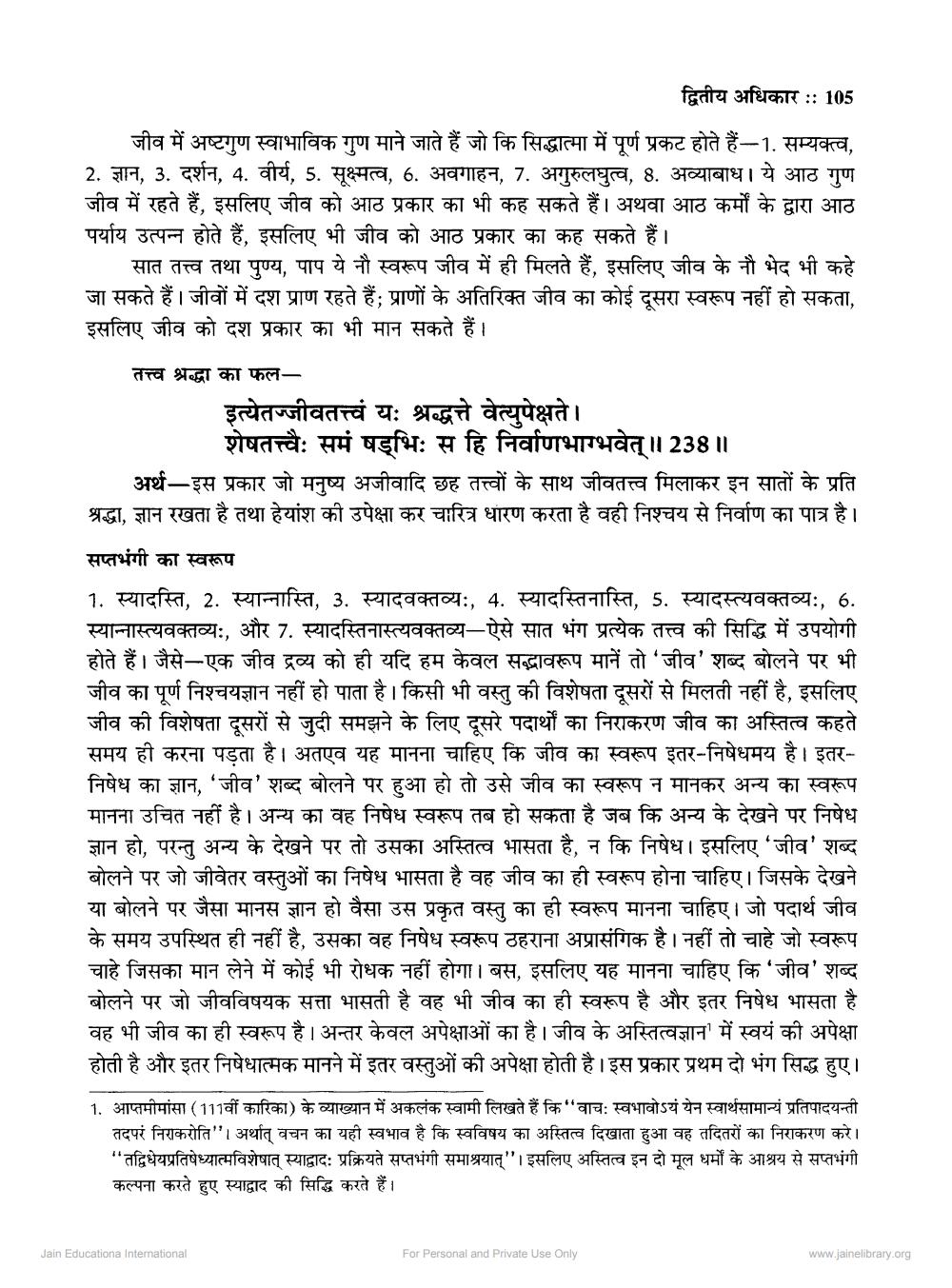________________
द्वितीय अधिकार :: 105 जीव में अष्टगुण स्वाभाविक गुण माने जाते हैं जो कि सिद्धात्मा में पूर्ण प्रकट होते हैं-1. सम्यक्त्व, 2. ज्ञान, 3. दर्शन, 4. वीर्य, 5. सूक्ष्मत्व, 6. अवगाहन, 7. अगुरुलघुत्व, 8. अव्याबाध। ये आठ गुण जीव में रहते हैं, इसलिए जीव को आठ प्रकार का भी कह सकते हैं। अथवा आठ कर्मों के द्वारा आठ पर्याय उत्पन्न होते हैं, इसलिए भी जीव को आठ प्रकार का कह सकते हैं।
सात तत्त्व तथा पुण्य, पाप ये नौ स्वरूप जीव में ही मिलते हैं, इसलिए जीव के नौ भेद भी कहे जा सकते हैं। जीवों में दश प्राण रहते हैं; प्राणों के अतिरिक्त जीव का कोई दूसरा स्वरूप नहीं हो सकता, इसलिए जीव को दश प्रकार का भी मान सकते हैं।
तत्त्व श्रद्धा का फल
इत्येतज्जीवतत्त्वं यः श्रद्धत्ते वेत्युपेक्षते।
शेषतत्त्वैः समं षड्भिः स हि निर्वाणभाग्भवेत्॥ 238॥ अर्थ-इस प्रकार जो मनुष्य अजीवादि छह तत्त्वों के साथ जीवतत्त्व मिलाकर इन सातों के प्रति श्रद्धा, ज्ञान रखता है तथा हेयांश की उपेक्षा कर चारित्र धारण करता है वही निश्चय से निर्वाण का पात्र है।
सप्तभंगी का स्वरूप
1. स्यादस्ति, 2. स्यान्नास्ति, 3. स्यादवक्तव्यः, 4. स्यादस्तिनास्ति, 5. स्यादस्त्यवक्तव्यः, 6. स्यान्नास्त्यवक्तव्यः, और 7. स्यादस्तिनास्त्यवक्तव्य-ऐसे सात भंग प्रत्येक तत्त्व की सिद्धि में उपयोगी होते हैं। जैसे-एक जीव द्रव्य को ही यदि हम केवल सद्भावरूप मानें तो 'जीव' शब्द बोलने पर भी जीव का पूर्ण निश्चयज्ञान नहीं हो पाता है। किसी भी वस्तु की विशेषता दूसरों से मिलती नहीं है, इसलिए जीव की विशेषता दूसरों से जुदी समझने के लिए दूसरे पदार्थों का निराकरण जीव का अस्तित्व कहते समय ही करना पड़ता है। अतएव यह मानना चाहिए कि जीव का स्वरूप इतर-निषेधमय है। इतरनिषेध का ज्ञान, 'जीव' शब्द बोलने पर हुआ हो तो उसे जीव का स्वरूप न मानकर अन्य का स्वरूप मानना उचित नहीं है। अन्य का वह निषेध स्वरूप तब हो सकता है जब कि अन्य के देखने पर निषेध ज्ञान हो, परन्तु अन्य के देखने पर तो उसका अस्तित्व भासता है, न कि निषेध। इसलिए 'जीव' शब्द बोलने पर जो जीवेतर वस्तुओं का निषेध भासता है वह जीव का ही स्वरूप होना चाहिए। जिसके देखने या बोलने पर जैसा मानस ज्ञान हो वैसा उस प्रकृत वस्तु का ही स्वरूप मानना चाहिए। जो पदार्थ जीव के समय उपस्थित ही नहीं है, उसका वह निषेध स्वरूप ठहराना अप्रासंगिक है। नहीं तो चाहे जो स्वरूप चाहे जिसका मान लेने में कोई भी रोधक नहीं होगा। बस, इसलिए यह मानना चाहिए कि 'जीव' शब्द बोलने पर जो जीवविषयक सत्ता भासती है वह भी जीव का ही स्वरूप है और इतर निषेध भासता है वह भी जीव का ही स्वरूप है। अन्तर केवल अपेक्षाओं का है। जीव के अस्तित्वज्ञान' में स्वयं की अपेक्षा होती है और इतर निषेधात्मक मानने में इतर वस्तुओं की अपेक्षा होती है। इस प्रकार प्रथम दो भंग सिद्ध हुए। 1. आप्तमीमांसा (111वीं कारिका) के व्याख्यान में अकलंक स्वामी लिखते हैं कि "वाचः स्वभावोऽयं येन स्वार्थसामान्यं प्रतिपादयन्ती तदपरं निराकरोति"। अर्थात् वचन का यही स्वभाव है कि स्वविषय का अस्तित्व दिखाता हुआ वह तदितरों का निराकरण करे। "तद्विधेयप्रतिषेध्यात्मविशेषात् स्याद्वादः प्रक्रियते सप्तभंगी समाश्रयात्"। इसलिए अस्तित्व इन दो मूल धर्मों के आश्रय से सप्तभंगी कल्पना करते हुए स्याद्वाद की सिद्धि करते हैं।
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org