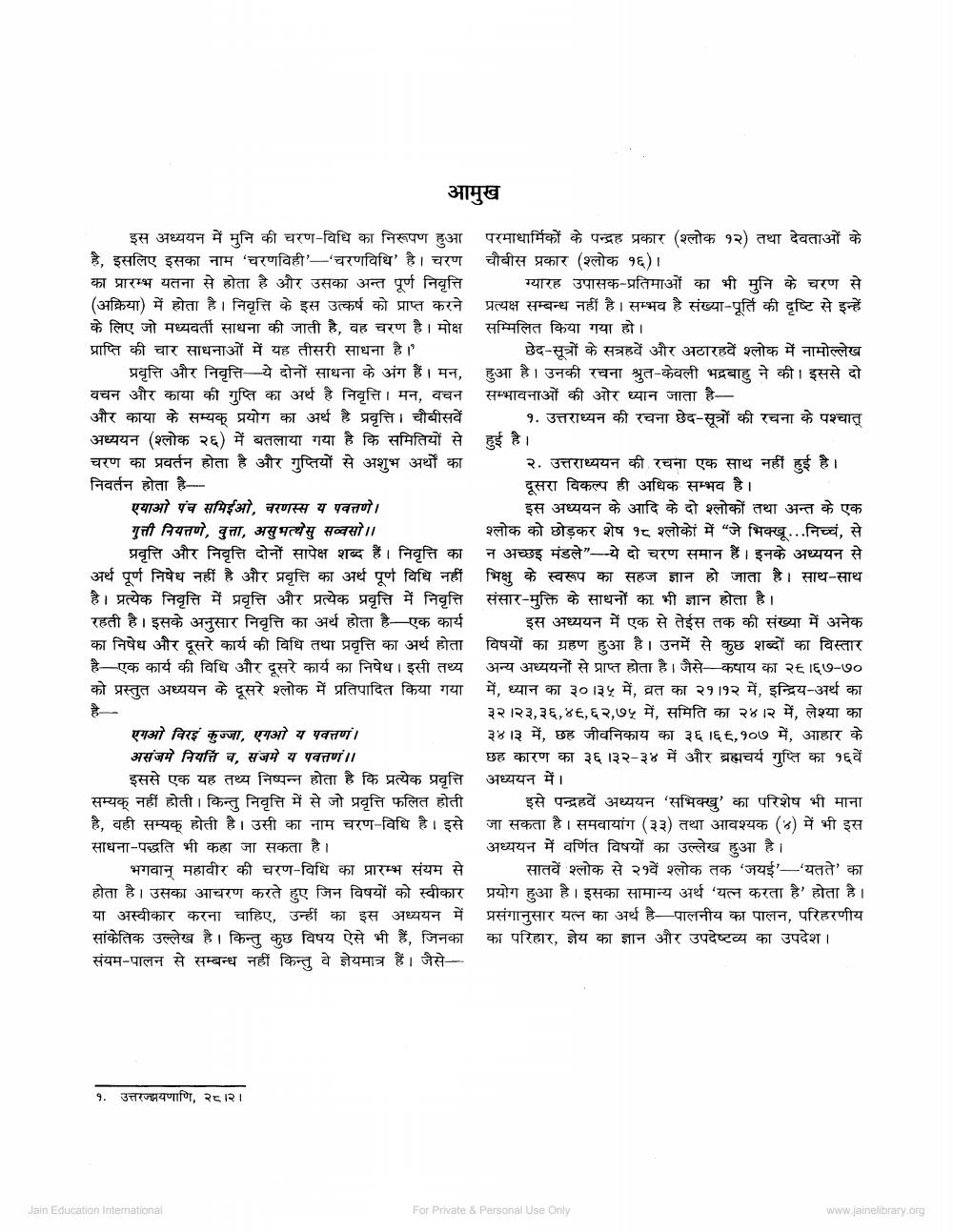________________
आमुख
इस अध्ययन में मुनि की चरण-विधि का निरूपण हुआ है, इसलिए इसका नाम 'चरणविही' – 'चरणविधि' है । चरण का प्रारम्भ यतना से होता है और उसका अन्त पूर्ण निवृत्ति ( अक्रिया) में होता है । निवृत्ति के इस उत्कर्ष को प्राप्त करने के लिए जो मध्यवर्ती साधना की जाती है, वह चरण है। मोक्ष प्राप्ति की चार साधनाओं में यह तीसरी साधना है ।"
प्रवृत्ति और निवृत्ति — ये दोनों साधना के अंग हैं। मन, वचन और काया की गुप्ति का अर्थ है निवृत्ति। मन, वचन और काया के सम्यक् प्रयोग का अर्थ है प्रवृत्ति। चौबीसवें अध्ययन (श्लोक २६ ) में बतलाया गया है कि समितियों से चरण का प्रवर्तन होता है और गुप्तियों से अशुभ अर्थों का निवर्तन होता है
एयाओ पंच समिईओ, चरणस्स य पवत्तणे ।
गुली नियतणे, बुता, असुभत्वे सव्यो ।
प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों सापेक्ष शब्द हैं। निवृत्ति का अर्थ पूर्ण निषेध नहीं है और प्रवृत्ति का अर्थ पूर्ण विधि नहीं है। प्रत्येक निवृत्ति में प्रवृत्ति और प्रत्येक प्रवृत्ति में निवृत्ति रहती है। इसके अनुसार निवृत्ति का अर्थ होता है—एक कार्य का निषेध और दूसरे कार्य की विधि तथा प्रवृत्ति का अर्थ होता है— एक कार्य की विधि और दूसरे कार्य का निषेध । इसी तथ्य को प्रस्तुत अध्ययन के दूसरे श्लोक में प्रतिपादित किया गया है
एगओ विरइं कुज्जा, एगओ य पवत्तणं । असं जमे नियति च, संजमे य पवत्तणं ॥
इससे एक यह तथ्य निष्पन्न होता है कि प्रत्येक प्रवृत्ति सम्यकू नहीं होती । किन्तु निवृत्ति में से जो प्रवृत्ति फलित होती है, वही सम्यक् होती है। उसी का नाम चरण - विधि है। इसे साधना पद्धति भी कहा जा सकता है।
भगवान् महावीर की चरण-विधि का प्रारम्भ संयम से होता है। उसका आचरण करते हुए जिन विषयों को स्वीकार या अस्वीकार करना चाहिए, उन्हीं का इस अध्ययन में सांकेतिक उल्लेख है किन्तु कुछ विषय ऐसे भी हैं, जिनका संयम - पालन से सम्बन्ध नहीं किन्तु वे ज्ञेयमात्र हैं। जैसे
1
१. उत्तरज्झयणाणि, २८ ।२ ।
Jain Education International
परमाधार्मिकों के पन्द्रह प्रकार (श्लोक १२) तथा देवताओं के चौबीस प्रकार (श्लोक १६ ) |
ग्यारह उपासक-प्रतिमाओं का भी मुनि के चरण से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है । सम्भव है संख्या- पूर्ति की दृष्टि से इन्हें सम्मिलित किया गया हो ।
छेद- सूत्रों के सत्रहवें और अठारहवें श्लोक में नामोल्लेख हुआ है। उनकी रचना श्रुत-केवली भद्रबाहु ने की। इससे दो सम्भावनाओं की ओर ध्यान जाता है
१. उत्तराध्यन की रचना छेद सूत्रों की रचना के पश्चात्
हुई है ।
२. उत्तराध्ययन की रचना एक साथ नहीं हुई है। दूसरा विकल्प ही अधिक सम्भव है।
इस अध्ययन के आदि के दो श्लोकों तथा अन्त के एक श्लोक को छोड़कर शेष १८ श्लोकों में "जे भिक्खू... निच्वं, से न अच्छइ मंडले” – ये दो चरण समान हैं। इनके अध्ययन से भिक्षु के स्वरूप का सहज ज्ञान हो जाता है । साथ-साथ संसार- मुक्ति के साधनों का भी ज्ञान होता है ।
इस अध्ययन में एक से तेईस तक की संख्या में अनेक विषयों का ग्रहण हुआ है । उनमें से कुछ शब्दों का विस्तार अन्य अध्ययनों से प्राप्त होता है। जैसे— कषाय का २६।६७-७० में, ध्यान का ३० । ३५ में, व्रत का २१1१२ में, इन्द्रिय-अर्थ का ३२।२३, ३६, ४६,६२,७५ में, समिति का २४।२ में लेश्या का ३४ ।३ में, छह जीवनिकाय का ३६ ।६६, १०७ में, आहार के छह कारण का ३६ ॥३२-३४ में और ब्रह्मचर्य गुप्ति का १६ वें अध्ययन में।
इसे पन्द्रहवें अध्ययन 'सभिक्खु' का परिशेष भी माना जा सकता है। समवायांग (३३) तथा आवश्यक ( ४ ) में भी इस अध्ययन में वर्णित विषयों का उल्लेख हुआ है।
सातवें श्लोक से २१वें श्लोक तक 'जयई' - 'यतते' का प्रयोग हुआ है। इसका सामान्य अर्थ 'यत्न करता है' होता है । प्रसंगानुसार यत्न का अर्थ है–पालनीय का पालन, परिहरणीय का परिहार, ज्ञेय का ज्ञान और उपदेष्टव्य का उपदेश ।
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org