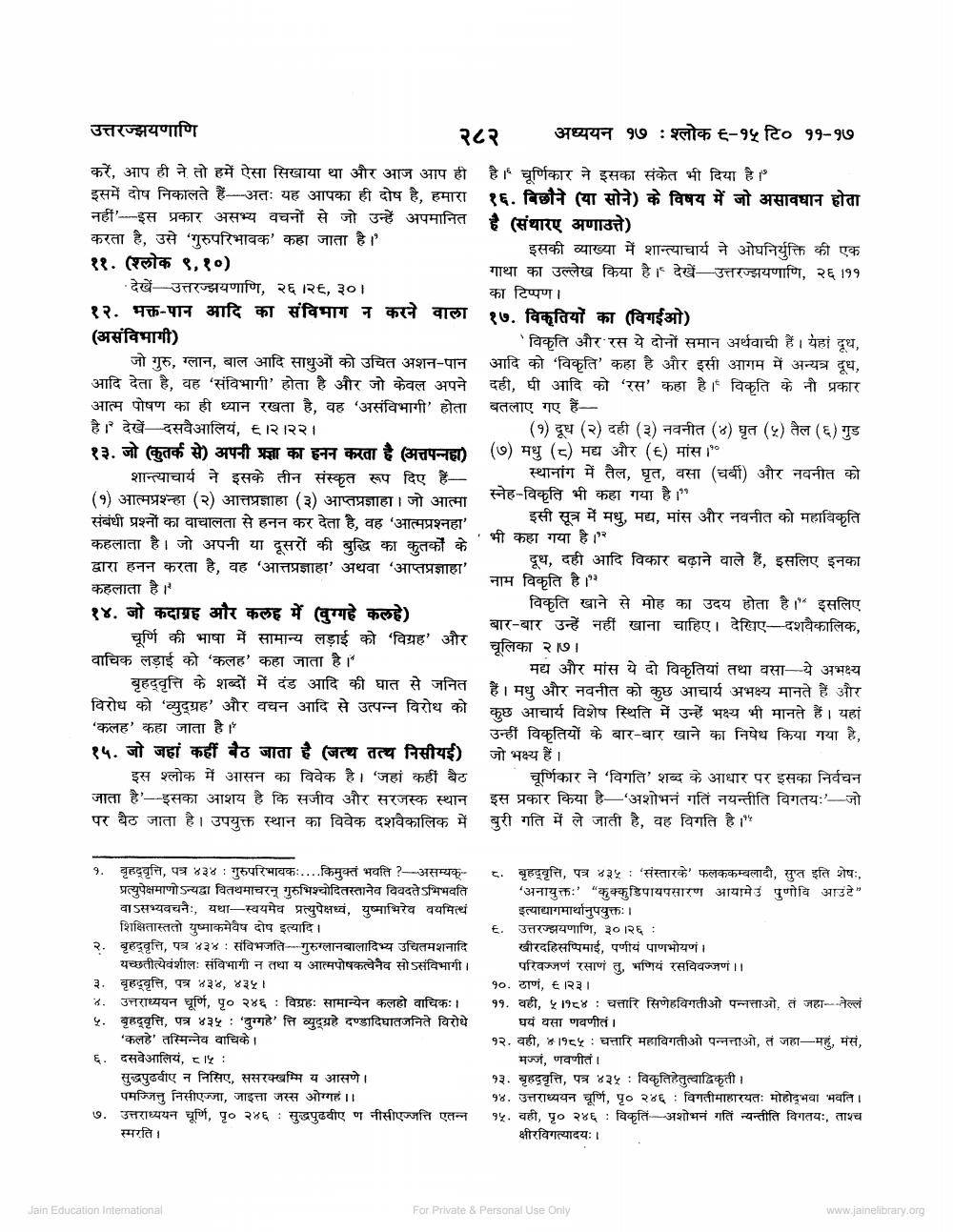________________
उत्तरज्झयणाणि
२८२
करें, आप ही ने तो हमें ऐसा सिखाया था और आज आप ही इसमें दोष निकालते हैं अतः यह आपका ही दोष है, हमारा नहीं'---इस प्रकार असभ्य वचनों से जो उन्हें अपमानित करता है, उसे 'गुरुपरिभावक' कहा जाता है।' ११. (श्लोक ९, १० )
- देखें— उत्तरज्झयणाणि, २६ २६, ३० । १२. भक्त पान आदि का संविभाग न करने वाला (असंविभागी )
जो गुरु, ग्लान, बाल आदि साधुओं को उचित अशन-पान आदि देता है, वह 'संविभागी' होता है और जो केवल अपने आत्म पोषण का ही ध्यान रखता है, वह 'असंविभागी होता है। देखें—– दसवै आलियं, ६।२।२२।
१३. जो (कुतर्क से) अपनी प्रज्ञा का हनन करता है (अत्तपन्नहा) शान्त्याचार्य ने इसके तीन संस्कृत रूप दिए हैं(१) आत्मप्रश्न्हा ( २ ) आत्तप्रज्ञाहा (३) आप्तप्रज्ञाहा। जो आत्मा संबंधी प्रश्नों का वाचालता से हनन कर देता है, वह 'आत्मप्रश्नहा' कहलाता है। जो अपनी या दूसरों की बुद्धि का कुतकों के द्वारा हनन करता है, वह 'आत्तप्रज्ञाहा' अथवा 'आप्तप्रज्ञाहा' कहलाता है।
१४. जो कदाग्रह और कलह में (वुग्गहे कलहे)
चूर्णि की भाषा में सामान्य लड़ाई को 'विग्रह' और वाचिक लड़ाई को 'कलह' कहा जाता है।*
बृहद्वृत्ति के शब्दों में दंड आदि की घात से जनित विरोध को 'व्युद्ग्रह' और वचन आदि से उत्पन्न विरोध को 'कलह' कहा जाता है।*
१५. जो जहां कहीं बैठ जाता है (जत्थ तत्थ निसीयई)
इस श्लोक में आसन का विवेक है। 'जहां कहीं बैठ जाता है-इसका आशय है कि सजीव और सरजस्क स्थान पर बैठ जाता है। उपयुक्त स्थान का विवेक दशवैकालिक में
१. बृहद्वृत्ति, पत्र ४३४ गुरुपरिभावकः किमुक्तं भवति ? - असम्यक्प्रत्युपेक्षमाणोऽन्यद्वा वितथमाचरन् गुरुभिश्चोदितस्तानेव विवदतेऽभिभवति वाऽसभ्यवचनैः, यथा - स्वयमेव प्रत्युपेक्षध्वं युष्माभिरेव वयमित्थं शिक्षितास्ततो युष्माकमेवैष दोष इत्यादि ।
२. बृहद्वृत्ति, पत्र ४३४ : संविभजति गुरुग्लानवालादिभ्य उचितमशनादि यच्छतीत्येवंशीलः संविभागी न तथा य आत्मपोषकत्वेनैव सोऽसंविभागी । ३. बृहद्वृत्ति, पत्र ४३४, ४३५ ।
४.
उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २४६ : विग्रहः सामान्येन कलहो वाचिकः ।
५. बृहद्वृत्ति, पत्र ४३५ : 'दुग्गहे' त्ति व्युद्ग्रहे दण्डादिघातजनिते विरोधे
'कलहे' तस्मिन्नेव वाचिके ।
६. दसवेआलियं ८५
७
सुद्धपुढवीए न निसिए, ससरक्खम्मि य आसणे ।
पमज्जित्तु निसीएज्जा, जाइत्ता जस्स ओग्गहं ।।
उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २४६ : सुद्धपुढवीए ण नीसीएज्जत्ति एतन्न स्मरति ।
Jain Education International
.
अध्ययन १७ : श्लोक ६-१५ टि० ११-१७
है।
चूर्णिकार ने इसका संकेत भी दिया है।"
१६. बिछौने (या सोने) के विषय में जो असावधान होता है (संथारए अणावत्ते )
इसकी व्याख्या में शान्त्याचार्य ने ओपनियुक्ति की एक गाथा का उल्लेख किया है। देखें— उत्तरज्झयणाणि २६ 199 का टिप्पण ।
१७. विकृतियों का (विगईओ)
'विकृति और रस ये दोनों समान अर्थवाची हैं। यहां दूध, आदि को 'विकृति' कहा है और इसी आगम में अन्यत्र दूध, दही, घी आदि को 'रस' कहा है। विकृति के नौ प्रकार बतलाए गए हैं—
"
(१) दूध (२) दही (३) नवनीत (४) घृत (५) तैल (६) गुड (७) मधु (८) मद्य और (६) मांस।
स्थानांग में तैल, घृत, वसा ( चर्बी ) और नवनीत को स्नेह - विकृति भी कहा गया है।"
इसी सूत्र में मधु, मद्य, मांस और नवनीत को महाविकृति भी कहा गया है।
दूध, दही आदि विकार बढ़ाने वाले हैं, इसलिए इनका नाम विकृति है ।
विकृति खाने से मोह का उदय होता है। इसलिए बार-बार उन्हें नहीं खाना चाहिए। देखिए - दशवैकालिक, चूलिका २७ ।
मद्य और मांस ये दो विकृतियां तथा वसा-ये अभक्ष्य हैं। मधु और नवनीत को कुछ आचार्य अभक्ष्य मानते हैं और कुछ आचार्य विशेष स्थिति में उन्हें भक्ष्य भी मानते हैं। यहां उन्हीं विकृतियों के बार-बार खाने का निषेध किया गया है, जो भक्ष्य हैं।
चूर्णिकार ने 'विगति' शब्द के आधार पर इसका निर्वचन इस प्रकार किया है—'अशोभनं गतिं नयन्तीति विगतयः' जो बुरी गति में ले जाती है, वह विगति है । "
८. बृहद्वृत्ति, पत्र ४३५ : 'संस्तारके' फलककम्बलादी, सुप्त इति शेषः, 'अनायुक्तः ' "कुक्कुडिपायपसारण आयामेउं पुणोवि आउंटे" इत्याद्यागमार्थानुपयुक्तः ।
६. उत्तरज्झयणाणि, ३० । २६ :
खीरदहिसप्पिमाई, पणीयं पाणभोयणं ।
परिवज्जणं रसाणं तु, भणियं रसविवज्जणं ।।
१०. ठाणं, ६।२३।
११. वही, ५।१८४ चत्तारि सिणेहविगतीओ पन्नत्ताओ, तं जहा--- -तेल्ल घयं वसा णवणीतं ।
१२. वही, ४।१८५ चत्तारि महाविगतीओ पन्नत्ताओ, तं जहा—महुं, मंसं, मज्जे, णवणीतं ।
१३. बृहद्वृत्ति, पत्र ४३५ विकृतिहेतुत्वाद्विकृती ।
१४. उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २४६ : विगतीमाहारयतः मोहोद्भवा भवति । १५. वहीं, पृ० २४६ विकृति अशोभनं गतिं न्यन्तीति विगतयः, ताश्च क्षीरविगत्यादयः ।
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org