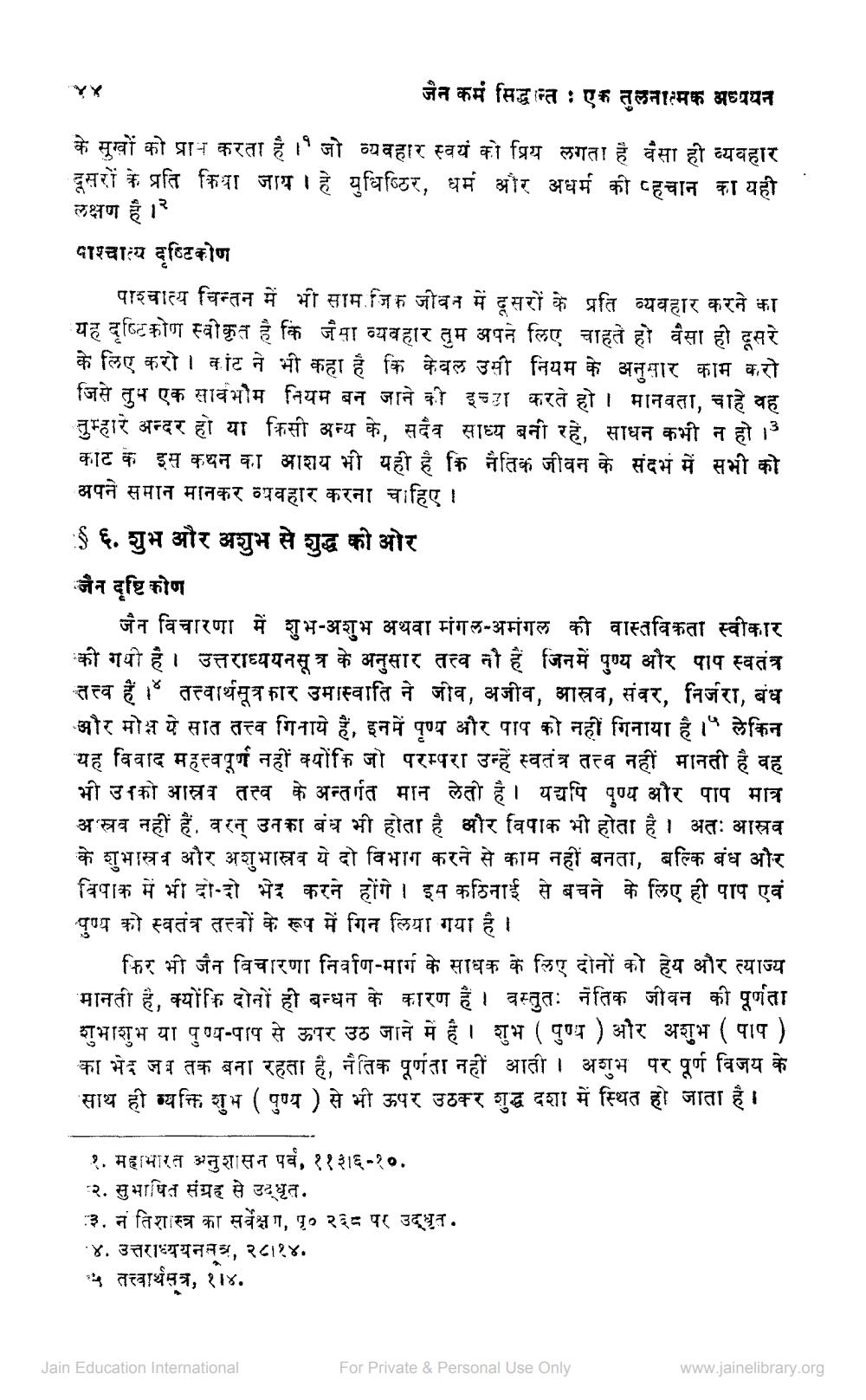________________
जैन कम सिद्धान्त : एक तुलनात्मक अध्ययन
के सुखों को प्रान करता है । जो व्यवहार स्वयं को प्रिय लगता है वैसा ही व्यवहार दूसरों के प्रति किया जाय । हे युधिष्ठिर, धर्म और अधर्म की पहचान का यही लक्षण है। पाश्चात्य दृष्टिकोण
पाश्चात्य चिन्तन में भी सामाजिक जीवन में दूसरों के प्रति व्यवहार करने का यह दृष्टिकोण स्वीकृत है कि जैसा व्यवहार तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही दूसरे के लिए करो। कांट ने भी कहा है कि केवल उसी नियम के अनुसार काम करो जिसे तुम एक सार्वभौम नियम बन जाने की इच्छा करते हो । मानवता, चाहे वह तुम्हारे अन्दर हो या किसी अन्य के, सदैव साध्य बनी रहे, साधन कभी न हो। काट के इस कथन का आशय भी यही है कि नैतिक जीवन के संदर्भ में सभी को अपने समान मानकर व्यवहार करना चाहिए ।
६. शुभ और अशुभ से शुद्ध को ओर जैन दृष्टि कोण __ जैन विचारणा में शुभ-अशुभ अथवा मंगल-अमंगल की वास्तविकता स्वीकार की गयी है। उत्तराध्ययनसूत्र के अनुसार तत्व नौ हैं जिनमें पुण्य और पाप स्वतंत्र तत्त्व हैं। तत्त्वार्थसूत्र कार उमास्वाति ने जीव, अजीव, आस्रव, संवर, निर्जरा, बंध
और मोक्ष ये सात तत्त्व गिनाये है, इनमें पुण्य और पाप को नहीं गिनाया है। लेकिन यह विवाद महत्त्वपूर्ण नहीं क्योंकि जो परम्परा उन्हें स्वतंत्र तत्त्व नहीं मानती है वह भी उसको आस्रव तत्त्व के अन्तर्गत मान लेती है। यद्यपि पुण्य और पाप मात्र अस्रव नहीं हैं. वरन् उनका बंध भी होता है और विपाक भी होता है। अतः आस्रव के शुभास्रव और अशुभास्रव ये दो विभाग करने से काम नहीं बनता, बल्कि बंध और विपाक में भी दो-दो भेद करने होंगे। इस कठिनाई से बचने के लिए ही पाप एवं पुण्य को स्वतंत्र तत्त्वों के रूप में गिन लिया गया है ।
फिर भी जैन विचारणा निर्वाण-मार्ग के साधक के लिए दोनों को हेय और त्याज्य मानती है, क्योंकि दोनों ही बन्धन के कारण है। वस्तुतः नैतिक जीवन की पूर्णता शुभाशुभ या पुण्य-पाप से ऊपर उठ जाने में है। शुभ ( पुण्य ) और अशुभ (पाप) का भेद जब तक बना रहता है, नैतिक पूर्णता नहीं आती। अशुभ पर पूर्ण विजय के साथ ही व्यक्ति शुभ ( पुण्य ) से भी ऊपर उठकर शुद्ध दशा में स्थित हो जाता है।
१. महाभारत अनुशासन पर्व, ११३।६-१०. २. सुभाषित संग्रह से उद्धृत. ३. नं तिशास्त्र का सर्वेक्ष ग, पृ० २६८ पर उद्धृत. ४. उत्तराध्ययनलत्र, २८११४. ५ तत्त्वार्थसत्र, १४.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org