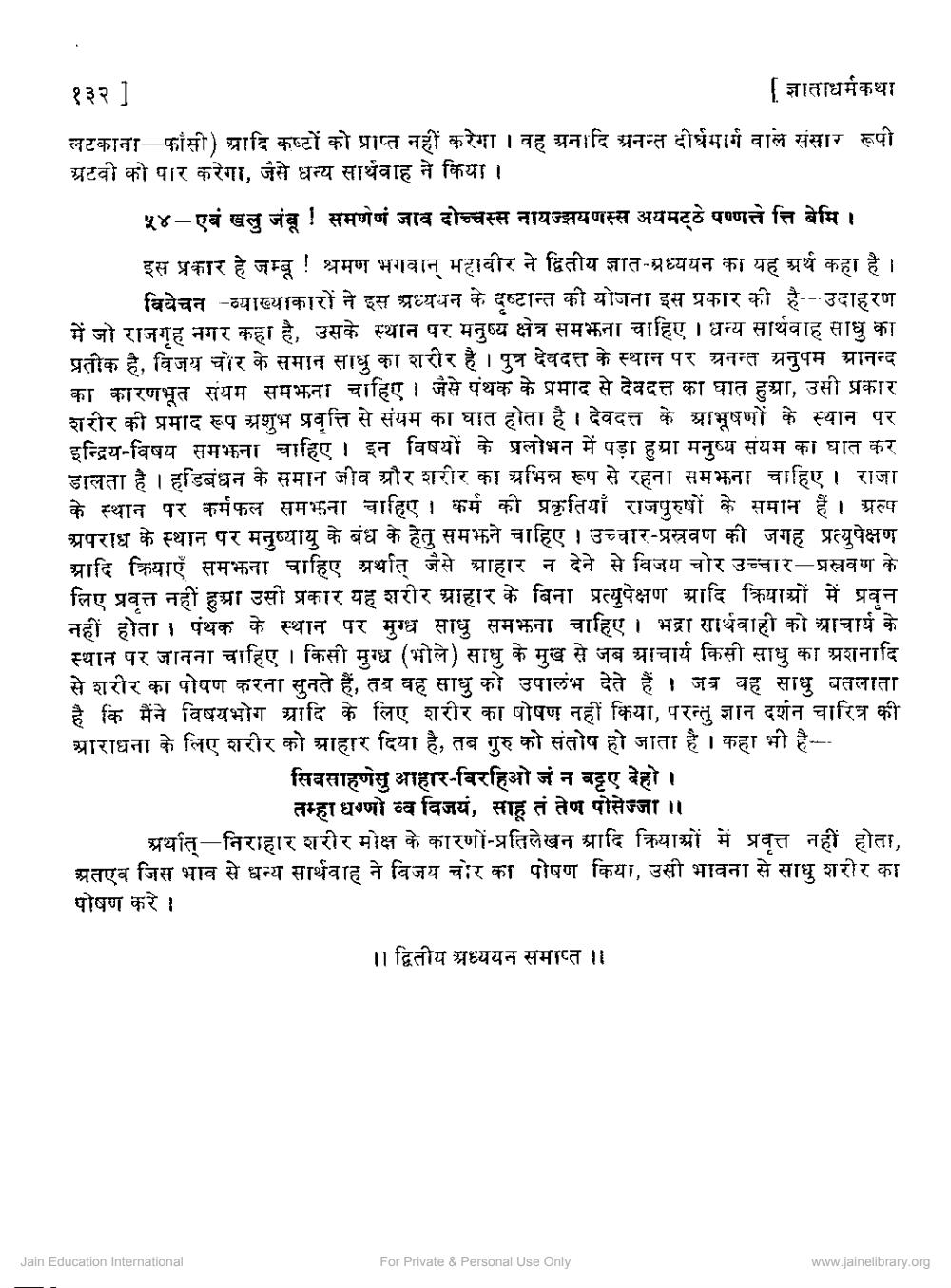________________ 132] [ज्ञाताधर्मकथा लटकाना—फांसी) अादि कष्टों को प्राप्त नहीं करेगा / वह अनादि अनन्त दीर्घमार्ग वाले संसार रूपी अटवी को पार करेगा, जैसे धन्य सार्थवाह ने किया। ५४–एवं खलु जंबू ! समणेणं जाव दोच्चस्स नायज्झयणस्स अयमढे पण्णत्ते त्ति बेमि / इस प्रकार हे जम्बू ! श्रमण भगवान् महावीर ने द्वितीय ज्ञात अध्ययन का यह अर्थ कहा है। विवेचन -व्याख्याकारों ने इस अध्ययन के दृष्टान्त की योजना इस प्रकार की है--- उदाहरण में जो राजगृह नगर कहा है, उसके स्थान पर मनुष्य क्षेत्र समझना चाहिए / धन्य सार्थवाह साधु का प्रतीक है, विजय चौर के समान साधु का शरीर है / पुत्र देवदत्त के स्थान पर अनन्त अनुपम आनन्द का कारणभूत संयम समझना चाहिए। जैसे पंथक के प्रमाद से देवदत्त का घात हया. उसी प्रकार शरीर की प्रमाद रूप अशुभ प्रवृत्ति से संयम का घात होता है / देवदत्त के आभूषणों के स्थान पर इन्द्रिय-विषय समझना चाहिए / इन विषयों के प्रलोभन में पड़ा हुअा मनुष्य संयम का घात कर डालता है। हडिबंधन के समान जीव और शरीर का अभिन्न रूप से रहना समझना चाहिए। राजा के स्थान पर कर्मफल समझना चाहिए। कर्म को प्रकृतियाँ राजपुरुषों के समान हैं। अल्प अपराध के स्थान पर मनुष्यायु के बंध के हेतु समझने चाहिए / उच्चार-प्रस्रवण की जगह प्रत्युपेक्षण आदि क्रियाएँ समझना चाहिए अर्थात् जैसे आहार न देने से विजय चोर उच्चार–प्रस्रवण के लिए प्रवृत्त नहीं हुआ उसी प्रकार यह शरीर पाहार के बिना प्रत्युपेक्षण आदि क्रियाओं में प्रवन नहीं होता। पंथक के स्थान पर मुग्ध साधु समझना चाहिए। भद्रा सार्थवाही को आचार्य के स्थान पर जानना चाहिए / किसी मुग्ध (भोले) साधु के मुख से जब प्राचार्य किसी साधु का अशनादि से शरीर का पोषण करना सुनते हैं, तब वह साधु को उपालंभ देते हैं / जब वह साधु बतलाता है कि मैंने विषयभोग प्रादि के लिए शरीर का षोषण नहीं किया, परन्तु ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना के लिए शरीर को आहार दिया है, तब गुरु को संतोष हो जाता है / कहा भी है-- सिवसाहणेसु आहार-विरहिओ जं न वट्टए देहो। तम्हा धग्णो व्व विजयं, साहू तं तेण पोसेज्जा // अर्थात-निराहार शरीर मोक्ष के कारणों-प्रतिलेखन आदि क्रियाओं में प्रवृत्त नहीं होता, अतएव जिस भाव से धन्य सार्थवाह ने विजय चोर का पोषण किया, उसी भावना से साधु शरीर का पोषण करे। / / द्वितीय अध्ययन समाप्त / / Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org