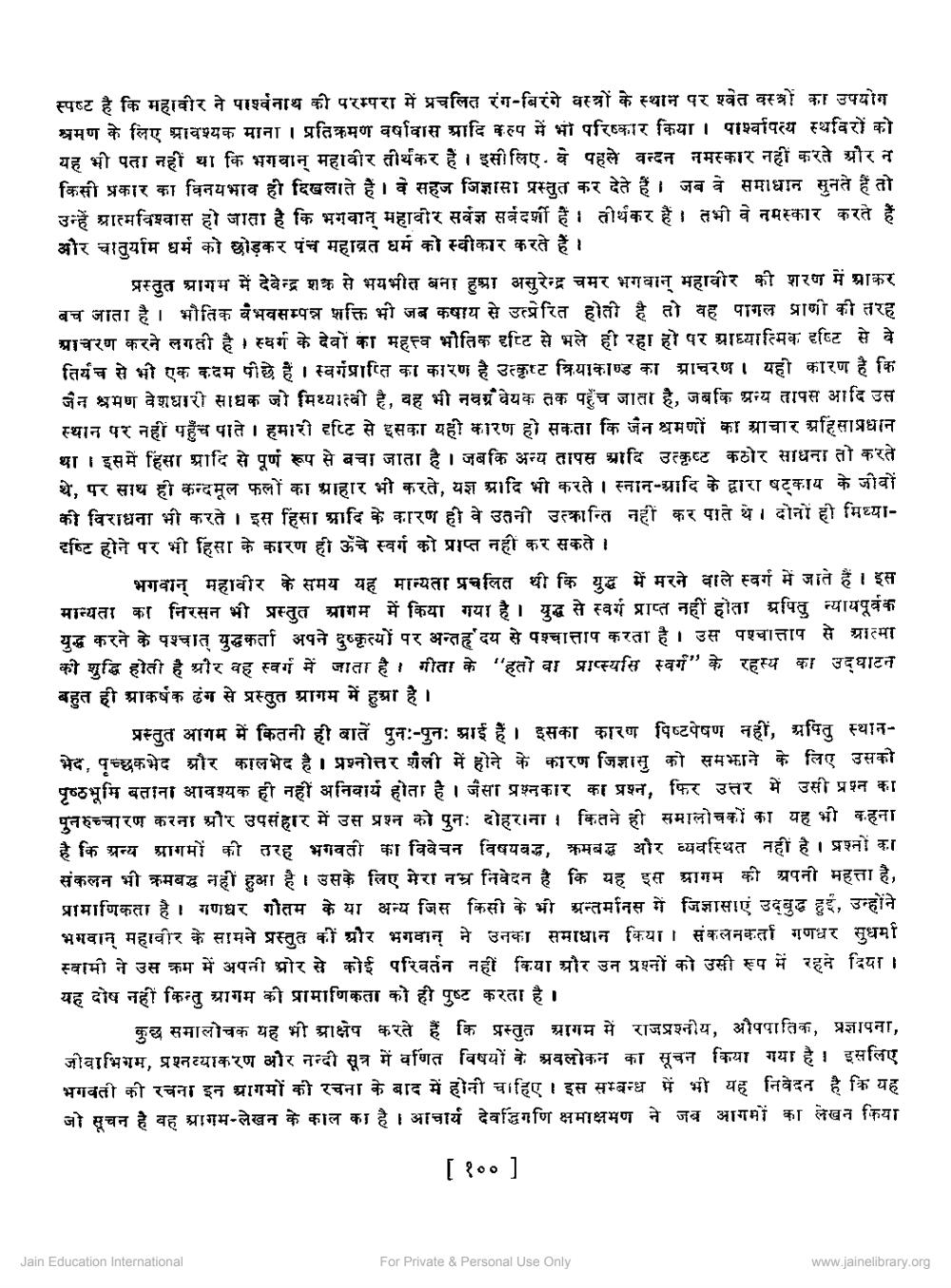________________ स्पष्ट है कि महावीर ने पार्श्वनाथ की परम्परा में प्रचलित रंग-बिरंगे वस्त्रों के स्थान पर श्वेत वस्त्रों का उपयोग श्रमण के लिए प्रावश्यक माना / प्रतिक्रमण वर्षावास प्रादि रूप में भी परिष्कार किया। पापित्य स्थविरों को यह भी पता नहीं था कि भगवान महावीर तीर्थकर हैं। इसीलिए. वे पहले वन्दन नमस्कार नहीं करते और न किसी प्रकार का विनयभाव ही दिखलाते हैं। वे सहज जिज्ञासा प्रस्तुत कर देते हैं। जब वे समाधान सुनते हैं तो उन्हें प्रात्मविश्वास हो जाता है कि भगवान महावीर सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं। तीर्थकर हैं। तभी वे नमस्कार करते हैं और चातुर्याम धर्म को छोड़कर पंच महाव्रत धर्म को स्वीकार करते हैं। प्रस्तुत प्रागम में देवेन्द्र शक्र से भयभीत बना हुअा असुरेन्द्र चमर भगवान् महावीर की शरण में प्राकर बच जाता है। भौतिक वैभवसम्पन्न शक्ति भी जब कषाय से उत्प्रेरित होती है तो वह पागल प्राणी की तरह आचरण करने लगती है। स्वर्ग के देवों का महत्व भौतिक दृष्टि से भले ही रहा हो पर प्राध्यात्मिक दृष्टि से वे तिर्य च से भी एक कदम पीछे है / स्वर्गप्राप्ति का कारण है उत्कृष्ट क्रियाकाण्ड का प्राचरण / यही कारण है कि जैन श्रमण वेशधारी साधक जो मिथ्यात्वी है, वह भी नवग्रं वेयक तक पहुँच जाता है, जबकि अन्य तापस आदि उस स्थान पर नहीं पहुँच पाते / हमारी दृष्टि से इसका यही कारण हो सकता कि जैन श्रमणों का प्राचार अहिंसाप्रधान था। इसमें हिंसा प्रादि से पूर्ण रूप से बचा जाता है। जबकि अन्य तापस आदि उत्कृष्ट कठोर साधना तो करते थे, पर साथ ही कन्दमूल फलों का आहार भी करते, यज्ञ आदि भी करते / स्नान आदि के द्वारा षट्काय के जीवों की विराधना भी करते / इस हिंसा आदि के कारण ही वे उतनी उत्क्रान्ति नहीं कर पाते थे। दोनों ही मिथ्यादृष्टि होने पर भी हिसा के कारण ही ऊँचे स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान महावीर के समय यह मान्यता प्रचलित थी कि युद्ध में मरने वाले स्वर्ग में जाते हैं। इस मान्यता का निरसन भी प्रस्तुत प्रागम में किया गया है। युद्ध से स्वर्ग प्राप्त नहीं होता अपितु न्यायपूर्वक युद्ध करने के पश्चात् युद्धकर्ता अपने दुष्कृत्यों पर अन्तर्हदय से पश्चात्ताप करता है। उस पश्चात्ताप से यात्मा की शुद्धि होती है और वह स्वर्ग में जाता है। गीता के "हतो बा प्राप्स्यसि स्वर्ग" के रहस्य का उद्घाटन बहुत ही आकर्षक ढंग से प्रस्तुत पागम में हुआ है। प्रस्तुत आगम में कितनी ही बातें पुन:-पुनः आई हैं। इसका कारण पिष्टपेषण नहीं, अपितु स्थानभेद, पृच्छक भेद और कालभेद है। प्रश्नोत्तर शैली में होने के कारण जिज्ञासु को समझाने के लिए उसको पृष्ठभूमि बताना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य होता है। जैसा प्रश्न कार का प्रश्न, फिर उत्तर में उसी प्रश्न का पुनरुच्चारण करना और उपसंहार में उस प्रश्न को पुनः दोहराना / कितने ही समालोचकों का यह भी कहना है कि अन्य आगमों की तरह भगवती का विवेचन विषयबद्ध, क्रमबद्ध और व्यवस्थित नहीं है। प्रश्नों का संकलन भी क्रमबद्ध नहीं हुआ है। उसके लिए मेरा नम्र निवेदन है कि यह इस प्रागम की अपनी महत्ता है, प्रामाणिकता है। गणधर गौतम के या अन्य जिस किसी के भी अन्तर्मानस में जिज्ञासाएं उदबुद्ध हुई, उन्होंने भगवान् महावीर के सामने प्रस्तुत की और भगवान् ने उनका समाधान किया। संकलनकर्ता गणधर सुधर्मा स्वामी ने उस क्रम में अपनी ओर से कोई परिवर्तन नहीं किया और उन प्रश्नों को उसी रूप में रहने दिया। यह दोष नहीं किन्तु पागम की प्रामाणिकता को ही पुष्ट करता है। कुछ समालोचक यह भी आक्षेप करते हैं कि प्रस्तुत प्रागम में राजप्रश्नीय, औपपातिक, प्रज्ञापना, जीवाभिगम, प्रश्न व्याकरण और नन्दी सूत्र में वर्णित विषयों के अवलोकन का सूचन किया गया है। इसलिए भगवती की रचना इन पागमों की रचना के बाद में होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में भी यह निवेदन है कि यह जो सुचन है बह आगम-लेखन के काल का है। आचार्य देवद्धिगणि क्षमाक्षमण ने जब आगमों का लेखन किया [ 100 ] Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org