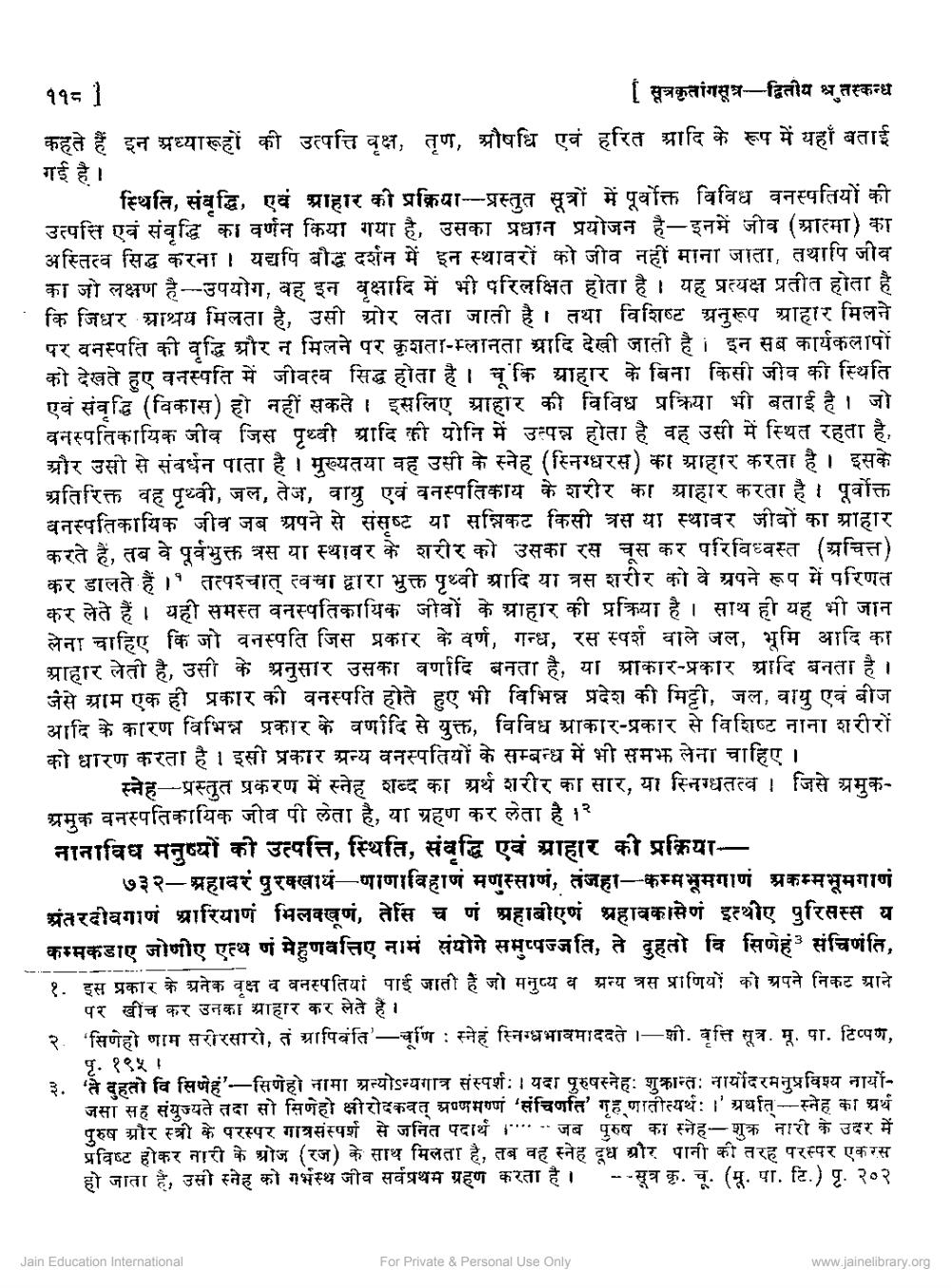________________ 118 1 [ सूत्रकृतांगसूत्र-द्वितीय श्रुतस्कन्ध कहते हैं इन अध्यारूहों की उत्पत्ति वृक्ष, तृण, औषधि एवं हरित आदि के रूप में यहाँ बताई गई है। स्थिति, संवृद्धि, एवं प्राहार की प्रक्रिया-प्रस्तुत सूत्रों में पूर्वोक्त विविध वनस्पतियों की उत्पत्ति एवं संवृद्धि का वर्णन किया गया है, उसका प्रधान प्रयोजन है-इनमें जीव (आत्मा) का अस्तित्व सिद्ध करना / यद्यपि बौद्ध दर्शन में इन स्थावरों को जीव नहीं माना जाता, तथापि जीव का जो लक्षण है--उपयोग, वह इन वृक्षादि में भी परिलक्षित होता है। यह प्रत्यक्ष प्रतीत होता है कि जिधर पाश्रय मिलता है, उसी अोर लता जाती है। तथा विशिष्ट अनुरूप आहार मिलने पर वनस्पति की वृद्धि और न मिलने पर कृशता-मलानता आदि देखी जाती है। इन सब कार्यकलापों को देखते हुए वनस्पति में जीवत्व सिद्ध होता है। चूकि पाहार के बिना किसी जीव की स्थिति एवं संवद्धि (विकास) हो नहीं सकते। इसलिए आहार की विविध प्रक्रिया भी बताई है। जो वनस्पतिकायिक जीव जिस पृथ्वी आदि की योनि में उत्पन्न होता है वह उसी में स्थित रहता है, और उसो से संवर्धन पाता है / मुख्यतया वह उसी के स्नेह (स्निग्धरस) का आहार करता है। इसके अतिरिक्त वह पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं वनस्पतिकाय के शरीर का अाहार करता है। पूर्वोक्त बनस्पतिकायिक जीव जब अपने से संसृष्ट या सन्निकट किसी त्रस या स्थावर जीवों का आहार करते हैं, तब वे पूर्वभुक्त त्रस या स्थावर के शरीर को उसका रस चूस कर परिविध्वस्त (अचित्त) कर डालते हैं।' तत्पश्चात् त्वचा द्वारा भुक्त पृथ्वी आदि या त्रस शरीर को वे अपने रूप में परिणत कर लेते हैं। यही समस्त वनस्पतिकायिक जीवों के आहार की प्रक्रिया है। साथ ही यह भी जान लेना चाहिए कि जो वनस्पति जिस प्रकार के वर्ण, गन्ध, रस स्पर्श वाले जल, भूमि आदि का आहार लेती है, उसी के अनुसार उसका वर्णादि बनता है, या आकार-प्रकार प्रादि बनता है। जैसे ग्राम एक ही प्रकार की वनस्पति होते हुए भी विभिन्न प्रदेश की मिट्टी, जल, वायु एवं बीज आदि के कारण विभिन्न प्रकार के वर्णादि से युक्त, विविध आकार-प्रकार से विशिष्ट नाना शरीरों को धारण करता है / इसी प्रकार अन्य वनस्पतियों के सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिए। स्नेह-प्रस्तुत प्रकरण में स्नेह शब्द का अर्थ शरीर का सार, या स्निग्धतत्व / जिसे अमुकअमुक वनस्पतिकायिक जीव पी लेता है, या ग्रहण कर लेता है / 2 / नानाविध मनुष्यों की उत्पत्ति, स्थिति, संवृद्धि एवं आहार की प्रक्रिया 732- प्रहावरं पुरक्खायं—णाणाविहाणं मणुस्साणं, तंजहा-कम्मभूमगाणं प्रकम्मभूमगाणं अंतरदीवगाणं प्रारियाणं मिलक्खूणं, तेसि च णं अहाबीएणं अहावकासेणं इत्थीए पुरिसस्स य कम्मकडाए जोणीए एत्थ णं मेहुणवत्तिए नामं संयोगे समुप्पज्जति, ते दुहतो वि सिणेहं संचिणंति, 1. इस प्रकार के अनेक वृक्ष व वनस्पतियां पाई जाती हैं जो मनुष्य व अन्य त्रस प्राणियों को अपने निकट पाने पर खींच कर उनका प्रहार कर लेते है। 2. 'सिणेहो णाम सरीरसारो, तं प्रापिवंति'-चूणि : स्नेहं स्निग्धभावमाददते ।—शी. वृत्ति सूत्र. मू. पा. टिप्पण, 3. 'ते दहतो वि सिणेह-सिणेहो नामा अन्योऽन्यगात्र संस्पर्शः। यदा पुरुषस्नेहः शुक्रान्त: नार्योदरमनप्रविश्य नार्यो जसा सह संयुज्यते तदा सो सिणेहो क्षीरोदकवत् अण्णमण्णं 'संचिति' गृहाणातीत्यर्थः / ' अर्थात् स्नेह का अर्थ पुरुष और स्त्री के परस्पर गात्रसंस्पर्श से जनित पदार्थ / " जब पुरुष का स्नेह-शुक्र नारी के उदर में प्रविष्ट होकर नारी के प्रोज (रज) के साथ मिलता है, तब वह स्नेह दूध और पानी की तरह परस्पर एक रस हो जाता है, उसी स्नेह को गर्भस्थ जीव सर्वप्रथम ग्रहण करता है। --सूत्र कृ. च. (म. पा. टि.) पृ. 202 Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org