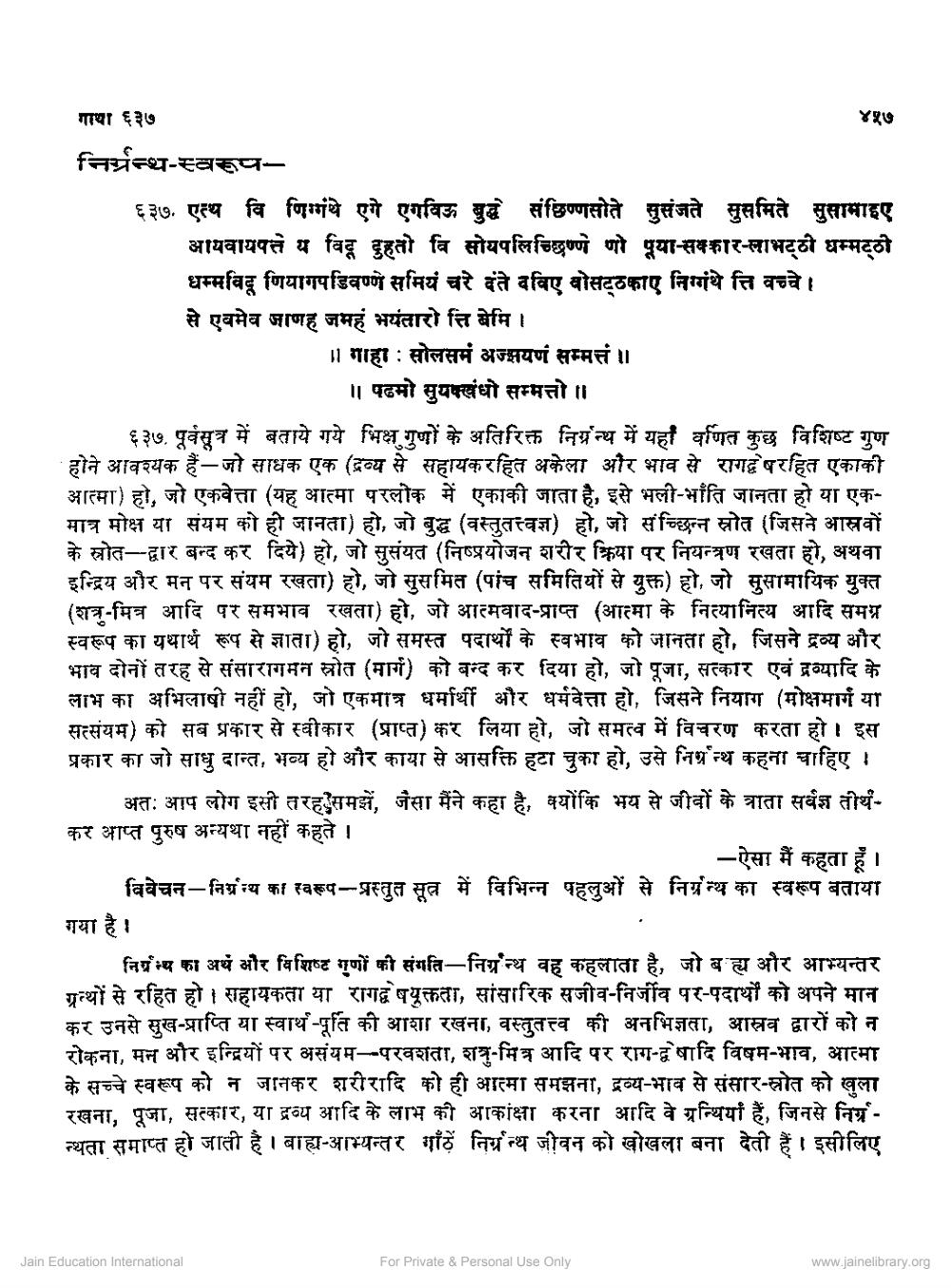________________ 457 गाथा 637 निर्ग्रन्थ-स्वरुप६३७. एस्थ वि णिग्गंथे एगे एगविऊ बुद्ध संछिण्णसोते सुसंजते सुसमिते सुसामाइए आयवायपत्ते य विदू दुहतो वि सोयपलिच्छिण्णे णो पूया-सक्कार-लाभट्ठी धम्मट्ठी धम्मविद् णियागपडिवण्णे समियं चरे वंते दविए वोसट्ठकाए निग्गंथे त्ति वच्चे। से एवमेव जाणह जमहं भयंतारो ति बेमि / // गाहा : सोलसमं अज्झयणं सम्मत्तं // // पढमो सुयक्खंधो सम्मत्तो।। 637. पूर्वसूत्र में बताये गये भिक्ष गुणों के अतिरिक्त निर्ग्रन्थ में यहाँ वणित कुछ विशिष्ट गुण होने आवश्यक हैं-जो साधक एक (द्रव्य से सहायकरहित अकेला और भाव से रागद्वेषरहित एकाकी आत्मा) हो, जो एकवेत्ता (यह आत्मा परलोक में एकाकी जाता है, इसे भली-भाँति जानता हो या एक यम को ही जानता) हो, जो बुद्ध (वस्तुतत्त्वज्ञ) हो, जो संच्छिन्न स्रोत (जिसने आस्रवों के स्रोत-द्वार बन्द कर दिये) हो, जो सुसंयत (निष्प्रयोजन शरीर क्रिया पर नियन्त्रण रखता हो, अथवा इन्द्रिय और मन पर संयम रखता) हो, जो सुसमित (पांच समितियों से युक्त) हो, जो सुसामायिक युक्त (शत्रु-मित्र आदि पर समभाव रखता) हो, जो आत्मवाद-प्राप्त (आत्मा के नित्यानित्य आदि समग्र स्वरूप का यथार्थ रूप से ज्ञाता) हो, जो समस्त पदार्थों के स्वभाव को जानता हो, जिसने द्रव्य और भाव दोनों तरह से संसारागमन स्रोत (मार्ग) को बन्द कर दिया हो, जो पूजा, सत्कार एवं द्रव्यादि के लाभ का अभिलाषी नहीं हो, जो एकमात्र धर्मार्थी और धर्मवेत्ता हो, जिसने नियाग (मोक्षमार्ग या सत्संयम) को सब प्रकार से स्वीकार (प्राप्त कर लिया हो, जो समत्व में विचरण करता हो। इस प्रकार का जो साधु दान्त, भव्य हो और काया से आसक्ति हटा चुका हो, उसे निम्रन्थ कहना चाहिए / अतः आप लोग इसी तरह समझें, जैसा मैंने कहा है, क्योंकि भय से जीवों के त्राता सर्वज्ञ तीर्थकर आप्त पुरुष अन्यथा नहीं कहते / -ऐसा मैं कहता हूँ। विवेचन-निग्रंन्य का स्वरूप-प्रस्तुत सूत्र में विभिन्न पहलुओं से निर्ग्रन्थ का स्वरूप बताया गया है। निर्गन्य का अर्थ और विशिष्ट गणों की संगति-निग्रन्थ वह कहलाता है, जो ब ह्य और आभ्यन्तर ग्रन्थों से रहित हो। सहायकता या रागद्वेषयुक्तता, सांसारिक सजीव-निर्जीव पर-पदार्थों को अपने मान कर उनसे सुख-प्राप्ति या स्वार्थ पूर्ति की आशा रखना, वस्तुतत्त्व की अनभिज्ञता, आस्रव द्वारों को न रोकना, मन और इन्द्रियों पर असंयम-परवशता, शत्रु-मित्र आदि पर राग-द्वषादि विषम-भाव, आत्मा के सच्चे स्वरूप को न जानकर शरीरादि को ही आत्मा समझना, द्रव्य-भाव से संसार-स्रोत को खुला रखना, पूजा, सत्कार, या द्रव्य आदि के लाभ की आकांक्षा करना आदि वे ग्रन्थियां हैं, जिनसे निग्रंन्यता समाप्त हो जाती है / बाह्य-आभ्यन्तर गाँठे निर्ग्रन्थ जीवन को खोखला बना देती हैं। इसीलिए Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org