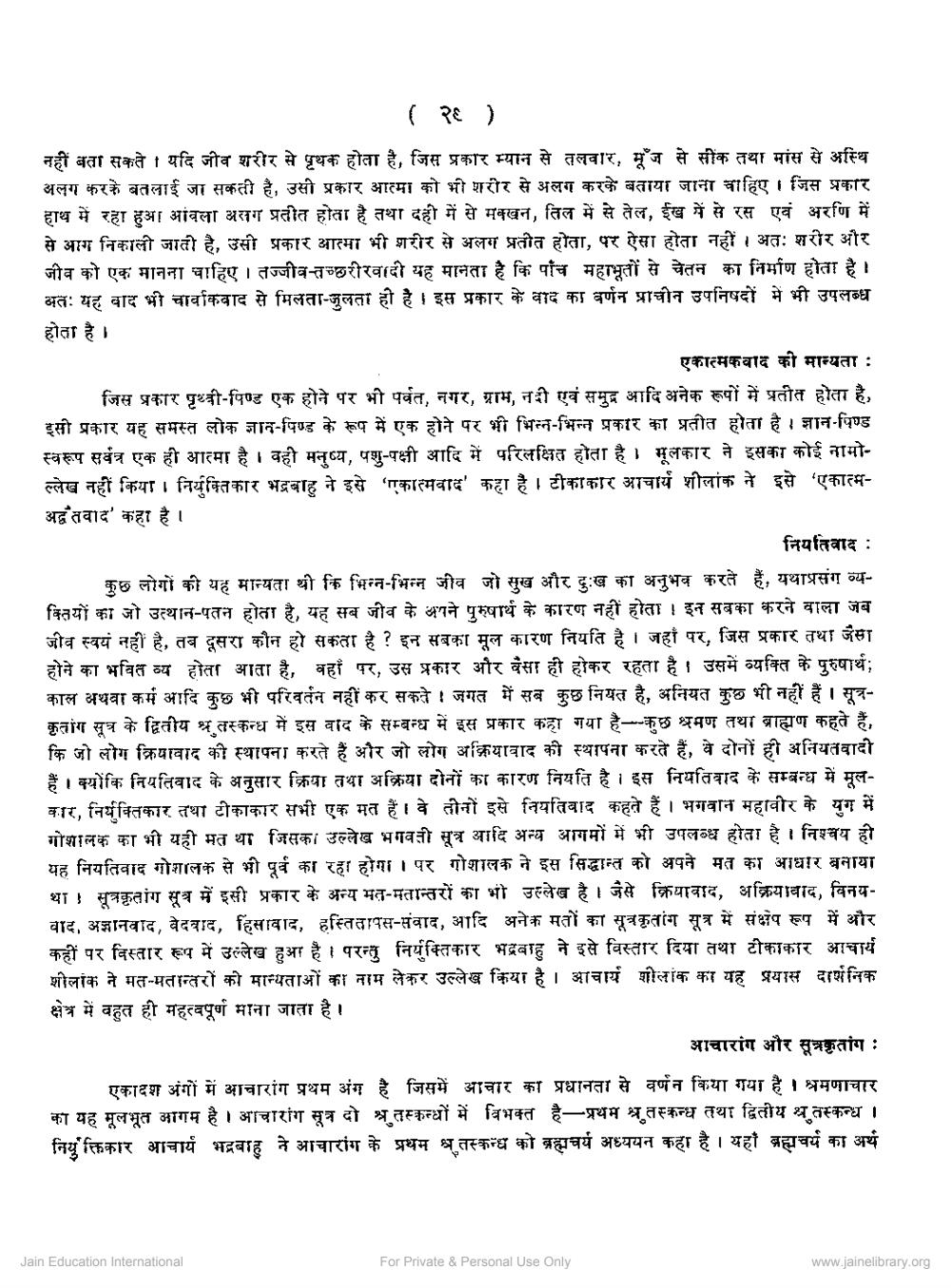________________ ( 26 ) नहीं बता सकते / यदि जीव शरीर से पृथक होता है, जिस प्रकार म्यान से तलवार, मज से सीक तथा मांस से अस्थि अलग करके बतलाई जा सकती है, उसी प्रकार आत्मा को भी शरीर से अलग करके बताया जाना चाहिए / जिस प्रकार हाथ में रहा हुआ आंवला असग प्रतीत होता है तथा दही में से मक्खन, तिल में से तेल, ईख में से रस एवं अरणि में से आग निकाली जाती है, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर से अलग प्रतीत होता, पर ऐसा होता नहीं। अतः शरीर और जीव को एक मानना चाहिए। तज्जीव-तच्छरीरवादी यह मानता है कि पांच महाभूतों से चेतन का निर्माण होता है। अतः यह बाद भी चार्वाकवाद से मिलता-जुलता ही है / इस प्रकार के बाद का वर्णन प्राचीन उपनिषदों में भी उपलब्ध होता है। एकात्मकवाद की मान्यता : जिस प्रकार पृथ्वी-पिण्ड एक होने पर भी पर्वत, नगर, ग्राम, नदी एवं समुद्र आदि अनेक रूपों में प्रतीत होता है, इसी प्रकार यह समस्त लोक ज्ञान-पिण्ड के रूप में एक होने पर भी भिन्न-भिन्न प्रकार का प्रतीत होता है / ज्ञान-पिण्ड स्वरूप सर्वत्र एक ही आत्मा है। वही मनुष्य, पशु-पक्षी आदि में परिलक्षित होता है। मलकार ने इसका कोई नामोल्लेख नहीं किया। नियुक्तिकार भद्रबाह ने इसे 'एकात्मवाद' कहा है / टीकाकार आचार्य शीलांक ने इसे 'एकात्मअद्वैतवाद' कहा है। नियतिवाद : कुछ लोगों की यह मान्यता थी कि भिन्न-भिन्न जीव जो सुख और दुःख का अनुभव करते हैं, यथाप्रसंग व्यक्तियों का जो उत्थान-पतन होता है, यह सब जीव के अपने पुरुषार्थ के कारण नहीं होता। इन सबका करने वाला जब जीव स्वयं नहीं है, तब दूसरा कौन हो सकता है ? इन सबका मूल कारण नियति है / जहाँ पर, जिस प्रकार तथा जैसा होने का भवित व्य होता आता है, वहाँ पर, उस प्रकार और वैसा ही होकर रहता है। उसमें व्यक्ति के पुरुषार्थ; काल अथवा कर्म आदि कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते / जगत में सब कुछ नियत है, अनियत कुछ भी नहीं हैं / सूत्रकृतांग सूत्र के द्वितीय श्रू तस्कन्ध में इस वाद के सम्बन्ध में इस प्रकार कहा गया है कुछ श्रमण तथा ब्राह्मण कहते हैं, कि जो लोग क्रियावाद की स्थापना करते हैं और जो लोग अक्रियावाद की स्थापना करते हैं, वे दोनों ही अनियतवादी हैं। क्योंकि नियतिवाद के अनुसार क्रिया तथा अक्रिया दोनों का कारण नियति है। इस नियतिवाद के सम्बन्ध में मूलकार, नियुक्तिकार तथा टीकाकार सभी एक मत हैं। वे तीनों इसे नियतिवाद कहते हैं। भगवान महावीर के युग में गोशालक का भी यही मत था जिसका उल्लेख भगवती सूत्र आदि अन्य आगमों में भी उपलब्ध होता है। निश्चय ही यह नियतिवाद गोशालक से भी पूर्व का रहा होगा / पर गोशालक ने इस सिद्धान्त को अपने मत का आधार बनाया था। सूत्रकृतांग सूत्र में इसी प्रकार के अन्य भत-मतान्तरों का भी उल्लेख है। जैसे क्रियावाद, अक्रियावाद, विनयवाद, अज्ञानवाद, वेदवाद, हिंसावाद, हस्तितापस-संवाद, आदि अनेक मतों का सूत्रकृतांग सूत्र में संक्षेप रूप में और कहीं पर विस्तार रूप में उल्लेख हुआ है। परन्तु नियुक्तिकार भद्रबाहु ने इसे विस्तार दिया तथा टीकाकार आचार्य शीलांक ने मत-मतान्तरों को मान्यताओं का नाम लेकर उल्लेख किया है। आचार्य शीलांक का यह प्रयास दार्शनिक क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आचारांग और सूत्रकृतांग : एकादश अंगों में आचारांग प्रथम अंग है जिसमें आचार का प्रधानता से वर्णन किया गया है। श्रमणाचार का यह मूलभूत आगम है। आचारांग सूत्र दो श्रु तस्कन्धों में विभक्त है-प्रथम श्रुतस्कन्ध तथा द्वितीय श्रुतस्कन्ध / नियुक्तिकार आचार्य भद्रबाह ने आचारांग के प्रथम श्र तस्कन्ध को ब्रह्मचर्य अध्ययन कहा है। यहाँ ब्रह्मचर्य का अर्थ Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org