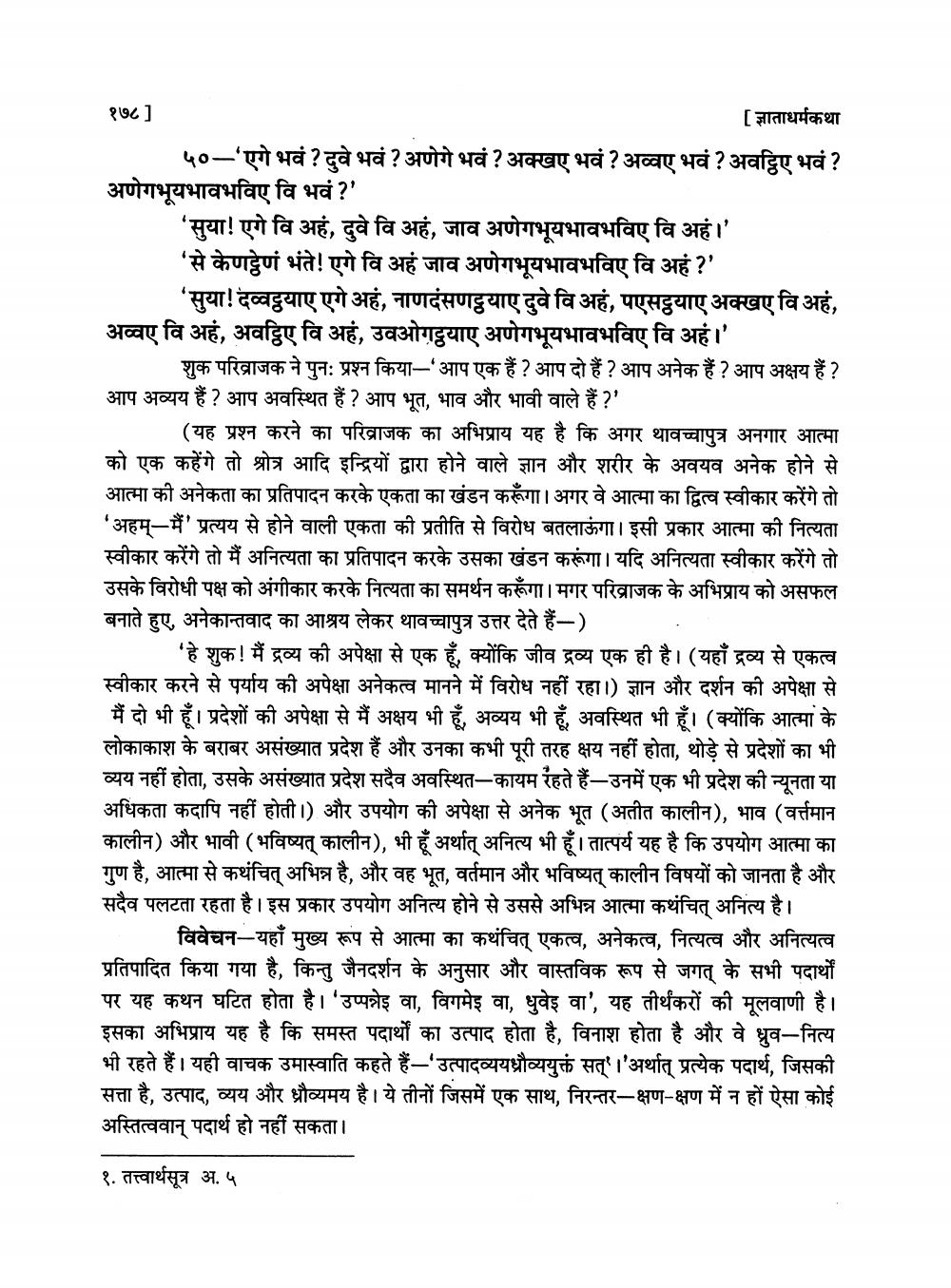________________
१७८ ]
[ ज्ञाताधर्मकथा
५० - ' एगे भवं ? दुवे भवं ? अणेगे भवं ? अक्खए भवं ? अव्वए भवं ? अवट्ठिए भवं ? अणेगभूयभावभविए वि भवं ?"
'सुया! एगे वि अहं, दुवे वि अहं, जाव अणेगभूयभावभविए वि अहं ।' 'से केणट्टेणं भंते! एगे वि अहं जाव अणेगभूयभावभविए वि अहं ?'
'सुया ! 'दव्वट्टयाए एगे अहं, नाणदंसणट्टयाए दुवे वि अहं, पएसट्टयाए अक्खए वि अहं, अव्वए वि अहं, अवट्ठिए वि अहं, उवओगट्टयाए अणेगभूयभावभविए वि अहं ।'
शुक परिव्राजक ने पुनः प्रश्न किया- 'आप एक हैं? आप दो हैं? आप अनेक हैं ? आप अक्षय हैं ? आप अव्यय हैं ? आप अवस्थित हैं ? आप भूत, भाव और भावी वाले हैं ?'
( यह प्रश्न करने का परिव्राजक का अभिप्राय यह है कि अगर थावच्चापुत्र अनगार आत्मा को एक कहेंगे तो श्रोत्र आदि इन्द्रियों द्वारा होने वाले ज्ञान और शरीर के अवयव अनेक होने से आत्मा की अनेकता का प्रतिपादन करके एकता का खंडन करूँगा। अगर वे आत्मा का द्वित्व स्वीकार करेंगे तो 'अहम् - मैं' प्रत्यय से होने वाली एकता की प्रतीति से विरोध बतलाऊंगा । इसी प्रकार आत्मा की नित्यता स्वीकार करेंगे तो मैं अनित्यता का प्रतिपादन करके उसका खंडन करूंगा । यदि अनित्यता स्वीकार करेंगे तो उसके विरोधी पक्ष को अंगीकार करके नित्यता का समर्थन करूँगा । मगर परिव्राजक के अभिप्राय को असफल बनाते हुए, अनेकान्तवाद का आश्रय लेकर थावच्चापुत्र उत्तर देते हैं -)
' हे शुक! मैं द्रव्य की अपेक्षा से एक हूँ, क्योंकि जीव द्रव्य एक ही है। (यहाँ द्रव्य से एकत्व स्वीकार करने से पर्याय की अपेक्षा अनेकत्व मानने में विरोध नहीं रहा ।) ज्ञान और दर्शन की अपेक्षा से मैं दो भी हूँ । प्रदेशों की अपेक्षा से मैं अक्षय भी हूँ, अव्यय भी हूँ, अवस्थित भी हूँ। ( क्योंकि आत्मा के लोकाकाश के बराबर असंख्यात प्रदेश हैं और उनका कभी पूरी तरह क्षय नहीं होता, थोड़े से प्रदेशों का भी व्यय नहीं होता, उसके असंख्यात प्रदेश सदैव अवस्थित — कायम रहते हैं - उनमें एक भी प्रदेश की न्यूनता या अधिकता कदापि नहीं होती।) और उपयोग की अपेक्षा से अनेक भूत (अतीत कालीन), भाव ( वर्त्तमान कालीन) और भावी (भविष्यत् कालीन), भी हूँ अर्थात् अनित्य भी हूँ । तात्पर्य यह है कि उपयोग आत्मा का गुण है, आत्मा से कथंचित् अभिन्न है, और वह भूत, वर्तमान और भविष्यत् कालीन विषयों को जानता है और सदैव पलटता रहता है। इस प्रकार उपयोग अनित्य होने से उससे अभिन्न आत्मा कथंचित् अनित्य है ।
विवेचन - यहाँ मुख्य रूप से आत्मा का कथंचित् एकत्व, अनेकत्व, नित्यत्व और अनित्यत्व प्रतिपादित किया गया है, किन्तु जैनदर्शन के अनुसार और वास्तविक रूप से जगत् के सभी पदार्थों पर यह कथन घटित होता है । 'उप्पन्नेइ वा, विगमेइ वा, धुवेइ वा', यह तीर्थंकरों की मूलवाणी है । इसका अभिप्राय यह है कि समस्त पदार्थों का उत्पाद होता है, विनाश होता है और वे ध्रुव - नित्य भी रहते हैं। यही वाचक उमास्वाति कहते हैं - 'उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्' ।' अर्थात् प्रत्येक पदार्थ, जिसकी सत्ता है, उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यमय है। ये तीनों जिसमें एक साथ, निरन्तर - क्षण-क्षण में न हों ऐसा कोई अस्तित्ववान् पदार्थ हो नहीं सकता ।
१. तत्त्वार्थसूत्र अ. ५