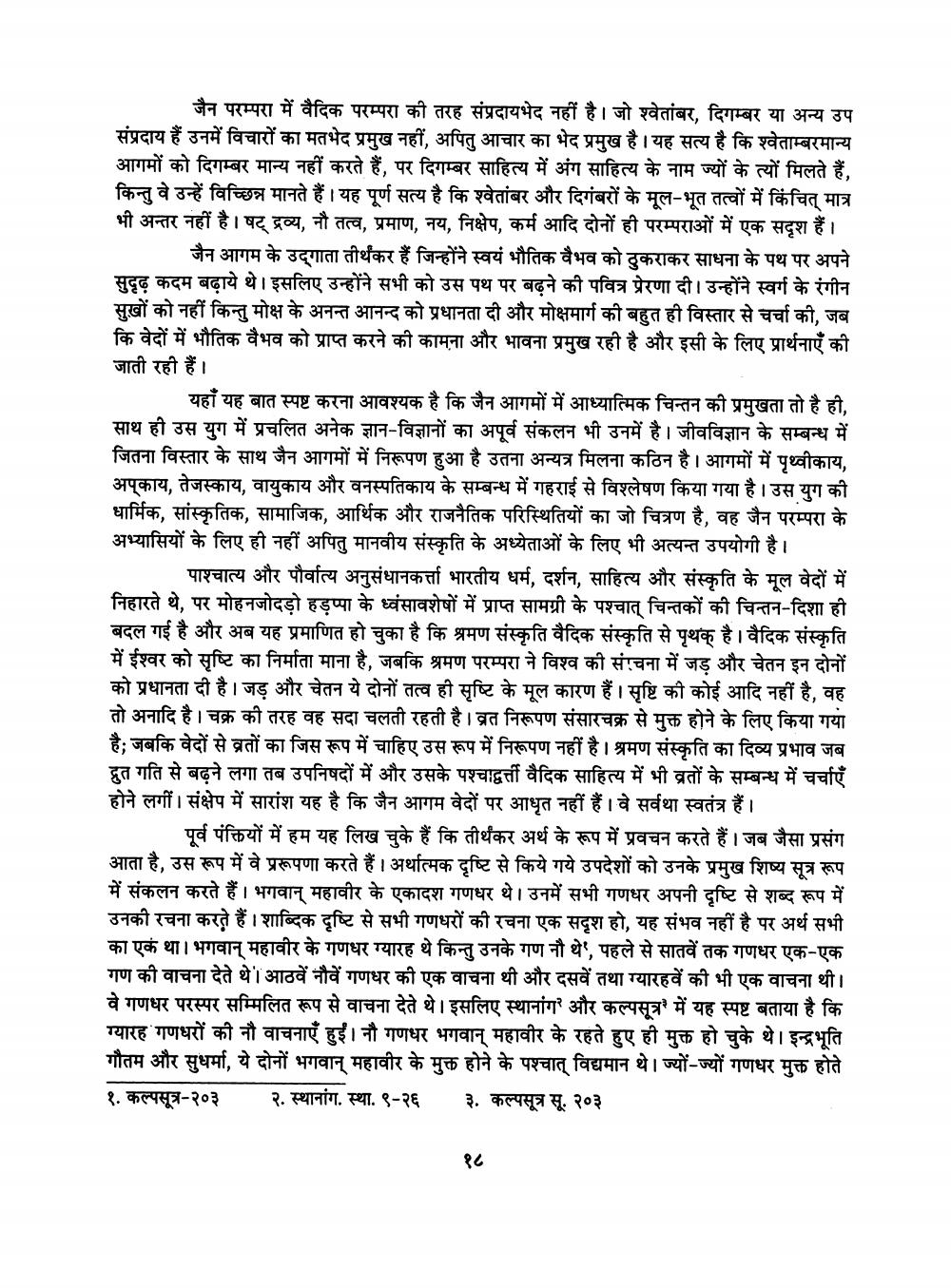________________
जैन परम्परा में वैदिक परम्परा की तरह संप्रदायभेद नहीं है। जो श्वेतांबर, दिगम्बर या अन्य उप संप्रदाय हैं उनमें विचारों का मतभेद प्रमुख नहीं, अपितु आचार का भेद प्रमुख है। यह सत्य है कि श्वेताम्बरमान्य आगमों को दिगम्बर मान्य नहीं करते हैं, पर दिगम्बर साहित्य में अंग साहित्य के नाम ज्यों के त्यों मिलते हैं, किन्तु वे उन्हें विच्छिन्न मानते हैं। यह पूर्ण सत्य है कि श्वेतांबर और दिगंबरों के मूलभूत तत्वों में किंचित् मात्र भी अन्तर नहीं है । षट् द्रव्य, नौ तत्व, प्रमाण, नय, निक्षेप, कर्म आदि दोनों ही परम्पराओं में एक सदृश हैं । जैन आगम के उद्गाता तीर्थंकर हैं जिन्होंने स्वयं भौतिक वैभव को ठुकराकर साधना के पथ पर अपने सुदृढ़ कदम बढ़ाये थे । इसलिए उन्होंने सभी को उस पथ पर बढ़ने की पवित्र प्रेरणा दी। उन्होंने स्वर्ग के रंगीन सुखों को नहीं किन्तु मोक्ष के अनन्त आनन्द को प्रधानता दी और मोक्षमार्ग की बहुत ही विस्तार से चर्चा की, जब कि वेदों में भौतिक वैभव को प्राप्त करने की कामना और भावना प्रमुख रही है और इसी के लिए प्रार्थनाएँ की जाती रही हैं।
यहाँ यह बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि जैन आगमों में आध्यात्मिक चिन्तन की प्रमुखता तो है ही, साथ ही उस युग में प्रचलित अनेक ज्ञान-विज्ञानों का अपूर्व संकलन भी उनमें है। जीवविज्ञान के सम्बन्ध में जितना विस्तार के साथ जैन आगमों में निरूपण हुआ है उतना अन्यत्र मिलना कठिन है। आगमों में पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय और वनस्पतिकाय के सम्बन्ध में गहराई से विश्लेषण किया गया है। उस युग की धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिस्थितियों का जो चित्रण है, वह जैन परम्परा के अभ्यासियों के लिए ही नहीं अपितु मानवीय संस्कृति के अध्येताओं के लिए भी अत्यन्त उपयोगी है।
पाश्चात्य और पौर्वात्य अनुसंधानकर्त्ता भारतीय धर्म, दर्शन, साहित्य और संस्कृति के मूल वेदों में निहारते थे, पर मोहनजोदड़ो हड़प्पा के ध्वंसावशेषों में प्राप्त सामग्री के पश्चात् चिन्तकों की चिन्तन-दिशा ही बदल गई है और अब यह प्रमाणित हो चुका है कि श्रमण संस्कृति वैदिक संस्कृति से पृथक् है। वैदिक संस्कृति में ईश्वर को सृष्टि का निर्माता माना है, जबकि श्रमण परम्परा ने विश्व की संरचना में जड़ और चेतन इन दोनों
प्रधानता दी है। जड़ और चेतन ये दोनों तत्व ही सृष्टि के मूल कारण हैं। सृष्टि की कोई आदि नहीं है, वह तो अनादि है । चक्र की तरह वह सदा चलती रहती है। व्रत निरूपण संसारचक्र से मुक्त होने के लिए किया गया है; जबकि वेदों से व्रतों का जिस रूप में चाहिए उस रूप में निरूपण नहीं है। श्रमण संस्कृति का दिव्य प्रभाव जब द्रुत गति से बढ़ने लगा तब उपनिषदों में और उसके पश्चाद्वर्त्ती वैदिक साहित्य में भी व्रतों के सम्बन्ध में चर्चाएँ होने लगीं। संक्षेप में सारांश यह है कि जैन आगम वेदों पर आधृत नहीं हैं। वे सर्वथा स्वतंत्र हैं ।
पूर्व पंक्तियों में हम यह लिख चुके हैं कि तीर्थंकर अर्थ के रूप में प्रवचन करते हैं। जब जैसा प्रसंग आता है, उस रूप में वे प्ररूपणा करते हैं । अर्थात्मक दृष्टि से किये गये उपदेशों को उनके प्रमुख शिष्य सूत्र रूप में संकलन करते हैं । भगवान् महावीर के एकादश गणधर थे। उनमें सभी गणधर अपनी दृष्टि से शब्द रूप में उनकी रचना करते हैं। शाब्दिक दृष्टि से सभी गणधरों की रचना एक सदृश हो, यह संभव नहीं है पर अर्थ सभी का एक था। भगवान् महावीर के गणधर ग्यारह थे किन्तु उनके गण नौ थे, पहले से सातवें तक गणधर एक-एक गण की वाचना देते थे। आठवें नौवें गणधर की एक वाचना थी और दसवें तथा ग्यारहवें की भी एक वाचना थी । वे गणधर परस्पर सम्मिलित रूप से वाचना देते थे । इसलिए स्थानांग और कल्पसूत्र में यह स्पष्ट बताया है कि ग्यारह गणधरों की नौ वाचनाएँ हुईं। नौ गणधर भगवान् महावीर के रहते हुए ही मुक्त हो चुके थे । इन्द्रभूति गौतम और सुधर्मा, ये दोनों भगवान् महावीर के मुक्त होने के पश्चात् विद्यमान थे। ज्यों-ज्यों गणधर मुक्त होते
१. कल्पसूत्र - २०३
२. स्थानांग. स्था. ९-२६
३. कल्पसूत्र सू. २०३
१८