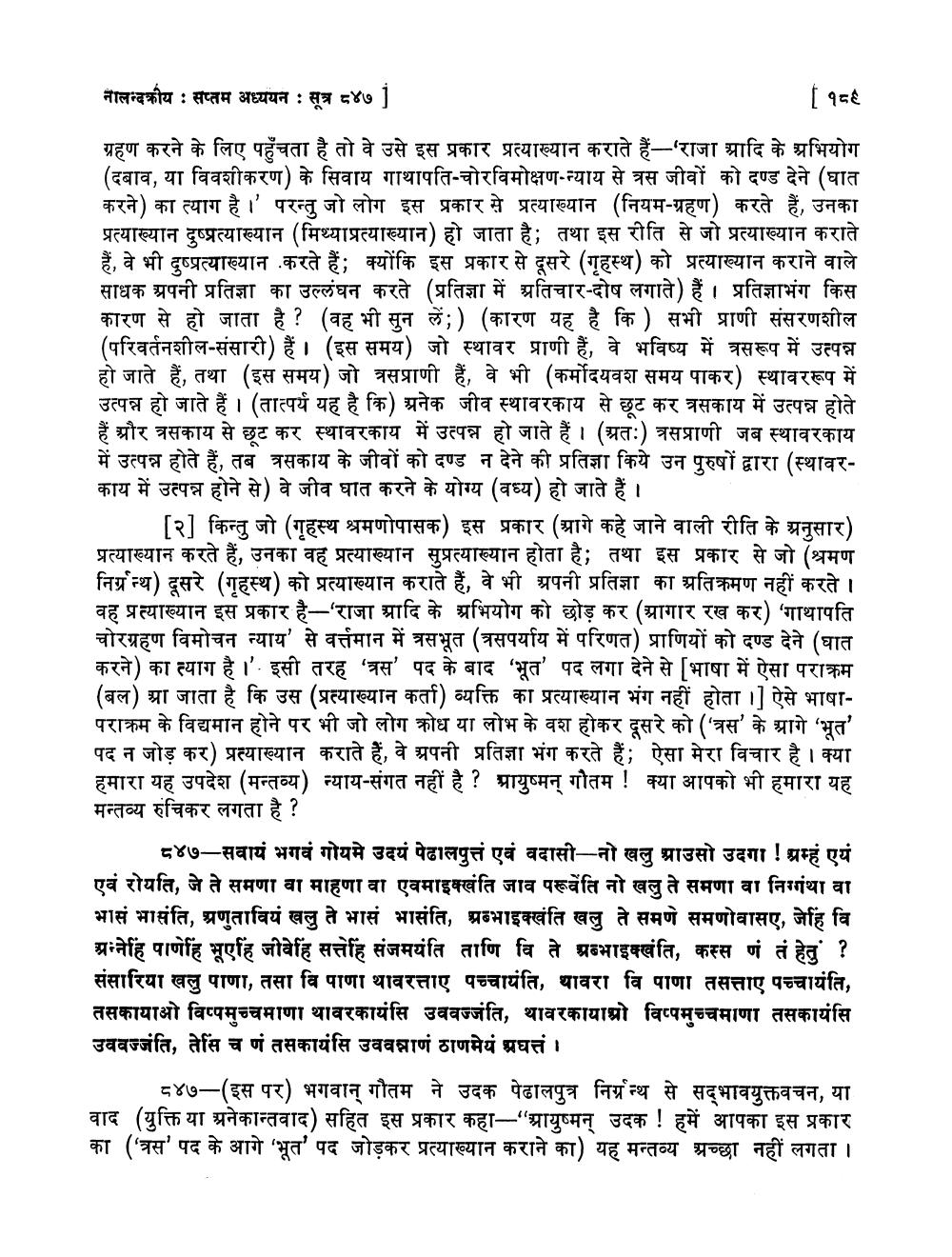________________
नान्दीय : सप्तम अध्ययन सूत्र ८४७ ]
[ १८
ग्रहण करने के लिए पहुँचता है तो वे उसे इस प्रकार प्रत्याख्यान कराते हैं- 'राजा आदि के अभियोग ( दबाव, या विवशीकरण) के सिवाय गाथापति - चोरविमोक्षण - न्याय से त्रस जीवों को दण्ड देने (घात करने) का त्याग है ।' परन्तु जो लोग इस प्रकार से प्रत्याख्यान (नियम- ग्रहण) करते हैं, उनका प्रत्याख्यान दुष्प्रत्याख्यान ( मिथ्याप्रत्याख्यान ) हो जाता है; तथा इस रीति से जो प्रत्याख्यान कराते हैं, वे भी दुष्प्रत्याख्यान करते हैं; क्योंकि इस प्रकार से दूसरे (गृहस्थ ) को प्रत्याख्यान कराने वाले साधक अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन करते ( प्रतिज्ञा में प्रतिचार - दोष लगाते ) हैं । प्रतिज्ञाभंग किस कारण से हो जाता है ? ( वह भी सुन लें ; ) ( कारण यह है कि ) सभी प्राणी संसरणशील (परिवर्तनशील - संसारी ) हैं । ( इस समय ) जो स्थावर प्राणी हैं, वे भविष्य में त्रसरूप में उत्पन्न हो जाते हैं, तथा ( इस समय ) जो त्रसप्राणी हैं, वे भी ( कर्मोदयवश समय पाकर ) स्थावररूप में उत्पन्न हो जाते हैं । (तात्पर्य यह है कि ) अनेक जीव स्थावरकाय से छूट कर त्रसकाय में उत्पन्न होते हैं और काय से छूट कर स्थावरकाय में उत्पन्न हो जाते हैं । ( अतः ) त्रसप्राणी जब स्थावर काय में उत्पन्न होते हैं, तब त्रसकाय के जीवों को दण्ड न देने की प्रतिज्ञा किये उन पुरुषों द्वारा (स्थावरकाय में उत्पन्न होने से) वे जीव घात करने के योग्य ( वध्य) हो जाते हैं ।
[२] किन्तु जो ( गृहस्थ श्रमणोपासक ) इस प्रकार ( आगे कहे जाने वाली रीति के अनुसार ) प्रत्याख्यान करते हैं, उनका वह प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान होता है; तथा इस प्रकार से जो ( श्रमण निर्ग्रन्थ) दूसरे (गृहस्थ ) को प्रत्याख्यान कराते हैं, वे भी अपनी प्रतिज्ञा का प्रतिक्रमण नहीं करते । वह प्रत्याख्यान इस प्रकार है - 'राजा आदि के अभियोग को छोड़ कर (आगार रख कर ) 'गाथापति चोरग्रहण विमोचन न्याय' से वर्त्तमान में सभूत ( सपर्याय में परिणत ) प्राणियों को दण्ड देने (घात करने) का त्याग है ।' इसी तरह ' त्रस' पद के बाद 'भूत' पद लगा देने से [ भाषा में ऐसा पराक्रम (बल) आ जाता है कि उस ( प्रत्याख्यान कर्ता ) व्यक्ति का प्रत्याख्यान भंग नहीं होता ।] ऐसे भाषापराक्रम के विद्यमान होने पर भी जो लोग क्रोध या लोभ के वश होकर दूसरे को ('स' के आगे 'भूत' पद न जोड़ कर ) प्रत्याख्यान कराते हैं, वे अपनी प्रतिज्ञा भंग करते हैं; ऐसा मेरा विचार है । क्या हमारा यह उपदेश (मन्तव्य ) न्याय संगत नहीं है ? श्रायुष्मन् गौतम ! क्या आपको भी हमारा यह मन्तव्य रुचिकर लगता है ?
८४७ - स्वायं भगवं गोयमे उदयं पेढालपुत्तं एवं वदासी - नो खलु श्राउसो उदगा ! श्रम्हं एवं एवं रोयति, जे ते समणा वा माहणा वा एवमाइक्खंति जाव परूवेंति नो खलु ते समणा वा निग्गंथा वा भासं भासंति, श्रणुतावियं खलु ते भासं भासंति, प्रब्भाइक्खति खलु ते समणे समणोवासए, जेहिं वि पाहि भूहि जीवहि सत्तेह संजमयंति ताणि वि ते प्रब्भाइक्खति, कस्स णं तं हेतु ? संसारिया खलु पाणा, तसा वि पाणा थावरत्ताए पच्चायंति, थावरा वि पाणा तसत्ताए पच्चायंति, तसकायाओ विष्पमुच्चमाणा थावरकायंसि उववज्जंति, थावरकायाश्रो विप्पमुच्चमाणा तसकायंसि उववज्जंति, तेसि च णं तसकायंसि उववन्नाणं ठाणमेयं श्रघत्तं ।
८४७ - ( इस पर ) भगवान् गौतम ने उदक पेढालपुत्र निर्ग्रन्थ से सद्भावयुक्तवचन, या वाद (युक्ति या अनेकान्तवाद) सहित इस प्रकार कहा - "आयुष्मन् उदक ! हमें आपका इस प्रकार का ('स' पद के आगे 'भूत' पद जोड़कर प्रत्याख्यान कराने का ) यह मन्तव्य अच्छा नहीं लगता ।