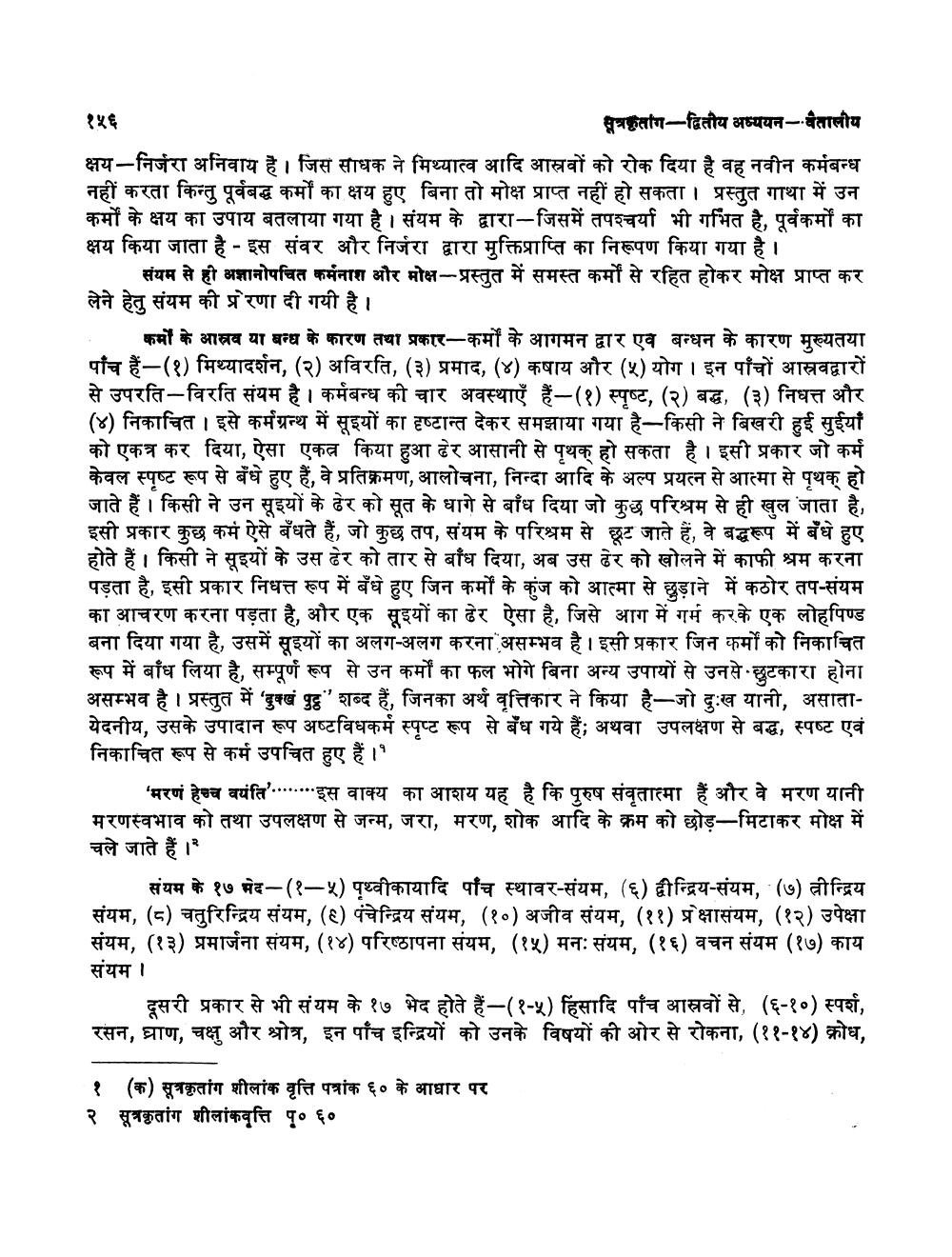________________
१५६
सूत्रकृतांग-द्वितीय अध्ययन-वैतालीय क्षय-निर्जरा अनिवाय है। जिस साधक ने मिथ्यात्व आदि आस्रवों को रोक दिया है वह नवीन कर्मबन्ध नहीं करता किन्तु पूर्वबद्ध कर्मों का क्षय हुए बिना तो मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। प्रस्तुत गाथा में उन
अय का उपाय बतलाया गया है। संयम के द्वारा-जिसमें तपश्चर्या भी गभित है. पूर्वकर्मों का क्षय किया जाता है - इस संवर और निर्जरा द्वारा मूक्तिप्राप्ति का निरूपण किया गया है।
संयम से ही अज्ञानोपचित कर्मनाश और मोक्ष-प्रस्तुत में समस्त कर्मों से रहित होकर मोक्ष प्राप्त कर लेने हेतु संयम की प्रेरणा दी गयी है।
कर्मों के आस्रव या बन्ध के कारण तथा प्रकार-कर्मों के आगमन द्वार एव बन्धन के कारण मूख्यतया पांच हैं-(१) मिथ्यादर्शन, (२) अविरति, (३) प्रमाद, (४) कषाय और (५) योग । इन पांचों आस्रवद्वारों से उपरति-विरति संयम है। कर्मबन्ध की चार अवस्थाएँ हैं-(१) स्पृष्ट, (२) बद्ध, (३) निधत्त और (४) निकाचित । इसे कर्मग्रन्थ में सूइयों का दृष्टान्त देकर समझाया गया है-किसी ने बिखरी हुई सुईयां को एकत्र कर दिया, ऐसा एकत्र किया हुआ ढेर आसानी से पथक हो सकता है। इसी प्रकार जो कर्म केवल स्पृष्ट रूप से बँधे हुए हैं, वे प्रतिक्रमण, आलोचना, निन्दा आदि के अल्प प्रयत्न से आत्मा से पृथक् हो जाते हैं। किसी ने उन सूइयों के ढेर को सूत के धागे से बाँध दिया जो कुछ परिश्रम से ही खुल जाता है, इसी प्रकार कुछ कर्म ऐसे बँधते हैं, जो कुछ तप, संयम के परिश्रम से छूट जाते हैं, वे बद्धरूप में बंधे हुए होते हैं। किसी ने सूइयों के उस ढेर को तार से बाँध दिया, अब उस ढेर को खोलने में काफी श्रम करना पड़ता है, इसी प्रकार निधत्त रूप में बँधे हुए जिन कर्मों के कुंज को आत्मा से छुड़ाने में कठोर तप-संयम का आचरण करना पड़ता है, और एक सूइयों का ढेर ऐसा है, जिसे आग में गर्म करके एक लोहपिण्ड बना दिया गया है, उसमें सूइयों का अलग-अलग करना असम्भव है। इसी प्रकार जिन कर्मों को निकाचित रूप में बाँध लिया है, सम्पूर्ण रूप से उन कर्मों का फल भोगे बिना अन्य उपायों से उनसे छुटकारा होना असम्भव है। प्रस्तुत में 'दुक्खं पुट्ट' शब्द हैं, जिनका अर्थ वृत्तिकार ने किया है जो दुःख यानी, असातायेदनीय, उसके उपादान रूप अष्टविधकर्म स्पृष्ट रूप से बँध गये हैं; अथवा उपलक्षण से बद्ध, स्पष्ट एवं निकाचित रूप से कर्म उपचित हुए हैं।'
'मरणं हेच्च वयंति'....."इस वाक्य का आशय यह है कि पुरुष संवृतात्मा हैं और वे मरण यानी मरणस्वभाव को तथा उपलक्षण से जन्म, जरा, मरण, शोक आदि के क्रम को छोड़-मिटाकर मोक्ष में चले जाते हैं।
संयम के १७ भेद-(१-५) पृथ्वीकायादि पांच स्थावर-संयम, (६) द्वीन्द्रिय-संयम, (७) त्रीन्द्रिय संयम, (८) चतुरिन्द्रिय संयम, (6) पंचेन्द्रिय संयम, (१०) अजीव संयम, (११) प्रक्षासंयम, (१२) उपेक्षा संयम, (१३) प्रमार्जना संयम, (१४) परिष्ठापना संयम, (१५) मनः संयम, (१६) वचन संयम (१७) काय संयम ।
दूसरी प्रकार से भी संयम के १७ भेद होते हैं-(१-५) हिंसादि पाँच आस्रवों से, (६-१०) स्पर्श, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, इन पाँच इन्द्रियों को उनके विषयों की ओर से रोकना, (११-१४) क्रोध,
१ (क) सूत्रकृतांग शीलांक वृत्ति पत्रांक ६० के आधार पर २ सूत्रकृतांग शीलांकवृत्ति पु० ६०