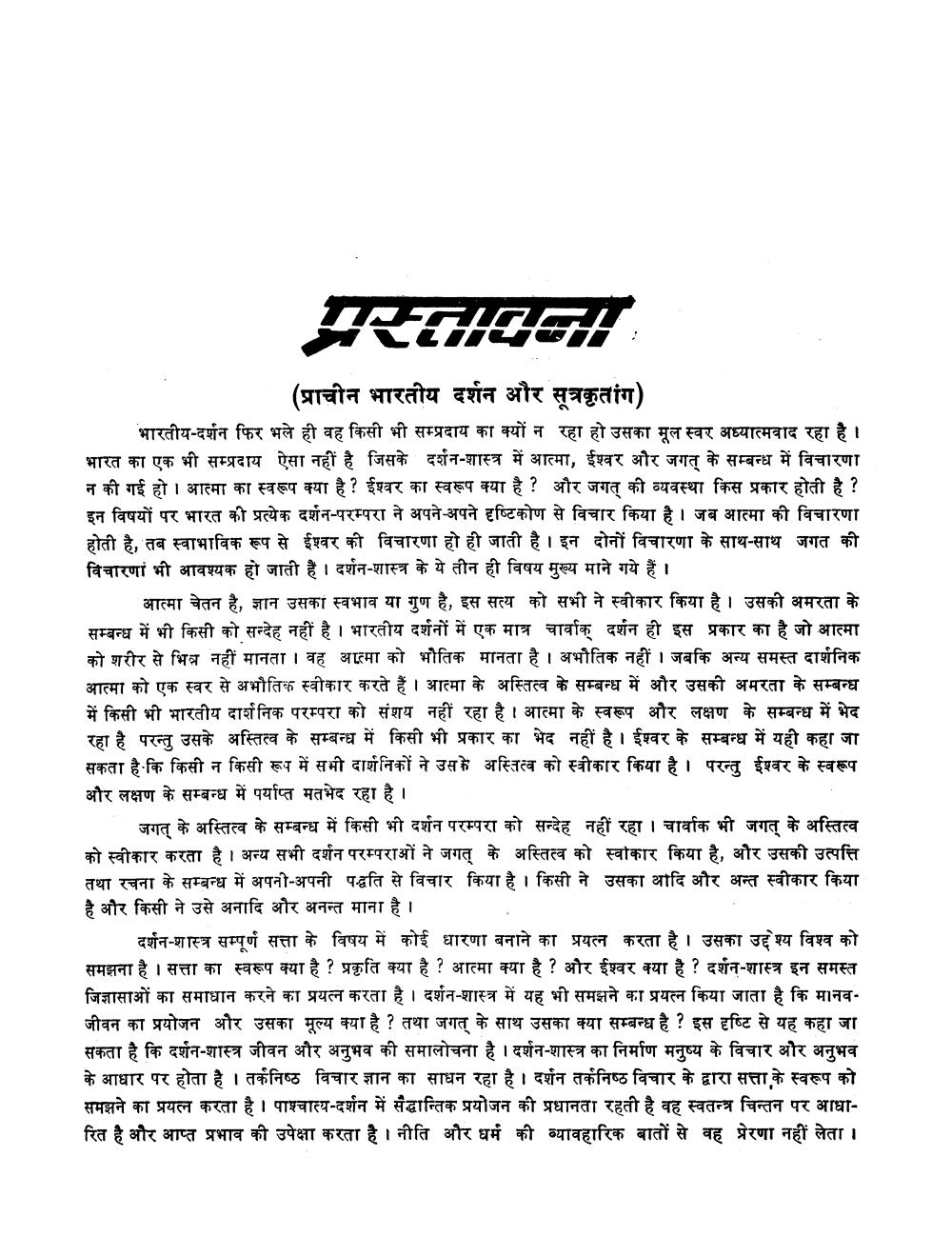________________
प्रस्तावना
(प्राचीन भारतीय दर्शन और सूत्रकृतांग) भारतीय-दर्शन फिर भले ही वह किसी भी सम्प्रदाय का क्यों न रहा हो उसका मूल स्वर अध्यात्मवाद रहा है। भारत का एक भी सम्प्रदाय ऐसा नहीं है जिसके दर्शन-शास्त्र में आत्मा, ईश्वर और जगत के सम्बन्ध में विचारणा न की गई हो । आत्मा का स्वरूप क्या है ? ईश्वर का स्वरूप क्या है ? और जगत् की व्यवस्था किस प्रकार होती है ? इन विषयों पर भारत की प्रत्येक दर्शन-परम्परा ने अपने-अपने दृष्टिकोण से विचार किया है। जब आत्मा की विचारणा होती है, तब स्वाभाविक रूप से ईश्वर की विचारणा हो ही जाती है। इन दोनों विचारणा के साथ-साथ जगत की विचारणां भी आवश्यक हो जाती हैं । दर्शन-शास्त्र के ये तीन ही विषय मुख्य माने गये हैं।
आत्मा चेतन है, ज्ञान उसका स्वभाव या गुण है, इस सत्य को सभी ने स्वीकार किया है। उसकी अमरता के सम्बन्ध में भी किसी को सन्देह नहीं है। भारतीय दर्शनों में एक मात्र चार्वाक दर्शन ही इस प्रकार का है जो आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं मानता । वह आत्मा को भौतिक मानता है । अभौतिक नहीं । जबकि अन्य समस्त दार्शनिक आत्मा को एक स्वर से अभौतिक स्वीकार करते हैं । आत्मा के अस्तित्व के सम्बन्ध में और उसकी अमरता के सम्बन्ध में किसी भी भारतीय दार्शनिक परम्परा को संशय नहीं रहा है । आत्मा के स्वरूप और लक्षण के सम्बन्ध में भेद रहा है परन्तु उसके अस्तित्व के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। ईश्वर के सम्बन्ध में यही कहा जा सकता है कि किसी न किसी रूप में सभी दार्शनिकों ने उसके अस्तित्व को स्वीकार किया है। परन्तु ईश्वर के स्वरूप और लक्षण के सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद रहा है।
__ जगत के अस्तित्व के सम्बन्ध में किसी भी दर्शन परम्परा को सन्देह नहीं रहा । चार्वाक भी जगत् के अस्तित्व को स्वीकार करता है। अन्य सभी दर्शन परम्पराओं ने जगत् के अस्तित्व को स्वीकार किया है, और उसकी उत्पत्ति तथा रचना के सम्बन्ध में अपनी-अपनी पद्धति से विचार किया है। किसी ने उसका आदि और अन्त स्वीकार किया है और किसी ने उसे अनादि और अनन्त माना है।
दर्शन-शास्त्र सम्पूर्ण सत्ता के विषय में कोई धारणा बनाने का प्रयत्न करता है। उसका उद्देश्य विश्व को समझना है । सत्ता का स्वरूप क्या है ? प्रकृति क्या है ? आत्मा क्या है ? और ईश्वर क्या है ? दर्शन-शास्त्र इन समस्त जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयत्न करता है । दर्शन-शास्त्र में यह भी समझने का प्रयत्न किया जाता है कि मानवजीवन का प्रयोजन और उसका मूल्य क्या है ? तथा जगत् के साथ उसका क्या सम्बन्ध है ? इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि दर्शन-शास्त्र जीवन और अनुभव की समालोचना है । दर्शन-शास्त्र का निर्माण मनुष्य के विचार और अनुभव के आधार पर होता है । तर्कनिष्ठ विचार ज्ञान का साधन रहा है । दर्शन तर्कनिष्ठ विचार के द्वारा सत्ता के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करता है। पाश्चात्य-दर्शन में सैद्धान्तिक प्रयोजन की प्रधानता रहती है वह स्वतन्त्र चिन्तन पर आधारित है और आप्त प्रभाव की उपेक्षा करता है। नीति और धर्म की व्यावहारिक बातों से वह प्रेरणा नहीं लेता।