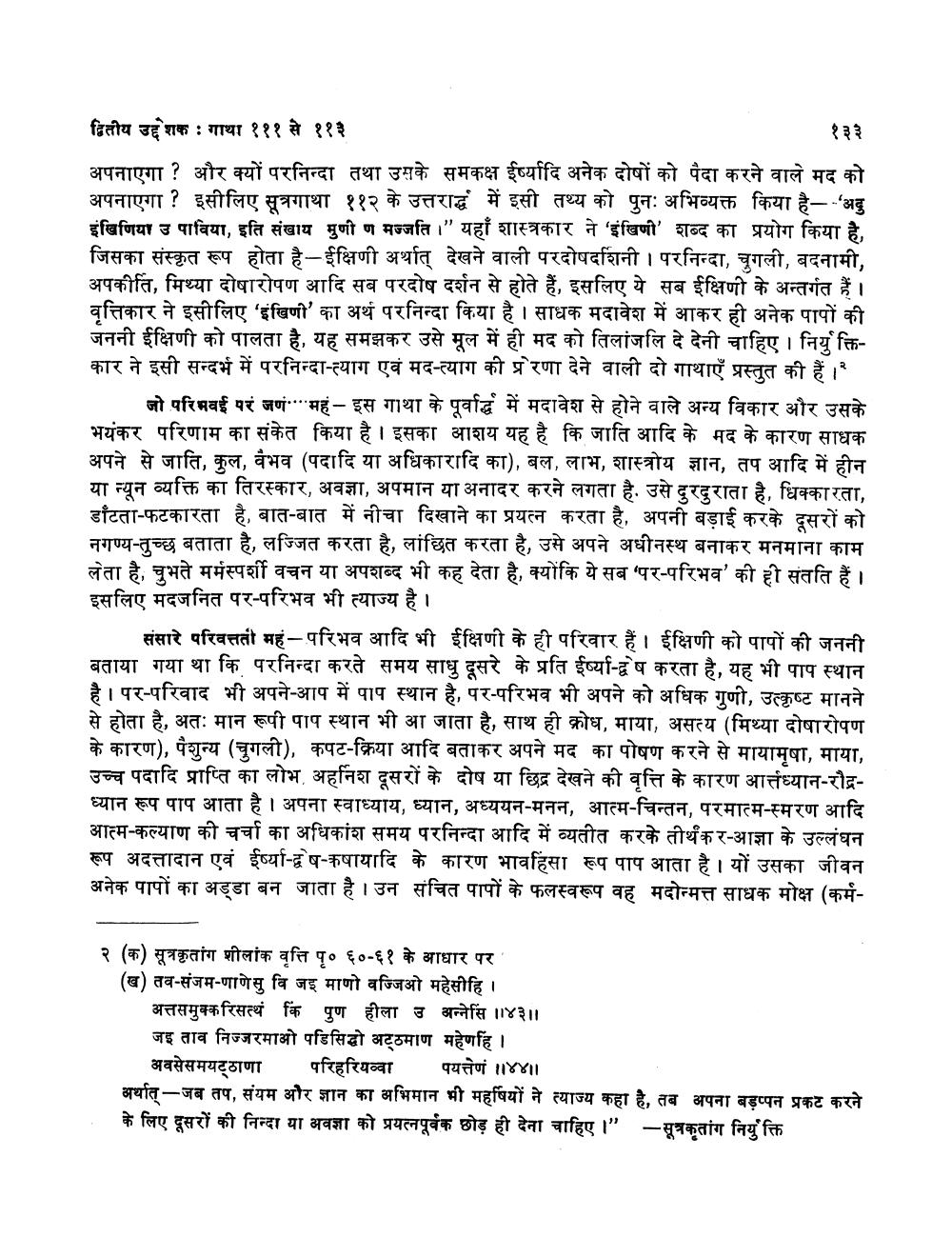________________
द्वितीय उद्देशक : गाथा १११ से ११३ अपनाएगा? और क्यों परनिन्दा तथा उसके समकक्ष ईर्ष्यादि अनेक दोषों को पैदा करने वाले मद को अपनाएगा? इसीलिए सूत्रगाथा ११२ के उत्तरार्द्ध में इसी तथ्य को पुनः अभिव्यक्त किया है- 'अदु इंखिणिया उ पाविया, इति संखाय मुणी ण मज्जति ।" यहाँ शास्त्रकार ने 'इंखिणी' शब्द का प्रयोग किया है. जिसका संस्कृत रूप होता है-ईक्षिणी अर्थात् देखने वाली परदोषदर्शिनी । परनिन्दा, चुगली, बदनामी, अपकीर्ति, मिथ्या दोषारोपण आदि सब परदोष दर्शन से होते हैं, इसलिए ये सब ईक्षिणी के अन्तर्गत हैं। वत्तिकार ने इसीलिए 'इंखिणी' का अर्थ परनिन्दा किया है। साधक मदावेश में आकर ही अनेक पापों की जननी ईक्षिणी को पालता है, यह समझकर उसे मूल में ही मद को तिलांजलि दे देनी चाहिए। नियुक्तिकार ने इसी सन्दर्भ में परनिन्दा-त्याग एवं मद-त्याग की प्रेरणा देने वाली दो गाथाएँ प्रस्तुत की हैं।
जो परिमवई परं जणं महं- इस गाथा के पूर्वार्द्ध में मदावेश से होने वाले अन्य विकार और उसके भयंकर परिणाम का संकेत किया है । इसका आशय यह है कि जाति आदि के मद के कारण साधक अपने से जाति, कल, वैभव (पदादि या अधिकारादि का), बल, लाभ, शास्त्रीय ज्ञान, तप आदि में हीन या न्यून व्यक्ति का तिरस्कार, अवज्ञा, अपमान या अनादर करने लगता है. उसे दुरदुराता है, धिक्कारता, डाँटता-फटकारता है, बात-बात में नीचा दिखाने का प्रयत्न करता है, अपनी बड़ाई करके दूसरों को नगण्य-तुच्छ बताता है, लज्जित करता है, लांछित करता है, उसे अपने अधीनस्थ बनाकर मनमाना काम लेता है, चुभते मर्मस्पर्शी वचन या अपशब्द भी कह देता है, क्योंकि ये सब 'पर-परिभव' की ही संतति हैं। इसलिए मदजनित पर-परिभव भी त्याज्य है।
___ संसारे परिवत्तती महं-परिभव आदि भी ईक्षिणी के ही परिवार हैं। ईक्षिणी को पापों की जननी बताया गया था कि परनिन्दा करते समय साधु दूसरे के प्रति ईर्ष्या-द्वेष करता है, यह भी पाप स्थान
परिवाद भी अपने-आप में पाप स्थान है, पर-परिभव भी अपने को अधिक गूणी, उत्कृष्ट मानने से होता है, अतः मान रूपी पाप स्थान भी आ जाता है, साथ ही क्रोध, माया, असत्य (मिथ्या दोषारोपण के कारण), पैशुन्य (चुगली), कपट-क्रिया आदि बताकर अपने मद का पोषण करने से मायामृषा, माया, उच्च पदादि प्राप्ति का लोभ अहर्निश दूसरों के दोष या छिद्र देखने की वृत्ति के कारण आर्तध्यान-रौद्रध्यान रूप पाप आता है। अपना स्वाध्याय, ध्यान, अध्ययन-मनन, आत्म-चिन्तन, परमात्म-स्मरण आदि आत्म-कल्याण की चर्चा का अधिकांश समय परनिन्दा आदि में व्यतीत करके तीर्थंकर-आज्ञा के उल्लंघन रूप अदत्तादान एवं ईर्ष्या-द्वेष-कषायादि के कारण भावहिंसा रूप पाप आता है। यों उसका जीवन अनेक पापों का अड्डा बन जाता है। उन संचित पापों के फलस्वरूप वह मदोन्मत्त साधक मोक्ष (कर्म
२ (क) सूत्रकृतांग शीलांक वृत्ति पृ०६०-६१ के आधार पर (ख) तव-संजम-णाणेसु वि जइ माणो वज्जिओ महेसीहि ।
अत्तसमुक्क रिसत्थं कि पुण हीला उ अन्नेसि ॥४३॥ जइ ताव निज्जरमाओ पडिसिद्धो अट्ठमाण महेणहि ।
अवसेसमयट्ठाणा परिहरियव्वा पयत्तेणं ॥४४॥ अर्थात्-जब तप, संयम और ज्ञान का अभिमान भी महर्षियों ने त्याज्य कहा है, तब अपना बड़प्पन प्रकट करने के लिए दूसरों की निन्दा या अवज्ञा को प्रयत्नपूर्वक छोड़ ही देना चाहिए।" -सूत्रकृतांग नियुक्ति