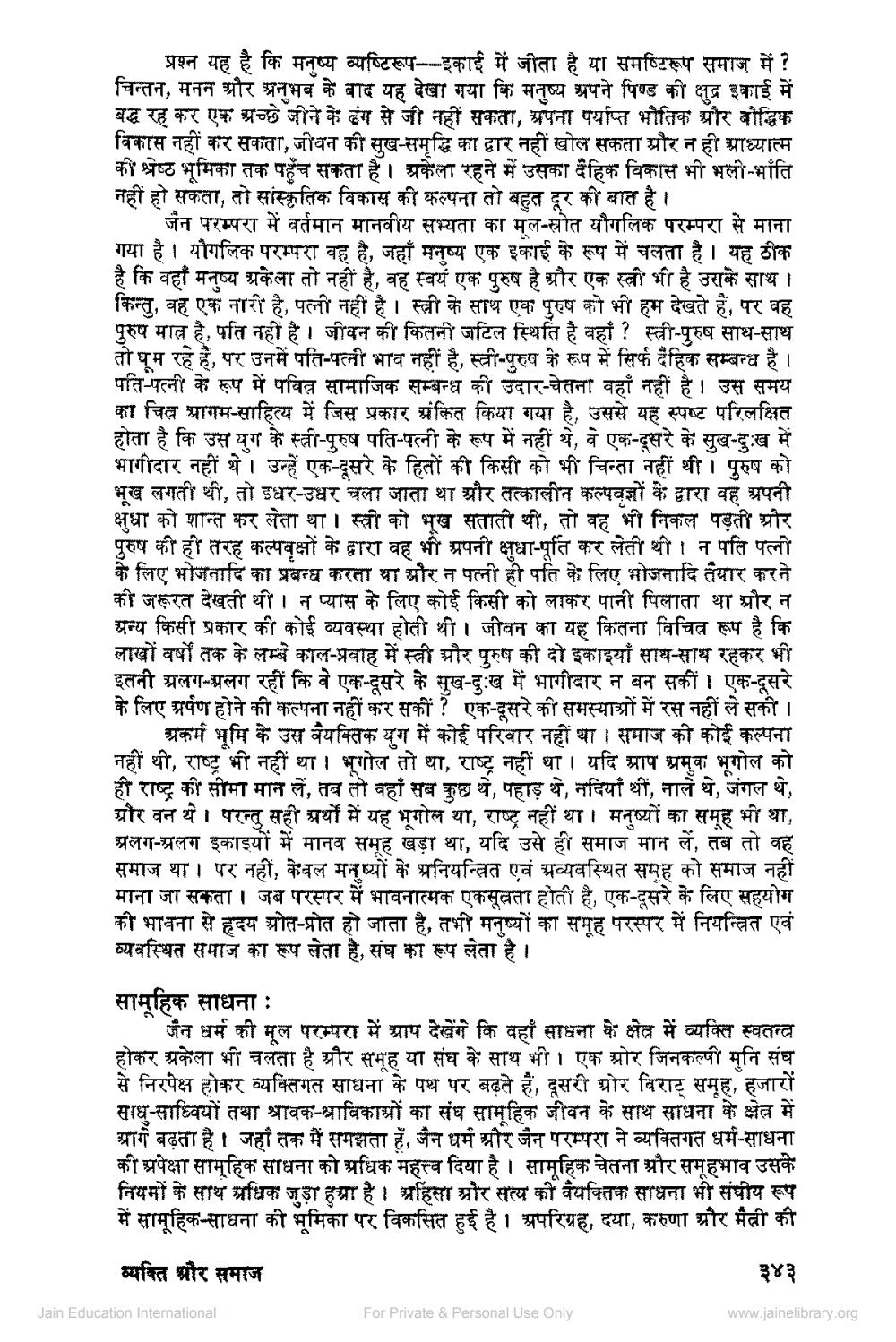________________
प्रश्न यह है कि मनुष्य व्यष्टिरूप-इकाई में जीता है या समष्टिरूप समाज में ? चिन्तन, मनन और अनुभव के बाद यह देखा गया कि मनुष्य अपने पिण्ड की क्षुद्र इकाई में बद्ध रह कर एक अच्छे जीने के ढंग से जी नहीं सकता, अपना पर्याप्त भौतिक और बौद्धिक विकास नहीं कर सकता, जीवन की सुख-समृद्धि का द्वार नहीं खोल सकता और न ही आध्यात्म की श्रेष्ठ भूमिका तक पहुँच सकता है। अकेला रहने में उसका दैहिक विकास भी भली-भाँति नहीं हो सकता, तो सांस्कृतिक विकास की कल्पना तो बहुत दूर की बात है।
जैन परम्परा में वर्तमान मानवीय सभ्यता का मल-स्रोत यौगलिक परम्परा से माना गया है। यौगलिक परम्परा वह है, जहाँ मनुष्य एक इकाई के रूप में चलता है । यह ठीक है कि वहाँ मनुष्य अकेला तो नहीं है, वह स्वयं एक पुरुष है और एक स्त्री भी है उसके साथ । किन्तु, वह एक नारी है, पत्नी नहीं है। स्त्री के साथ एक पुरुष को भी हम देखते हैं, पर वह पुरुष मात्र है, पति नहीं है। जीवन की कितनी जटिल स्थिति है वहाँ ? स्त्री-पुरुष साथ-साथ तो घूम रहे हैं, पर उनमें पति-पत्नी भाव नहीं है, स्त्री-पुरुष के रूप में सिर्फ दैहिक सम्बन्ध है। पति-पत्नी के रूप में पवित्र सामाजिक सम्बन्ध की उदार-चेतना वहाँ नहीं है। उस समय का चित्र आगम-साहित्य में जिस प्रकार अंकित किया गया है, उससे यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि उस युग के स्त्री-पुरुष पति-पत्नी के रूप में नहीं थे, वे एक-दूसरे के सुख-दुःख में भागीदार नहीं थे। उन्हें एक-दूसरे के हितों की किसी को भी चिन्ता नहीं थी। पूरुष को भूख लगती थी, तो इधर-उधर चला जाता था और तत्कालीन कल्पवज्ञों के द्वारा वह अपनी क्षुधा को शान्त कर लेता था। स्त्री को भूख सताती थी, तो वह भी निकल पड़ती और पुरुष की ही तरह कल्पवृक्षों के द्वारा वह भी अपनी क्षुधा-पूर्ति कर लेती थी। न पति पत्नी के लिए भोजनादि का प्रबन्ध करता था और न पत्नी ही पति के लिए भोजनादि तैयार करने की जरूरत देखती थी। न प्यास के लिए कोई किसी को लाकर पानी पिलाता था और न अन्य किसी प्रकार की कोई व्यवस्था होती थी। जीवन का यह कितना विचित्र रूप है कि लाखों वर्षों तक के लम्बे काल-प्रवाह में स्त्री और पुरुष की दो इकाइयाँ साथ-साथ रहकर भी इतनी अलग-अलग रहीं कि वे एक-दूसरे के सुख-दुःख में भागीदार न बन सकीं। एक-दूसरे के लिए अर्पण होने की कल्पना नहीं कर सकीं? एक-दूसरे की समस्याओं में रस नहीं ले सकी।
अकर्म भूमि के उस वैयक्तिक युग में कोई परिवार नहीं था। समाज की कोई कल्पना नहीं थी, राष्ट्र भी नहीं था। भूगोल तो था, राष्ट्र नहीं था। यदि आप अमुक भूगोल को ही राष्ट्र की सीमा मान लें, तब तो वहाँ सब कुछ थे, पहाड़ थे, नदियाँ थीं, नाले थे, जंगल थे, और वन थे। परन्तु सही अर्थों में यह भूगोल था, राष्ट्र नहीं था। मनुष्यों का समूह भी था, अलग-अलग इकाइयों में मानव समूह खड़ा था, यदि उसे ही समाज मान लें, तब तो वह समाज था। पर नहीं, केवल मनुष्यों के अनियन्त्रित एवं अव्यवस्थित समूह को समाज नहीं माना जा सकता। जब परस्पर में भावनात्मक एकसूत्रता होती है, एक-दूसरे के लिए सहयोग की भावना से हृदय प्रोत-प्रोत हो जाता है, तभी मनुष्यों का समूह परस्पर में नियन्त्रित एवं व्यवस्थित समाज का रूप लेता है, संघ का रूप लेता है।
सामूहिक साधना :
"जैन धर्म की मूल परम्परा में आप देखेंगे कि वहाँ साधना के क्षेत्र में व्यक्ति स्वतन्त्र होकर अकेला भी चलता है और समूह या संघ के साथ भी। एक ओर जिनकल्पी मुनि संघ से निरपेक्ष होकर व्यक्तिगत साधना के पथ पर बढ़ते हैं, दूसरी ओर विराट् समूह, हजारों साधु-साध्वियों तथा श्रावक-श्राविकाओं का संघ सामुहिक जीवन के साथ साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जैन धर्म और जैन परम्परा ने व्यक्तिगत धर्म-साधना की अपेक्षा सामूहिक साधना को अधिक महत्त्व दिया है। सामूहिक चेतना और समूहभाव उसके नियमों के साथ अधिक जुड़ा हुआ है। अहिंसा और सत्य की वैयक्तिक साधना भी संघीय रूप में सामूहिक-साधना की भूमिका पर विकसित हुई है । अपरिग्रह, दया, करुणा और मैत्री की
व्यक्ति और समाज
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org