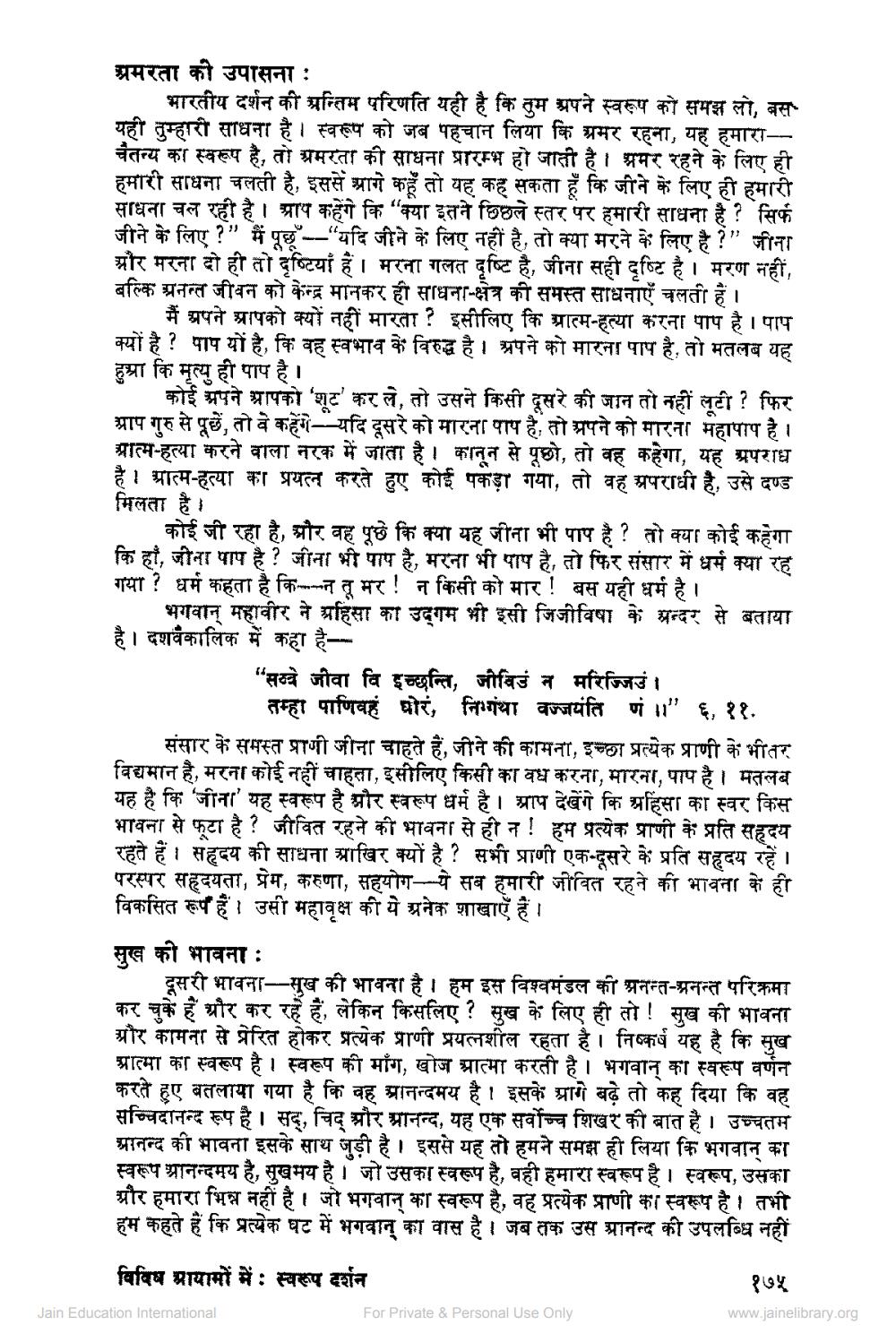________________
अमरता की उपासना : ___ भारतीय दर्शन की अन्तिम परिणति यही है कि तुम अपने स्वरूप को समझ लो, बसयही तुम्हारी साधना है। स्वरूप को जब पहचान लिया कि अमर रहना, यह हमाराचैतन्य का स्वरूप है, तो अमरता की साधना प्रारम्भ हो जाती है। अमर रहने के लिए ही हमारी साधना चलती है, इससे आगे कहूँ तो यह कह सकता हूँ कि जीने के लिए ही हमारी साधना चल रही है। आप कहेंगे कि “क्या इतने छिछले स्तर पर हमारी साधना है ? सिर्फ जीने के लिए ?" मैं पूछ-"यदि जीने के लिए नहीं है, तो क्या मरने के लिए है ?" जीना
और मरना दो ही तो दृष्टियां हैं। मरना गलत दृष्टि है, जीना सही दृष्टि है । मरण नहीं, बल्कि अनन्त जीवन को केन्द्र मानकर ही साधना-क्षेत्र की समस्त साधनाएँ चलती है। ____ मैं अपने आपको क्यों नहीं मारता? इसीलिए कि प्रात्म-हत्या करना पाप है । पाप क्यों है ? पाप यों है, कि वह स्वभाव के विरुद्ध है। अपने को मारना पाप है, तो मतलब यह हुअा कि मृत्यु ही पाप है। * कोई अपने आपको 'शूट' कर ले, तो उसने किसी दूसरे की जान तो नहीं लूटी? फिर आप गुरु से पूछे, तो वे कहेंगे- यदि दूसरे को मारना पाप है, तो अपने को मारना महापाप है । आत्म-हत्या करने वाला नरक में जाता है। कानून से पूछो, तो वह कहेगा, यह अपराध है। आत्म-हत्या का प्रयत्न करते हुए कोई पकड़ा गया, तो वह अपराधी है, उसे दण्ड मिलता है।
कोई जी रहा है, और वह पूछे कि क्या यह जीना भी पाप है ? तो क्या कोई कहेगा कि हाँ, जीना पाप है ? जीना भी पाप है, मरना भी पाप है, तो फिर संसार में धर्म क्या रह गया? धर्म कहता है कि न तू मर ! न किसी को मार ! बस यही धर्म है।
भगवान् महावीर ने अहिंसा का उद्गम भी इसी जिजीविषा के अन्दर से बताया है। दशवकालिक में कहा है
"सम्बे जीवा वि इच्छन्ति, जीविडं न मरिज्जिउं।
तम्हा पाणिवहं घोरं, निगंथा वज्जयंति णं ॥" ६, ११. संसार के समस्त प्राणी जीना चाहते हैं, जीने की कामना, इच्छा प्रत्येक प्राणी के भीतर विद्यमान है, मरना कोई नहीं चाहता, इसीलिए किसी का वध करना, मारना, पाप है। मतलब यह है कि 'जीना' यह स्वरूप है और स्वरूप धर्म है। आप देखेंगे कि अहिंसा का स्वर किस भावना से फूटा है ? जीवित रहने की भावना से ही न ! हम प्रत्येक प्राणी के प्रति सहृदय रहते हैं। सहृदय की साधना आखिर क्यों है ? सभी प्राणी एक-दूसरे के प्रति सहृदय रहें । परस्पर सहृदयता, प्रेम, करुणा, सहयोग-ये सब हमारी जीवित रहने की भावना के ही विकसित रूप है। उसी महावृक्ष की ये अनेक शाखाएँ हैं। सुख की भावना:
दूसरी भावना-सुख की भावना है। हम इस विश्वमंडल की अनन्त-अनन्त परिक्रमा कर चुके हैं और कर रहे हैं, लेकिन किसलिए? सुख के लिए ही तो! सुख की भावना और कामना से प्रेरित होकर प्रत्येक प्राणी प्रयत्नशील रहता है। निष्कर्ष यह है कि सुख आत्मा का स्वरूप है। स्वरूप की माँग, खोज प्रात्मा करती है। भगवान् का स्वरूप वर्णन करते हुए बतलाया गया है कि वह आनन्दमय है। इसके आगे बढ़े तो कह दिया कि वह सच्चिदानन्द रूप है। सद्, चिद् और आनन्द, यह एक सर्वोच्च शिखर की बात है। उच्चतम आनन्द की भावना इसके साथ जुड़ी है। इससे यह तो हमने समझ ही लिया कि भगवान का स्वरूप प्रानन्दमय है, सुखमय है। जो उसका स्वरूप है, वही हमारा स्वरूप है। स्वरूप, उसका
और हमारा भिन्न नहीं है । जो भगवान् का स्वरूप है, वह प्रत्येक प्राणी का स्वरूप है। तभी हम कहते हैं कि प्रत्येक घट में भगवान् का वास है। जब तक उस आनन्द की उपलब्धि नहीं
विविध आयामों में : स्वरूप दर्शन Jain Education International
For Private & Personal Use Only
१७५ www.jainelibrary.org