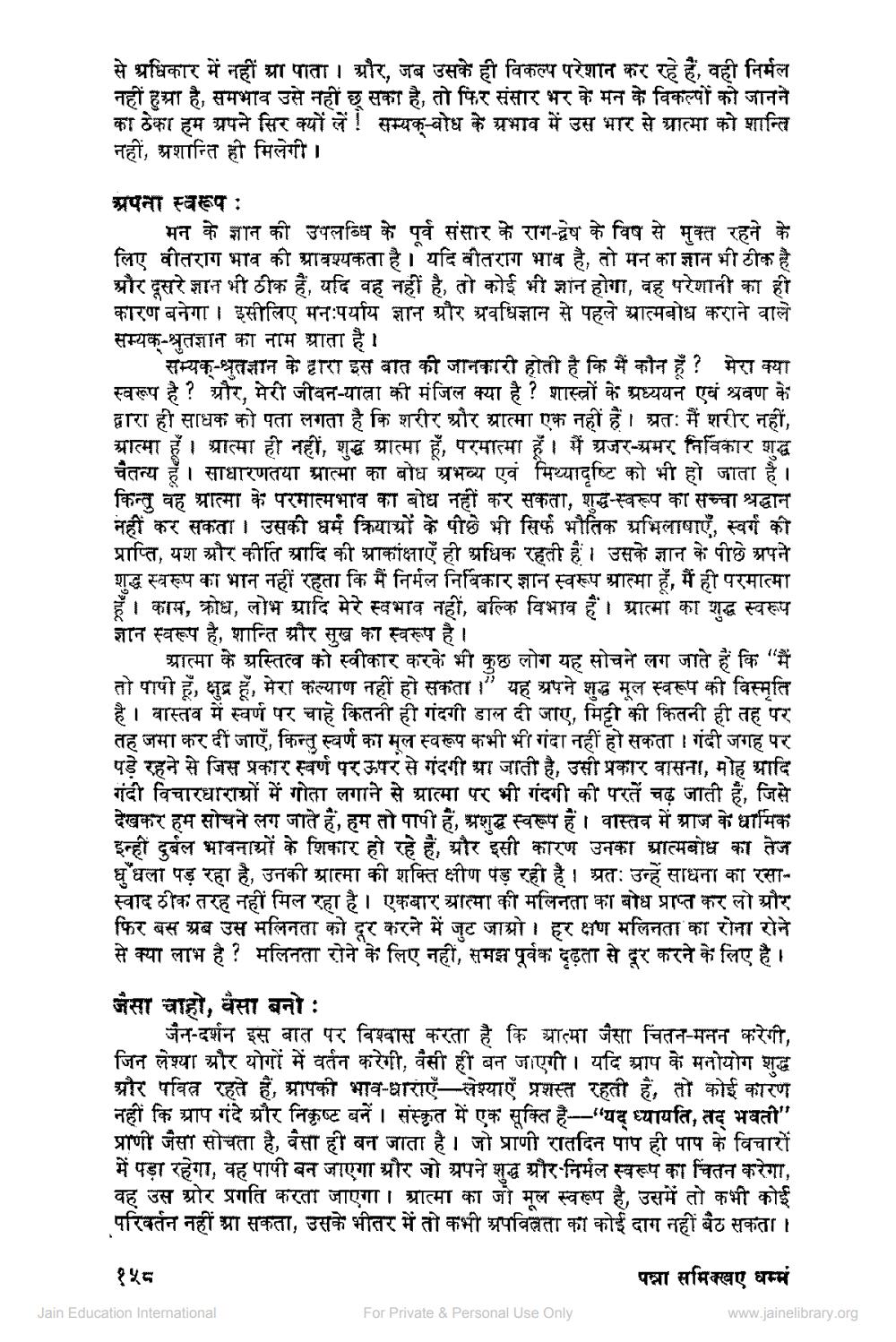________________
से अधिकार में नहीं आ पाता। और, जब उसके ही विकल्प परेशान कर रहे हैं, वही निर्मल नहीं हुआ है, समभाव उसे नहीं छू सका है, तो फिर संसार भर के मन के विकल्पों को जानने का ठेका हम अपने सिर क्यों लें! सम्यक-बोध के अभाव में उस भार से प्रात्मा को शान्ति नहीं, अशान्ति ही मिलेगी।
अपना स्वरूप:
मन के ज्ञान की उपलब्धि के पूर्व संसार के राग-द्वेष के विष से मुक्त रहने के लिए वीतराग भाव की आवश्यकता है। यदि वीतराग भाव है, तो मन का ज्ञान भी ठीक है
और दूसरे ज्ञान भी ठीक है, यदि वह नहीं है, तो कोई भी ज्ञान होगा, वह परेशानी का ही कारण बनेगा। इसीलिए मनःपर्याय ज्ञान और अवधिज्ञान से पहले आत्मबोध कराने वाले सम्यक-श्रुतज्ञान का नाम आता है।
सम्यक्-श्रुतज्ञान के द्वारा इस बात की जानकारी होती है कि मैं कौन हूँ? मेरा क्या स्वरूप है ? और, मेरी जीवन-यात्रा की मंजिल क्या है ? शास्त्रों के अध्ययन एवं श्रवण के द्वारा ही साधक को पता लगता है कि शरीर और आत्मा एक नहीं है। अतः मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। प्रात्मा ही नहीं, शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ। मैं अजर-अमर निर्विकार शुद्ध चैतन्य हूँ। साधारणतया प्रात्मा का बोध अभव्य एवं मिथ्यादृष्टि को भी हो जाता है। किन्तु वह प्रात्मा के परमात्मभाव का बोध नहीं कर सकता, शुद्ध-स्वरूप का सच्चा श्रद्धान नहीं कर सकता। उसकी धर्म क्रियाओं के पीछे भी सिर्फ भौतिक अभिलाषाएँ, स्वर्ग की प्राप्ति, यश और कीर्ति आदि की आकांक्षाएँ ही अधिक रहती है। उसके ज्ञान के पीछे अपने शद्ध स्वरूप का भान नहीं रहता कि मैं निर्मल निर्विकार ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं, मैं ही परमात्मा हूँ। काम, क्रोध, लोभ आदि मेरे स्वभाव नहीं, बल्कि विभाव हैं। प्रात्मा का शुद्ध स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, शान्ति और सुख का स्वरूप है।
आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करके भी कुछ लोग यह सोचने लग जाते हैं कि "मैं तो पापी हूँ, क्षुद्र हूँ, मेरा कल्याण नहीं हो सकता।" यह अपने शुद्ध मूल स्वरूप की विस्मृति है। वास्तव में स्वर्ण पर चाहे कितनी ही गंदगी डाल दी जाए, मिट्टी की कितनी ही तह पर तह जमा कर दी जाएँ, किन्तु स्वर्ण का मूल स्वरूप कभी भी गंदा नहीं हो सकता। गंदी जगह पर पड़े रहने से जिस प्रकार स्वर्ण पर ऊपर से गंदगी आ जाती है, उसी प्रकार वासना, मोह आदि गंदी विचारधाराओं में गोता लगाने से प्रात्मा पर भी गंदगी की परतें चढ़ जाती हैं, जिसे देखकर हम सोचने लग जाते हैं, हम तो पापी हैं, अशुद्ध स्वरूप हैं। वास्तव में आज के धार्मिक इन्हीं दुर्बल भावनाओं के शिकार हो रहे हैं, और इसी कारण उनका आत्मबोध का तेज धु धला पड़ रहा है, उनकी आत्मा की शक्ति क्षीण पड़ रही है। अत: उन्हें साधना का रसास्वाद ठीक तरह नहीं मिल रहा है। एकबार अात्मा की मलिनता का बोध प्राप्त कर लो और फिर बस अब उस मलिनता को दूर करने में जुट जाओ। हर क्षण मलिनता का रोना रोने से क्या लाभ है ? मलिनता रोने के लिए नहीं, समझ पूर्वक दृढ़ता से दूर करने के लिए है।
जैसा चाहो, वैसा बनो:
जैन-दर्शन इस बात पर विश्वास करता है कि आत्मा जैसा चिंतन-मनन करेगी, जिन लेश्या और योगों में वर्तन करेगी, वैसी ही बन जाएगी। यदि आप के मनोयोग शुद्ध
और पवित्र रहते हैं, आपकी भाव-धाराएँ-लेश्याएँ प्रशस्त रहती हैं, तो कोई कारण नहीं कि आप गंदे और निकृष्ट बनें । संस्कृत में एक सूक्ति है-"यद् ध्यायति, तद् भवती" प्राणी जैसा सोचता है, वैसा ही बन जाता है। जो प्राणी रातदिन पाप ही पाप के विचारों में पड़ा रहेगा, वह पापी बन जाएगा और जो अपने शुद्ध और निर्मल स्वरूप का चिंतन करेगा, वह उस ओर प्रगति करता जाएगा। प्रात्मा का जो मल स्वरूप है. उसमें तो कभी कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, उसके भीतर में तो कभी अपवित्रता का कोई दाग नहीं बैठ सकता।
__ पन्ना समिक्खए धम्म
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org