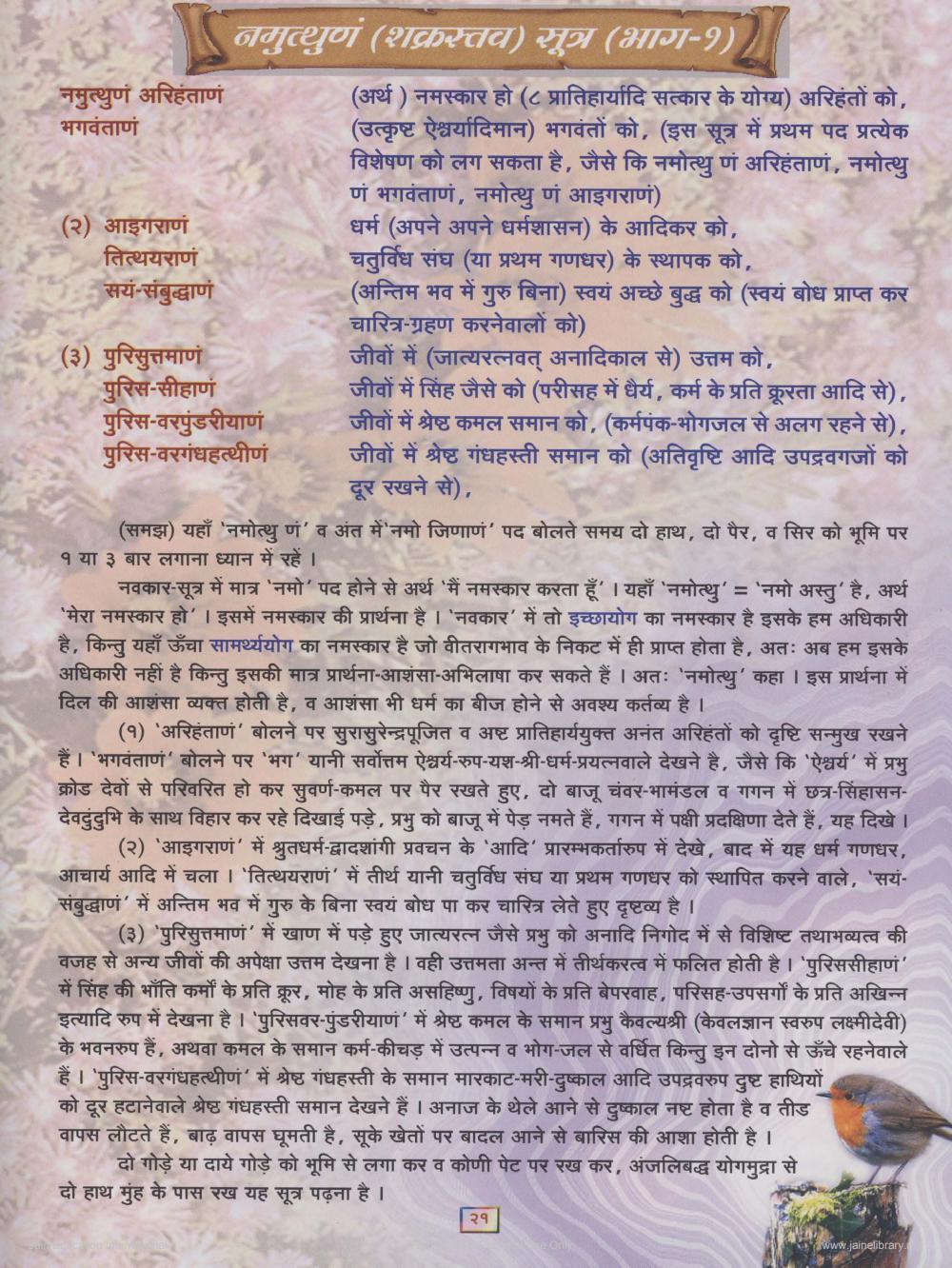________________
नमुत्थुणं (शक्रस्तव) सुत्र (भाग-१) नमुत्थुणं अरिहंताणं
(अर्थ) नमस्कार हो (८ प्रातिहार्यादि सत्कार के योग्य) अरिहंतों को, भगवंताणं
(उत्कष्ट ऐश्वर्यादिमान) भगवंतों को. (इस सत्र में प्रथम पद प्रत्येक विशेषण को लग सकता है, जैसे कि नमोत्थु णं अरिहंताणं, नमोत्थु
णं भगवंताणं, नमोत्थु णं आइगराणं) (२) आइगराणं
धर्म (अपने अपने धर्मशासन) के आदिकर को, तित्थयराणं
चतुर्विध संघ (या प्रथम गणधर) के स्थापक को, सयं-संबुद्धाणं
(अन्तिम भव में गुरु बिना) स्वयं अच्छे बुद्ध को (स्वयं बोध प्राप्त कर
चारित्र-ग्रहण करनेवालों को) (३) पुरिसुत्तमाणं
जीवों में (जात्यरत्नवत् अनादिकाल से) उत्तम को, पुरिस-सीहाणं
जीवों में सिंह जैसे को (परीसह में धैर्य, कर्म के प्रति क्रूरता आदि से), पुरिस-वरपुंडरीयाणं जीवों में श्रेष्ठ कमल समान को, (कर्मपंक-भोगजल से अलग रहने से), पुरिस-वरगंधहत्थीणं जीवों में श्रेष्ठ गंधहस्ती समान को (अतिवृष्टि आदि उपद्रवगजों को
दूर रखने से), (समझ) यहाँ 'नमोत्यु णं' व अंत में नमो जिणाणं' पद बोलते समय दो हाथ, दो पैर, व सिर को भूमि पर १ या ३ बार लगाना ध्यान में रहें ।
नवकार-सूत्र में मात्र 'नमो' पद होने से अर्थ 'मैं नमस्कार करता हूँ' । यहाँ 'नमोत्थु' = 'नमो अस्तु' है, अर्थ 'मेरा नमस्कार हो' । इसमें नमस्कार की प्रार्थना है । 'नवकार' में तो इच्छायोग का नमस्कार है इसके हम अधिकारी है, किन्तु यहाँ ऊँचा सामर्थ्ययोग का नमस्कार है जो वीतरागभाव के निकट में ही प्राप्त होता है, अतः अब हम इसके अधिकारी नहीं है किन्तु इसकी मात्र प्रार्थना-आशंसा-अभिलाषा कर सकते हैं । अतः 'नमोत्थ' कहा । इस प्रार्थना में दिल की आशंसा व्यक्त होती है, व आशंसा भी धर्म का बीज होने से अवश्य कर्तव्य है।
(१) 'अरिहंताणं' बोलने पर सुरासुरेन्द्रपूजित व अष्ट प्रातिहार्ययुक्त अनंत अरिहंतों को दृष्टि सन्मुख रखने हैं। 'भगवंताणं' बोलने पर 'भग' यानी सर्वोत्तम ऐश्वर्य-रुप-यश-श्री-धर्म-प्रयत्नवाले देखने है, जैसे कि 'ऐश्वर्य' में प्रभु क्रोड देवों से परिवरित हो कर सुवर्ण-कमल पर पैर रखते हुए, दो बाजू चंवर-भामंडल व गगन में छत्र-सिंहासनदेवदंदभि के साथ विहार कर रहे दिखाई पडे, प्रभ को बाज में पेड नमते हैं. गगन में पक्षी प्रदक्षिणा देते हैं यह टिखे ।
(२) 'आइगराणं' में श्रुतधर्म-द्वादशांगी प्रवचन के 'आदि' प्रारम्भकर्तारुप में देखे, बाद में यह धर्म गणधर, आचार्य आदि में चला । 'तित्थयराणं' में तीर्थ यानी चतुर्विध संघ या प्रथम गणधर को स्थापित करने वाले, 'सयंसंबुद्धाणं' में अन्तिम भव में गुरु के बिना स्वयं बोध पा कर चारित्र लेते हुए दृष्टव्य है।
(३) 'पुरिसुत्तमाणं' में खाण में पड़े हुए जात्यरत्न जैसे प्रभु को अनादि निगोद में से विशिष्ट तथाभव्यत्व की वजह से अन्य जीवों की अपेक्षा उत्तम देखना है । वही उत्तमता अन्त में तीर्थकरत्व में फलित होती है । 'पुरिससीहाणं' में सिंह की भाँति कर्मों के प्रति क्रूर, मोह के प्रति असहिष्णु, विषयों के प्रति बेपरवाह, परिसह-उपसर्गों के प्रति अखिन्न इत्यादि रुप में देखना है । 'पुरिसवर-पुंडरीयाणं' में श्रेष्ठ कमल के समान प्रभु कैवल्यश्री (केवलज्ञान स्वरुप लक्ष्मीदेवी) के भवनरुप हैं, अथवा कमल के समान कर्म-कीचड़ में उत्पन्न व भोग-जल से वर्धित किन्तु इन दोनो से ऊँचे रहनेवाले हैं । 'पुरिस-वरगंधहत्थीणं' में श्रेष्ठ गंधहस्ती के समान मारकाट-मरी-दुष्काल आदि उपद्रवरुप दुष्ट हाथियों को दूर हटानेवाले श्रेष्ठ गंधहस्ती समान देखने हैं । अनाज के थेले आने से दुष्काल नष्ट होता है व तीड वापस लौटते हैं, बाढ़ वापस घूमती है, सूके खेतों पर बादल आने से बारिस की आशा होती है। 50/दो गोड़े या दाये गोड़े को भूमि से लगा कर व कोणी पेट पर रख कर, अंजलिबद्ध योगमुद्रा से दो हाथ मुंह के पास रख यह सूत्र पढ़ना है ।
www.jainelibrary.