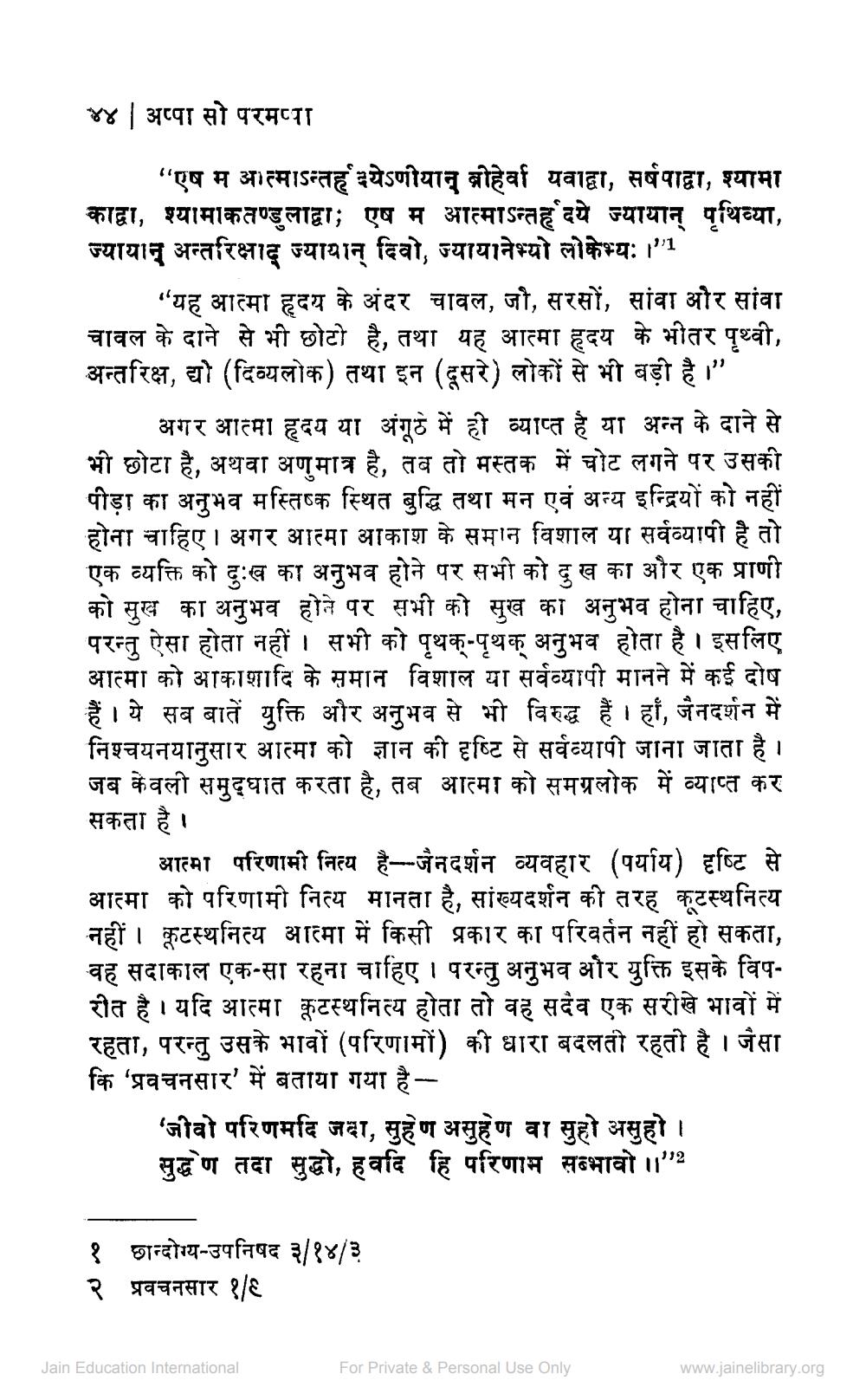________________
४४ | अप्पा सो परमप्पा
"एष म आत्माऽन्तर्ह दयेऽणीयान् ब्रीहेर्वा यवाहा, सर्षपाद्वा, श्यामा काद्वा, श्यामाकतण्डुलाद्वा; एष म आत्माऽन्तर्ह दये ज्यायान् पृथिव्या, ज्यायान अन्तरिक्षाद् ज्यायान् दिवो, ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः ।"1
"यह आत्मा हृदय के अंदर चावल, जौ, सरसों, सांवा और सांवा चावल के दाने से भी छोटो है, तथा यह आत्मा हृदय के भीतर पृथ्वी, अन्तरिक्ष, द्यो (दिव्यलोक) तथा इन (दूसरे) लोकों से भी बड़ी है।"
अगर आत्मा हृदय या अंगूठे में ही व्याप्त है या अन्न के दाने से भी छोटा है, अथवा अणुमात्र है, तब तो मस्तक में चोट लगने पर उसकी पीड़ा का अनुभव मस्तिष्क स्थित बुद्धि तथा मन एवं अन्य इन्द्रियों को नहीं होना चाहिए। अगर आत्मा आकाश के समान विशाल या सर्वव्यापी है तो एक व्यक्ति को दुःख का अनुभव होने पर सभी को दु ख का और एक प्राणी को सुख का अनुभव होने पर सभी को सुख का अनुभव होना चाहिए, परन्तु ऐसा होता नहीं। सभी को पृथक्-पृथक अनुभव होता है। इसलिए आत्मा को आकाशादि के समान विशाल या सर्वव्यापी मानने में कई दोष हैं। ये सब बातें युक्ति और अनुभव से भी विरुद्ध हैं। हाँ, जैनदर्शन में निश्चयनयानुसार आत्मा को ज्ञान की दृष्टि से सर्वव्यापी जाना जाता है । जब के वली समुद्घात करता है, तब आत्मा को समग्रलोक में व्याप्त कर सकता है।
आत्मा परिणामी नित्य है-जैनदर्शन व्यवहार (पर्याय) दृष्टि से आत्मा को परिणामी नित्य मानता है, सांख्यदर्शन की तरह कूटस्थनित्य नहीं। कूटस्थनित्य आत्मा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता, वह सदाकाल एक-सा रहना चाहिए । परन्तु अनुभव और युक्ति इसके विपरीत है। यदि आत्मा कूटस्थनित्य होता तो वह सदैव एक सरीखे भावों में रहता, परन्तु उसके भावों (परिणामों) की धारा बदलती रहती है । जैसा कि 'प्रवचनसार' में बताया गया है
'जीवो परिणमदि जदा, सुहेण असुहेण वा सुहो असुहो । सुद्धण तदा सुद्धो, हवदि हि परिणाम सब्भावो ।।"2
१ छान्दोग्य-उपनिषद ३/१४/३ २ प्रवचनसार १/४
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org