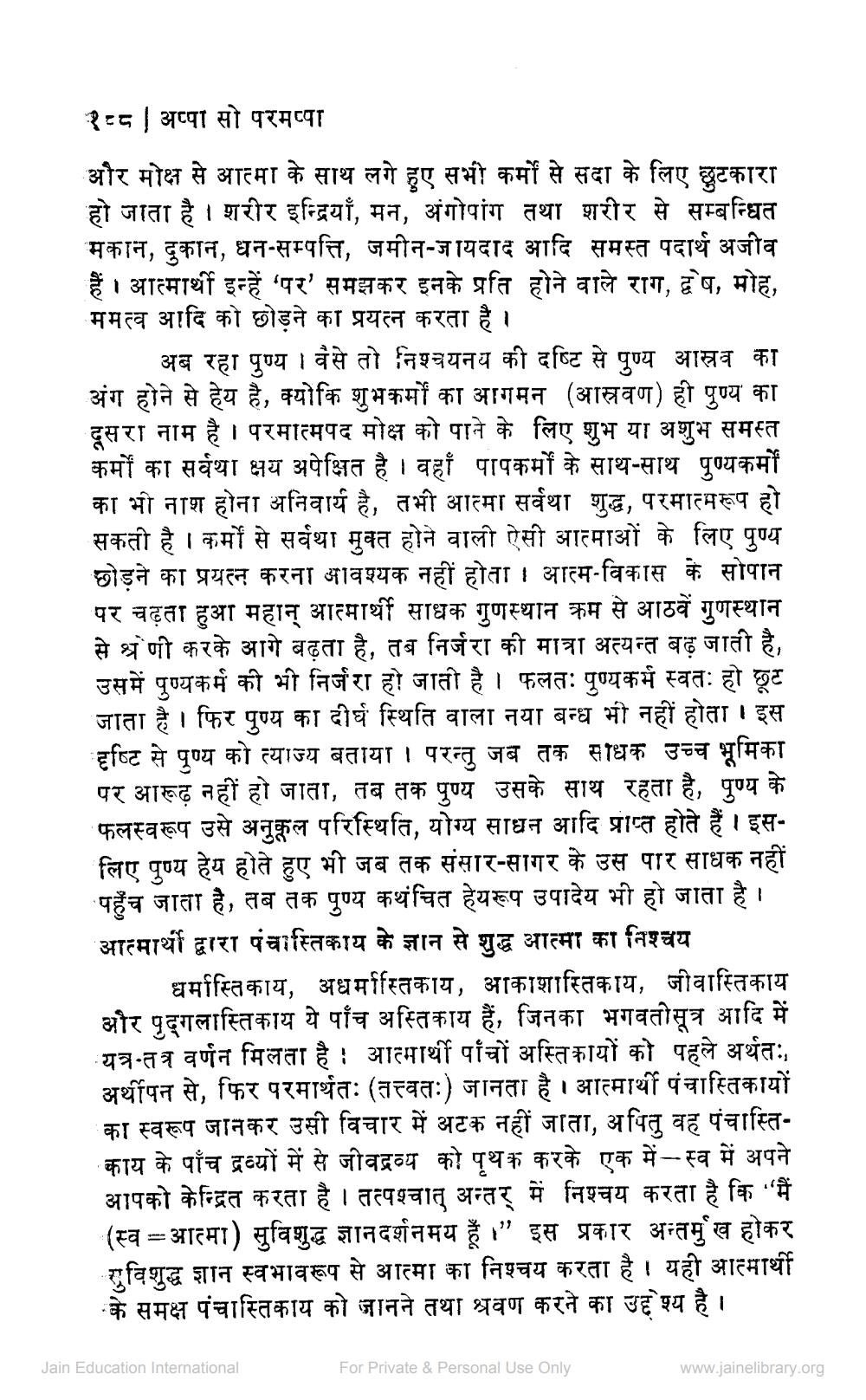________________
१८८ | अप्पा सो परमप्पा
और मोक्ष से आत्मा के साथ लगे हुए सभी कर्मों से सदा के लिए छुटकारा हो जाता है । शरीर इन्द्रियाँ, मन, अंगोपांग तथा शरीर से सम्बन्धित मकान, दुकान, धन-सम्पत्ति, जमीन-जायदाद आदि समस्त पदार्थ अजीव हैं | आत्मार्थी इन्हें 'पर' समझकर इनके प्रति होने वाले राग, द्वेष, मोह, ममत्व आदि को छोड़ने का प्रयत्न करता है।
अब रहा पुण्य । वैसे तो निश्चयनय की दष्टि से पुण्य आस्रव का अंग होने से हेय है, क्योंकि शुभकर्मों का आगमन (आस्रवण) ही पुण्य का दूसरा नाम है । परमात्मपद मोक्ष को पाने के लिए शुभ या अशुभ समस्त कर्मों का सर्वथा क्षय अपेक्षित है । वहाँ पापकर्मों के साथ-साथ पुण्यकर्मों का भी नाश होना अनिवार्य है, तभी आत्मा सर्वथा शुद्ध, परमात्मरूप हो सकती है । कर्मों से सर्वथा मुक्त होने वाली ऐसी आत्माओं के लिए पुण्य छोड़ने का प्रयत्न करना आवश्यक नहीं होता । आत्म-विकास के सोपान पर चढ़ता हुआ महान् आत्मार्थी साधक गुणस्थान क्रम से आठवें गुणस्थान से श्र ेणी करके आगे बढ़ता है, तब निर्जरा की मात्रा अत्यन्त बढ़ जाती है, उसमें पुण्यकर्म की भी निर्जरा हो जाती है । फलतः पुण्यकर्म स्वतः हो छूट जाता है । फिर पुण्य का दीर्घ स्थिति वाला नया बन्ध भी नहीं होता । इस दृष्टि से पुण्य को त्याज्य बताया। परन्तु जब तक साधक उच्च भूमिका पर आरूढ़ नहीं हो जाता, तब तक पुण्य उसके साथ रहता है, पुण्य फलस्वरूप उसे अनुकूल परिस्थिति, योग्य साधन आदि प्राप्त होते हैं । इसलिए पुण्य हेय होते हुए भी जब तक संसार - सागर के उस पार साधक नहीं पहुँच जाता है, तब तक पुण्य कथंचित हेयरूप उपादेय भी हो जाता है । आत्मार्थी द्वारा पंचास्तिकाय के ज्ञान से शुद्ध आत्मा का निश्चय
के
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय ये पाँच अस्तिकाय हैं, जिनका भगवतीसूत्र आदि में यत्र-तत्र वर्णन मिलता है ! आत्मार्थी पाँचों अस्तिकायों को पहले अर्थतः, अर्थीपन से, फिर परमार्थतः (तत्त्वतः ) जानता है । आत्मार्थी पंचास्तिकायों का स्वरूप जानकर उसी विचार में अटक नहीं जाता, अपितु वह पंचास्तिकाय के पाँच द्रव्यों में से जीवद्रव्य को पृथक करके एक में - स्व में अपने आपको केन्द्रित करता है । तत्पश्चात् अन्तर् में निश्चय करता है कि "मैं ( स्व = आत्मा) सुविशुद्ध ज्ञानदर्शनमय हूँ ।" इस प्रकार अन्तर्मुख होकर सुविशुद्ध ज्ञान स्वभावरूप से आत्मा का निश्चय करता है । यही आत्मार्थी के समक्ष पंचास्तिकाय को जानने तथा श्रवण करने का उद्देश्य है ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org