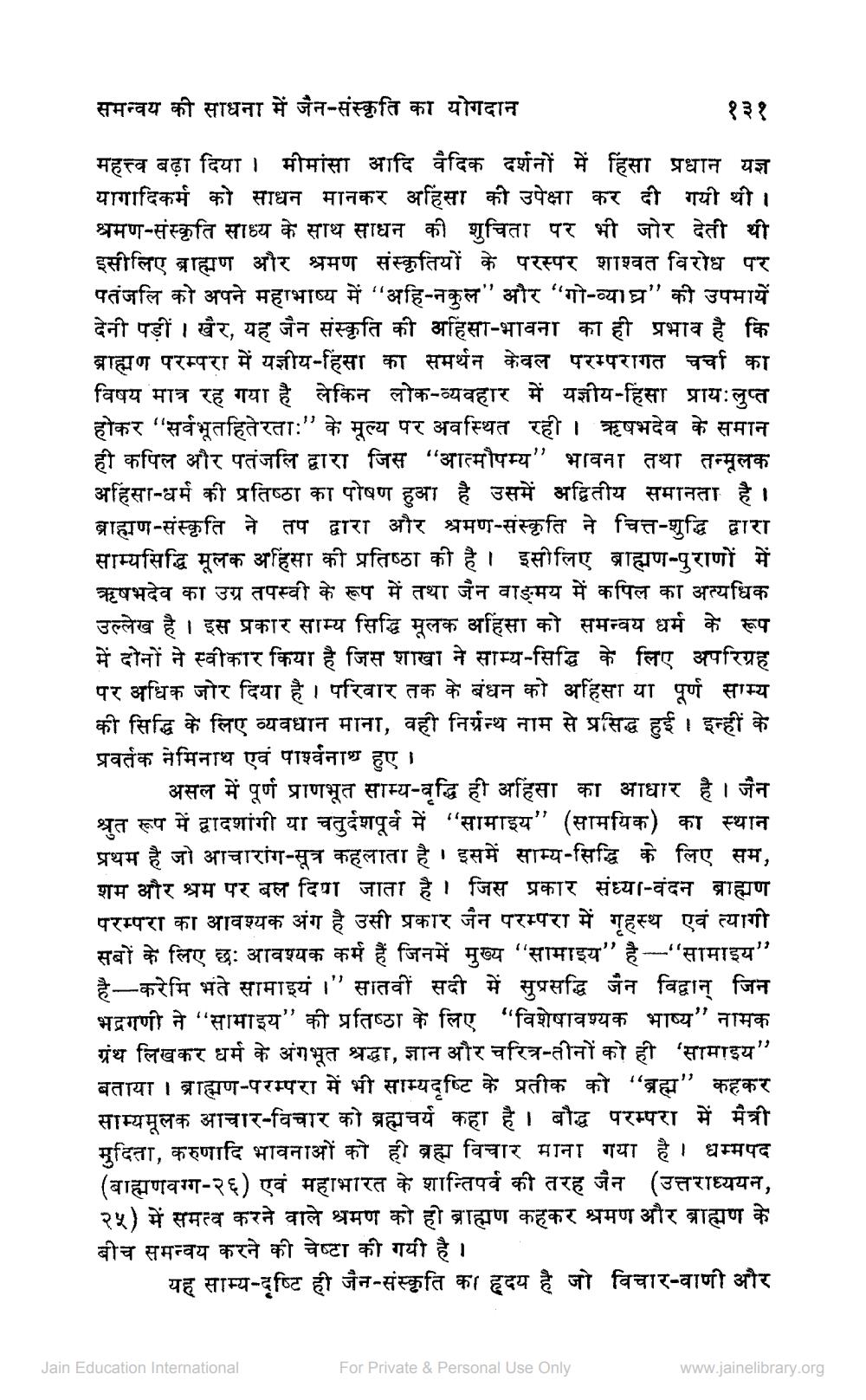________________
समन्वय की साधना में जैन-संस्कृति का योगदान
१३१
महत्त्व बढ़ा दिया । मीमांसा आदि वैदिक दर्शनों में हिंसा प्रधान यज्ञ यागादिकर्म को साधन मानकर अहिंसा की उपेक्षा कर दी गयी थी । श्रमण-संस्कृति साध्य के साथ साधन की शुचिता पर भी जोर देती थी इसीलिए ब्राह्मण और श्रमण संस्कृतियों के परस्पर शाश्वत विरोध पर पतंजलि को अपने महाभाष्य में " अहि-नकुल" और "गो-व्याघ्र" की उपमायें देनी पड़ीं। खैर, यह जैन संस्कृति की अहिंसा - भावना का ही प्रभाव है कि ब्राह्मण परम्परा में यज्ञीय हिंसा का समर्थन केवल परम्परागत चर्चा का विषय मात्र रह गया है लेकिन लोक व्यवहार में यज्ञीय - हिंसा प्रायः लुप्त होकर "सर्वभूतहिते रताः " के मूल्य पर अवस्थित रही । ऋषभदेव के समान ही कपिल और पतंजलि द्वारा जिस "आत्मौपम्य" भावना तथा तन्मूलक अहिंसा-धर्म की प्रतिष्ठा का पोषण हुआ है उसमें अद्वितीय समानता है । ब्राह्मण-संस्कृति ने तप द्वारा और श्रमण संस्कृति ने चित्त-शुद्धि द्वारा साम्यसिद्धि मूलक अहिंसा की प्रतिष्ठा की है । इसीलिए ब्राह्मण-पुराणों में ऋषभदेव का उग्र तपस्वी के रूप में तथा जैन वाङ्मय में कपिल का अत्यधिक उल्लेख है । इस प्रकार साम्य सिद्धि मूलक अहिंसा को समन्वय धर्म के रूप में दोनों ने स्वीकार किया है जिस शाखा ने साम्य-सिद्धि के लिए अपरिग्रह पर अधिक जोर दिया है। परिवार तक के बंधन को अहिंसा या पूर्ण साम्य की सिद्धि के लिए व्यवधान माना, वही निर्ग्रन्थ नाम से प्रसिद्ध हुई । इन्हीं के प्रवर्तक नेमिनाथ एवं पार्श्वनाथ हुए।
असल में पूर्ण प्राणभूत साम्य वृद्धि ही अहिंसा का आधार है । जैन श्रुत रूप में द्वादशांगी या चतुर्दशपूर्व में "सामाइय" (सामयिक ) का स्थान प्रथम है जो आचारांग सूत्र कहलाता है । इसमें साम्य-सिद्धि के लिए सम, शम और श्रम पर बल दिया जाता है । जिस प्रकार संध्या वंदन ब्राह्मण परम्परा का आवश्यक अंग है उसी प्रकार जैन परम्परा में गृहस्थ एवं त्यागी सबों के लिए छ: आवश्यक कर्म हैं जिनमें मुख्य "सामाइय" है - "सामाइय" है— करेमि भंते सामाइयं ।" सातवीं सदी में सुप्रसद्धि जैन विद्वान् जिन भद्रगणी ने "सामाइय" की प्रतिष्ठा के लिए " विशेषावश्यक भाष्य" नामक ग्रंथ लिखकर धर्म के अंगभूत श्रद्धा, ज्ञान और चरित्र-तीनों को ही 'सामाइय" बताया । ब्राह्मण-परम्परा में भी साम्यदृष्टि के प्रतीक को "ब्रह्म" कहकर साम्यमूलक आचार-विचार को ब्रह्मचर्य कहा है । बौद्ध परम्परा में मैत्री मुदिता, करुणादि भावनाओं को ही ब्रह्म विचार माना गया है। धम्मपद (बाह्मणवग्ग - २६) एवं महाभारत के शान्तिपर्व की तरह जैन (उत्तराध्ययन, २५) में समत्व करने वाले श्रमण को ही ब्राह्मण कहकर श्रमण और ब्राह्मण के बीच समन्वय करने की चेष्टा की गयी है ।
यह साम्यय-दृष्टि ही जैन संस्कृति का हृदय है जो विचार - वाणी और
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org