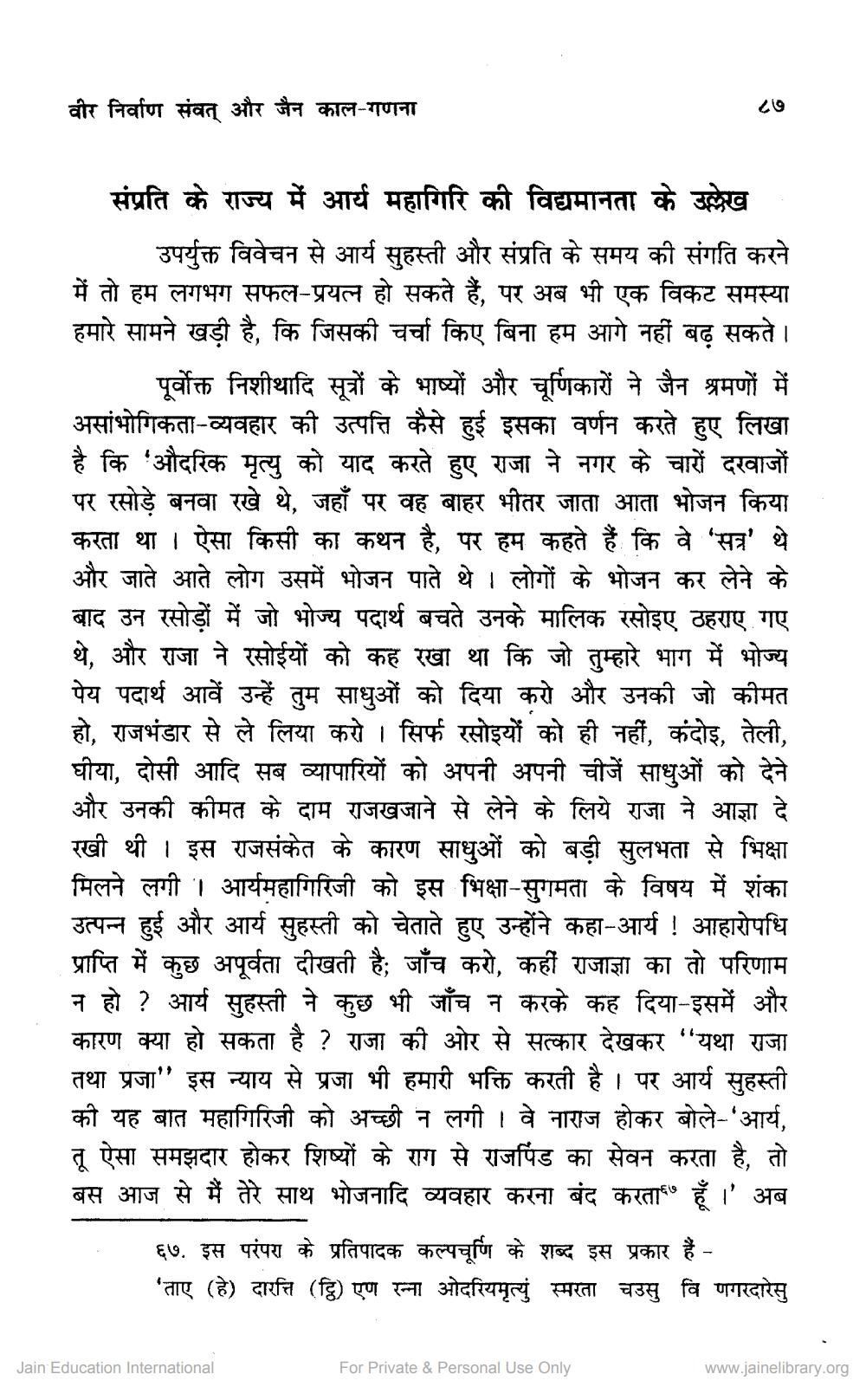________________
वीर निर्वाण संवत् और जैन काल-गणना
संप्रति के राज्य में आर्य महागिरि की विद्यमानता के उल्लेख
उपर्युक्त विवेचन से आर्य सुहस्ती और संप्रति के समय की संगति करने में तो हम लगभग सफल प्रयत्न हो सकते हैं, पर अब भी एक विकट समस्या हमारे सामने खड़ी है, कि जिसकी चर्चा किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते ।
८७
पूर्वोक्त निशीथादि सूत्रों के भाष्यों और चूर्णिकारों ने जैन श्रमणों में असांभोगिकता - - व्यवहार की उत्पत्ति कैसे हुई इसका वर्णन करते हुए लिखा है कि 'औदरिक मृत्यु को याद करते हुए राजा ने नगर के चारों दरवाजों पर रसोड़े बनवा रखे थे, जहाँ पर वह बाहर भीतर जाता आता भोजन किया करता था । ऐसा किसी का कथन है, पर हम कहते हैं कि वे 'सत्र' थे और जाते आते लोग उसमें भोजन पाते थे । लोगों के भोजन कर लेने के बाद उन रसोड़ों में जो भोज्य पदार्थ बचते उनके मालिक रसोइए ठहराए गए थे, और राजा ने रसोईयों को कह रखा था कि जो तुम्हारे भाग में भोज्य पेय पदार्थ आवें उन्हें तुम साधुओं को दिया करो और उनकी जो कीमत हो, राजभंडार से ले लिया करो । सिर्फ रसोइयों को ही नहीं, कंदोई, तेली, घीया, दोसी आदि सब व्यापारियों को अपनी अपनी चीजें साधुओं को देने और उनकी कीमत के दाम राजखजाने से लेने के लिये राजा ने आज्ञा दे रखी थी । इस राजसंकेत के कारण साधुओं को बड़ी सुलभता से भिक्षा मिलने लगी । आर्यमहागिरिजी को इस भिक्षा-सुगमता के विषय में शंका उत्पन्न हुई और आर्य सुहस्ती को चेताते हुए उन्होंने कहा- आर्य ! आहारोपधि प्राप्ति में कुछ अपूर्वता दीखती है; जाँच करो, कहीं राजाज्ञा का तो परिणाम न हो ? आर्य सुहस्ती ने कुछ भी जाँच न करके कह दिया- इसमें और कारण क्या हो सकता है ? राजा की ओर से सत्कार देखकर " यथा राजा तथा प्रजा" इस न्याय से प्रजा भी हमारी भक्ति करती है । पर आर्य सुहस्ती की यह बात महागिरिजी को अच्छी न लगी । वे नाराज होकर बोले- 'आर्य, तू ऐसा समझदार होकर शिष्यों के राग से राजपिंड का सेवन करता है, तो बस आज से मैं तेरे साथ भोजनादि व्यवहार करना बंद करता हूँ ।' अब
६७. इस परंपरा के प्रतिपादक कल्पचूर्णि के शब्द इस प्रकार हैं 'ताए (हे) दारत्ति (ट्ठि) एण रन्ना ओदरियमृत्युं स्मरता चउसु वि णगरदारेसु
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org