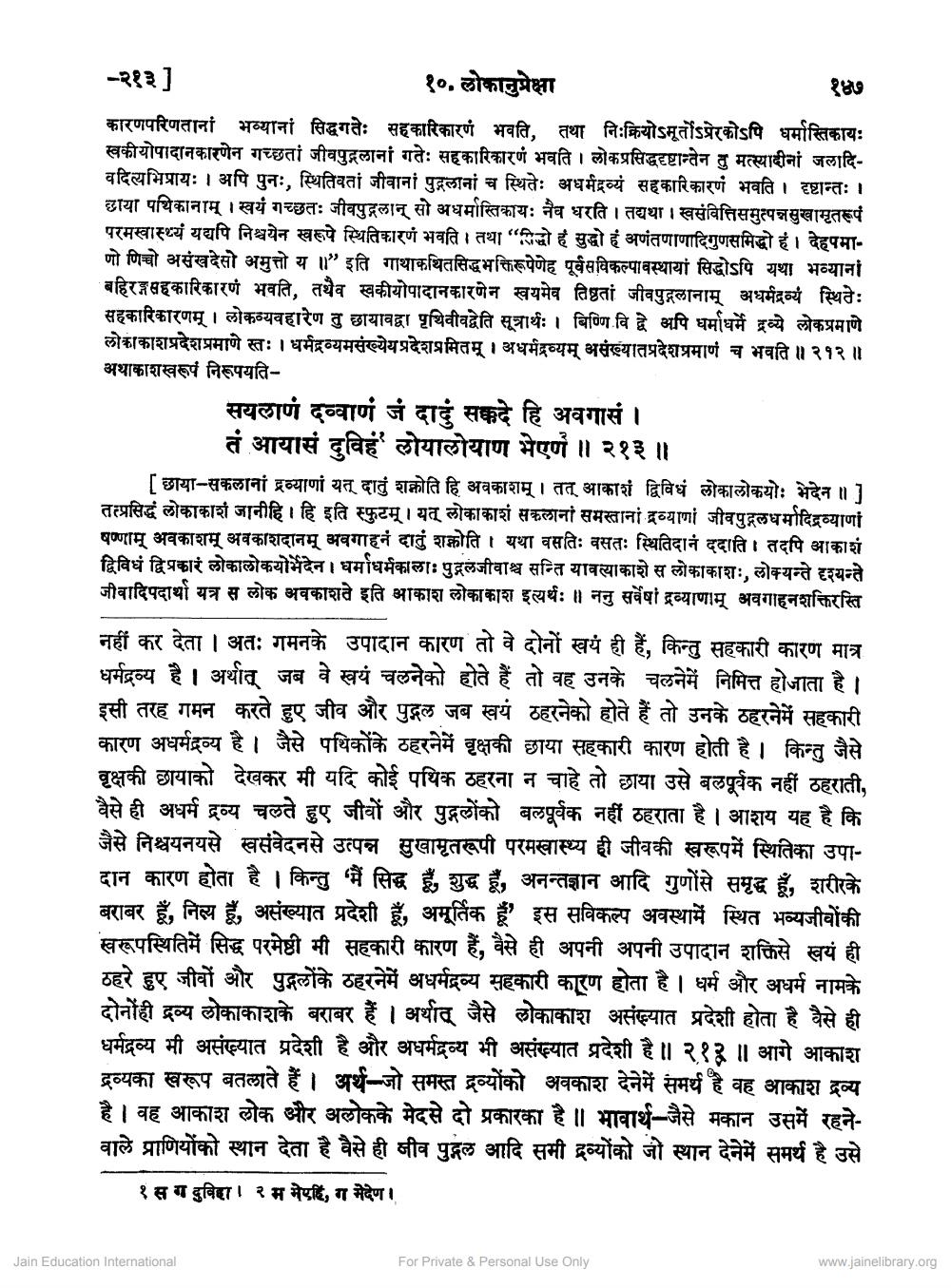________________
१४७
-२१३]
१०. लोकानुप्रेक्षा कारणपरिणतानां भव्यानां सिद्धगतेः सहकारिकारणं भवति. तथा निःक्रियोऽमूर्तोऽप्रेरकोऽपि धर्मास्तिकायः खकीयोपादानकारणेन गच्छतां जीवपुद्गलानां गतेः सहकारिकारणं भवति । लोकप्रसिद्धदृष्टान्तेन तु मत्स्यादीनां जलादिवदित्यभिप्रायः । अपि पुनः, स्थितिवतां जीवानां पुद्गलानां च स्थितेः अधर्मद्रव्यं सहकारि कारणं भवति । दृष्टान्तः । छाया पथिकानाम् । खयं गच्छतः जीवपुद्गलान् सो अधर्मास्तिकायः नैव धरति । तद्यथा । खसंवित्तिसमुत्पन्नसुखामृतरूपं परमस्वास्थ्यं यद्यपि निश्चयेन खरूपे स्थितिकारणं भवति । तथा "सिद्धो है सुद्धो हं अणंतणाणादिगुणसमिद्धो है। देहपमाणो णिच्चो असंखदेसो अमुत्तो य ॥” इति गाथाकथितसिद्धभक्तिरूपेणेह पूर्वसविकल्पावस्थायां सिद्धोऽपि यथा भव्यानां बहिरङ्गसहकारिकारणं भवति, तथैव स्वकीयोपादानकारणेन खयमेव तिष्ठतां जीवपुद्गलानाम् अधर्मद्रव्यं स्थिते: सहकारिकारणम् । लोकव्यवहारेण तु छायावद्वा पृथिवीवद्वेति सूत्रार्थः । बिण्णि वि द्वे अपि धर्माधर्मे द्रव्ये लोकप्रमाणे लोकाकाशप्रदेशप्रमाणे स्तः । धर्मद्रव्यमसंख्येयप्रदेशप्रमितम् । अधर्मद्रव्यम् असंख्यातप्रदेशप्रमाणं च भवति ॥२१२॥ अथाकाशखरूपं निरूपयति
सयलाणं दव्वाणं जं दादु सक्कदे हि अवगासं ।
तं आयासं दुविहं' लोयालोयाण भेएणे ॥ २१३ ॥ [छाया-सकलानां द्रव्याणां यत् दातुं शक्नोति हि अवकाशम् । तत् आकाशं द्विविधं लोकालोकयोः भेदेन ॥1 तत्प्रसिद्ध लोकाकाशं जानीहि। हि इति स्फुटम् । यत् लोकाकाशं सकलानां समस्तानां द्रव्याणां जीवपुद्गलधर्मादिद्रव्याणां षण्णाम् अवकाशम् अवकाशदानम् अवगाहनं दातुं शक्नोति । यथा वसतिः वसतः स्थितिदानं ददाति। तदपि आकाशं द्विविधं द्विप्रकारं लोकालोकयोमैदेन। धर्माधर्मकालाः पुद्गलजीवाश्च सन्ति यावत्याकाशे स लोकाकाशः, लोक्यन्ते दृश्यन्ते जीवादिपदार्था यत्र स लोक अवकाशते इति आकाश लोकाकाश इत्यर्थः ॥ ननु सर्वेषां द्रव्याणाम् अवगाहनशक्तिरस्ति
नहीं कर देता । अतः गमनके उपादान कारण तो वे दोनों खयं ही हैं, किन्तु सहकारी कारण मात्र धर्मद्रव्य है । अर्थात् जब वे खयं चलनेको होते हैं तो वह उनके चलनेमें निमित्त होजाता है। इसी तरह गमन करते हुए जीव और पुद्गल जब स्वयं ठहरनेको होते हैं तो उनके ठहरनेमें सहकारी कारण अधर्मद्रव्य है। जैसे पथिकोंके ठहरनेमें वृक्षकी छाया सहकारी कारण होती है। किन्तु जैसे वृक्षकी छायाको देखकर मी यदि कोई पथिक ठहरना न चाहे तो छाया उसे बलपूर्वक नहीं ठहराती, वैसे ही अधर्म द्रव्य चलते हुए जीवों और पुद्गलोंको बलपूर्वक नहीं ठहराता है । आशय यह है कि जैसे निश्चयनयसे स्वसंवेदनसे उत्पन्न सुखामृतरूपी परमखास्थ्य ही जीवकी खरूपमें स्थितिका उपादान कारण होता है । किन्तु 'मैं सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, अनन्तज्ञान आदि गुणोंसे समृद्ध हूँ, शरीरके बराबर हूँ, नित्य हूँ, असंख्यात प्रदेशी हूँ, अमूर्तिक हूँ' इस सविकल्प अवस्थामें स्थित भव्यजीवोंकी खरूपस्थितिमें सिद्ध परमेष्ठी मी सहकारी कारण हैं, वैसे ही अपनी अपनी उपादान शक्तिसे स्वयं ही ठहरे हुए जीवों और पुद्गलोंके ठहरनेमें अधर्मद्रव्य सहकारी कारण होता है । धर्म और अधर्म नामके दोनोंही द्रव्य लोकाकाशके बराबर हैं । अर्थात् जैसे लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी होता है वैसे ही धर्मद्रव्य मी असंख्यात प्रदेशी है और अधर्मद्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है ॥ २१३ ॥ आगे आकाश द्रव्यका खरूप बतलाते हैं। अर्थ-जो समस्त द्रव्योंको अवकाश देनेमें समर्थ है वह आकाश द्रव्य है । वह आकाश लोक और अलोकके मेदसे दो प्रकारका है ॥ भावार्थ-जैसे मकान उसमें रहनेवाले प्राणियोंको स्थान देता है वैसे ही जीव पुद्गल आदि समी द्रव्योंको जो स्थान देनेमें समर्थ है उसे
१ स ग दुविहा । २ म मेएहिं, ग मेदेण।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org