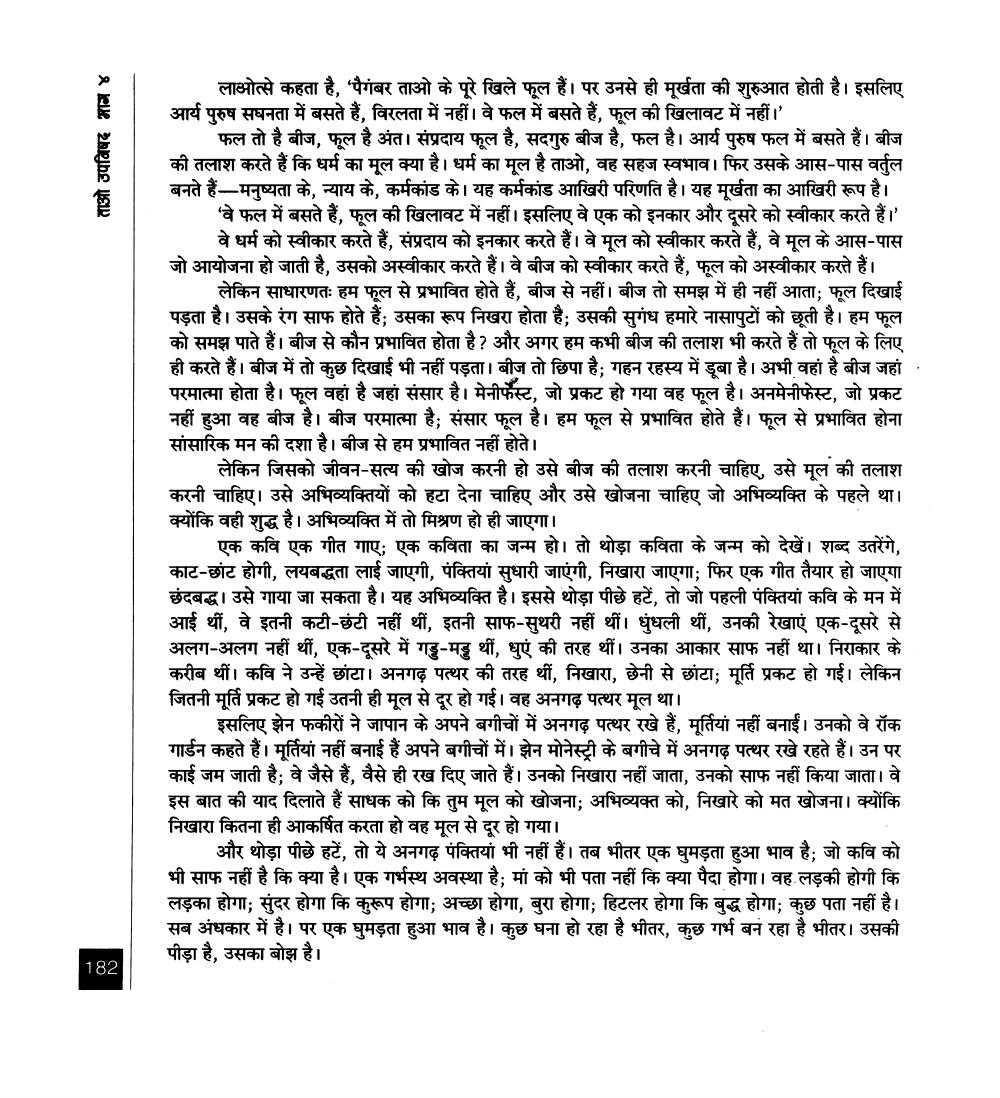________________
ताओ उपनिषद भाग ४
182
लाओत्से कहता है, 'पैगंबर ताओ के पूरे खिले फूल हैं। पर उनसे ही मूर्खता की शुरुआत होती है। इसलिए आर्य पुरुष सघनता में बसते हैं, विरलता में नहीं । वे फल में बसते हैं, फूल की खिलावट में नहीं ।'
फल तो है बीज, फूल है अंत। संप्रदाय फूल है, सदगुरु बीज है, फल है। आर्य पुरुष फल में बसते हैं। बीज की तलाश करते हैं कि धर्म का मूल क्या है। धर्म का मूल है ताओ, वह सहज स्वभाव । फिर उसके आस-पास वर्तुल बनते हैं— मनुष्यता के, न्याय के, कर्मकांड के। यह कर्मकांड आखिरी परिणति है । यह मूर्खता का आखिरी रूप है। 'वे फल में बसते हैं, फूल की खिलावट में नहीं। इसलिए वे एक को इनकार और दूसरे को स्वीकार करते हैं।' वे धर्म को स्वीकार करते हैं, संप्रदाय को इनकार करते हैं। वे मूल को स्वीकार करते हैं, वे मूल के आस-पास जो आयोजना हो जाती है, उसको अस्वीकार करते हैं। वे बीज को स्वीकार करते हैं, फूल को अस्वीकार करते हैं। लेकिन साधारणतः हम फूल से प्रभावित होते हैं, बीज से नहीं। बीज तो समझ में ही नहीं आता; फूल दिखाई पड़ता है। उसके रंग साफ होते हैं; उसका रूप निखरा होता है; उसकी सुगंध हमारे नासापुटों को छूती है। हम फूल को समझ पाते हैं। बीज से कौन प्रभावित होता है ? और अगर हम कभी बीज की तलाश भी करते हैं तो फूल के लिए
करते हैं। बीज में तो कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता। बीज तो छिपा है; गहन रहस्य में डूबा है। अभी वहां है बीज जहां परमात्मा होता है। फूल वहां है जहां संसार है। मेनीफँस्ट, जो प्रकट हो गया वह फूल है । अनमेनीफेस्ट, जो प्रकट नहीं हुआ वह बीज है। बीज परमात्मा है; संसार फूल है। हम फूल से प्रभावित होते हैं। फूल से प्रभावित होना सांसारिक मन की दशा है। बीज से हम प्रभावित नहीं होते।
लेकिन जिसको जीवन-सत्य की खोज करनी हो उसे बीज की तलाश करनी चाहिए, उसे मूल की तलाश करनी चाहिए। उसे अभिव्यक्तियों को हटा देना चाहिए और उसे खोजना चाहिए जो अभिव्यक्ति के पहले था। क्योंकि वही शुद्ध है। अभिव्यक्ति में तो मिश्रण हो ही जाएगा।
एक कवि एक गीत गाए; एक कविता का जन्म हो। तो थोड़ा कविता के जन्म को देखें । शब्द उतरेंगे, काट-छांट होगी, लयबद्धता लाई जाएगी, पंक्तियां सुधारी जाएंगी, निखारा जाएगा; फिर एक गीत तैयार हो जाएगा छंदबद्ध। उसे गाया जा सकता है। यह अभिव्यक्ति है। इससे थोड़ा पीछे हटें, तो जो पहली पंक्तियां कवि के मन में आई थीं, वे इतनी कटी-छंटी नहीं थीं, इतनी साफ-सुथरी नहीं थीं । धुंधली थीं, उनकी रेखाएं एक-दूसरे से अलग-अलग नहीं थीं, एक-दूसरे में गड्डमड्ड थीं, धुएं की तरह थीं। उनका आकार साफ नहीं था । निराकार के करीब थीं। कवि ने उन्हें छांटा। अनगढ़ पत्थर की तरह थीं, निखारा, छेनी से छांटा; मूर्ति प्रकट हो गई। लेकिन जितनी मूर्ति प्रकट हो गई उतनी ही मूल से दूर हो गई। वह अनगढ़ पत्थर मूल था।
इसलिए झेन फकीरों ने जापान के अपने बगीचों में अनगढ़ पत्थर रखे हैं, मूर्तियां नहीं बनाईं। उनको वे रॉक गार्डन कहते हैं। मूर्तियां नहीं बनाई हैं अपने बगीचों में । झेन मोनेस्ट्री के बगीचे में अनगढ़ पत्थर रखे रहते हैं। उन पर काई जम जाती है; वे जैसे हैं, वैसे ही रख दिए जाते हैं। उनको निखारा नहीं जाता, उनको साफ नहीं किया जाता। वे इस बात की याद दिलाते हैं साधक को कि तुम मूल को खोजना; अभिव्यक्त को, निखारे को मत खोजना। क्योंकि निखारा कितना ही आकर्षित करता हो वह मूल से दूर हो गया।
और थोड़ा पीछे हटें, तो ये अनगढ़ पंक्तियां भी नहीं हैं। तब भीतर एक घुमड़ता हुआ भाव है; जो कवि को भी साफ नहीं है कि क्या है । एक गर्भस्थ अवस्था है; मां को भी पता नहीं कि क्या पैदा होगा। वह लड़की होगी कि लड़का होगा; सुंदर होगा कि कुरूप होगा; अच्छा होगा, बुरा होगा; हिटलर होगा कि बुद्ध होगा; कुछ पता नहीं है । सब अंधकार में है। पर एक घुमड़ता हुआ भाव है । कुछ घना हो रहा है भीतर, कुछ गर्भ बन रहा है भीतर। उसकी पीड़ा है, उसका बोझ है ।