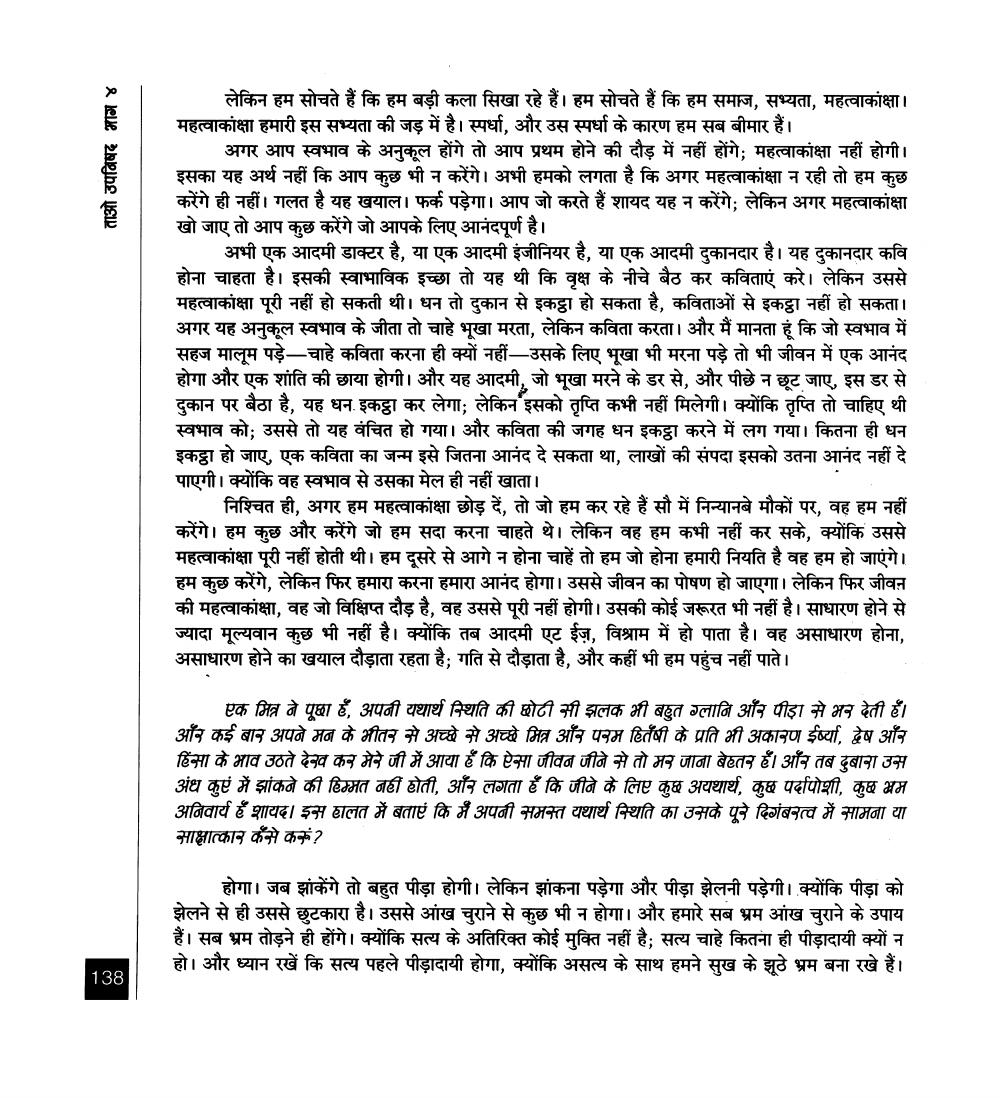________________
ताओ उपनिषद भाग ४
138
लेकिन हम सोचते हैं कि हम बड़ी कला सिखा रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम समाज, सभ्यता, महत्वाकांक्षा । महत्वाकांक्षा हमारी इस सभ्यता की जड़ में है । स्पर्धा, और उस स्पर्धा के कारण हम सब बीमार हैं।
अगर आप स्वभाव के अनुकूल होंगे तो आप प्रथम होने की दौड़ में नहीं होंगे; महत्वाकांक्षा नहीं होगी । इसका यह अर्थ नहीं कि आप कुछ भी न करेंगे। अभी हमको लगता है कि अगर महत्वाकांक्षा न रही तो हम कुछ करेंगे ही नहीं । गलत है यह खयाल । फर्क पड़ेगा। आप जो करते हैं शायद यह न करेंगे; लेकिन अगर महत्वाकांक्षा खो जाए तो आप कुछ करेंगे जो आपके लिए आनंदपूर्ण है।
अभी एक आदमी डाक्टर है, या एक आदमी इंजीनियर है, या एक आदमी दुकानदार है। यह दुकानदार कवि होना चाहता है। इसकी स्वाभाविक इच्छा तो यह थी कि वृक्ष के नीचे बैठ कर कविताएं करे। लेकिन उससे महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो सकती थी। धन तो दुकान से इकट्ठा हो सकता है, कविताओं से इकट्ठा नहीं हो सकता । अगर यह अनुकूल स्वभाव के जीता तो चाहे भूखा मरता, लेकिन कविता करता । और मैं मानता हूं कि जो स्वभाव में सहज मालूम पड़े - चाहे कविता करना ही क्यों नहीं— उसके लिए भूखा भी मरना पड़े तो भी जीवन में एक आनंद होगा और एक शांति की छाया होगी। और यह आदमी, जो भूखा मरने के डर से, और पीछे न छूट जाए, इस डर से दुकान पर बैठा है, यह धन इकट्ठा कर लेगा; लेकिन इसको तृप्ति कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि तृप्ति तो चाहिए थी स्वभाव को; उससे तो यह वंचित हो गया । और कविता की जगह धन इकट्ठा करने में लग गया। कितना ही धन इकट्ठा हो जाए, एक कविता का जन्म इसे जितना आनंद दे सकता था, लाखों की संपदा इसको उतना आनंद नहीं दे पाएगी। क्योंकि वह स्वभाव से उसका मेल ही नहीं खाता ।
निश्चित ही, अगर हम महत्वाकांक्षा छोड़ दें, तो जो हम कर रहे हैं सौ में निन्यानबे मौकों पर, वह हम नहीं करेंगे। हम कुछ और करेंगे जो हम सदा करना चाहते थे। लेकिन वह हम कभी नहीं कर सके, क्योंकि उससे महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती थी। हम दूसरे से आगे न होना चाहें तो हम जो होना हमारी नियति है वह हम हो जाएंगे। हम कुछ करेंगे, लेकिन फिर हमारा करना हमारा आनंद होगा। उससे जीवन का पोषण हो जाएगा। लेकिन फिर जीवन की महत्वाकांक्षा, वह जो विक्षिप्त दौड़ है, वह उससे पूरी नहीं होगी। उसकी कोई जरूरत भी नहीं है । साधारण होने से ज्यादा मूल्यवान कुछ भी नहीं है। क्योंकि तब आदमी एट ईज़, विश्राम में हो पाता है। वह असाधारण होना, असाधारण होने का खयाल दौड़ाता रहता है; गति से दौड़ाता है, और कहीं भी हम पहुंच नहीं पाते।
एक मित्र ने पूछा हैं, अपनी यथार्थ स्थिति की छोटी सी झलक भी बहुत ग्लानि और पीड़ा से भर देती हैं। और कई बार अपने मन के भीतर से अच्छे से अच्छे मित्र और परम हितैषी के प्रति भी अकारण ईर्ष्या, द्वेष और हिंसा के भाव उठते देख कर मेरे जी में आया हैं कि ऐसा जीवन जीने से तो मर जाना बेहतर हैं। और तब दुबारा उस अंध कुएं में झांकने की हिम्मत नहीं होती, और लगता हैं कि जीने के लिए कुछ अयथार्थ, कुछ पर्दापोशी, कुछ भ्रम अनिवार्य हैं शायद । इस हालत में बताएं कि मैं अपनी समस्त यथार्थ स्थिति का उसके पूरे दिगंबरत्व में सामना या साक्षात्कार कैसे करूं?
होगा। जब झांकेंगे तो बहुत पीड़ा होगी। लेकिन झांकना पड़ेगा और पीड़ा झेलनी पड़ेगी। क्योंकि पीड़ा को झेलने से ही उससे छुटकारा है। उससे आंख चुराने से कुछ भी न होगा। और हमारे सब भ्रम आंख चुराने के उपाय हैं। सब भ्रम तोड़ने ही होंगे। क्योंकि सत्य के अतिरिक्त कोई मुक्ति नहीं है; सत्य चाहे कितना ही पीड़ादायी क्यों न हो। और ध्यान रखें कि सत्य पहले पीड़ादायी होगा, क्योंकि असत्य के साथ हमने सुख के झूठे भ्रम बना रखे हैं।