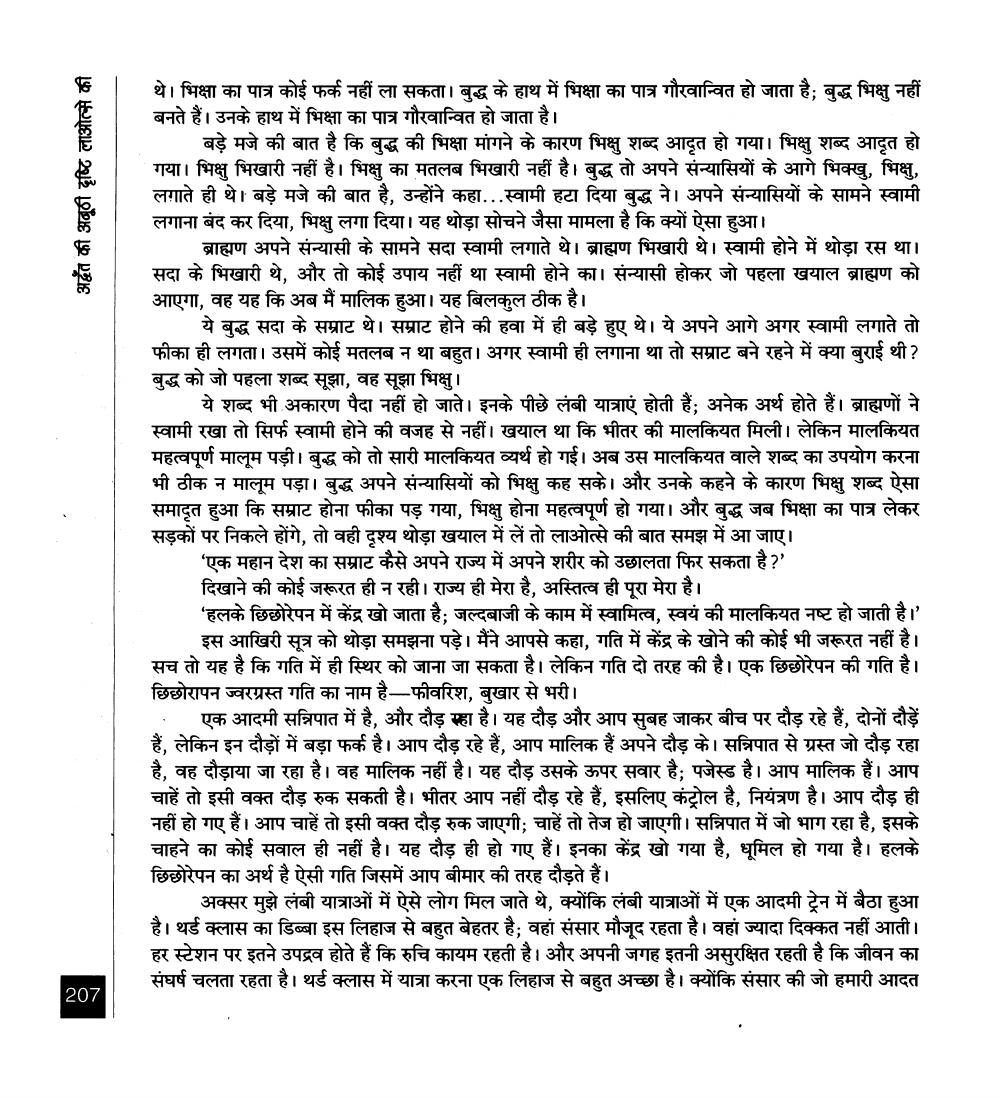________________
अद्वैत की अनूठी दृष्टि लाओत्से की
थे। भिक्षा का पात्र कोई फर्क नहीं ला सकता। बुद्ध के हाथ में भिक्षा का पात्र गौरवान्वित हो जाता है; बुद्ध भिक्षु नहीं बनते हैं। उनके हाथ में भिक्षा का पात्र गौरवान्वित हो जाता है।
बड़े मजे की बात है कि बुद्ध की भिक्षा मांगने के कारण भिक्षु शब्द आदृत हो गया। भिक्षु शब्द आदृत हो गया। भिक्षु भिखारी नहीं है। भिक्षु का मतलब भिखारी नहीं है। बुद्ध तो अपने संन्यासियों के आगे भिक्खु, भिक्षु, लगाते ही थे। बड़े मजे की बात है, उन्होंने कहा...स्वामी हटा दिया बुद्ध ने। अपने संन्यासियों के सामने स्वामी लगाना बंद कर दिया, भिक्षु लगा दिया। यह थोड़ा सोचने जैसा मामला है कि क्यों ऐसा हुआ।
ब्राह्मण अपने संन्यासी के सामने सदा स्वामी लगाते थे। ब्राह्मण भिखारी थे। स्वामी होने में थोड़ा रस था। सदा के भिखारी थे, और तो कोई उपाय नहीं था स्वामी होने का। संन्यासी होकर जो पहला खयाल ब्राह्मण को आएगा, वह यह कि अब मैं मालिक हुआ। यह बिलकुल ठीक है।
ये बुद्ध सदा के सम्राट थे। सम्राट होने की हवा में ही बड़े हुए थे। ये अपने आगे अगर स्वामी लगाते तो फीका ही लगता। उसमें कोई मतलब न था बहुत। अगर स्वामी ही लगाना था तो सम्राट बने रहने में क्या बुराई थी? बुद्ध को जो पहला शब्द सूझा, वह सूझा भिक्षु।
ये शब्द भी अकारण पैदा नहीं हो जाते। इनके पीछे लंबी यात्राएं होती हैं; अनेक अर्थ होते हैं। ब्राह्मणों ने स्वामी रखा तो सिर्फ स्वामी होने की वजह से नहीं। खयाल था कि भीतर की मालकियत मिली। लेकिन मालकियत महत्वपूर्ण मालूम पड़ी। बुद्ध को तो सारी मालकियत व्यर्थ हो गई। अब उस मालकियत वाले शब्द का उपयोग करना भी ठीक न मालूम पड़ा। बुद्ध अपने संन्यासियों को भिक्षु कह सके। और उनके कहने के कारण भिक्षु शब्द ऐसा समादृत हुआ कि सम्राट होना फीका पड़ गया, भिक्षु होना महत्वपूर्ण हो गया। और बुद्ध जब भिक्षा का पात्र लेकर सड़कों पर निकले होंगे, तो वही दृश्य थोड़ा खयाल में लें तो लाओत्से की बात समझ में आ जाए।
'एक महान देश का सम्राट कैसे अपने राज्य में अपने शरीर को उछालता फिर सकता है?' दिखाने की कोई जरूरत ही न रही। राज्य ही मेरा है, अस्तित्व ही पूरा मेरा है। 'हलके छिछोरेपन में केंद्र खो जाता है; जल्दबाजी के काम में स्वामित्व, स्वयं की मालकियत नष्ट हो जाती है।'
इस आखिरी सूत्र को थोड़ा समझना पड़े। मैंने आपसे कहा, गति में केंद्र के खोने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच तो यह है कि गति में ही स्थिर को जाना जा सकता है। लेकिन गति दो तरह की है। एक छिछोरेपन की गति है। छिछोरापन ज्वरग्रस्त गति का नाम है-फीवरिश, बुखार से भरी।
एक आदमी सन्निपात में है, और दौड़ रहा है। यह दौड़ और आप सुबह जाकर बीच पर दौड़ रहे हैं, दोनों दौड़ें हैं, लेकिन इन दौड़ों में बड़ा फर्क है। आप दौड़ रहे हैं, आप मालिक हैं अपने दौड़ के। सन्निपात से ग्रस्त जो दौड़ रहा है, वह दौड़ाया जा रहा है। वह मालिक नहीं है। यह दौड़ उसके ऊपर सवार है; पजेस्ड है। आप मालिक हैं। आप चाहें तो इसी वक्त दौड़ रुक सकती है। भीतर आप नहीं दौड़ रहे हैं, इसलिए कंट्रोल है, नियंत्रण है। आप दौड़ ही नहीं हो गए हैं। आप चाहें तो इसी वक्त दौड़ रुक जाएगी; चाहें तो तेज हो जाएगी। सन्निपात में जो भाग रहा है, इसके चाहने का कोई सवाल ही नहीं है। यह दौड़ ही हो गए हैं। इनका केंद्र खो गया है, धूमिल हो गया है। हलके छिछोरेपन का अर्थ है ऐसी गति जिसमें आप बीमार की तरह दौड़ते हैं।
अक्सर मुझे लंबी यात्राओं में ऐसे लोग मिल जाते थे, क्योंकि लंबी यात्राओं में एक आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है। थर्ड क्लास का डिब्बा इस लिहाज से बहुत बेहतर है; वहां संसार मौजूद रहता है। वहां ज्यादा दिक्कत नहीं आती। हर स्टेशन पर इतने उपद्रव होते हैं कि रुचि कायम रहती है। और अपनी जगह इतनी असुरक्षित रहती है कि जीवन का संघर्ष चलता रहता है। थर्ड क्लास में यात्रा करना एक लिहाज से बहुत अच्छा है। क्योंकि संसार की जो हमारी आदत
207