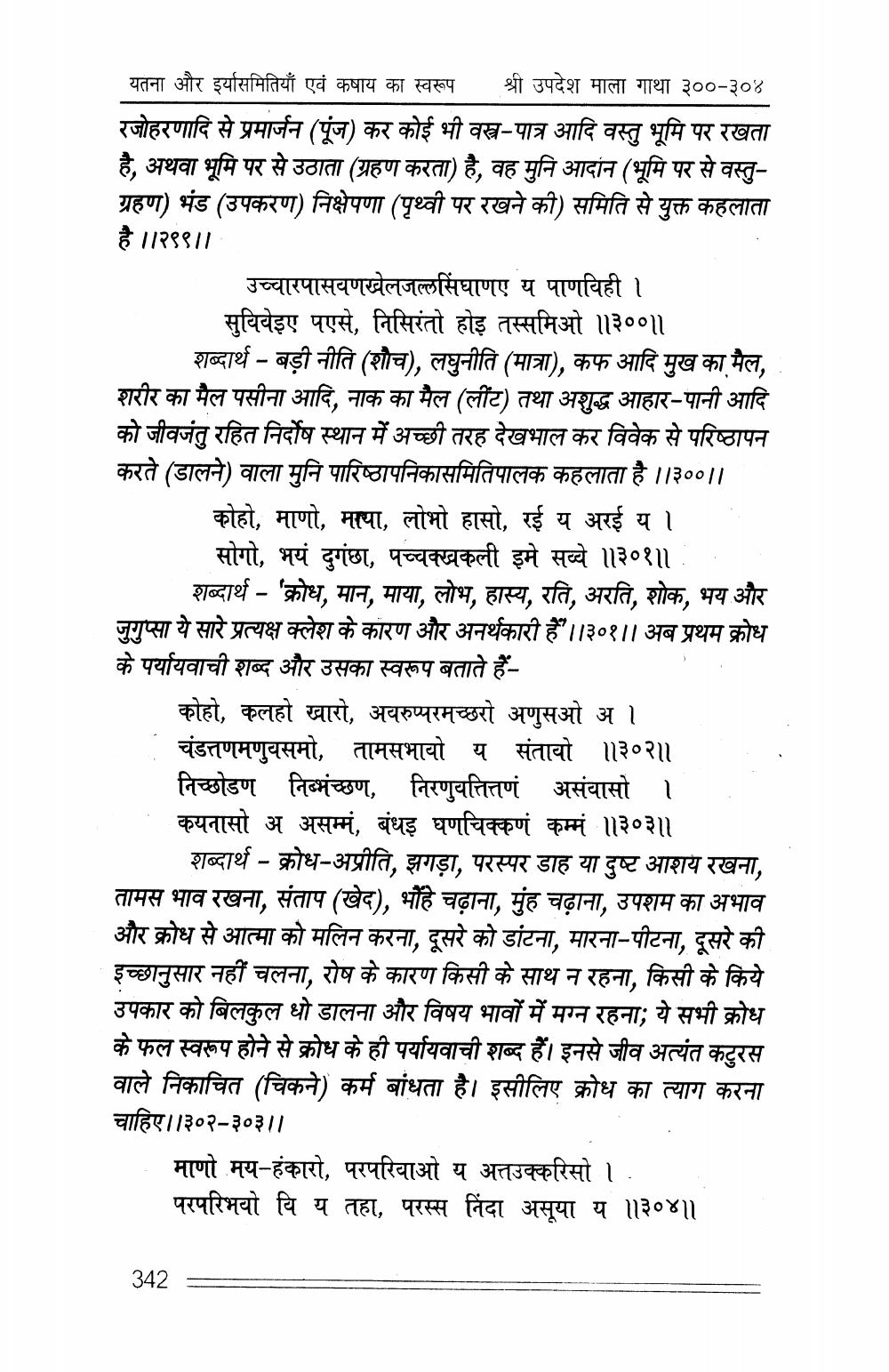________________
यतना और इर्यासमितियाँ एवं कषाय का स्वरूप श्री उपदेश माला गाथा ३००-३०४ रजोहरणादि से प्रमार्जन (पूंज) कर कोई भी वस्त्र-पात्र आदि वस्तु भूमि पर रखता है, अथवा भूमि पर से उठाता (ग्रहण करता) है, वह मुनि आदांन (भूमि पर से वस्तुग्रहण) भंड (उपकरण) निक्षेपणा (पृथ्वी पर रखने की) समिति से युक्त कहलाता है ॥२९९।।
उच्चारपासवणनेलजल्लसिंघाणए य पाणविही । सुविवेइए पएसे, निसिरंतो होइ तस्समिओ ॥३००॥
शब्दार्थ - बड़ी नीति (शौच), लघुनीति (मात्रा), कफ आदि मुख का मैल, शरीर का मैल पसीना आदि, नाक का मैल (लीट) तथा अशुद्ध आहार-पानी आदि को जीवजंतु रहित निर्दोष स्थान में अच्छी तरह देखभाल कर विवेक से परिष्ठापन करते (डालने) वाला मुनि पारिष्ठापनिकासमितिपालक कहलाता है ।।३००।।
कोहो, माणो, माया, लोभो हासो, रई य अरई य ।
सोगो, भयं दुगंछा, पच्चक्खकली इमे सव्ये ॥३०१॥
शब्दार्थ - 'क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा ये सारे प्रत्यक्ष क्लेश के कारण और अनर्थकारी हैं ।।३०१।। अब प्रथम क्रोध के पर्यायवाची शब्द और उसका स्वरूप बताते हैं
कोहो, कलहो खारो, अवरुप्परमच्छरो अणुसओ अ । चंडत्तणमणुवसमो, तामसभायो य संतावो ॥३०२॥ निच्छोडण निभच्छण, निरणुयत्तित्तणं असंवासो । क्यनासो अ असम्म, बंधड़ घणचिक्कणं कम्मं ॥३०३॥
शब्दार्थ - क्रोध-अप्रीति, झगड़ा, परस्पर डाह या दुष्ट आशय रखना, तामस भाव रखना, संताप (खेद), भौहे चढ़ाना, मुंह चढ़ाना, उपशम का अभाव
और क्रोध से आत्मा को मलिन करना, दूसरे को डांटना, मारना-पीटना, दूसरे की इच्छानुसार नहीं चलना, रोष के कारण किसी के साथ न रहना, किसी के किये उपकार को बिलकुल धो डालना और विषय भावों में मग्न रहना; ये सभी क्रोध के फल स्वरूप होने से क्रोध के ही पर्यायवाची शब्द हैं। इनसे जीव अत्यंत कटुरस वाले निकाचित (चिकने) कर्म बांधता है। इसीलिए क्रोध का त्याग करना चाहिए।।३०२-३०३।।
माणो मय-हंकारो, पपरिवाओ य अतउक्करिसो । . परपरिभयो वि य तहा, परस्स निंदा असूया य ॥३०४॥
342