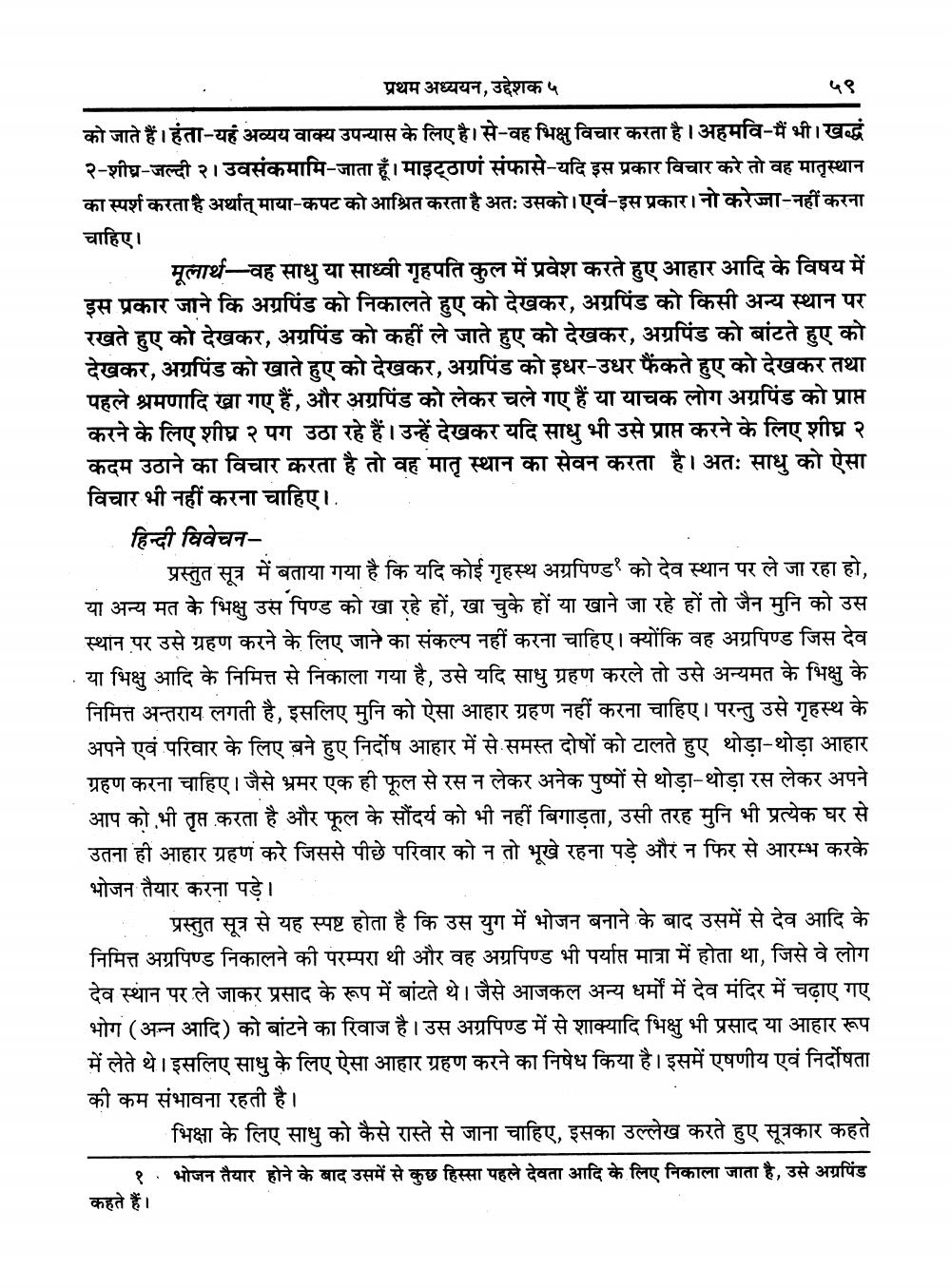________________
प्रथम अध्ययन, उद्देशक ५
५९
को जाते हैं। हंता-यह अव्यय वाक्य उपन्यास के लिए है। से वह भिक्षु विचार करता है । अहमवि- मैं भी । खद्धं २- शीघ्र-जल्दी २। उवसंकमामि जाता हूँ । माइट्ठाणं संफासे-यदि इस प्रकार विचार करे तो वह मातृस्थान का स्पर्श करता है अर्थात् माया-कपट को आश्रित करता है अतः उसको। एवं - इस प्रकार । नो करेज्जा- नहीं करना चाहिए।
मूलार्थ – वह साधु या साध्वी गृहपति कुल में प्रवेश करते हुए आहार आदि के विषय में इस प्रकार जाने कि अग्रपिंड को निकालते हुए को देखकर, अग्रपिंड को किसी अन्य स्थान पर रखते हुए को देखकर, अग्रपिंड को कहीं ले जाते हुए को देखकर, अग्रपिंड को बांटते हुए को देखकर, अग्रपिंड को खाते हुए को देखकर, अग्रपिंड को इधर-उधर फैंकते हुए को देखकर तथा पहले श्रमणादि खा गए हैं, और अग्रपिंड को लेकर चले गए हैं या याचक लोग अग्रपिंड को प्राप्त करने के लिए शीघ्र २ पग उठा रहे हैं। उन्हें देखकर यदि साधु भी उसे प्राप्त करने के लिए शीघ्र २ कदम उठाने का विचार करता है तो वह मातृ स्थान का सेवन करता है। अतः साधु को ऐसा विचार भी नहीं करना चाहिए।.
हिन्दी विवेचन
प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि कोई गृहस्थ अग्रपिण्ड' को देव स्थान पर ले जा रहा हो, या अन्य मत के भिक्षु उस पिण्ड को खा रहे हों, खा चुके हों या खाने जा रहे तो जैन मुनि को उस स्थान पर उसे ग्रहण करने के लिए जाने का संकल्प नहीं करना चाहिए। क्योंकि वह अग्रपिण्ड जिस देव या भिक्षु आदि के निमित्त से निकाला गया है, उसे यदि साधु ग्रहण करले तो उसे अन्यमत के भिक्षु के निमित्त अन्तराय लगती है, इसलिए मुनि को ऐसा आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। परन्तु उसे गृहस्थ के अपने एवं परिवार के लिए बने हुए निर्दोष आहार में से समस्त दोषों को टालते हुए थोड़ा-थोड़ा आहार ग्रहण करना चाहिए। जैसे भ्रमर एक ही फूल से रस न लेकर अनेक पुष्पों से थोड़ा-थोड़ा रस लेकर अपने आप को भी तृप्त करता है और फूल के सौंदर्य को भी नहीं बिगाड़ता, उसी तरह मुनि भी प्रत्येक घर से उतना ही आहार ग्रहण करे जिससे पीछे परिवार को न तो भूखे रहना पड़े और न फिर से आरम्भ करके भोजन तैयार करना पड़े ।
प्रस्तुत सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि उस युग में भोजन बनाने के बाद उसमें से देव आदि के निमित्त अग्रपिण्ड निकालने की परम्परा थी और वह अग्रपिण्ड भी पर्याप्त मात्रा में होता था, जिसे वे लोग देव स्थान पर ले जाकर प्रसाद के रूप में बांटते थे। जैसे आजकल अन्य धर्मों में देव मंदिर में चढ़ाए गए भोग (अन्न आदि) को बांटने का रिवाज है। उस अग्रपिण्ड में से शाक्यादि भिक्षु भी प्रसाद या आहार रूप में लेते थे। इसलिए साधु के लिए ऐसा आहार ग्रहण करने का निषेध किया है। इसमें एषणीय एवं निर्दोषता की कम संभावना रहती है।
भिक्षा के लिए साधु को कैसे रास्ते से जाना चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते
१ . भोजन तैयार होने के बाद उसमें से कुछ हिस्सा पहले देवता आदि के लिए निकाला जाता है, उसे अग्रपिंड
कहते हैं।