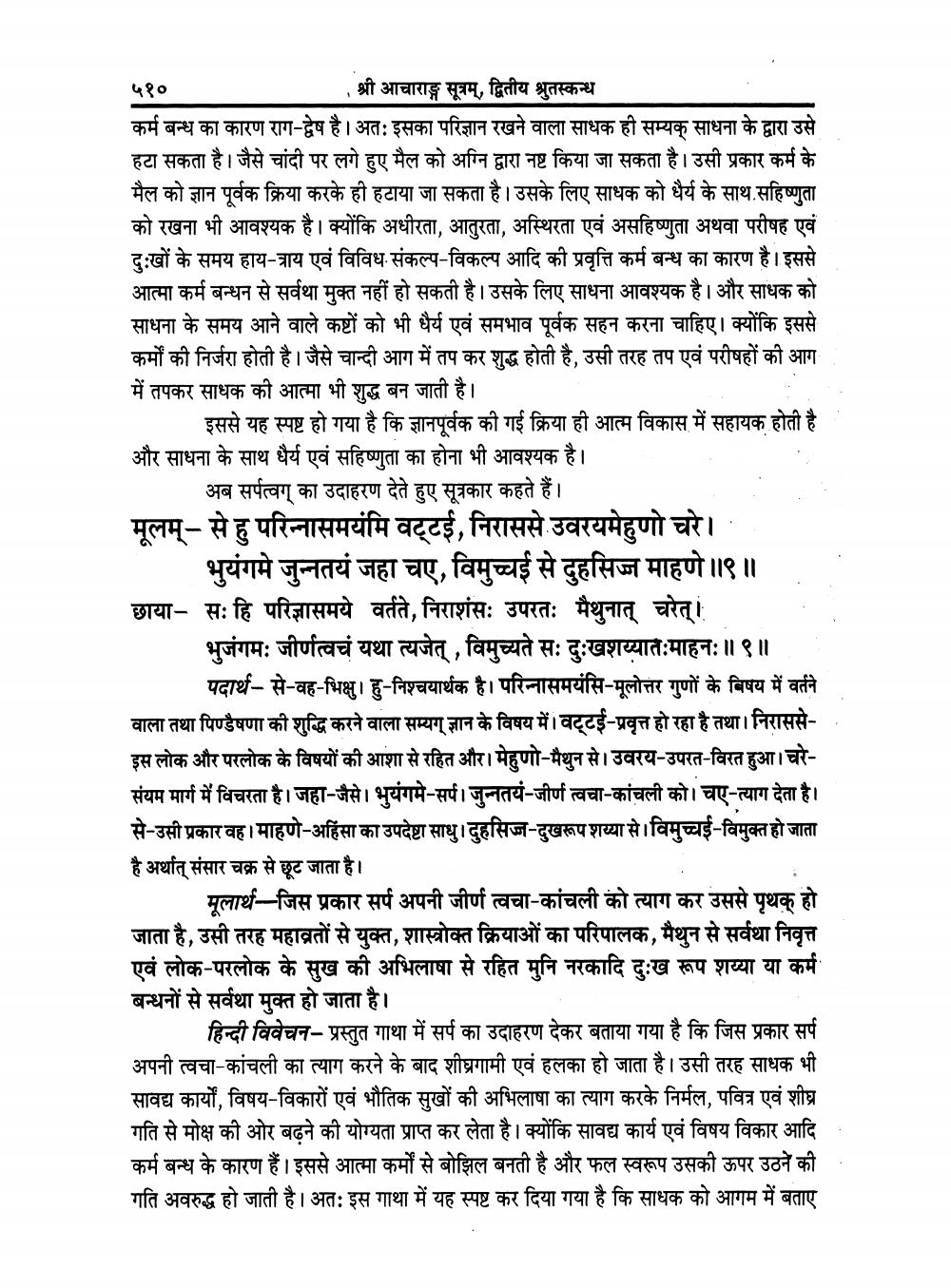________________
५१०
, श्री आचाराङ्ग सूत्रम्, द्वितीय श्रुतस्कन्ध कर्म बन्ध का कारण राग-द्वेष है। अतः इसका परिज्ञान रखने वाला साधक ही सम्यक् साधना के द्वारा उसे हटा सकता है। जैसे चांदी पर लगे हुए मैल को अग्नि द्वारा नष्ट किया जा सकता है। उसी प्रकार कर्म के मैल को ज्ञान पूर्वक क्रिया करके ही हटाया जा सकता है। उसके लिए साधक को धैर्य के साथ.सहिष्णुता को रखना भी आवश्यक है। क्योंकि अधीरता, आतुरता, अस्थिरता एवं असहिष्णुता अथवा परीषह एवं दुःखों के समय हाय-त्राय एवं विविध संकल्प-विकल्प आदि की प्रवृत्ति कर्म बन्ध का कारण है। इससे आत्मा कर्म बन्धन से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकती है। उसके लिए साधना आवश्यक है। और साधक को साधना के समय आने वाले कष्टों को भी धैर्य एवं समभाव पूर्वक सहन करना चाहिए। क्योंकि इससे कर्मों की निर्जरा होती है। जैसे चान्दी आग में तप कर शुद्ध होती है, उसी तरह तप एवं परीषहों की आग में तपकर साधक की आत्मा भी शुद्ध बन जाती है।
इससे यह स्पष्ट हो गया है कि ज्ञानपूर्वक की गई क्रिया ही आत्म विकास में सहायक होती है और साधना के साथ धैर्य एवं सहिष्णुता का होना भी आवश्यक है।
अब सर्पत्वग् का उदाहरण देते हुए सूत्रकार कहते हैं। मूलम्- से हु परिन्नासमयंमि वट्टई, निराससे उवरयमेहुणो चरे।
भुयंगमे जुन्नतयं जहा चए, विमुच्चई से दुहसिज माहणे॥९॥ . छाया- सः हि परिज्ञासमये वर्तते, निराशंसः उपरतः मैथुनात् चरेत्।
भुजंगमः जीर्णत्वचं यथा त्यजेत् , विमुच्यते सः दुःखशय्यातःमाहनः॥९॥
पदार्थ- से-वह-भिक्षु। हु-निश्चयार्थक है। परिन्नासमयंसि-मूलोत्तर गुणों के विषय में वर्तने वाला तथा पिण्डैषणा की शुद्धि करने वाला सम्यग् ज्ञान के विषय में। वट्टई-प्रवृत्त हो रहा है तथा। निराससेइस लोक और परलोक के विषयों की आशा से रहित और। मेहुणो-मैथुन से। उवरय-उपरत-विरत हुआ। चरेसंयम मार्ग में विचरता है। जहा-जैसे। भुयंगमे-सर्प। जुन्नतयं-जीर्ण त्वचा-कांचली को। चए-त्याग देता है। से-उसी प्रकार वह।माहणे-अहिंसा का उपदेष्टा साधु। दुहसिज्ज-दुखरूप शय्या से।विमुच्चई-विमुक्त हो जाता है अर्थात् संसार चक्र से छूट जाता है।
मूलार्थ-जिस प्रकार सर्प अपनी जीर्ण त्वचा-कांचली को त्याग कर उससे पृथक् हो जाता है, उसी तरह महाव्रतों से युक्त, शास्त्रोक्त क्रियाओं का परिपालक, मैथुन से सर्वथा निवृत्त एवं लोक-परलोक के सुख की अभिलाषा से रहित मुनि नरकादि दुःख रूप शय्या या कर्म बन्धनों से सर्वथा मुक्त हो जाता है।
हिन्दी विवेचन- प्रस्तुत गाथा में सर्प का उदाहरण देकर बताया गया है कि जिस प्रकार सर्प अपनी त्वचा-कांचली का त्याग करने के बाद शीघ्रगामी एवं हलका हो जाता है। उसी तरह साधक भी सावध कार्यों, विषय-विकारों एवं भौतिक सुखों की अभिलाषा का त्याग करके निर्मल, पवित्र एवं शीघ्र गति से मोक्ष की ओर बढ़ने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। क्योंकि सावध कार्य एवं विषय विकार आदि कर्म बन्ध के कारण हैं। इससे आत्मा कर्मों से बोझिल बनती है और फल स्वरूप उसकी ऊपर उठने की गति अवरुद्ध हो जाती है। अतः इस गाथा में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि साधक को आगम में बताए