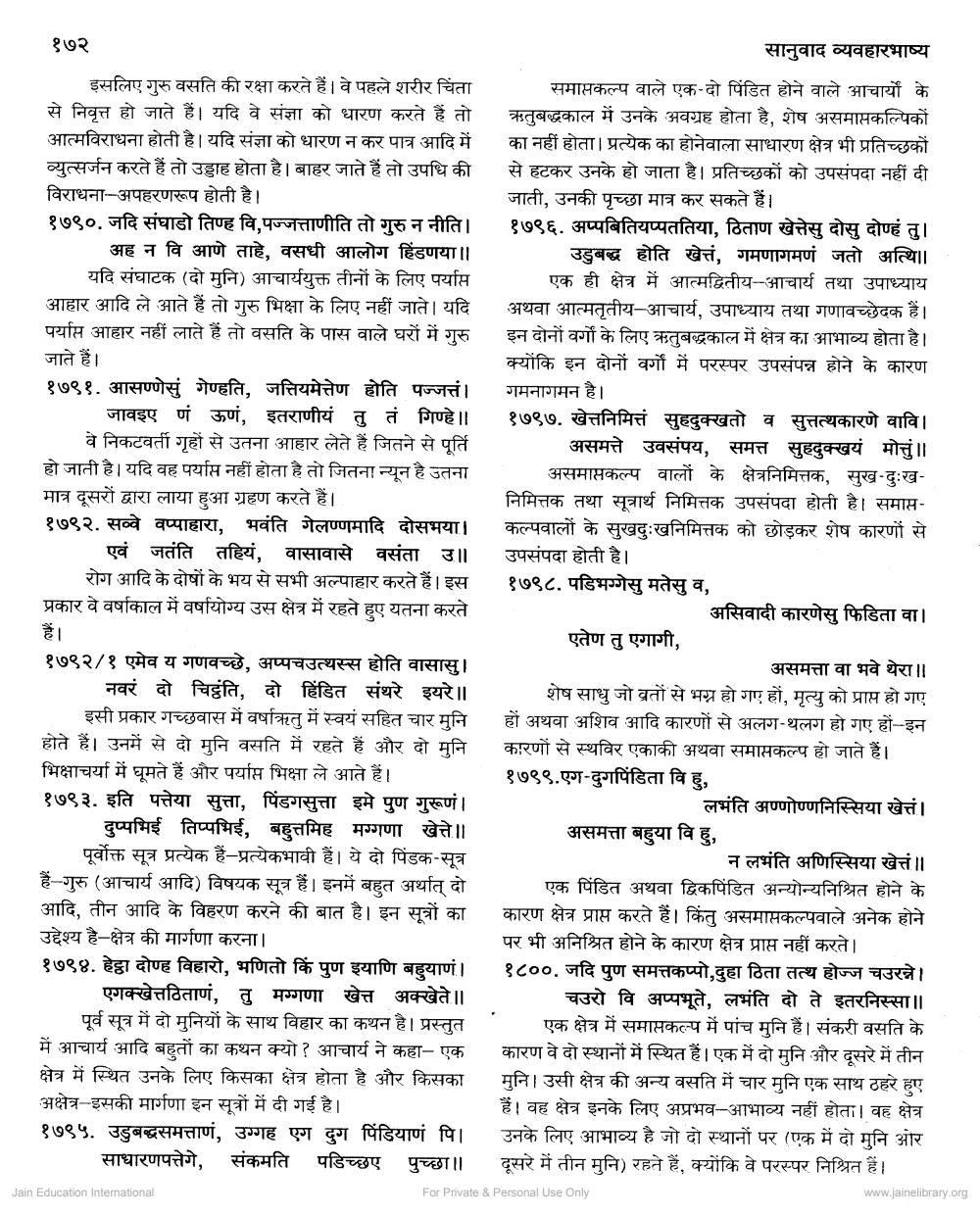________________
१७२
सानुवाद व्यवहारभाष्य इसलिए गुरु वसति की रक्षा करते हैं। वे पहले शरीर चिंता समाप्सकल्प वाले एक-दो पिंडित होने वाले आचार्यों के से निवृत्त हो जाते हैं। यदि वे संज्ञा को धारण करते हैं तो ऋतुबद्धकाल में उनके अवग्रह होता है, शेष असमाप्तकल्पिकों आत्मविराधना होती है। यदि संज्ञा को धारण न कर पात्र आदि में का नहीं होता। प्रत्येक का होनेवाला साधारण क्षेत्र भी प्रतिच्छकों व्युत्सर्जन करते हैं तो उड्डाह होता है। बाहर जाते हैं तो उपधि की से हटकर उनके हो जाता है। प्रतिच्छकों को उपसंपदा नहीं दी विराधना-अपहरणरूप होती है।
जाती, उनकी पृच्छा मात्र कर सकते हैं। १७९०. जदि संघाडो तिण्ह वि,पज्जत्ताणीति तो गुरु न नीति। १७९६. अप्पबितियप्पततिया, ठिताण खेत्तेसु दोसु दोण्हं तु। ____ अह न वि आणे ताहे, वसधी आलोग हिंडणया।।
उडुबद्ध होति खेत्तं, गमणागमणं जतो अत्थि।। यदि संघाटक (दो मुनि) आचार्ययुक्त तीनों के लिए पर्याप्त एक ही क्षेत्र में आत्मद्वितीय-आचार्य तथा उपाध्याय आहार आदि ले आते हैं तो गुरु भिक्षा के लिए नहीं जाते। यदि अथवा आत्मतृतीय-आचार्य, उपाध्याय तथा गणावच्छेदक हैं। पर्याप्त आहार नहीं लाते हैं तो वसति के पास वाले घरों में गुरु इन दोनों वर्गों के लिए ऋतुबद्धकाल में क्षेत्र का आभाव्य होता है। जाते हैं।
क्योंकि इन दोनों वर्गों में परस्पर उपसंपन्न होने के कारण १७९१. आसण्णेसुं गेण्हति, जत्तियमेत्तेण होति पज्जत्तं। गमनागमन है।
जावइए णं ऊणं, इतराणीयं तु तं गिण्हे॥ १७९७. खेत्तनिमित्तं सुहदुक्खतो व सुत्तत्थकारणे वावि। वे निकटवर्ती गृहों से उतना आहार लेते हैं जितने से पूर्ति
असमत्ते उवसंपय, समत्त सुहदुक्खयं मोत्तुं॥ हो जाती है। यदि वह पर्याप्त नहीं होता है तो जितना न्यून है उतना असमाप्तकल्प वालों के क्षेत्रनिमित्तक, सुख-दुःखमात्र दूसरों द्वारा लाया हुआ ग्रहण करते हैं।
निमित्तक तथा सूत्रार्थ निमित्तक उपसंपदा होती है। समास१७९२. सव्वे वप्पाहारा, भवंति गेलण्णमादि दोसभया। कल्पवालों के सुखदुःखनिमित्तक को छोड़कर शेष कारणों से
__ एवं जतंति तहियं, वासावासे वसंता उ॥ उपसंपदा होती है।
रोग आदि के दोषों के भय से सभी अल्पाहार करते हैं। इस १७९८. पडिभग्गेसु मतेसु व, प्रकार वे वर्षाकाल में वर्षायोग्य उस क्षेत्र में रहते हुए यतना करते
असिवादी कारणेसु फिडिता वा।
एतेण तु एगागी, १७९२/१ एमेव य गणवच्छे, अप्पचउत्थस्स होति वासासु।
असमत्ता वा भवे थेरा॥ नवरं दो चिट्ठति, दो हिंडित संथरे इयरे।। शेष साधु जो व्रतों से भग्न हो गए हों, मृत्यु को प्राप्त हो गए
इसी प्रकार गच्छवास में वर्षाऋतु में स्वयं सहित चार मुनि हों अथवा अशिव आदि कारणों से अलग-थलग हो गए हों-इन होते हैं। उनमें से दो मुनि वसति में रहते हैं और दो मुनि कारणों से स्थविर एकाकी अथवा समासकल्प हो जाते हैं। भिक्षाचर्या में घूमते हैं और पर्याप्त भिक्षा ले आते हैं।
१७९९.एग-दुगपिडिता वि हु, १७९३. इति पत्तेया सुत्ता, पिंडगसुत्ता इमे पुण गुरूणं ।
लभंति अण्णोण्णनिस्सिया खेत्तं । __ दुप्पभिई तिप्पभिई, बहुत्तमिह मग्गणा खेत्ते॥
असमत्ता बहुया वि हु, पूर्वोक्त सूत्र प्रत्येक हैं-प्रत्येकभावी हैं। ये दो पिंडक-सूत्र
न लभंति अणिस्सिया खेत्तं॥ हैं-गुरु (आचार्य आदि) विषयक सूत्र हैं। इनमें बहुत अर्थात् दो एक पिंडित अथवा द्विकपिडित अन्योन्यनिश्रित होने के आदि, तीन आदि के विहरण करने की बात है। इन सूत्रों का कारण क्षेत्र प्राप्त करते हैं। किंतु असमाप्तकल्पवाले अनेक होने उद्देश्य है-क्षेत्र की मार्गणा करना।
पर भी अनिश्रित होने के कारण क्षेत्र प्राप्त नहीं करते। १७९४. हेट्ठा दोण्ह विहारो, भणितो किं पुण इयाणि बहुयाणं। १८००. जदि पुण समत्तकप्पो,दुहा ठिता तत्थ होज्ज चउरन्ने। एगक्खेत्तठिताणं, तु मग्गणा खेत्त अक्खेते॥
चउरो वि अप्पभूते, लभंति दो ते इतरनिस्सा॥ पूर्व सूत्र में दो मुनियों के साथ विहार का कथन है। प्रस्तुत एक क्षेत्र में समाप्तकल्प में पांच मुनि हैं। संकरी वसति के में आचार्य आदि बहुतों का कथन क्यो? आचार्य ने कहा- एक ___कारण वे दो स्थानों में स्थित हैं। एक में दो मुनि और दूसरे में तीन क्षेत्र में स्थित उनके लिए किसका क्षेत्र होता है और किसका। मुनि। उसी क्षेत्र की अन्य वसति में चार मुनि एक साथ ठहरे हुए अक्षेत्र-इसकी मार्गणा इन सूत्रों में दी गई है।
हैं। वह क्षेत्र इनके लिए अप्रभव-आभाव्य नहीं होता। वह क्षेत्र १७९५. उडुबद्धसमत्ताणं, उग्गह एग दुग पिंडियाणं पि। उनके लिए आभाव्य है जो दो स्थानों पर (एक में दो मुनि ओर
साधारणपत्तेगे, संकमति पडिच्छए पुच्छा॥ दूसरे में तीन मुनि) रहते हैं, क्योंकि वे परस्पर निश्रित हैं। Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org