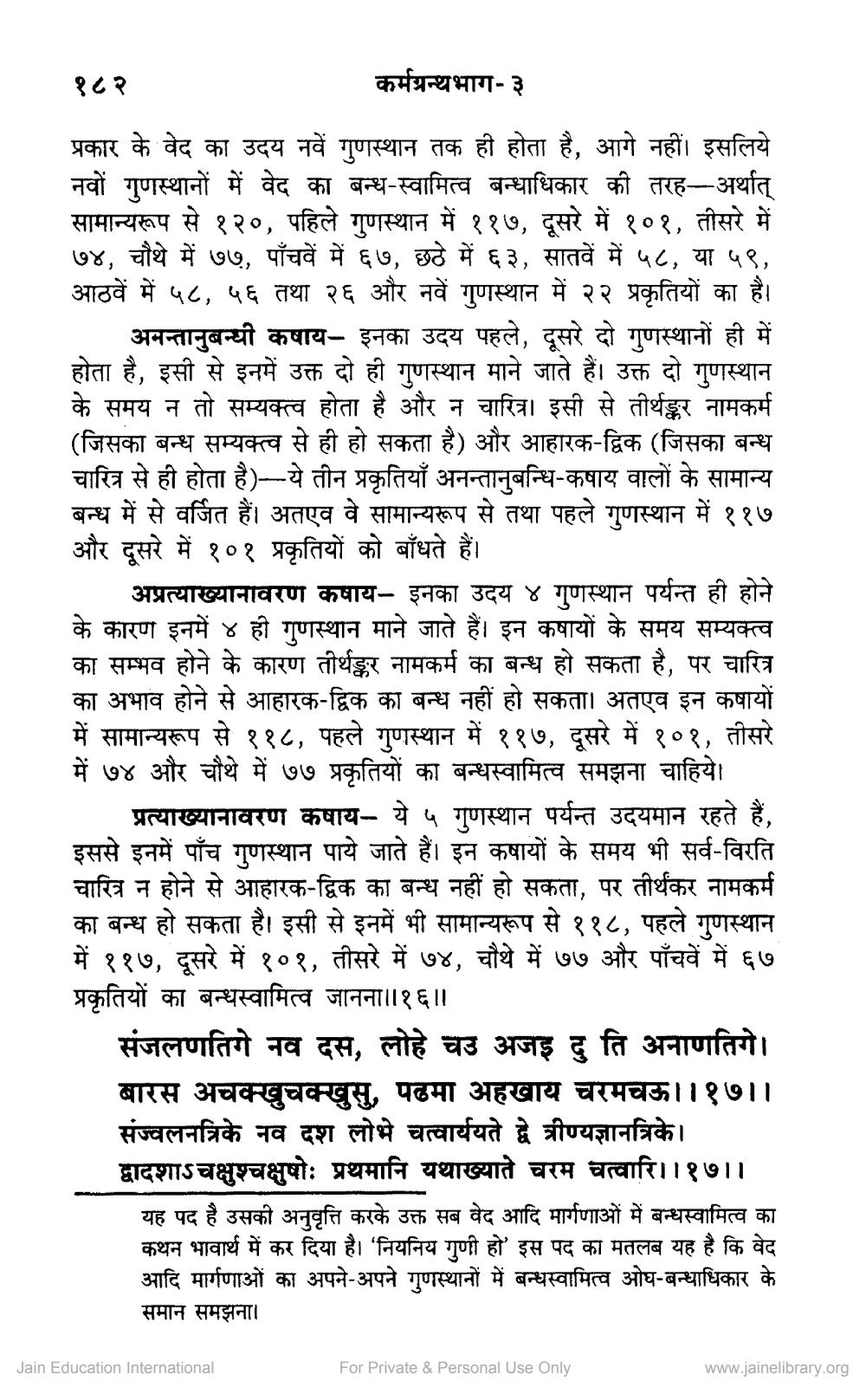________________
१८२
कर्मग्रन्थभाग-३
प्रकार के वेद का उदय नवें गुणस्थान तक ही होता है, आगे नहीं। इसलिये नवों गुणस्थानों में वेद का बन्ध-स्वामित्व बन्धाधिकार की तरह-अर्थात् सामान्यरूप से १२०, पहिले गुणस्थान में ११७, दूसरे में १०१, तीसरे में ७४, चौथे में ७७, पाँचवें में ६७, छठे में ६३, सातवें में ५८, या ५९, आठवें में ५८, ५६ तथा २६ और नवें गुणस्थान में २२ प्रकृतियों का है।
अमन्तानुबन्धी कषाय- इनका उदय पहले, दूसरे दो गुणस्थानों ही में होता है, इसी से इनमें उक्त दो ही गुणस्थान माने जाते हैं। उक्त दो गुणस्थान के समय न तो सम्यक्त्व होता है और न चारित्र। इसी से तीर्थङ्कर नामकर्म (जिसका बन्ध सम्यक्त्व से ही हो सकता है) और आहारक-द्विक (जिसका बन्ध चारित्र से ही होता है)-ये तीन प्रकृतियाँ अनन्तानुबन्धि-कषाय वालों के सामान्य बन्ध में से वर्जित हैं। अतएव वे सामान्यरूप से तथा पहले गुणस्थान में ११७ और दूसरे में १०१ प्रकृतियों को बाँधते हैं।
अप्रत्याख्यानावरण कषाय- इनका उदय ४ गुणस्थान पर्यन्त ही होने के कारण इनमें ४ ही गुणस्थान माने जाते हैं। इन कषायों के समय सम्यक्त्व का सम्भव होने के कारण तीर्थङ्कर नामकर्म का बन्ध हो सकता है, पर चारित्र का अभाव होने से आहारक-द्विक का बन्ध नहीं हो सकता। अतएव इन कषायों में सामान्यरूप से ११८, पहले गुणस्थान में ११७, दूसरे में १०१, तीसरे में ७४ और चौथे में ७७ प्रकृतियों का बन्धस्वामित्व समझना चाहिये।
प्रत्याख्यानावरण कषाय- ये ५ गुणस्थान पर्यन्त उदयमान रहते हैं, इससे इनमें पाँच गुणस्थान पाये जाते हैं। इन कषायों के समय भी सर्व-विरति चारित्र न होने से आहारक-द्विक का बन्ध नहीं हो सकता, पर तीर्थंकर नामकर्म का बन्ध हो सकता है। इसी से इनमें भी सामान्यरूप से ११८, पहले गणस्थान में ११७, दूसरे में १०१, तीसरे में ७४, चौथे में ७७ और पाँचवें में ६७ प्रकृतियों का बन्धस्वामित्व जानना।।१६।।
संजलणतिगे नव दस, लोहे चउ अजइ दु ति अनाणतिगे। बारस अचक्खुचक्खुसु, पढमा अहखाय चरमचऊ।।१७।। संज्वलनत्रिके नव दश लोभे चत्वार्ययते द्वे त्रीण्यज्ञानत्रिके। द्वादशाऽचक्षुश्चक्षुषोः प्रथमानि यथाख्याते चरम चत्वारि।।१७।। यह पद है उसकी अनुवृत्ति करके उक्त सब वेद आदि मार्गणाओं में बन्धस्वामित्व का कथन भावार्थ में कर दिया है। 'नियनिय गुणी हो' इस पद का मतलब यह है कि वेद आदि मार्गणाओं का अपने-अपने गुणस्थानों में बन्धस्वामित्व ओघ-बन्धाधिकार के समान समझना।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org