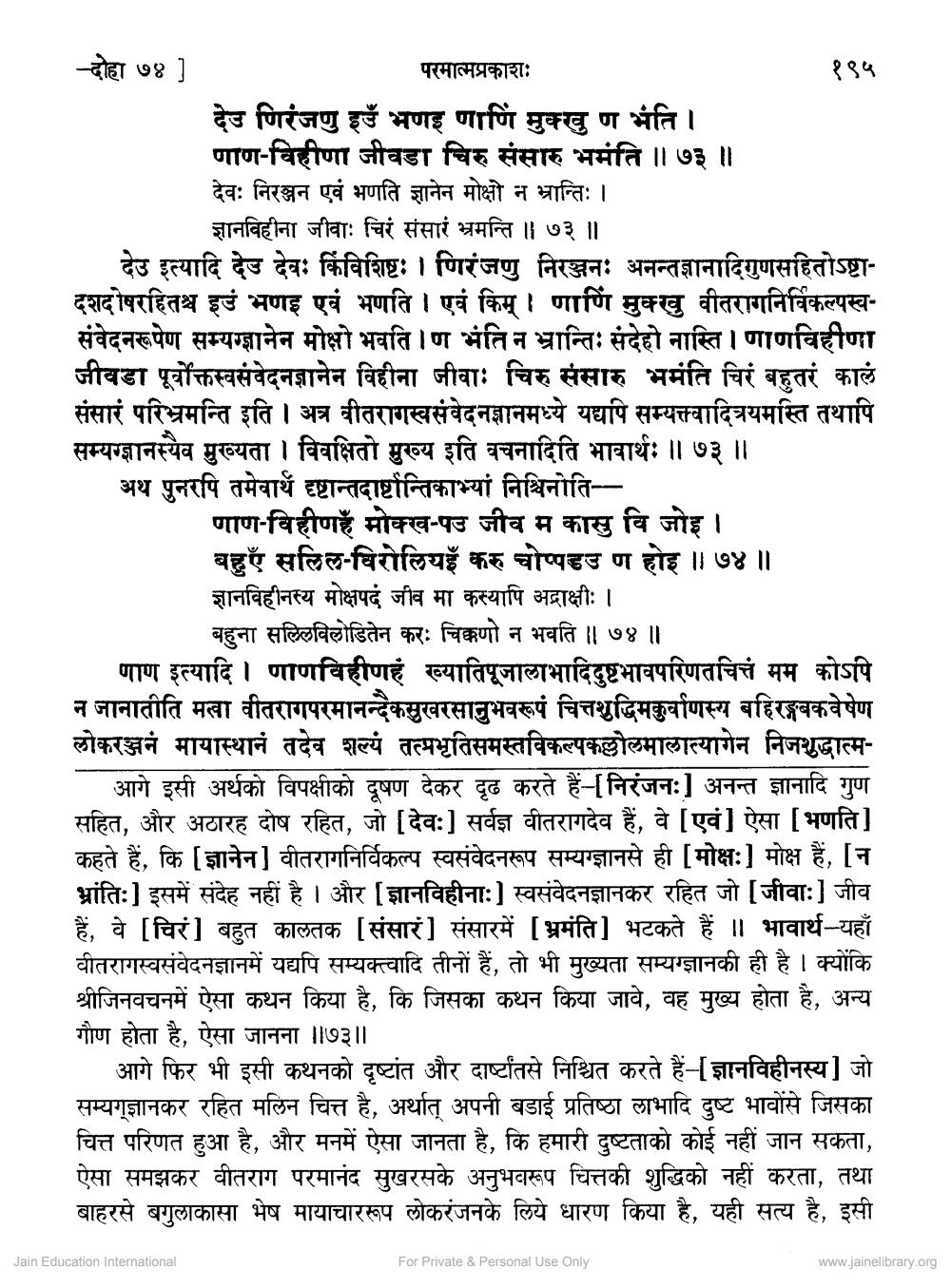________________
१९५
-दोहा ७४ ]
परमात्मप्रकाशः देउ णिरंजणु इउँ भणइ णाणि मुक्खु ण भंति । णाण-विहीणा जीवडा चिरु संसारु भमंति ।। ७३ ॥ देवः निरञ्जन एवं भणति ज्ञानेन मोक्षो न भ्रान्तिः ।
ज्ञानविहीना जीवाः चिरं संसारं भ्रमन्ति ॥ ७३ ॥ देउ इत्यादि देउ देवः किंविशिष्टः । णिरंजणु निरञ्जनः अनन्तज्ञानादिगुणसहितोऽष्टादशदोषरहितश्च इउं भणइ एवं भणति । एवं किम् । णाणिं मुक्खु वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदनरूपेण सम्यग्ज्ञानेन मोक्षो भवति ।ण भंति न भ्रान्तिः संदेहो नास्ति । णाणविहीणा जीवडा पूर्वोक्तस्वसंवेदनज्ञानेन विहीना जीवाः चिरु संसारु भमंति चिरं बहुतरं कालं संसारं परिभ्रमन्ति इति । अत्र वीतरागस्वसंवेदनज्ञानमध्ये यद्यपि सम्यक्त्वादित्रयमस्ति तथापि सम्यग्ज्ञानस्यैव मुख्यता। विवक्षितो मुख्य इति वचनादिति भावार्थः ॥ ७३ ।। अथ पुनरपि तमेवार्थ दृष्टान्तदान्तिकाभ्यां निश्चिनोति
णाण-विहीणहँ मोक्ख-पउ जीव म कासु वि जोइ । बहुएँ सलिल-विरोलियइँ करु चोप्पडउ ण होइ ।। ७४ ॥ ज्ञानविहीनस्य मोक्षपदं जीव मा कस्यापि अद्राक्षीः ।
बहुना सलिलविलोडितेन करः चिक्कणो न भवति ॥ ७४ ॥ णाण इत्यादि । णाणविहीणहं ख्यातिपूजालाभादिदुष्टभावपरिणतचित्तं मम कोऽपि न जानातीति मखा वीतरागपरमानन्दैकसुखरसानुभवरूपं चित्तशुद्धिमकुर्वाणस्य बहिरङ्गबकवेषेण लोकरञ्जनं मायास्थानं तदेव शल्यं तत्मभृतिसमस्तविकल्पकल्लोलमालात्यागेन निजशुद्धात्म
आगे इसी अर्थको विपक्षीको दूषण देकर दृढ करते हैं-[निरंजनः] अनन्त ज्ञानादि गुण सहित, और अठारह दोष रहित, जो [देवः] सर्वज्ञ वीतरागदेव हैं, वे [एवं] ऐसा [भणति] कहते हैं, कि [ज्ञानेन] वीतरागनिर्विकल्प स्वसंवेदनरूप सम्यग्ज्ञानसे ही [मोक्षः] मोक्ष हैं, [न भ्रांतिः] इसमें संदेह नहीं है । और [ज्ञानविहीनाः] स्वसंवेदनानकर रहित जो [जीवाः] जीव हैं, वे [चिरं] बहुत कालतक [संसारं] संसारमें [भ्रमंति] भटकते हैं ॥ भावार्थ-यहाँ वीतरागस्वसंवेदनज्ञानमें यद्यपि सम्यक्त्वादि तीनों हैं, तो भी मुख्यता सम्यग्ज्ञानकी ही है । क्योंकि श्रीजिनवचनमें ऐसा कथन किया है, कि जिसका कथन किया जावे, वह मुख्य होता है, अन्य गौण होता है, ऐसा जानना ॥७३॥ ____ आगे फिर भी इसी कथनको दृष्टांत और दाष्र्टातसे निश्चित करते हैं-[ज्ञानविहीनस्य] जो सम्यग्ज्ञानकर रहित मलिन चित्त है, अर्थात् अपनी बडाई प्रतिष्ठा लाभादि दुष्ट भावोंसे जिसका चित्त परिणत हुआ है, और मनमें ऐसा जानता है, कि हमारी दुष्टताको कोई नहीं जान सकता, ऐसा समझकर वीतराग परमानंद सुखरसके अनुभवरूप चित्तकी शुद्धिको नहीं करता, तथा बाहरसे बगुलाकासा भेष मायाचाररूप लोकरंजनके लिये धारण किया है, यही सत्य है, इसी
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org