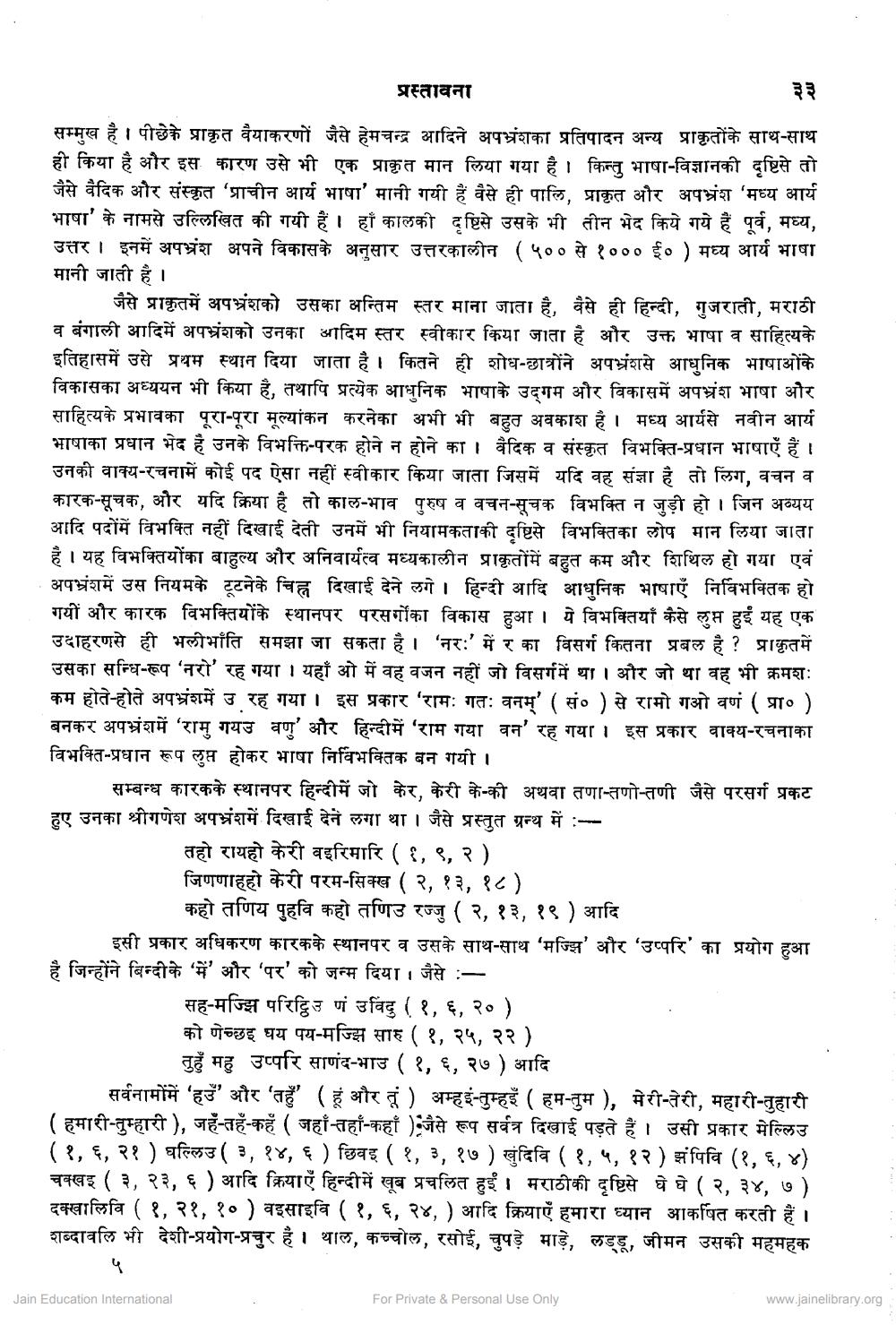________________
प्रस्तावना
सम्मुख है । पीछेके प्राकृत वैयाकरणों जैसे हेमचन्द्र आदिने अपभ्रंशका प्रतिपादन अन्य प्राकृतोंके साथ-साथ ही किया है और इस कारण उसे भी एक प्राकृत मान लिया गया है। किन्त भाषा-विज्ञानकी जैसे वैदिक और संस्कृत 'प्राचीन आर्य भाषा' मानी गयी हैं वैसे ही पालि, प्राकृत और अपभ्रंश 'मध्य आर्य भाषा' के नामसे उल्लिखित की गयी हैं। हाँ कालकी दृष्टिसे उसके भी तीन भेद किये गये हैं पूर्व, मध्य, उत्तर। इनमें अपभ्रंश अपने विकासके अनसार उत्तरकालीन (५०० से १००० ई०) मध्य आर्य भाषा मानी जाती है।
जैसे प्राकृतमें अपभ्रंशको उसका अन्तिम स्तर माना जाता है, वैसे ही हिन्दी, गुजराती, मराठी व बंगाली आदिमें अपभ्रंशको उनका आदिम स्तर स्वीकार किया जाता है और उक्त भाषा व साहित्यके इतिहासमें उसे प्रथम स्थान दिया जाता है। कितने ही शोध-छात्रोंने अपभ्रंशसे आधुनिक भाषाओंके विकासका अध्ययन भी किया है, तथापि प्रत्येक आधुनिक भाषाके उदगम और विकासमें अपभ्रंश भाषा और साहित्यके प्रभावका पूरा-पूरा मूल्यांकन करनेका अभी भी बहुत अवकाश है। मध्य आर्यसे नवीन आर्य भाषाका प्रधान भेद है उनके विभक्ति-परक होने न होने का। वैदिक व संस्कृत विभक्ति-प्रधान भाषाएँ हैं । उनकी वाक्य-रचनामें कोई पद ऐसा नहीं स्वीकार किया जाता जिसमें यदि वह संज्ञा है तो लिंग, वचन व कारक-सूचक, और यदि क्रिया है तो काल-भाव पुरुष व वचन-सूचक विभक्ति न जुड़ी हो । जिन अव्यय आदि पदोंमें विभक्ति नहीं दिखाई देती उनमें भी नियामकताकी दृष्टिसे विभक्तिका लोप मान लिया जाता है । यह विभक्तियोंका बाहुल्य और अनिवार्यत्व मध्यकालीन प्राकृतोंमें बहुत कम और शिथिल हो गया एवं अपभ्रंशमें उस नियमके टूटनेके चिह्न दिखाई देने लगे। हिन्दी आदि आधुनिक भाषाएँ निर्विभक्तिक हो गयीं और कारक विभक्तियोंके स्थानपर परसर्गोका विकास हुआ। ये विभक्तियाँ कैसे लुप्त हुई यह एक उदाहरणसे ही भलीभांति समझा जा सकता है । 'नरः' में र का विसर्ग कितना प्रबल है ? प्राकृतमें उसका सन्धि-रूप 'नरो' रह गया । यहाँ ओ में वह वजन नहीं जो विसर्गमें था। और जो था वह भी क्रमशः कम होते-होते अपभ्रंशमें उ रह गया। इस प्रकार 'रामः गतः वनम्' ( सं० ) से रामो गओ वणं ( प्रा० ) बनकर अपभ्रंशमें 'रामु गयउ वणु' और हिन्दीमें 'राम गया वन' रह गया। इस प्रकार वाक्य-रचनाका विभक्ति-प्रधान रूप लुप्त होकर भाषा निर्विभक्तिक बन गयी।
सम्बन्ध कारकके स्थानपर हिन्दी में जो केर, केरी के-की अथवा तणा-तणो-तणी जैसे परसर्ग प्रकट हुए उनका श्रीगणेश अपभ्रंशमें दिखाई देने लगा था। जैसे प्रस्तुत ग्रन्थ में :
तहो रायहो केरी वइरिमारि ( १, ९, २) जिणणाहहो केरी परम-सिक्ख ( २, १३, १८)
कहो तणिय पुहवि कहो तणिउ रज्जु ( २, १३, १९) आदि इसी प्रकार अधिकरण कारकके स्थानपर व उसके साथ-साथ 'मज्झि' और 'उप्परि' का प्रयोग हुआ है जिन्होंने बिन्दीके 'मैं' और 'पर' को जन्म दिया। जैसे :
सह-मज्झि परिट्ठि उ णं उविंदु ( १, ६, २०) को णेच्छइ घय पय-मज्झि सारु ( १, २५, २२)
तुहुँ महु उप्परि साणंद-भाउ ( १, ६, २७ ) आदि सर्वनामोंमें 'हउँ' और 'तहुँ' (हूं और तूं ) अम्हइं-तुम्हइँ ( हम-तुम ), मेरी-तेरी, महारी-तुहारी ( हमारी-तुम्हारी ), जहँ-तहँ-कह ( जहाँ-तहाँ-कहाँ ) जैसे रूप सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं। उसी प्रकार मेल्लिउ ( १, ६, २१ ) घल्लिउ ( ३, १४, ६ ) छिवइ ( १, ३, १७ ) खुंदिवि ( १, ५, १२) झंपिवि (१, ६, ४) चक्खइ ( ३, २३, ६ ) आदि क्रियाएँ हिन्दीमें खूब प्रचलित हुई। मराठीकी दृष्टिसे घे घे ( २, ३४, ७) दक्खालिवि (१.२१. १० ) वइसाइवि (१.६.२४. ) आदि क्रियाएँ हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं। शब्दावलि भी देशी-प्रयोग-प्रचुर है । थाल, कच्चोल, रसोई, चुपड़े माड़े, लड्डू, जीमन उसकी महमहक
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org -