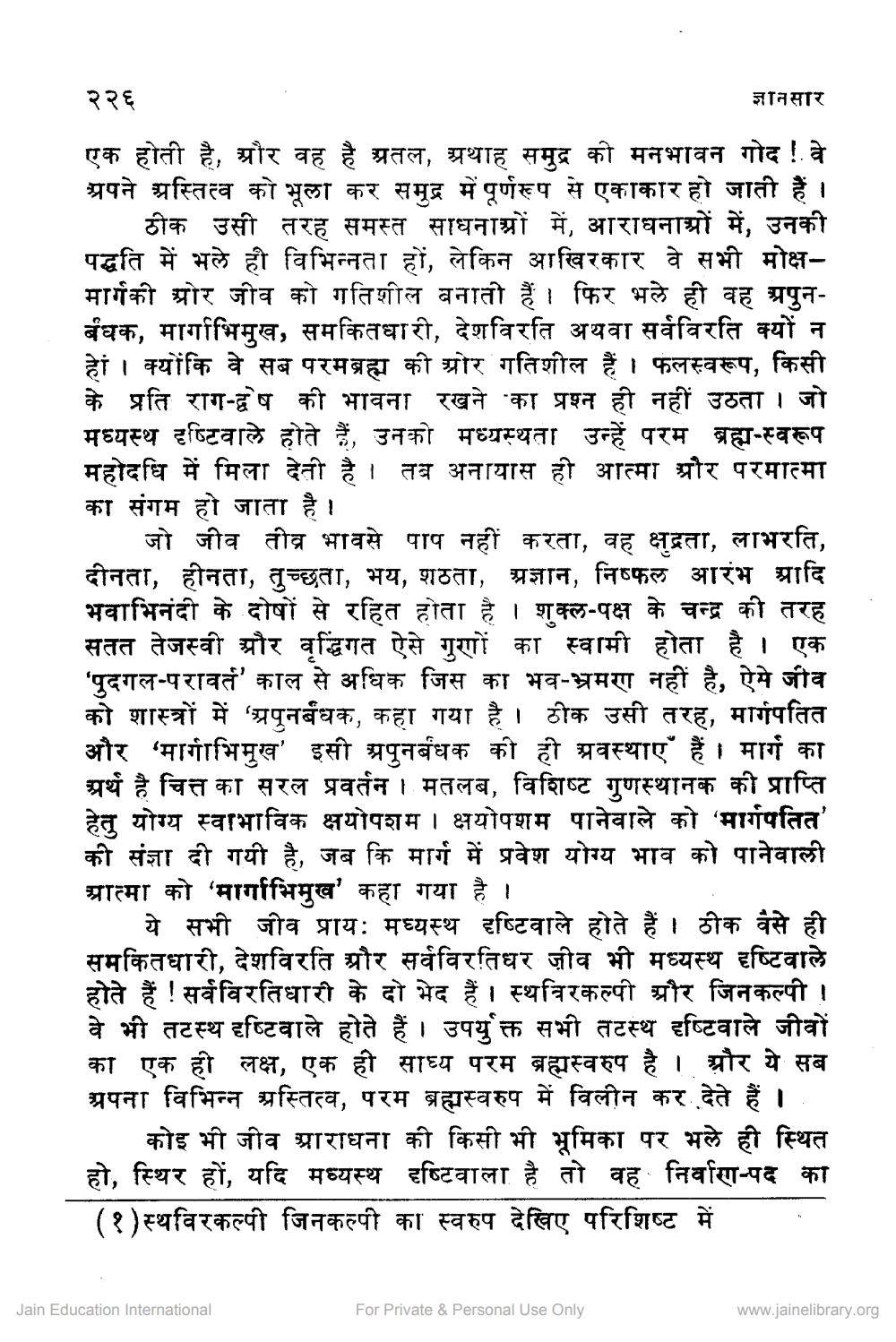________________
२२६
ज्ञानसार
एक होती है, और वह है अतल, अथाह समूद्र की मनभावन गोद ! वे अपने अस्तित्व को भूला कर समुद्र में पूर्णरूप से एकाकार हो जाती हैं।
ठीक उसी तरह समस्त साधनाओं में, आराधनाओं में, उनकी पद्धति में भले ही विभिन्नता हों, लेकिन आखिरकार वे सभी मोक्षमार्गकी ओर जीव को गतिशील बनाती हैं। फिर भले ही वह अपुनबंधक, मार्गाभिमुख, समकितधारी, देशविरति अथवा सर्वविरति क्यों न हों। क्योंकि वे सब परमब्रह्म की ओर गतिशील हैं। फलस्वरूप, किसी के प्रति राग-द्वेष की भावना रखने का प्रश्न ही नहीं उठता । जो मध्यस्थ दृष्टिवाले होते हैं, उनको मध्यस्थता उन्हें परम ब्रह्म-स्वरूप महोदधि में मिला देती है। तब अनायास ही आत्मा और परमात्मा का संगम हो जाता है।
जो जीव तीव्र भावसे पाप नहीं करता, वह क्षद्रता, लाभरति, दीनता, हीनता, तुच्छता, भय, शठता, अज्ञान, निष्फल आरंभ आदि भवाभिनंदी के दोषों से रहित होता है । शक्ल-पक्ष के चन्द्र की तरह सतत तेजस्वी और वृद्धिंगत ऐसे गुणों का स्वामी होता है। एक 'पुदगल-परावर्त' काल से अधिक जिस का भव-भ्रमण नहीं है, ऐसे जीव को शास्त्रों में 'अपुनर्बंधक, कहा गया है। ठीक उसी तरह, मार्गपतित और 'मागाभिमुख' इसी अपुनबंधक की ही अवस्थाएँ हैं। मार्ग का अर्थ है चित्त का सरल प्रवर्तन । मतलब, विशिष्ट गुणस्थानक की प्राप्ति हेतु योग्य स्वाभाविक क्षयोपशम । क्षयोपशम पानेवाले को 'मार्गपतित' की संज्ञा दी गयी है, जब कि मार्ग में प्रवेश योग्य भाव को पानेवाली प्रात्मा को 'मार्गाभिमुख' कहा गया है।
ये सभी जीव प्राय: मध्यस्थ दृष्टिवाले होते हैं। ठीक वैसे ही समकितधारी, देशविरति और सर्वविरतिधर जीव भी मध्यस्थ दृष्टिवाले होते हैं ! सर्वविरतिधारी के दो भेद हैं। स्थविरकल्पी और जिनकल्पी । वे भी तटस्थ दृष्टिवाले होते हैं। उपर्युक्त सभी तटस्थ दृष्टिवाले जीवों का एक ही लक्ष, एक ही साध्य परम ब्रह्मस्वरुप है। और ये सब अपना विभिन्न अस्तित्व, परम ब्रह्मस्वरुप में विलीन कर देते हैं।
कोइ भी जीव आराधना की किसी भी भूमिका पर भले ही स्थित हो, स्थिर हों, यदि मध्यस्थ दृष्टिवाला है तो वह निर्वाण-पद का (१)स्थविरकल्पी जिनकल्पी का स्वरुप देखिए परिशिष्ट में
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org